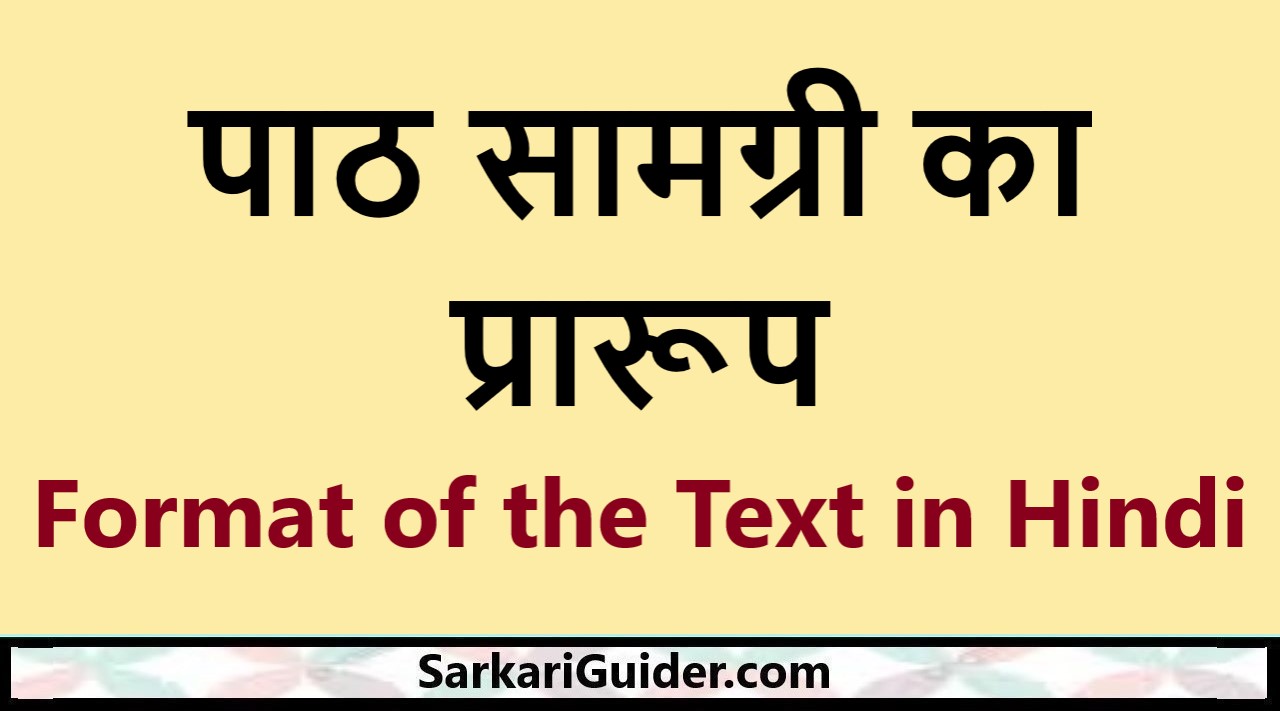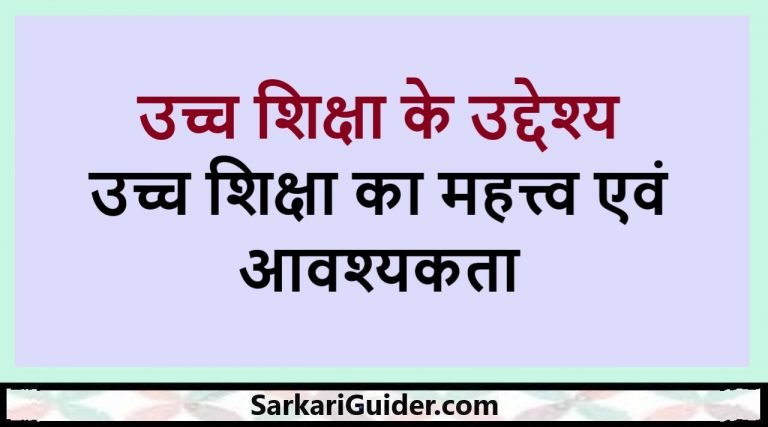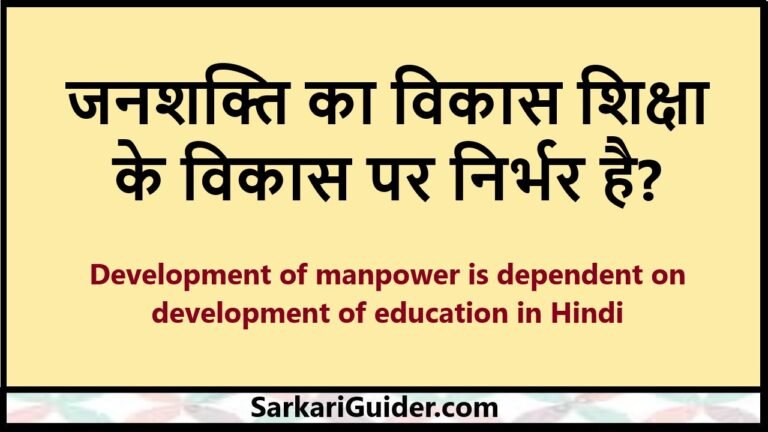पाठ सामग्री का प्रारूप | Format of the Text in Hindi

पाठ सामग्री का प्रारूप | Format of the Text in Hindi
पाठ सामग्री का प्रारूप (Format of the Text)-
अच्छी साज-सज्जा एवं सुव्यवस्थित दिखने वाली वस्तु की ओर व्यक्ति का ध्यान आकृष्ट होना स्वाभाविक होता है। इसी प्रकार सुन्दर सजी-धजी पुस्तक को देखकर शिक्षार्थीं को भी प्रसन्नता होती है। किन्तु यहाँ पर प्रश्न यह है कि क्या अच्छी साज-सज्जा एवं व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की गई सामग्री वाली पुस्तक का कोई शैक्षिक महत्त्व भी है अथवा नहीं? इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी।
दूरस्थ शिक्षार्थी अध्ययन के प्रति स्वतः अभिप्रेरित होता है। अतः सामान्य दृष्टि से पाठ सामग्री को प्रस्तुत करने का ढंग उसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है किन्तु ऐसा कुछ प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के साथ ही होता है। अधिकांश शिक्षार्थी पाठ सामग्री के प्रस्तुत करने के ढंग अर्थात् आकर्षक शीर्षक, मोटा टाइप /मुद्रण, अच्छे रेखाचित्र, रंगीन सामग्री, सुन्दर आवरण पृष्ठ तथा अच्छे कागज आदि से अध्ययन की ओर अभिप्रेरित होते हैं तथा इनके अभाव में अध्ययन के प्रति निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं ।
पाठ सामग्री को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में तीन बिन्दुओं पर मुख्य रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है-
(i) पठनीयता अथवा पढ़ने में स्पष्टता,
(ii) आकर्षणशीलता तथा
(iii) सुगम्यता ।
पाठ सामग्री के प्रारूप की उपयुक्त तीनों विशेषताएँ जहाँ एक ओर उसे व्यवस्थित रूप प्रदान करती हैं वहीं दूसरी ओर पाठ सामग्री की प्रभावशीलता में भी वद्धि करती है। अतः इन तीन बिन्दुओं पर हम कुछ अधिक विस्तार से चर्चा करना उपयुक्त समझते हैं।
(i) पठनीयता (Legibility)-
पठनीयता को प्रभावित करने वाले कारकों में टाइप आकार एवं शैली, टाइप को व्यवस्थित करने का ढंग, प्रयुक्त किये गये कागज का आकार एवं प्रकार आदि प्रमुख होते हैं।
टाइप (मुद्रण हेतु प्रयुक्त अक्षर) का आकार अध्ययनकर्त्ता की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। जैसे शीर्षकों को बड़े आकार के अक्षरों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उपशीर्षकों के अक्षर शीर्षक के अक्षर से थोड़े छोटे आकार एव मोटाई के होने चाहिए तथा सामग्री को प्रस्तुत करने वाले पैराग्राफ के अक्षर सामान्य आकार एवं मोटाई के होने चाहिए। इसी प्रकार टाइप की शैली भी आवश्यकतानुसार सामान्य, तिरछी अथवा हल्की मोटाई वाली हो सकती है। किन्तु अधिकांश सामग्री अक्षरों में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए क्योंकि पाठक के लिए अधिक देर तक पढ़ने में ऐसे अक्षर ही उपयुक्त होते हैं। प्रयोगों के आधार पर भी इस तथ्य की पुष्टि की जा चुकी है।
टाइप को व्यवस्थित करने का ढंग भी अध्ययन को प्रभावित करता है। वही व्यवस्था सबसे अच्छी होती है जिसे आँखें प्रभावशाली ढंग से ग्रहण कर सकती हों। इसमें सबसे प्रमुख विचारणीय बिन्दु वाक्यों की लम्बाई होती है। लम्बे वाक्यों को पढ़ने में आँखों को पीछे की ओर बार-बार ले जाना होता है तथा उन्हें समझने में भी अधिक समय लगता है। इनमें गलतियों तथा गलत समझने की भी अधिक सम्भावना रहती है। सामान्यतया यह देखा गया है कि 60 अक्षरों से अधिक अक्षरों वाली लाइनों (वाक्यों) को पढ़ने में प्रायः त्रुटि हो जाती है। अतः वाक्य अधिक लम्बे नहीं होने चाहिए। सामग्री को बहुत छोटे वाक्यों में प्रस्तुत करने से पढ़ने तथा आँखों द्वारा उन्हें एक साथ ग्रहण करने में सुविधा होती है। किन्तु सम्पूर्ण को बहुत छोटे वाक्यों में प्रस्तुत कर पाना भी सम्भव नहीं होता है। इसलिए मध्यम लम्बाई के वाक्यों को अधिक प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार पैराग्राफ़ भी आवश्यकता से बहुत बड़े नहीं होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ किसी एक विचार अथवा अवधारणा से जुड़ा होना चाहिए। नया पैराग्राफ पर्याप्त स्थान छोड़ते हुए प्रारम्भ किया जाना चाहिए।
पाठ सामग्री की पठनीयता उसके लिए प्रयुक्त किये गये कागज के आकार, उसके रंग एवं गुणवत्ता से भी प्रभावित होती है। अच्छे कागज पर अच्छे एवं उपयुक्त रंग की स्याही में मुद्रित सामग्री पाठक को स्वयमेव अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त स्पष्ट ढंग से मुद्रित ग्राफ, चार्ट, प्रयोग प्रदर्शन और आँकड़े आदि भी पठनीयता को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं।
(ii) आकर्षणशीलता (Attractiveness)-
अनुदेशनात्मक सामग्री को प्राप्त करने पर शिक्षार्थी सर्वप्रथम उसकी पैकिंग, आवरण पृष्ठ तथा आवरण पृष्ठ पर मुद्रित शीर्षक की देखता है। इसके पश्चात वह कागज के रंग, रूप, आकार तथा मुद्रण शाली की ओर ध्यान देता है तथा अन्त में अन्तर्वस्तु की ओर आकृष्ट होता है। अतः अनुदेशनात्मक सामग्री की इकाई अथवा पाठ का आवरण अच्छे एवं मोटे कागज का होना चाहिए तथा उस पर शीर्षक मोटे टाइप में मुद्रित होना चाहिए। आवरण प्रष्ठ पर इकाई से सम्बन्धित कोई महत्त्वपूर्ण चित्र (उपयुक्त रंगों से युक्त) भी बना होना चाहिए जिससे शिक्षार्थी उसे देखते ही उसकी ओर आकृष्ट हो सके। इकाई के मुद्रण में पठनीयता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए तथा मुद्रण की नवीन तकनीकों कानअथासंभव प्रयोग किया जाना चाहिए। अन्तर्वस्त शिक्षार्थी के लिए उपयोगी होनी चाहिए तथा, उसके प्रस्तुतीकरण में पृष्ठपोषण का विशेष प्रावधान होना चाहिए।
उपर्युक्त सभी विशेषताओं से युक्त सामग्री शिक्षार्थी को अपनी ओर स्वतः आकर्षित करता है तथा वह अध्ययन हेतु अधिक अभिप्रेरित होता है।
(iii) सुगम्यता (Accessibility)-
दूरवर्ती शिक्षा की स्वतः अनुदेशनात्मक सामग्री शिक्षार्थी केन्द्रित होती है। अतः यह सामग्री ऐसे होनी चाहिए जिसे शिक्षार्थी अपने अनुसार प्रयुक्त कर सके। इसीलिए एक अच्छी दूरवर्ती शिक्षण इकाई बहुत सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित होनी चाहिए जिससे शिक्षार्थी उस तक सरलता से पहुँच सके एवं उसे ग्रहण कर सके। सामग्री की सुगम्यता ही इसकी उपयोगिता को बढ़ाती है। सुव्यवस्थित सामग्री शिक्षार्थी को आग बढ़ते रहने में सहायता प्रदान करती है तथा अधिगम को प्रभावी बनाती है।
अनुदशनात्मक सामग्री को सुगम्य बनाने हेतु विभिन्न संरचनात्मक विधियों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इन विधियों में उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, उपयुक्त शीर्षक प्रदान करना, आवश्यकतानुसार साराश प्रस्तुत करना, इकाई को विभिन्न भागों एवं उपभागों में विभक्त करना आदि प्रमुख हैं। ये विधियाँ शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार सामग्री तक पहुँचने एवं उन्हें ग्रहण करने में सहायक होती है। दूरवर्ती शिक्षा में सुगम्य विधियों का प्रयोग इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि शिक्षार्थी को स्वतः अध्ययन करना होता है। ये विधियाँ दूरस्थ शिक्षार्थी को निम्नलिखित रूपों में सहायक होती है-
- विषय सामग्री तथा अन्तर्वस्तु की ओर ध्यान आकृष्ट करती है।
- प्रमुख अध्ययन बिन्दुओं के चयन में सहायक होती है।
- मुख्य बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करती है।
- अध्ययन सामग्री तथा अध्ययन समय में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है।
- सामग्री को दुहराने तथा उसकी समीक्षा करने में सहायक होती है।
- शिक्षार्थी को अपने अनुसार अध्ययन को प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान करती है।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- दूरदर्शन | दूरदर्शन का शैक्षिक उपयोग | दूरदर्शन का गुण तथा दोष | शैक्षणिक टेलीविजन की प्रमुख योजनाएँ
- ओवर हेड प्रोजेक्टर | OHP की कार्यप्रणाली | OHP की संरचना | ओवर-हेड प्रोजेक्टर की विशेषतायें
- ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग | ओवरहेड प्रोजेक्टर के लाभ
- रेडियो | भारत में शैक्षिक रेडियो का विकासात्मक इतिहास | रेडियो के उपयोग | रेडियो द्वारा शिक्षण | शैक्षिक समाचारों में रेडियो
- वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कम्प्यूटर का प्रयोग | Use of computer in current education system in Hindi
- टेलीकांफ्रेंसिंग का अर्थ | टेलीकांफ्रेंसिंग के प्रकार | The meaning of teleconferencing in Hindi | Types of teleconferencing in Hindi
- शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर का प्रयोग | Use of computer in the field of education in Hindi
- पाठ्यक्रम का अर्थ | दूरवर्ती शिक्षा मे पाठ्यक्रम विकास के आवश्यक तत्त्व
- पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया | पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान
- अनुदेशनात्मक सामग्री की इकाई संरचना | Unit Structure of Instructional Material in Hindi
- अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री | अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री की विशेषतायें
- इण्टरनेट का अर्थ | इंटरनेट के उपयोग | The meaning of internet in Hindi | Uses of Internet in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]