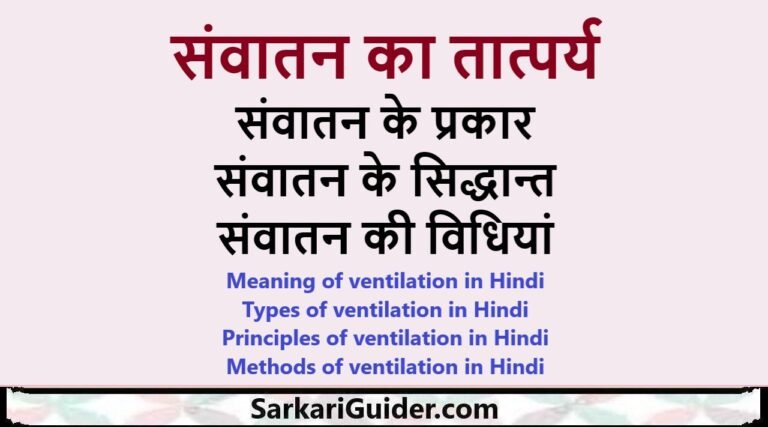बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य | बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध धर्म का प्रसार

बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य | बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध धर्म का प्रसार
बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य
(Aims of Buddhist Education)
बौद्ध कालीन शिक्षा में आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल न देकर नैतिकता पर अधिक ध्यान दिया जाता था। नैतिक चरित्र में अन्य गुणो के साथ-साथ जीवन में पवित्रता, कर्त्तव्य-पालन निष्ठा, मधुर स्वभाव एवं अच्छा आचरण जैसे गुण भी निहित थे। बौद्ध कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य संक्षेप में निम्न प्रकार है-
(1) बौद्ध धर्म का प्रसार करना-
बौद्ध काल की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना वास्तव में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुकों को तैयार करने के लिये की गयी थीं। शुरू में इन शिक्षा संस्थाओं अर्थात् बौद्ध मठों में केवल बौद्ध भिक्षुकों को प्रवेश दिया जाता था इन बौद्ध मठों में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार तथा प्रसार करना था।
(2) नैतिक चरित्र का निर्माण करना-
बौद्ध काल की शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों के चरित्र के विकास करना था, क्योंकि बौद्ध काल में नैतिक आचरण पर अधिक बल दिया जाता था। इसलिए शिक्षा के द्वारा छात्रों में कर्त्तव्य-पालन, सत्य बोलने, धर्म का आचरण करने आदि नैतिक गुणों का विकास किया जाता
(3) जीवन ले लिए तैयार करना-
शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चरित्र के विकास करना था, क्योंकि बौद्ध काल में नेतिक आचरण पर अधिक बल दिया जाता था। इसलिए शिक्षा के द्वारा छात्रों में कर्त्तव्य पालन, सत्य बोलने, धर्म का आचरण करने आदि नेतिक गुणों का विकास किया जाता था।
(4) व्यक्तित्व का विकास करना-
बौद्ध काल की शिक्षा का एक और महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना था । बौद्ध मठों में छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके उन्हें श्रेष्ठ और कुशल व्यक्ति बनाने का प्रयत्न किया जाता था। जिससे वे पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों के उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभा सकें।
बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध धर्म का प्रसार
(Extansion of Buddh Dharm in Buddhist Education)
बौद्ध काल की शिक्षा संस्थायें मूलतः बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु बौद्ध भिक्षुओं को तैयार करने के लिए की गई थी। प्रारम्भ में इन शिक्षा संस्थाओं अर्थात् बौद्ध मतों में केवल बौद्ध भिक्षुओं को प्रवेश दिया जाता था छात्रों को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे गये चार सत्यों का ज्ञान कराया जाता था-
(1) संसार दु:खमय है,
(2) इन दुःखों से छुटकारा सम्भव है
(3) सांसारिक दु:खों से छुटकारा ही निर्वाण है और
(4) निर्वाण प्राप्ति के लिए जप-तप नहीं, मानवमात्र के प्रति कल्याण की भावना आवश्यक है।
तत्पश्चात् उन्हें निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग में प्रशिक्षित किया जाता था-
(1) सम्यक् दृष्टि,
(2) सम्यक् संकल्प,
(3) सम्यक् कर्मान्त,
(4) सम्यक् वाक्.
(5) सम्यक् आजीव,
(6) सम्यक् व्यायाम,
(7) सम्यक् स्मृति और
(8) सम्यक् समाधि ।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य | प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख आदर्श
- प्राचीनकालीन भारतीय शिक्षा के आधुनिक शिक्षा के लिये ग्रहणीय तत्त्व | Adaptive elements of ancient Indian education for modern education in Hindi
- वैदिक साहित्य में शिक्षा का अर्थ | प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएँ
- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य केन्द्र | वैदिककालीन शिक्षा के स्तर
- बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषतायें | बौद्धकालीन शिक्षा की आधुनिक भारतीय शिक्षा को देन
- मुस्लिमकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषतायें | मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषतायें
- मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य दोष | Chief Defects of Medieval Education System in Hindi
- वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली | Teaching System in Vedic Period in Hindi
- पब्बजा तथा उपसम्पदा संस्कार में अन्तर | प्रवज्या तथा उपसम्पदा संस्कार में अन्तर | Difference between Pabajja and Upsampada Sanskar in Hindi
- वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में समानताएँ | Similarities Between the Vedic Education System and Buddhist Education System in Hindi
- मुस्लिमकालीन शिक्षा व्यस्था | मुस्लिमकालीन शिक्षा के उद्देश्य | मुस्लिमकालीन शिक्षा के प्रमुख केन्द्र
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]