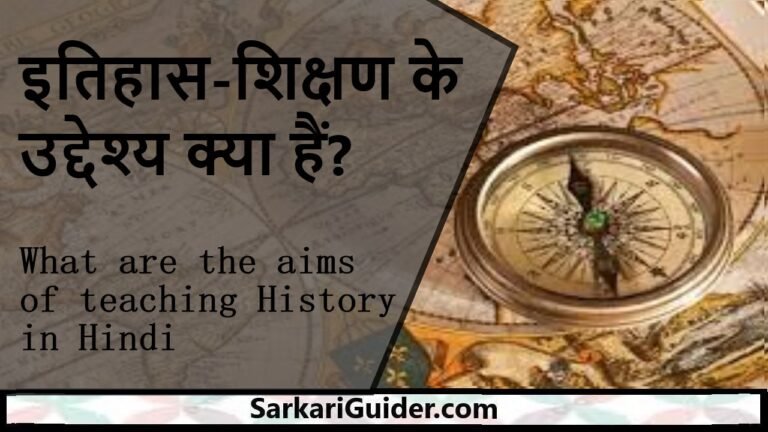उदारवादी कौन थे? | उदारवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति | उदारवादियों की उपलब्धियाँ
उदारवादी कौन थे? | उदारवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति | उदारवादियों की उपलब्धियाँ
उदारवादी कौन थे?
1885 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 से 1905 तक कांग्रेस की गतिवदियों पर उदारवादियों का प्रभुत्व बना रहा। इस काल में कांग्रेस की नीति अत्यन्त उदार रही। अतः इस काल को उदारवादी युग कहा जाता है। उदारवादी नेताओं में सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पण्डित मदनमोहन मालवीय आदि प्रमुख थे।
उदारवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति
उदारवादियों की विचारधारा और कार्यपद्धति को निम्नलिखित सूत्रों के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है-
(1) अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास- उदारवादी नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उनके विचार में अंग्रेज स्वतन्त्रता प्रेमी हैं और यदि उन्हें भारतीयों की योग्यता पर विश्वास हो जाए, तो वे उन्हें स्वशासन बिना संकोच के दे देंगे। 1890 में फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि “मुझे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अन्त में जाकर हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे।” सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का कहना था कि “हाँ अंग्रेजों की न्यायप्रियता तथा उदारता में पूर्ण विश्वास है।”
(2) ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति- उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति रखते थे। वे ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के कल्याण के लिये जो कार्य किये, थे उनके लिये वे बड़े कृतज्ञ थे। 1890 में फिरोज मेहता ने कहा था कि “हम आशा करते हैं कि अंग्रेज जाति हमारी राजभक्ति पर विश्वास करेगी। मेरी राजभक्ति चट्टान की तरह दृढ़ है।”
(3) पाश्चात्य सभ्यता के प्रबल समर्थक- उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। वे बर्क, मिल, मैकाले, हरबर्ट स्पेन्सर आदि के विचारों से बड़े अप्रभावित थे। उन्होंने पाश्चात्य विचारकों से ही स्वतन्त्रता, समानता, लोकतंत्र आदि के विचार ग्रहण किये थे। वे पाश्चात्य शिक्षा के प्रबल समर्थक थे।
(4) ब्रिटेन के साथ स्थायी सम्बन्ध बनाये रखने के समर्थक- उदारवादी ब्रिटिश शासन को भारत के लिये वरदान मानते थे। इसलिए वे ब्रिटेन के साथ स्थायी सम्बन्ध बनाये रखने के पक्ष में थे। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटेन के साथ स्थायी सम्बन्ध रखने से ही भारत का बहुमुखी विकास सम्भव है। अतः वे भारत की प्रगति के लिए ब्रिटिश शासन को आवश्यक मानते थे।
(5) संवैधानिक साधनों में विश्वास- उदारवादी संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। हिंसात्मक तथा क्रान्तिकारी मार्ग में उनकी तनिक भी आस्था नहीं थी। वे प्रार्थनाओं, प्रार्थना- पत्रों, स्मरणपत्रों और शिष्ट मण्डलों द्वारा सरकार से अपनी मांगों को मानने की प्रार्थना करते थे। वे सरकार के सामने अपनी मांगों को अत्यन्त नम्रतापूर्वक पेश करके उनको पूरी करने के लिये निवेदन करते थे। वे अपील, दलील तथा वकील के सिद्धान्त में विश्वास करते थे।
(6) क्रमिक सुधारों पर विश्वास- उदारवादी नेता राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे। वे राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में धीरे-धीरे सुधार लाये जाने के पक्ष में थे। वे क्रान्तिकारी परिवर्तनों के विरुद्ध थे।
(7) प्रशासनिक सुधारों की मांग- उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के सामने निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत की-
(i) धारा सभाओं का विस्तार हो, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सम्मिलित हों।
(ii) इण्डियन कौंसिल को समाप्त किया जाए।
(iii) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा सभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए।
(iv) सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयो को अधिक संख्या में लिया जाए।
(v) इण्डियन सिविल सर्विस की परीक्षाके लिए भारत में भी व्यवस्था की जाए तथा इन सेवाओं में प्रवेश की आयु बढ़ाई जाए।
(vi) औद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए।
(vii) कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए तथा न्याय व्यवस्था पर जूरी का अधिकार हो।
(viii) शासन तथा सेना सम्बन्धी खर्च कम किया जाए।
(ix) भारत-सचिव की कौंसिल में तथा प्रिवी कौंसिल में भारतीयों को स्थान दिया जाए।
(x) भारत मन्त्री के वेतन का भुगतान ब्रिटिश को से किया जाए।
(xi) किसानों पर लगे हुए भूमि-कर में कमी की जाए।
(xii) जनता पर लगे हुए करों में कमी की जाए।
(xiii) कृषि के विकास के लिये सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए तथा कृषि बैंक की स्थापना की जाए।
(xiv) विदेशों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा की व्यवस्था की जाए।
(xv) प्रेस पर नियन्त्रण कम कर उसे अधिक स्वतन्त्रता दी जाए।
(8) राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति पर बल देना- उदारवादी ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत ही स्वशासन चाहते थे। उनके विचारों में ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारतीयों को स्वशासन का काफी प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका था और अब भारत स्वशासन के लिये तैयार था। सुरेन्द्र बनर्जी का कहना था कि “स्वशासन भारतीयों के लिये कोई नई व्यवस्था नहीं तथा स्वतन्त्र संस्थाएँ देश के बौद्धिक एवं नैतिक संयम की सबसे अच्छी पाठशालाएँ होती हैं। इनके बिना स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन सम्भव नहीं।”
उदारवादियों की उपलब्धियाँ
उदारवादियों की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित थीं-
(1) राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना- उदारवादियों ने भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता आदि का विरोध किया और राष्ट्रीयता का प्रचार किया। उन्होंने देश की प्रमुख समस्याओं पर विचार करने के लिये एक रंगमंच तैयार किया और समस्त भारतवासियों को राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया। गुरुमुख निहाल सिंह का कथन है कि “कांग्रेस ने आरम्भ में लोगों में राष्ट्रीय जागृति, राजनीतिक शिक्षा तथा भारतीयों में संगठन की भावना उत्पन्न करने का कार्य किया और लोगों में सामान्य राष्ट्रीय चेतना जागृत की।”
(2) ब्रिटिश सरकार की त्रुटियों को प्रकट करना- उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की त्रुटियों का पर्दाफाश किया। उन्होंने सरकार की दमनकारी और शोषणकारी नीति की आलोचना की। दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार की धन निष्कासन की नीति को भारत की निर्धनता के लिए उत्तरदायी बताया।
(3) भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना- उदारवादियों ने भारतवासियों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उन्हें स्वशासन, प्रजातन्त्र तथा स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये प्रेरित किया। उन्होंने सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-विमर्श के लिये एक मंच तैयार किया और देश की प्रमुख समस्याओं पर एक प्रबल जनमत तैयार किया।
(4) भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना- उदारवादी नेताओं के भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की। डॉ० पट्टाभिसीतारमैया का कथन है । “जिस समय भारत के राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादियों ने पदार्पण किया, उस समय वे अकेले थे। उन्होंने जो नीतियाँ अपनाई, उनके लिये हम कोई दोष नहीं दे सकते। किसी भी आधुनिक इरमात की नींव में 6 फुट नीचे जो ईंट चूना, पत्थर गड़े हैं, क्या उन पर कोई दोष लगाया जा सकता है। क्योंकि वही तो आधार है जिसके ऊपर सारी इमारत खड़ी हो सकी है। सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वशासन, फिर साम्राज्य के अन्तर्गत होमरूल उसके बाद स्वराज्य तथा सबके शीर्ष पर पूर्ण स्वाधीनता की मंजिलें एक के बाद एक बन सकी हैं।
(5) भारतीय परिषद् अधिनियम (1892)- उदारवादियों के प्रयासों के फलस्वरूप 1892 ई० में भारतीय परिषद् अधिनियम पारित हुआ। यद्यपि यह अधिनियम भारतवासियों की आकाँक्षाओं को सन्तुष्ट नहीं कर सका, परन्तु फिर भी यह भारत में प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं के विकास की दिशा में पहला कदम था।
इतिहास – महत्वपूर्ण लिंक
- उग्रवादी कौन थे? | उग्रवादियों की विचारधारा की प्रमुख विशेषताएँ | उग्रवादियों की उपलब्धियाँ
- मुसोलिनी की विदेश नीति | मुसोलिनी की विदेश नीति के उद्देश्य | मुसोलिनी की विदेश नीति | मुसोलिनी की विदेश नीति का विश्व शान्ति पर प्रभाव
- इटली के एकीकरण में सहायक तत्व | Auxiliary elements in the unification of Italy in Hindi
- फासीवाद का अर्थ | इटली में फाँसीवाद के उदय के कारण | मुसोलिनी का उत्कर्ष | मुसोलिनी तथा फाँसीवाद का अन्त | मुसोलिनी के पतन के कारण | इटली में फाँसीवाद का विकास
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]