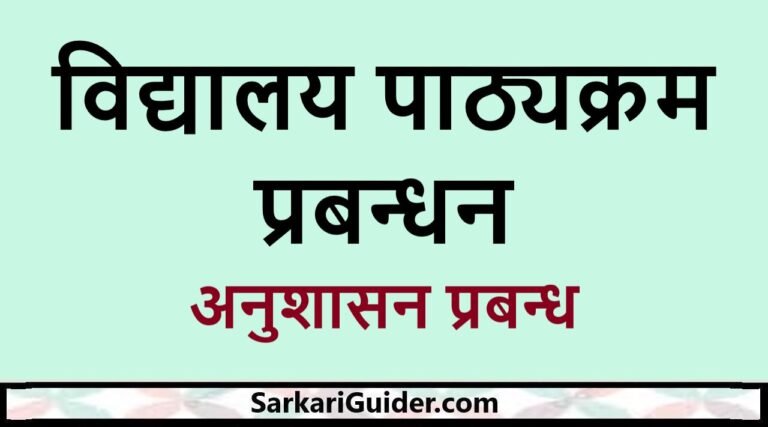मानसिक अस्वास्थ्य | मानसिक अस्वस्थता के प्रकार
मानसिक अस्वास्थ्य | मानसिक अस्वस्थता के प्रकार
मानसिक अस्वस्थता के प्रकार
जब व्यक्ति अपने कार्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर नहीं कर पाता या उनसे समायोजन नहीं स्थापित कर पाता तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और उसमें मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप उत्पन्न हुई कुण्ठा इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति सुरक्षा प्रक्रियाओं का अति प्रयोग करने लगता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य और भी खराब हो जाता है। कुसामञ्जस्य या कुसमायोजन से उत्पन्न हुई मानसिक अवस्था निम्नलिखित पाँच प्रकार की होती है-
(1) साधारण समायोजन दोष- यह ऐसी मानसिक अवस्था है जो हर व्यक्ति में पायी जाती है। मानसिक अस्वस्थता का यह बहुत ही सामान्य रूप है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अनेकों अवसर आते हैं जब वह किसी बाधा के कारण अपने काम को पूरा करने में असफल रहता है। ये व्यक्तियों में कुछ सामान्य दोष पैदा कर देते हैं जो न्यूनाधिक प्रत्येक व्यक्ति में पाये जाते हैं। ये हैं चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, हठ अतिशय संवेदनशीलता इत्यादि।
(2) आचारोन्मावित व्यक्तित्व- यह मनोरुग्णता समाज विरोधी कार्यों से सम्बन्धित है। इस कोटि में जो लोग आते हैं उनमें आचरण सम्बन्धी दोष होते हैं जैसे चोरी करना, दूसरों को धोखा देना, वेश्यागमन, झूठ बोलना, ठगना इत्यादि।
(3) मनोदैहिक रोग- इस वर्ग में वे मानसिक रोग शामिल हैं जिनका कारण शरीर में ही निहित होता है। वे शारीरिक व्याधि से उत्पन्न होते हैं। जैसे सिर में या शरीर के किसी भाग में चोट लग जाने से स्थायी दोष उत्पन्न हो गया है जो सदैव पीड़ा या कष्ट देता हो, मादक द्रवों या वस्तुओं के सेवन करने से भी मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सिगरेट, तम्बाकू, मदिरा, अफीम, गाँजा, चरस आदि । निम्न या उच्च रक्त चाप भी मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देता है। दमा-खाँसी, चिड़चिड़ापन पैदा कर देते हैं और कब्जियत या जिगर की बीमारियाँ मानसिक विकार उत्पन्न कर देती हैं।
इस वर्ग में कुछ ऐसे रोग भी शामिल हैं जो मानसिक कारणों से शरीर और मन दोनों को प्रभावित कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रवृत्ति के बलात् दमन किया गया तो वह हदय की धड़कन, श्वास प्रक्रिया, रक्त की रचना सभी को बदल देती है जिससे शरीर में स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है।
(4) मनस्ताप- जब समायोजन-दोष कुछ गम्भीर रूप ले लेते हैं तो वे मनस्ताप कहलाते हैं। इसके अन्तर्गत आने वाले दोष इतने गम्भीर नहीं होते हैं कि उन्हें ठीक करवाने के लिए चिकित्सालयों में जाना पड़े। ये व्यक्तित्व में केवल आंशिक दोष ही उत्पत्र करते हैं। मनस्ताप के अन्तर्गत निम्नलिखित मनोस्नायु विकृतियाँ या मानसिक रोग शामिल हैं-
(i) मनोस्नायु दौर्बल्य- इन मानसिक रोग का सर्वप्रधान लक्षण थकान है। रोगी को अकारण हमेशा यकान का अनुभव होता रहता है। इससे सम्बन्धित और भी लक्षण हैं-दिल धड़कना, मन्दाग्नि, काम करने की इच्छा न होना, शक्तिहीनता, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, कब्जियत, शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द, सम्भोग में असफलता इत्यादि। ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के विषय में सदैव चिन्तित रहता है और अपनी व्यथा कहने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है।
(ii) चिन्ता मनोस्नायु-विकृति- इस रोग में चिन्ता प्रधान होती है। वैसे तो थोड़ी बहुत चिन्ता हर व्यक्ति को होती है किन्तु इस प्रकार के रोगियों में यह प्रधान लक्षण हो जाती है। उसमें अकारण भावी चिन्तायें घर कर लेती हैं। उसे अपनी चिन्ताओं के कारण का पता नहीं होता किन्तु वह सदैव सशंकित आर भयभीत रहता है। वह किसी दुर्घटना, चोरी, डकैती, प्रियजन की मृत्यु, आग लगना, सर्पदंश आदि के विषय में सदैव सशंकित रहता है। ऐसे लोगों के रक्तचाप, श्वास-प्रक्रिया, दिल की धड़कन, नाड़ी की गति परिवर्तनशील होते हैं। वह चिड़चिड़ा, मलिन और दुःखी होता है।
(iii) विश्वासबाध्यता या माध्यता भनोस्नायुविकृत- इस रोग से पीड़ित व्यक्ति निराधार विचारों, कल्पनाओं और विश्वासों का पोषण करते रहते हैं। वाहने पर भी उनसे उन्हें छुटकारा नहीं मिल पाता। ये विचार प्रायः असंगत और आधारहीन होते हैं। कुछ लोग बराबर हाथ धोते रहते हैं, कुछ को हस्ताक्षर करने की धुन होती है, कुछ किसी शब्द विशेष को निरन्तर लिखते या बोलते हैं। एक व्यक्ति को हाथ मलने की बाध्यता थी। उसने 100 रु० का एक नोट हाथ मलते-मलते रगड़कर फाड़ डाला। इसका ज्ञान उसे तब हुआ जब वह समाप्त हो गया था। कुछ लोगों को अच्छे कार्यों के प्रति भी बाध्यता हो जाती है ये महान बन जाते हैं। ऊँचे वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं धार्मिक लोगों में यह बाध्यता होती है।
(iv) भीतियाँ- इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को कुछ वस्तुओं, जीवों या व्यक्तियों से अकारण भय उत्पन्न हो जाता है और वह अपेक्षाकृत स्थायीरूप ले लेता है। जैसे बड़े होने पर पानी से डरना, खुले आकाश के नीचे लेटने पर यह लगना कि आकाश मेरे ऊपर गिर पड़ेगा, भीड़ से डरना, बन्द जगह से डरना इत्यादि ।
(v) उन्माद- उन्माद के मानसिक रोग से भारतीय और दुनिया के अन्य लोग भी बहुत प्राचीन काल से परिचित हैं। भारत में आयुर्वेद में और यूनान में यूनानी चिकित्सा- पद्धति में इसके उपचार का वर्णन है। यह रोग शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त होता है। इनमें से कुछ लक्षण स्थायी और कुछ अस्थायी होते हैं। उन्माद इन रूपों में पाया जाता है-
(अ) अंग विक्षेपक आक्रमण- संवेगात्मक उपायों के कारण व्यक्ति कभी हाथ-पैर- पटकता है, दाँत किटकिटाता है, दाँत काटता है, कराहता है, कपड़ा नोचता है, भुंकता है, हँसता और चिल्लाता है।
(ब) स्वप्नचारिता- कुछ लोग सोते-सोते उठकर चलने लगते हैं और कुछ विशेष कार्य करके लेट जाते हैं। इस प्रकार के कार्यों में उन्हें चेतना नहीं होती। स्वप्न में निद्रावस्था में किये गये कार्यों का उन्हें कोई होश नहीं रहता। एक व्यक्ति रोज रात में उठकर रस्सी गगरे से कुएँ से पानी भरता था फिर अपना विस्तर तर करके सो जाता था और सुबह उठने पर मुहल्ले वालों को विस्तर में पानी डालने के लिए गाली देता था।
(स) आत्मविस्मृति- इस उन्माद में व्यक्ति अपने को भूल जाता है, उठकर कहीं चला जाता है। फिर जब होश आता है तो लौटता है। इस प्रकार की आत्म-विस्मृति महीनों रह सकती है।
(द) अनैच्छिक लयात्मक गति- रोगी के शारीरिक अंग एक निश्चित ढंग से गति करते हैं जैसे आँख फड़कना, मुँह सिकुड़ना, मुँह टेढ़ा होना इत्यादि । पेशीय संकोचन के कारण इस प्रकार की गतियाँ होती हैं। ये गतियाँ रोगी की इच्छा के विरुद्ध होती हैं और उन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता।
(इ) अंग शून्यता- उन्माद का सम्बन्ध स्नायुओं के लकवे से होता है। अंग सुन्न हो जाता है। यह लकवा सामान्य रूप से शारीरिक नहीं होता। कभी एक रोगी एक अंग देखता है और दूसरा रोगी दूसरा अंग देखता है। कभी अंग शून्यता से भूख का न मालूम होना या सुई की चुभन का अनुभव होने लगता है।
(फ) पीड़ा- रोगी के विभिन्न अंगों में भीषण पीड़ा होती है।
(5) मनोविकृति- इस रोग में गम्भीर से गम्भीरतम सभी प्रकार के मानसिक रोग शामिल होते हैं। ये जल्दी नहीं अच्छे होते और इनका उपचार भी बड़ा टेढ़ा और कठिन होता है। ऐसे रोगी अवास्तविकता के जगत् में पहुँच जाते हैं और यथार्थता से इनका सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। रोगी तरह-तरह के भ्रम एवं भ्रान्तियों का शिकार रहता है। मनोविकृति के निम्नलिखित तीन प्रमुख रूप हैं-
(i) मनोविदलता- इसे पहले मनोव्यापार-संतुष्टि कहते थे किन्तु अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका मुख्य काल किशोरावस्था से तीस वर्ष की आयु तक है। अपेक्षाकृत पुरुष इस रोग से अधिक पीड़ित होते हैं। इसके प्रमुख लक्षण ये हैं-
(1) व्यक्ति में सुख-दुःख की अनुभूति समाप्त हो जाती है। वह एक ओर चुपचाप बैठा एकटक ताकता रहता है। कभी-कभी वह सुख के स्थान पर दुःख और दुःख के स्थान पर सुख के संवेग का अनुभव करता है और उसी के अभिव्यक्ति भी करता है। उसके संवेग उलट-पलट जाते हैं। (2) वह अकारण चिल्लाता या सता है। (3) उसमें स्वाभाविकता का पूर्ण अभाव होता है। वह दिवास्वप्न में ही लिप्त रहता है। (4) उसमें ज्ञानेन्द्रियों के विभ्रम (विशेष रूप से ध्वनि सम्बन्धी) अधिक पाये जाते हैं। दुःखद विभ्रमों की अधिकता रहती है। (5) रोगी में अनेक व्यामोह (delusion) पाये जाते हैं लेकिन दण्ड व्यामोह की उसमें प्रधानता रहती है। दो व्यक्तियों को बात करते देखकर वह यही समझने लगता है कि वे उसे विष देने या मार डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। (6) कभी-कभी वह निरर्थक किन्तु सही और शुद्ध वाक्य बोलता है। कभी-कभी अपने को मृत समझकर चुप रहता है। कभी-कभी यह सोचकर चुप रहता है कि ईश्वर ने उसे बोलने के लिए मना कर दिया है। उसकी भाषा-शक्ति अस्त-व्यस्त हो जाती है। (7) रोगी की चिन्तन और तार्किक योग्यता भी लगभग समाप्त हो जाती है। (8) वह अतीत का स्मरण कर लेता है किन्तु वर्तमान का नहीं। (9) उसकी मानसिक क्रियाओं में कोई समन्वय नहीं होता। उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व टुकड़े-टुकड़े हो जाता है।
(ii) उत्साह-विषाद मनोविकृति (Manic-depressic psychoses)- पहले उत्साह और विषाद दोनों को अलग-अलग मनोविकृतियाँ माना जाता था किन्तु अब उन्हें एक ही विकार के दो पहलू मानते हैं। मनोविदलता के बाद यह सबसे अधिक व्यापक रोग है और अपेक्षाकृत स्त्रियों में इसका बाहुल्य है। गाँवों की अपेक्षा नगर वाले इससे अधिक पीड़ित होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी तो उत्साह से और कभी विषाद से पीड़ित होते हैं। उत्साह की अवस्था में अधिक सक्रिय रहता है। विषाद की अवस्था में उदासीन हो जाता है। रोगी में प्रत्यक्षीकरण की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। उसे देश, काल, परिस्थिति की केवल एक धुंधली चेतना मात्र रहती है। उसमें निर्णर की शक्ति समाप्त हो जाती है। उत्साह में रोगी में प्रसन्नता, अहंकार, कामुकता, अक्रामक की प्रधानता रहती है, इसलिए वह अक्रामक व्यवहार करता है। कभी-कभी वह नाचने, हंसने, बकने लग जाता है। विषाद में दु:खी, उदासीन निष्क्रिय और खिन्न हो जाता है।
(iii) स्थिर-भ्रम (Paranoia)- रोग की यह अवस्था धीरे-धीरे उत्पन्न होकर बढ़ती है। व्यक्ति में स्थायी और व्यवस्थित भ्रम की उपस्थिति देखी जाती है। वह किसी- न-किसी प्रकार के भ्रम से ग्रसित रहता है और चाहने पर भी उससे छुटकारा नहीं पा सकता। वैसे तो भ्रम सामान्य व्यक्तियों को भी हो जाते हैं लेकिन समझ में आने पर वह अपने को उनसे मुक्त कर लेता है।
रोग का प्रारम्भ सिर दर्द, अनिद्रा, मन्दाग्नि, अरुचि, शरीर के भार का कम होना, चिड़चिड़ापन, सन्देह, भावुकता आदि से होता है। बाद में रोगी आत्म-केन्द्रित हो जाता है। वह जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है। दूसरों के विचारों की उसे चिन्ता नहीं होती। वह दूसरों से घृणा करता है। उनसे उसे अविश्वास होता है। दूसरों को शत्रु समझता है। उसमें हास्य का सर्वथा अभाव होता है।
स्थिर भ्रम के कई रूप दिखाई पड़ते हैं। धार्मिक स्थिर-भ्रमवाले अपने को अवतार समझकर एक अनोखे धर्म का प्रचार करते हैं। कामुक स्थिर-भ्रमवाला ऐसा मान लेता है कि कोई युवती उसे प्रेम करती है। उसे वह प्रेमपत्र लिखता है तथा वह उससे ब्याह करने के लिए व्याकुल रहता है। सुधारात्मक स्थिर-भ्रम का रोगी विश्व को सुधारने का प्रयास करता है। दण्डात्मक स्थिर-भ्रमवाला रोगी दूसरी को शत्रु समझ लेता है और सदैव इस बात की आशंका से भरा होता है कि दूसरों उसकी हानि करने की कोशिश कर रहे हैं।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- किशोरावस्था की विशेषतायें | किशोरावस्था में शारीरिक विकास | किशोरावस्था में मानसिक विकास | किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास | किशोरावस्था में सामाजिक विकास
- परिवर्त्य का तात्पर्य | चर का तात्पर्य | बौद्धिक परिवर्त्य के प्रकार | व्यक्तित्व के परिवर्त्य के प्रकार | परिवर्त्य होने के कारण | अधिगम और बुद्धि एवं व्यक्तित्व के परिवर्त्य | परिवर्त्य के अधिगम | परिवर्त्य मापन से लाभ
- बुद्धि का अर्थ | बुद्धि की परिभाषा | बुद्धि के सिद्धान्तवाद | बुद्धि के प्रकार | बुद्धि मापन का तात्पर्य | मानसिक आयु और कालिक आयु | बुद्धि-लब्धि के प्रसार
- बुद्धि परीक्षण | बुद्धि परीक्षण के प्रकार | व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण | सामूहिक बुद्धि परीक्षण | निष्पादन बुद्धि परीक्षण | व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अन्तर | बुद्धि परीक्षण की शैक्षिक उपयोगिता
- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ | मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषाएँ | मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्त्व
- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र | विद्यालयी बालक की व्यवहार सम्बन्धी समस्यायें
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]