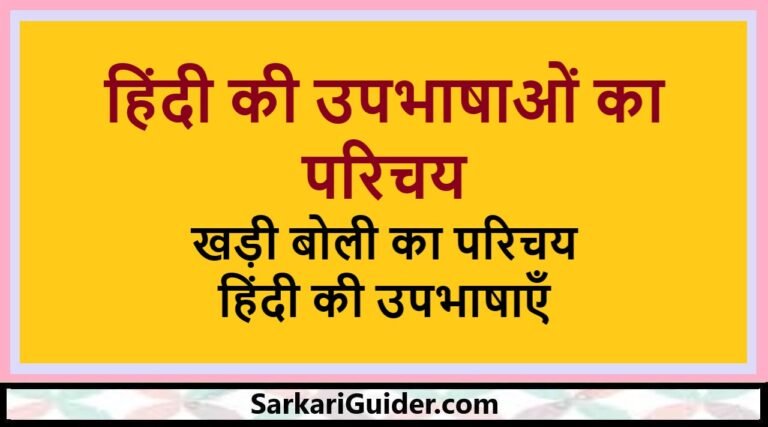हिन्दी की उपभाषा | मध्य भारतीय आर्य भाषा
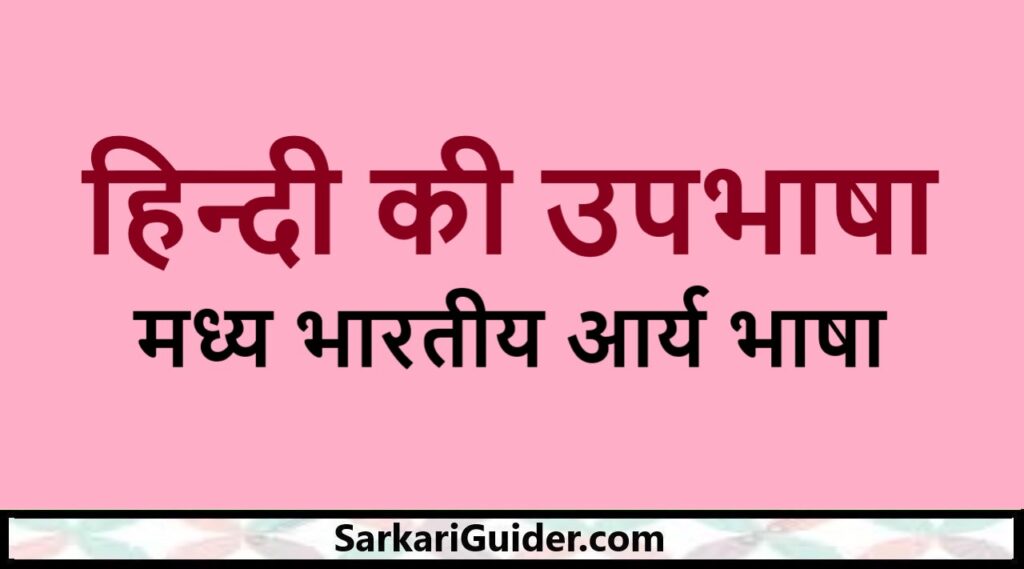
हिन्दी की उपभाषा | मध्य भारतीय आर्य भाषा
हिन्दी की उपभाषा
मध्य भारतीय आर्य भाषा
(500 ई0पू0 से 1000 ई0 तक)
इसका काल 500 ई0पू0 से लेकर 1000 ई0पू0 तक माना जाता है इस काल की भाषाओं के अंतर्गत अशोक के अभिलेखों की भाषा पालि, प्राकृत और अपभ्रंश की गणना होती है। ईसा से 1000-600 वर्ष पूर्व तक आर्यों के प्रसार के परिणामस्वरूप उत्तर-पश्चिमी में गांधार प्रदेश से लेकर पूर्व में विदेह एवं मगध पर्यंत आर्य राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। इसी बीच स्थानीय अनार्य जातियों का आर्यों की सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हो जाना स्वाभाविक था। आर्य- भाषा का भी उन पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ा और अन्य बातों की भाँति इसे भी इसका शुद्ध और सही रूप ग्रहण नहीं कर पाये। फलतः उनके मुख से आर्य-भाषा का प्राचीन रूप विकृत हो उठा।
आर्य-भाषा के मध्यकालीन विकास के सम्यक अध्ययन हेतु इसे तीन खंडों में विभाजित किया जाता है-
खंड 1. इसके अंतर्गत 500 ई0पू0 से 1 ई0पू0 तक की भाषा का विकास अंतर्निहित है। प्रमुख रूप से यह पालि और अशोक के अभिलेखों में प्राप्त भाषा का काल है। पालि किस प्रदेश की भाषा थी, इस विषय पर विद्वानों में परस्पर अत्यधिक वाद-विवाद होता रहा है। अंत में इसे मध्य-देश की भाषा सिद्ध किया गया। पठन की दृष्टि से पालि युद्धकालीन भाषा न सिद्ध होकर पर्याप्त अर्वाचीन प्रतीत होती है। अतः ऐसे समझा गया कि यद्यपि महात्मा बुद्ध ने किसी प्राच्य भाषा में उपदेश किया होगा, तथापि उनके निर्माण के दो सौ वर्षोपरान्त समस्त उपदेशों का अनुवाद किसी मध्यदेशी भाषा में हुआ जो संस्कृत के समकक्ष स्तर पर पहुँच गई थी। पालि भाषा में बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ, टीकायें, कथा-साहित्य, काव्य-कोष एवं व्याकरण आदि ।
खंड 2. यह 1 ई0 से लेकर 500 ई0 तक प्राकृत भाषाओं के विकास का काल है। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति प्राकृत का अर्थ भाषा के क्षेत्र में जन-साधारण की भाषा माना गया। शिष्ट समाज की भाषा संस्कृति थी और सामान्य जन की भाषा प्राकृत भाषाओं के मूल में संस्कृत का आधार माना गया है। डॉ० सरयू प्रसाद अग्रवाल के अनुसार- “प्राकृत भाषाओं की प्रकृति के मूल में कोई न कोई भाषा अवश्य होगी जिसका आधार लेकर प्राकृतों का विकास हुआ वह भाषा संस्कृत मानी गई।” इस संस्कृत का आशय वैदिक संस्कृत (छंदक) तथा उसके अनंतर लोक प्रचलित संस्कृत दोनों से है। मार्कण्डेय ने सोलह प्राकृत भाषाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने प्राकृतों को भाषा, विभाषा, अपभ्रंश और पैशाच चार वर्गों में विभाजित किया है। भाषा के अंतर्गत महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, आवन्ती, मागधी, दक्षिणात्य एवं आहूतों की विभीषिका के अंतर्गत शाकारी, चाण्डाली शाअरी, आधीरिकी, ढक्की के अंतर्गत नागर, उपनागर, मेचड़ (इनमें अपभ्रंश के 27 रूप अंतर्गत हैं), पैशाची के अंतर्गत कैकय, शौरसेन, पांचाल (इनमें 11 पैशाची विभाषाएँ अंतर्भूत हैं) की गणना की गई हैं।
समस्त प्राकृत भाषाओं में महाराष्ट्री प्राकृत प्रधान मानी गई है। कालांतर में प्राकृत भाषा साहित्य में प्रविष्ट होकर शिष्टजनों के पठन-पाठन एवं ग्रंथ निर्माण की भाषा बनकर रह गई। उनका स्वरूप लोक-प्रचलित सामान्य जन भाषा से भिन्न होता गया।
खंड 3. 500 ई0 से लेकर 1000 ई0 तक अपभ्रंश भाषाओं के विकास का युग है। प्राकृत भाषाओं के साहित्य रूढ़ और व्याकरण-बद्ध हो जाने के उपरांत बोल-चाल की भाषा अपनी स्वतंत्र धारा में प्रवाहित होती हुई जन सामान्य के पारस्परिक भाव-विनिमय का माध्यम बनी रही। इसे ही अपभ्रंश संज्ञा से अभिहित किया गया। अपभ्रंश नाम के मूल संस्कृत शब्दों के अपभ्रंश रूपों का ग्रहण कारण रूप में विद्यमान है। संस्कृत पंडितों ने तिरस्कार भाव से यह नाम दिया था। बाद में यही संज्ञा के रूप में प्रचलित हो गया। आरंभ में अपभ्रंश शब्द किसी भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं होता था। अशिक्षित जनों द्वारा बोले गए विकारग्रस्त अशुद्ध शब्द अपभ्रंश भाषाओं का साहित्य में प्रवेश ईसा की छठी शताब्दी से दृष्टिगोचर होता है। भामह एवं दंडि के उल्लेख तथा अल्मी के राजा धरसेन के शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस अपभ्रंश में साहित्य-रचना होने लगी थी। भामह ने वाक्य के गद्य और पद्य बनाकर भाषा की दृष्टि से तीन प्रकार की काव्य भाषाओं के नाम गिनाये हैं- संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश
“संस्कृत प्राकृतं चान्दयभ्रंश इति त्रिधा ।”
वैसे तो ईसा की दूसरी या तीसरी शताब्दी में लिखित ‘प्रेम चरित’ नामक प्रस्तुत ग्रंथ में भी अपभ्रंश के कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। कालिदास के विक्रमोर्वर्शीय नाटक में भी अपभ्रंश की छाया मुखरित है। यदि इनकी प्रामाणिकता पर विश्वास किया जाय तो अपभ्रंश का प्रारंभ काल पहले से ही मानना पड़ेगा परंतु यह विवादग्रस्त है।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषायें
(1000 ई0पू0 से अब तक)
इनका काल 1000 ई0 से आरंभ होकर वर्तमान युग तक चला आ रहा है। अपभ्रंशकाल के अवसान एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के अभ्युदय के बीच का काल इन भाषाओं के विकास का काल है, जिनका निश्चित और स्पष्ट स्वरूप निर्धारण नहीं हो सका। 12वीं शताब्दी में आचार्य हेमचंद्र के द्वारा अपभ्रंश व्याकरण का निर्माण सिद्ध करता है कि उस समय तक अपभ्रंश साहित्य रूढ़ भाषा हो चुकी थी। इस स्थिति में बोलचाल की भाषा का प्रवाह का अपना एक नवीन स्वरूप धारण कर रहा होगा, यह निश्चित है। इधर 16वीं शताब्दी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में साहित्य रचनायें प्राप्त होने लगती हैं। इस प्रकार सिद्ध होता है कि साहित्यिक स्तर पर आने के पूर्व ही इन आधुनिक आर्य-भाषाओं का अस्तिव विकसित हो चला था। आचार्य हेमचंद्र के पश्चात् 13 वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक का काल संक्रांति काल कहा जा सकता है, जिनमें अपभ्रंश के आवरण को त्याग कर भाषा का स्वरूप आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के तत्त्वों को धारण करता आ रहा था। इसी संक्राति कालीन भाषा को श्री गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का नाम दिया। अपने निबंध में उन्होंने अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का भेद स्पष्ट कर दिया है।
बाबूराम सक्सेना ने लिखा है, “इतना निश्चित समझना चाहिए कि जिन प्रांतों में प्राकृत बोली समझी जाती थी उनमें ही उत्तर-काल में उन प्रांतों के अपभ्रंशों का योग होने लगा।”
गुलेरी जी का मत है, “पुरानी अपभ्रंश, संस्कृत और प्राकृत से मिलती है, और पिछड़ी पुरानी हिंदी से अपभ्रंश कहाँ समाप्त होती हैं और पुरानी हिंदी कहाँ आराम्भ होती है, इसका निर्णय करना कठिन, किंतु रोचक और बड़े महत्त्व का है। इन दो भाषाओं के समय और देश के विषय में कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती है।”
आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति
|
अपभ्रंश |
आधुनिक भाषायें |
|
1. शौरसेनी |
पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती |
|
2. पैशाची |
लांहदा, पंजाबी |
|
3. ब्राचड़ |
सिंधी |
|
4. इस |
पहाड़ी |
|
5. महाराष्ट्री |
मराठी |
|
6. अर्द्ध-मागधी |
पूर्वी हिंदी, बिहारी |
|
7. मंगनी |
बंगाली, उड़िया, असमिया |
अतः स्तष्ट है कि हिंदी अपभ्रंश की उत्तराधिकरिणी है।
हिंदी भाषा एवं लिपि– महत्वपूर्ण लिंक
- भारतीय आर्य भाषाएँ | भारतीय आर्यभाषा का काल विभाजन | प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएँ | वैदिक भाषा की ध्वनियाँ | वैदिक भाषा की विशेषताएँ
- आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण | आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण संबंधी विभिन्न मत
- हिंदी शब्द की उत्पत्ति | भाषा की परिभाषा | हिंदी की विविध बोलियाँ | बुंदेली की व्याकरणिक विशेषतायें
- हिंदी की उपभाषाओं का परिचय | खड़ी बोली का परिचय | हिंदी की उपभाषाएँ
- पूर्वी हिन्दी तथा पश्चिमी हिन्दी में अन्तर
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]