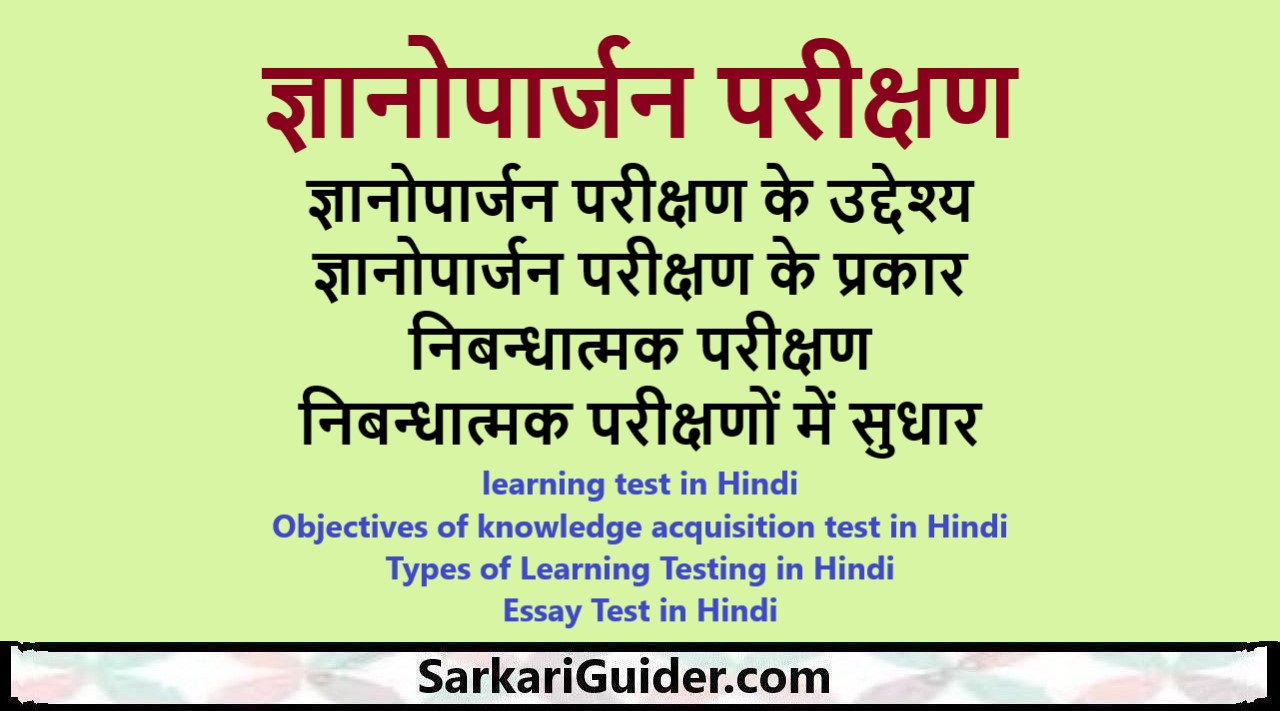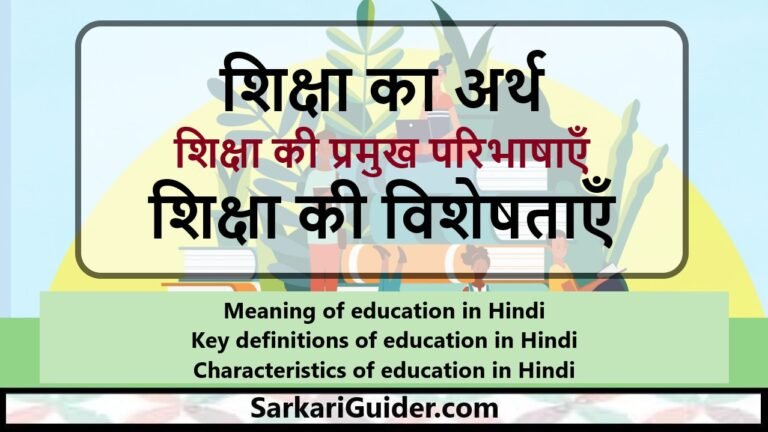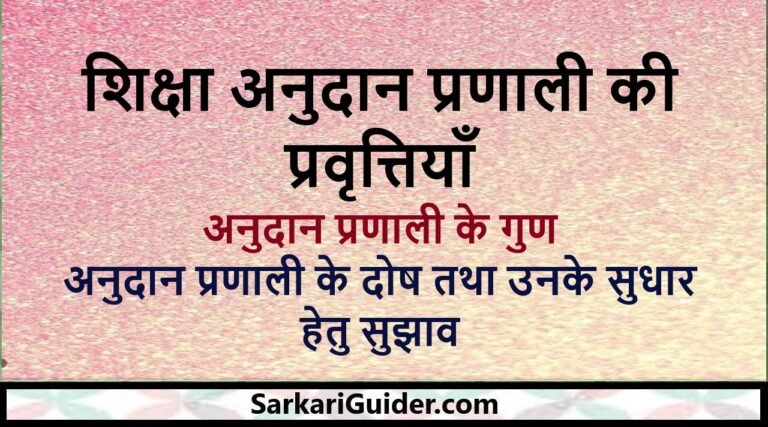ज्ञानोपार्जन परीक्षण | ज्ञानोपार्जन परीक्षण के उद्देश्य | ज्ञानोपार्जन परीक्षण के प्रकार | निबन्धात्मक परीक्षण | निबन्धात्मक परीक्षणों में सुधार
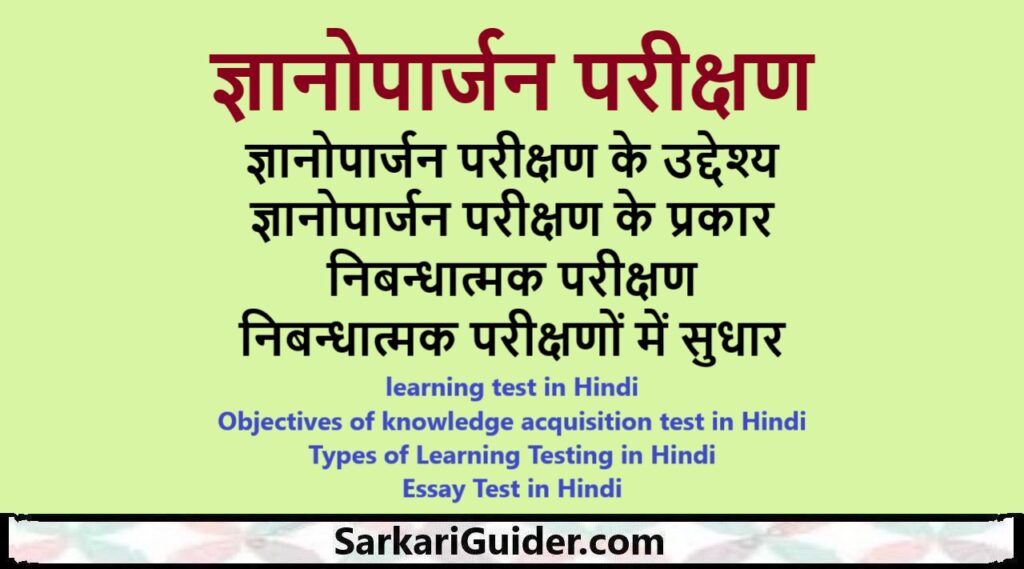
ज्ञानोपार्जन परीक्षण | ज्ञानोपार्जन परीक्षण के उद्देश्य | ज्ञानोपार्जन परीक्षण के प्रकार | निबन्धात्मक परीक्षण | निबन्धात्मक परीक्षणों में सुधार | learning test in Hindi | Objectives of knowledge acquisition test in Hindi | Types of Learning Testing in Hindi | Essay Test in Hindi | improvement in essay tests in Hindi
ज्ञानोपार्जन परीक्षण
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास करना है। इसमें बालक की व्यक्तित्व विभिन्नता को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। बालक की विशिष्ट योग्यता, अभिक्षमता एवं रुचि को जानकर ही हम उनकी शिक्षा का रूप निर्धारित करते हैं। जब कि बालक वर्ष भर किसी कक्षा में पढ़ता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि इस बात का पता लगाया जाय कि बालक ने वर्ष भर में कितना ज्ञान प्राप्त किया है। इसके लिए विभिन्न ज्ञानोपार्जन परीक्षणों को निर्मित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में ज्ञानोपार्जन का अर्थ, प्रकार एवं गुण-दोष पर प्रकाश जायेगा।
ज्ञानोपार्जन परीक्षण का अर्थ (Meaning of Achievement Test)
ज्ञानोपार्जन परोक्षण एक निश्चित कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसकी माप कहते हैं। कक्षा में सभी बालकों को वर्ष भर एक ही अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है लेकिन फिर भी कुछ बालक उतने ही समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और कुछ बालक बहुत कम ही ज्ञान उतने समय में प्राप्त कर पाते हैं लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी किस सीमा तक ज्ञान अर्जित करता है इस बात का पता ज्ञानोपाजन परीक्षा से ही लगता है। इस प्रकार ज्ञानोपार्जन परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से हैं जिसके द्वारा बालक के विभिन्न विषयों में प्राप्त ज्ञान की सीमा का पता लगाया जाता है।
ज्ञानोपार्जन परीक्षण के उद्देश्य (Aims of Intelligence Test)
ज्ञानोपार्जन परीक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं-
- इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है बालकों द्वारा अर्जित ज्ञान का पता लगाना ।
- उच्च, सामान्य एवं निम्न स्तर में बालकों को अलग करना।
- शिक्षकों के अध्ययन कार्य का मूल्यांकन करना।
- बालकों को कक्षोन्नति करना।
- प्रयोग की गयी शिक्षण पद्धति की उपयोगिता एवं गुण-दोष का पता लगाना।
- उपलब्धि परीक्षण के आधार पर चयन और श्रेणीकरण में सहायता मिलती है।
- शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देश के क्षेत्र में ज्ञानोपार्जन परीक्षण बहुत उपयोगी होते हैं।
ज्ञानोपार्जन परीक्षण के प्रकार (Kinds of Achievement Test)
ज्ञानोपार्जन परीक्षण मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं –
(अ) सामान्य ज्ञानोपार्जन General achievement) – इसमें व्यक्ति के ज्ञान के क्षेत्र का परीक्षण करते हैं और इस प्रकार लक्ष्य फलांक को हमारे लक्ष्य रखते हैं जो व्यक्ति का अर्जित ज्ञान बताता है।
(ब) नैदानिक परीक्षण (Diagnostic Tests)- इन परीक्षणों के द्वारा परीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से जिनमें वह दिया जाता है, बालक की सफलता और निर्बलता प्रकट होती है। नैदानिक परीक्षण के द्वारा शिक्षक यह समझ जाते हैं कि बालक किस स्थान पर अधिक कमजोर है। शिक्षक का शिक्षण कार्य कहाँ तक सफल है और कहाँ तक असफल है। इन सब बातों का पता ज्ञानोपार्जन परीक्षण से लगता है।
परीक्षा की दृष्टि से ज्ञानोपार्जन परीक्षण निम्न चार प्रकार के होते हैं-
1. मौखिक परीक्षण (Verbal Tests), 2. क्रियात्मक परीक्षण (Performance Tests), 3. वस्तुनिष्ठ परीक्षण (Objective Tests), 4. निबन्धात्मक परीक्षण (Essay type Tests)।
- मौखिक परीक्षण (Verbal Tests)- इन परीक्षणों में बालक को मौखिक प्रश्न दिये जाते हैं और यह जानने की चेष्टा की जाती है कि बालक ने पाठ पढ़ा है अथवा नहीं। इसका दोष यह है कि यह परीक्षण बालक की पूर्ण रूप से जाँन कर पाते हैं। इनमें पक्षपात भी होना सम्भव है। इसके साथ-साथ बालकों की त्रुटियाँ चिरस्थाई नहीं होती बल्कि पर्यावरण के साथ-साथ उनमें परिवर्तन होता रहता है। इसके परिणाम अधिक विश्वसनीय नहीं होते हैं।
- क्रियात्मक परीक्षण (Performance Tests)- इन परीक्षणों की सहायता से बालकों को क्रियात्मक दक्षता को जाँच होती है। इन परीक्षणों में चित्रों एवं क्रियाओं आदि का प्रयोग होता है। इन परीक्षणों में शाब्दिक योग्यता पर जोर नहीं दिया जाता है। व्यावसायिक क्षेत्र में कुशलता की जाँच के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।
- वस्तुनिष्ठ परीक्षण (Objective Test)- इस प्रकार के परीक्षणों में प्रश्न बहुत छोटे और सरल होते हैं। इस परीक्षण का आगे विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे।
- निबन्धात्मक परीक्षण (Essay type Tests)- इस प्रकार के परीक्षणों में प्रश्न इस प्रकार दिये जाते हैं कि इनका उत्तर निबन्ध के रूप में देना पड़ता है। इस प्रकार के परीक्षणों का विस्तृत वर्णन आगे कर रहे हैं।
निबन्धात्मक परीक्षण (Essay type Tests)
अर्थ (Meaning)- हमारे देश में प्रचलित प्रणाली निबन्धात्मक ही है। इसमें बालक को पाँच या छ: प्रश्न करने को दिये जाते हैं जिनका उत्तर बालक को निबन्ध के रूप में देना पड़ता है। यह परीक्षा प्रणाली प्रचलित होने के कारण इसे प्रचलित परीक्षा प्रणाली (Traditional type Examination) भी कहते हैं। इस प्रकार की परीक्षाओं में जो प्रश्न दिये जाते हैं वे सम्पूर्ण कोर्स के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं।
गुण (Merits) – 1. इस प्रणाली में प्रश्न रचना अत्यन्त सरल होती है। 2. इसमें अधिक समय नहीं लगता। 3. इसकी परीक्षण विधि सरल होती है। 4. इन परीक्षणों के द्वारा बालक की स्मरण-शक्ति, कल्पना शक्ति, पर्णनात्मक शक्ति, भाषा-ज्ञान एवं शैली की परीक्षा की जा सकती है। 5. निबन्धात्मक परीक्षण में बालक उत्तर देने में स्वतंत्र रहता है। 6. इन परीक्षणों के द्वारा बालक लिखावट एवं लेखन शक्ति का पता लगता है।
दोष (Demerits) – निबन्धात्मक परीक्षण प्रणाली में कुछ दोष भी पाये जाते हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है।
- यह सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की परीक्षा कर सकने में असफल रहते हैं। 2. बालक कुछ संभावित प्रश्नों को हो तैयार कर लेते हैं जिसके कारण सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का ज्ञान बालक को नहीं हो पाता है। 3. इन परीक्षाओं में यथार्थता एवं विश्वसनीयता का अभाव रहता है। 4. इन परीक्षणों में व्यक्तिनिष्टता (Subjectively) अधिक रहती है। 5. इसमें पक्षपात की सम्भावना रहती है। 6. इसमें बालक की योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं होता है। 7. इसमें रटने पर बल दिया जाता है। 8. बालकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। 9. विद्यार्थी वर्ष भर नहीं पढ़ते हैं।
निबन्धात्मक परीक्षणों में सुधार (Reform in Essay Tests ) –
नबन्धात्मक परीक्षण प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए निम्न सुधार किये जाने आवश्यक हैं।
1. प्रश्नों का निर्माण सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर करना चाहिए। 2. प्रश्न-पत्र में सरल एवं कठिन दोनों प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। यह सरल से कठिन के क्रम में रखने चाहिए। 3. प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों को अनिवार्य रखना चाहिए। 4. प्रश्न मौलिक तथा रचनात्मक प्रवृत्ति को उभारने वाले होने चाहिए। 5. प्रश्न भ्रमपूर्ण न होने चाहिए और प्रश्नों की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। 6. परीक्षक को पक्षपातरहित होकर मूल्यांकन करना चाहिए। 7. परीक्षक को मूल्यांकन करने से पूर्व मूल्यांकन का मापदण्ड बना लेना चाहिए। 8. उत्तर-पुस्तिका पर विद्यार्थी का नाम न लिखा होना चाहिए।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- परीक्षा का अर्थ | परीक्षाओं की उपयोगिता या महत्त्व | परीक्षा के उद्देश्य | परीक्षा के कार्य | परीक्षा के प्रकार
- साक्षात्कार | साक्षात्कार की परिभाषा | साक्षात्कार की विशेषताएँ | साक्षात्कार का उद्देश्य | साक्षात्कार का क्या महत्व
- प्रश्नावली | प्रश्नावली की परिभाषा | प्रश्नावली की विशेषताएँ | प्रश्नावली का वर्गीकरण
- श्रेणी मापनी विधि | दर मापक का नमूना | श्रेणी मापनी विधि को नमूना बनाकर स्पष्ट कीजिए
- व्यक्तित्व क्या है | व्यक्तित्व का अर्थ | व्यक्तित्व की परिभाषा | व्यक्तित्व के प्रकार
- बुद्धि और अनुवांशिकता | बुद्धि और वातावरण | बुद्धि, अनुवांशिकता एवं वातावरण
- बुद्धि | बुद्धि का अर्थ | बुद्धि की परिभाषा | बुद्धि का स्वरूप | बुद्धि के प्रकार | बुद्धि के सिद्धान्त | बुद्धि की संरचना | बुद्धि और ज्ञान में अन्तर
- बुद्धि मापन का तात्पर्य | मानसिक आयु और कालिक आयु | बुद्धि-लब्धि
- बुद्धि परीक्षण | बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार | बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]