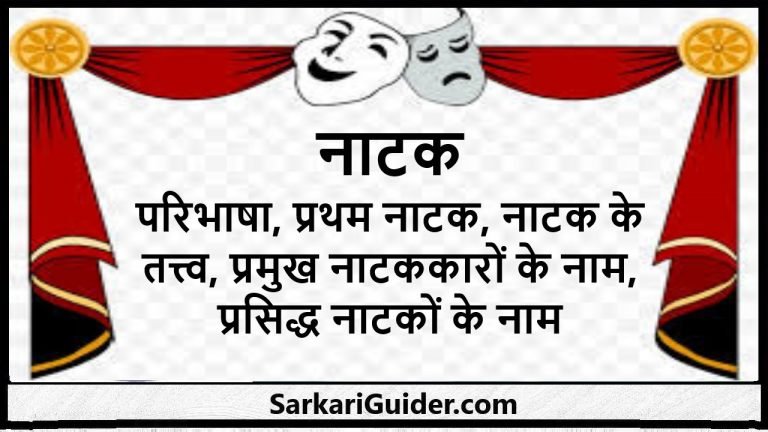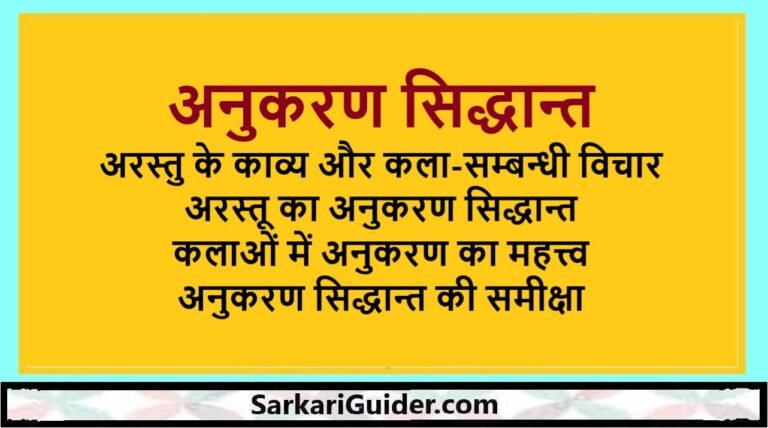मीरा की काव्य में प्रकृति | मीरा की काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग | मीरा की काव्य में अनुस्वार युक्त दीर्घ स्वरों का प्रयोग | मीरा के काव्य में मुहावरों का प्रयोग
मीरा की काव्य में प्रकृति | मीरा की काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग | मीरा की काव्य में अनुस्वार युक्त दीर्घ स्वरों का प्रयोग | मीरा के काव्य में मुहावरों का प्रयोग
मीरा की काव्य में प्रकृति
मिश्रित भाषा- मीरा के पदों का प्रचलन प्रायः समस्त उत्तरी भारत से है। अतः उनमें विभिन्न भाषाओं के शब्द मिल गये हैं। जिस प्रकार मीरा के पदों के पाठ और प्रामणिकता में एकरूपता नहीं है, उसी प्रकार भाषा में मीरा के पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती और कुछ पंजाबी के पद मिलते हैं।
मीरा की काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग-
यह विधि भक्ति कैसे होय।
मन की मैल हिय ते न छूटी, दियों तिलक सिर धोय।।
काम कूकर लोभ डोरी बाँधि मोह चण्डाल।
क्रोध कसाई रहत घट में कैसे मिलें गोपाल।
मीरा ने वृन्दावन में पाँच’छ: वर्ष व्यतीत किये। इसलिए ब्रजभाषा से उनका व्यापक परिचय होना स्वाभाविक ही था। राजस्थान में तो मीरा का जन्म ही हुआ था। इसलिए राजस्थानी भाषा की शब्दावली उनके पदों में व्यापक रूप से मिलती है।
मुझ अबला ने मोती नीराँत थई रे
छमलों घरेणु मारे पाँच रे।
झाँझरिया जग जीवन केरा कृष्ण जी कड़वा ने काँबीरे
बीधियाँ घूंघरा नाम नारायण ने अणवट अन्तरजामी रे।
जनश्रुति के अनुसार मीरा का अन्तिम जीवन द्वारा का (गुजरात) में ही व्यतीत हुआ। अतः उनके पदों में गुजराती प्रयोग भी मिलता है।
प्रेमनी प्रेमनी प्रेमनी रे, मन लागी कटारी प्रेमनी।
जल जमुनामाँ भरवाँ गायाँ वाँ हठो नागर माथे हेमनी रे।
नाचो वे वावणी हरजीए बाँकी, एक खेंचे तेम तैमनी रे।
मीरौ के प्रभु गिरधर नागर, शामली सुरत शुभ एमनी रे।
मीरा सम्भवतः कुछ समय तक पंजाब में भी रहीं। पंजाबी भाषा के शब्दों का प्रयोग इसका प्रमाण है।
लागी सोही जाणै, कृष्ण लगण दी पीर।
पित पड्याँ कोई निकटि न आवै, सुखमों सबको धीर॥
बाहरि घाव कछु नाहीं दीसै, रोम-रोम ही पीर।
जन मीराँ गिरधर के ऊपर सदवै करु शरीर।।
मीरा की काव्य-भाषा की विशेषताओं का उद्घाटन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है-
संगीतात्मकता- मीरा के काव्य की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता संगीतात्मकता है। संगीतात्मकता के लिए मीरा कहीं तो शब्दों के संयुक्त रूप को भंग कर देती हैं और कहीं उनको लोचयुक्त बना देती हैं। वे कहीं पर यदि शब्दों के रूप को विकृत कर देती हैं, तो कहीं पर एक छन्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करती है।
लोच-युक्त-
मुरली का मुरलिया
पपीहा का पपैया
गोविन्द से गोविन्दां
संयुक्त शब्दों का मंत्रीकरण-
अमृत से इमरत
प्रभात से परभात
नृत्य से निरत
श्री से सिरी
हृदय से हिरदां
विकृत प्रयोग-
स्नेह से नेहड़ा
जीव से जीवड़ा
निद्रा से नीदड़ी
कृष्ण से काण्हड़ो
एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द-
‘स’ के स्थान पर ‘श’ जैसे ‘तरसावो’ से ‘तरशावाँ’, और ‘ल’ के स्थान पर ‘ड’ जैसे नेहर से नेहड़ा’ और ‘बादल से बादड़’-रे, री,हेरी, आदि का प्रयोग भी मीरा के पदों को संगीतात्मकता देने में बहुत सहायक हुआ है, जैसे-
हेरी म्हाँ दरदे दिवाणी म्हौरा दरद न जान्याँ कोय।
मीरा की काव्य में अनुस्वार युक्त दीर्घ स्वरों का प्रयोग-
‘गिनते-गिनते’ से ‘गणताँ-गणताँ
रेखा से रेखाँ
आँगुरी से आँगुरियाँ
अलकारों का प्रयोग-
मीरा के काव्य में अलकारों का भी अधिक प्रयोग नहीं हुआ है। क्योकि मीरां का काव्य भावों को उमड़ता हुआ सागर है। अलकार-योजना भावों को उत्कर्ष करने में सहायक है।
छन्द-योजना- मीरा-काव्य गेय काव्य है। संगीत की कसौटी और भावस्तर पर खरे उतरने वाले विभिन्न छन्दों का प्रयोग मीरा ने किया है, किनतु मात्रिक छन्दों का प्रयोग बहुत हुआ है।
मीरा के काव्य में मुहावरों का प्रयोग –
मीरा के काव्य में मुहावरों का प्रयोग प्रायः कम ही हुआ है, लेकिन जितना भी है वह सफल है। निम्न उदाहरण में देखिये-
भाई री म्हाँ लिया गोविन्द मोल।
ये कह्यां, छाँणों महाँ कह्यां चौड़ये लिया बजन्ता ढोल।
ये कह्यां, मुहँगो, म्हाँ कह्यां सस्ते लियाँ री तराजाँ तोल।
यहाँ ‘मोल लेना’, ‘ढोल बजाकर मोल लेना’, तराजू में तोलना’ आदि मुहावरों का सफल प्रयोग हैं
प्रवाहात्मकता- मीरां का काव्य गेय है। उन्होंने अपने गेय पदों के संगीत को स्वर- लहरी के उतार-चढ़ाव के अनुकूल ही शब्दावली का प्रयोग किया है। यही कारण है कि उनकी भाषा में प्रवाहात्मक है। शब्दों की विकृति की और संयुक्त शब्दों का समीकरण प्रवाह को तीव्रतर कर देता है।
साँवरिया म्हारो चाय रह्या परेदश।
म्हाँरा विछड्या फेर न मिलया भेज्या था एक सन्देश।
रहण आभरण भूषण चाड्या खोर कियाँ सर कैस॥
भगवाँ भेस धर्यां थे कारण ढूंढ्या चारया देस।
मीरों के प्रभु स्याम मिलन विण जीवनि जनम अनेस॥
भाव-प्रवणता- मीरा के काव्य में भावुकता और मार्मिकता की अनुभूति का विस्तृत समावेश है। मीरा के दों में प्रेम पीर की भी मार्मिक कसक समाई हुई। उनका प्रत्येक शब्द सरल,मधुर और अनुभूति से भरा हुआ है। एक उदाहरण लीजिए-
हेरी म्हाँ दरदे दिवाणी म्हांरा दरद न जाण्या कोय।
घायल की गत घायल जाण्याँ हिवड़ों अगण संजोय॥
जौहर की गति जौहरी जाणैं क्या जाण्याँ जिण खीय।
दरद की मार्यां दर-दर डोलयाँ वैद मिलिमा नहिं कोय।
मीरां के प्रभु पीर मिटैगीं, जब वैद साँवरो होय।।
निष्कर्ष-
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भाषा की मधुरता और भाव उष्णता के कारण मीरा की काव्य जन-जन का कंठहार है। उनके पदों में भाषा का आडम्बर तनिक भी नहीं है। मीरा के कुछ पदों में परिष्कृत तथा शुद्ध साहित्यिक ब्रज-भाषा का प्रयोग भी मिलता है। मीरा की भाषा में भावों को व्यक्त करने की क्षमता है। वह भावातिरेक में स्वयं ही भावमयी हो गई है।
हिन्दी – महत्वपूर्ण लिंक
- तुलसीदास की भक्ति भावना | तुलसीदास की भक्ति पद्धति के स्वरूप का वर्णन | रामभक्त कवि के रूप में तुलसीदास की भक्ति का मूल्यांकन
- तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएँ | तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं पर आलोचनात्मक निबन्ध
- तुलसीदास के रामचरित मानस का महत्व | राम काव्य परम्परा के अन्तर्गत रामचरित मानस का महत्व
- तुलसीदास की भाषा | तुलसीदास की शैलीगत विशषताएँ | तुलसी के काव्य की छन्द विधान की विशषताएँ
- तुलसी के काव्य में वर्णित लोक आदर्श | तुलसी के काव्य में वर्णित सामाजिक आदर्श
- पद्मावत् के नागमती का विरह वर्णन | नागमती का विरह संपूर्ण भक्ति कालीन कविता में अद्वितीय है
- जायसी के रहस्यवाद की विशेषताएँ | जायसी के रहस्यावाद की समीक्षात्मक विवेचना
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]