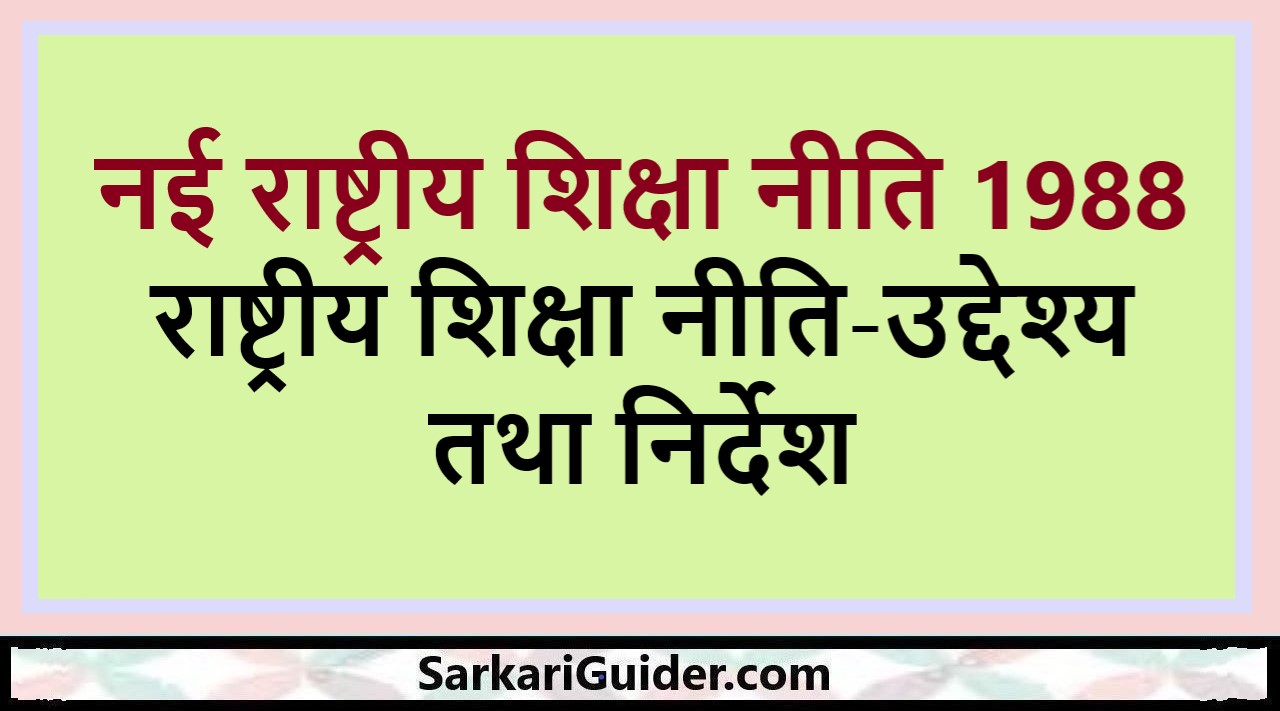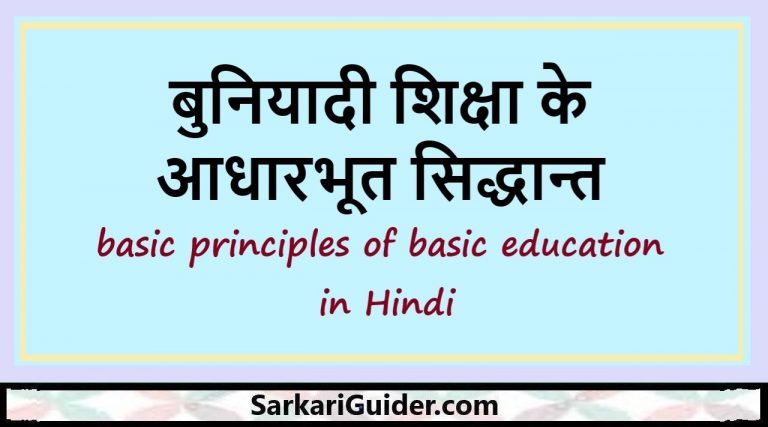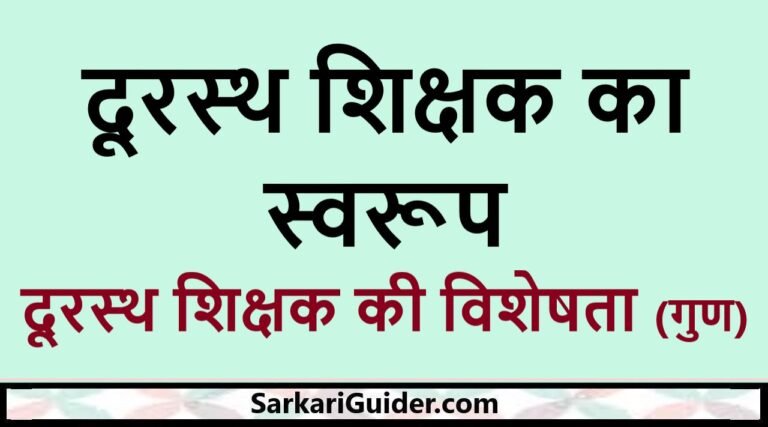नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति-उद्देश्य तथा निर्देश

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति-उद्देश्य तथा निर्देश
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988
(New National Education Policy 1986)
प्राचीन काल में भारत में बालक को शिक्षा का प्रारम्भ 5 वर्ष की आयु से होता था तथा 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करता था जिसमें ब्राह्मण 6, क्षत्रीय 11 और वैश्य 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के पश्चात् गुरूकुलों में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। शूद्रों के शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था न थी। शिक्षा के दो स्तर होते थे-
(1) प्रारम्भिक; (2) उच्च।
इसी प्रकार बौद्ध युग में भी शिक्षा के दो स्तर होते थे।
शिक्षा प्रणाली पर सर्वप्रथम 1882 में हण्टर कमीशन ने विचार किया। उसने शिक्षा के अनेक चरण प्रस्तावित किये। उस समय दस वर्ष की एन्ट्रेस, दो वर्ष की एफ० रा०, दो वर्ष की स्नातक और दो वर्ष की परास्नातक स्नातकोत्तर प्रणाली प्रचलित थी। 10 वर्ष की शिक्षा विद्यालयों में, शेष शिक्षा विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। 1917-19 में सैडलर कमीशन ने अनुभव किया कि शिक्षा की प्रकृति में परिवर्तन लाना आवश्यक है। अतएव उसने 10 + 2 + 3 शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए पृथक् बोर्ड गठित करने की सिफारिश की। 10 वर्ष की हाईस्कूल, 2 वर्ष का इण्टरमीडिएट, शिक्षा बोर्ड के अधीन कर 3 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत रखने का आग्रह किया।
सन् 1948-49 में राधाकृष्णन कमीशन ने भी 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू करने की सिफारिश की तथा माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर गठित करने की सिफारिश की।
सन् 1952-53 में मुदालियर कमीशन ने 8+3+3 शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की। 8 वर्ष की प्राथमिक, 3 वर्ष की हाईस्कूल एवं 3 वर्ष की स्नातक व्यवस्था को प्रस्तावित किया। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने पर बल दिया।
सन् 1960 में योजना आयोग ने 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा तथा 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा पर बल दिया। 1961 में कुलपतियों के अधिवेशन में भी यही तथ्य दोहराया गया। सन् 1962 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने भी इसी संकल्प को दोहराया एवं कोठारी कमीशन ने भी यही सिफारिश की और अन्त में सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सम्पूर्ण देश में 10 + 2 + 3 शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गयी।
शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का अर्थ
10+2+3 का अर्थ इस प्रकार समझा जा सकता है कि 10 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक को प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। यह शिक्षा 6 से 16 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है। +2 के अन्तर्गत कक्षा 11 व 12 तक की प्राप्त की जाने वाली शिक्षा आती है। इन दो वर्षों में सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जायेगी। वह शिक्षा 16 से 18 वर्ष की आयु तक चलेगी। +3 से तात्पर्य है कि 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात् 3 वर्षीय उच्च शिक्षा की प्रथम उपाधि (स्नातक उपाधि) हेतु निर्धारित अवधि होगी। इस अवधि में शिक्षार्थी को सामान्य एवं विशेष दोनों में किसी भी शिक्षा के विषयों की शिक्षा प्रदान की जायेगी। यह शिक्षा 18 से 21 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है।
सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में तीन वर्ष का डिग्री (स्नातक) पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-उद्देश्य तथा निर्देश
(National Education Policy-Instruction and Objective)
-
प्रस्तावना
(1) मानव इतिहास के उदय से लेकर अब तक शिक्षा ने विकास तथा अभिवृद्धि की प्रक्रिया को सातत्य प्रदान किया है। हर देश ने अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिये अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित की और समय की चुनौती को स्वीकार किया। इतिहास में ऐसे भी क्षण आये हैं जब परम्परागत प्रक्रिया को नई दिशा दी गयी। ऐसा ही क्षण आज है।
(2) देश, आर्थिक, तकनीकी विकास की उस अवस्था पर पहुँच गया है, जहाँ सृजित परिसम्पत्तियों (Assets) का अधिकतम लाभ सभी वर्गों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाना है। शिक्षा इस उद्देश्य की प्राप्ति का राजमार्ग है।
(3) इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुये भारत सरकार ने जनवरी, 1985 में घोषणा की कि देश के लिये एक नई शिक्षा नीति की रचना की जायेगी। विद्यमान शिक्षा की सघन समीक्षा, देश भर में बहस कराकर की गयी। देश के विभिन्न भागों से प्राप्त विचारों तथा सुझावों का अध्ययन सर्तकतापूर्वक किया गया।
1968 की शिक्षा नीति और उसके बाद
(4) स्वतन्त्र भारत में 1968 की शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति, सामान्य नागरिकता तथा संस्कृति की भावना और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना रहा है। इसने शिक्षा प्रणाली के क्रान्तिकारी नव-निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी स्तरों पर शिक्षा के गुणात्मक सुधार, विज्ञान तथा तकनीकी पर विशेष ध्यान, नैतिक मूल्यों के विकास तथा शिक्षा और जीवन के पारस्परिक सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने पर बल दिया।
(5) 1968 की नीति के अनुसार शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार किया गया। एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ग्राम क्षेत्रों की 90% जनता के लिये विद्यालयी सुविधायें प्राप्त हैं। अन्य स्तरों पर भी वाँछित सुविधाओं में भी प्रगति हुई है।
(6) सम्पूर्ण देश में शिक्षा की सामान्य संरचना की स्वीकृति और अधिकांश राज्यों में 10+2+3 शिक्षा पद्धति का अनुसरण महत्त्वपूर्ण घटना है। लड़के-लड़कियों के सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विज्ञान तथा गणित की अनिवार्य शिक्षा, कार्यानुभव को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया।
(7) उपाधि स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना की गयी। स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा तथा अनुसंधान के लिये सेन्टर फॉर एडवांस्ड स्टेडीज खोले गये। जिससे शिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षमता प्राप्त हुई।
(8) यों तो उपरोक्त उपलब्धियाँ प्रभावशाली थीं किन्तु 1968 की शिक्षा नीति में सम्मिलित अनेक कार्यों को संगठनात्मक सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। उनकी रणनीति, विनियोग को आर्थिक सहायता न मिल सकी। परिणाम यह हुआ कि आधिक्य, गुण, मात्रा, उपयोग तथा आर्थिक ढाँचे में निरन्तर वृद्धि होती रही और अब इन सभी को प्राथमिकता देकर हल किया जाना आवश्यक है।
(9) भारत में शिक्षा आज चौराहे पर खड़ी है। सामान्य रेखीय प्रसार और न ही विद्यमान स्थिति और सुधार की प्रकृति इन परिस्थितियों का सामना कर सकती है।
(10) भारतीय चिन्तन के अनुसार मानव एक सकारात्मक एसेट (Asset) तथा बहुमूल्य राष्ट्रीय स्रोत है जिसका विकास सावधानीपूर्वक गतिशीलता के साथ किया जाना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति की अभिवृद्धि विभिन्न प्रकार की समस्याओं तथा आवश्यकताओं को प्रस्तुत करती है। जन्म से मरण तक चलने वाली शिक्षा की इस जटिल तथा गतिशील प्रक्रिया का नियोजन सुसंबद्ध रूप से किया जाना चाहिये और पूरी निष्ठा के साथ इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।
(11) भारत का राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन ऐसी अवस्था से गुजर रहा है, जहाँ पूर्ण स्वीकृत दीर्घकालीन मूल्यों का विनाश हो रहा है। इसी दबाव में धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, जनतन्त्र तथा व्यावसायिक नैतिकता पिस रहे हैं।
(12) निर्बल संरचना तथा समाजसेवा के कारण ग्राम क्षेत्रों को प्रशिक्षित युवाओं का लाभ उस समय तक नहीं मिल पायेगा जब तक नगर-ग्राम के भेद समाप्त नहीं हो और रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होगी।
(13) आने वाले दशकों में देश की जनसंख्या वृद्धि की गति को धीमा करना होगा। स्त्रियों में शिक्षा प्रसार तथा साक्षरता में वृद्धि इस समस्या को हल करेगी।
(14) आने वाले दशक अत्यन्त संघर्ष के होंगे। इनमें अनेक प्रकार के अवसर होंगे। नये वातावरण का लाभ उठाने के लिये मानव विकास के नये प्रतिमानों की रचना करनी होगी। नई पीढ़ी में नव विचार तथा सृजनात्मकता को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिये। सामाजिक न्याय तथा मानव मूल्यों के प्रति इस पीढ़ी में प्रतिबद्धता होनी चाहिये। इन सबका अर्थ है-उत्तम शिक्षा।
(15) इनके अतिरिक्त, सरकार के सपक्ष देश के लिये नई शिक्षा नीति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नवीन चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं ने उत्पन्न की है। परिस्थिति का सामना यों ही नहीं हो सकता।
(2) शिक्षा की भूमिका तथा मूल तत्व
(1) राष्ट्रीय सन्दर्भ में शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य है। हमारे सर्वांगीण विकास भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए यह आधारभूत तत्व है।
(2) शिक्षा उभय सांस्कृतिक भूमिका प्रस्तुत करती है। यह राष्ट्रीय एकता में योगदान देने वाली संवेदनशीलता तथा प्रतिबन्ध को परिष्कृत कर वैज्ञानिक मनोवृत्ति एवं मानसिक स्वतन्त्रता एवं भावना विकसित कर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा जनतन्त्र का विकास संविधान के अन्तर्गत करती है।
(3) अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर शिक्षा, जनशक्ति का विकास करती है, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की पूरी गारन्टी, शोध एवं विकास के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है।
(4) कुल मिलाकर, शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य में एक विशेष विनियोग (Investment) है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यह मूल कुंजी है।
-
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली
(1) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जिन आधारों पर विकसित हो रही है, उसके मूल सिद्धान्त संविधान द्वारा प्रदान किये गये हैं।
(2) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा यह है कि वाँछित स्तर तक, जाति, धर्म, क्षेत्र तथा लिंग के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर समान रूप से प्रदान किये जाने चाहिये। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त धन के साथ कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जायेंगे। 1968 की नीति में प्रस्तावित सामान्य शिक्षा प्रणाली (Common School System) को अपनाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने होंगे।
(3) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सामान्य शैक्षिक संरचना पर विचार करती है। देश के सभी भागों में 10+2+ 3 प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया है। 10 वर्षीय व्यवस्था के पुनर्विभाजन-5 वर्षीय आरम्भिक, 3 वर्षीय अपर प्राइमरी एवं 2 वर्षीय हाईस्कूल के प्रयास चल रहे हैं।
(4) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार एक सामान्य पाठ्यक्रम की संरचना है, जिसमें सामान्य मूल विषयों के साथ-साथ अन्य विषय लचीले होंगे। सामान्य मूल विषयों में भारतीय स्वाधीनता का इतिहास, संवैधानिक प्रतिबन्ध तथा राष्ट्रीय एकता के अन्य तत्व होंगे। ये तत्व विषय क्षेत्रों से पृथक् होंगे और इस प्रकार बनाये जायेंगे, जिससे भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, जनतंत्र, धर्म-निरपेक्षता के मूल्यों का विकास लिंगभेद के बिना होगा। वातावरण की रक्षा, सामाजिक बुराईयों को दूर करना, छोटे परिवार के मानकों का निर्माण तथा वैज्ञानिक स्वभाव विकसित हो। सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम इस प्रकार बनाये जायेंगे जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को पूरी निष्ठा के साथ विकसित करेंगे।
(5) भारत ने विश्व को एक परिवार माना है और इसी आधार पर राष्ट्रों के मध्य शान्ति एवं अवबोध बनाये रखने की आवश्यकता अनुभव की है। इस पुरातन परम्परा का निर्वाह करने के लिए इस विश्व मत को सशक्त बनाने हेतु, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को नई पीढ़ी में अभिप्रेरित करें। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता।
(6) समानता के विकास के लिये, समानता के अधिकतम अवसर प्रदान करने के साथ उसमें सफलता प्राप्त करना भी आवश्यक है। आधारभूत पाठ्यक्रम के माध्यम से आन्तरिक समानता को जागृत करना है, जन्म से प्राप्त तथा सामाजिक परिवेश से उत्पन्न पूर्वाग्रहों तथा जटिलताओं को समाप्त करना है।
(7) शिक्षा की प्रत्येक अवस्था के लिये अधिगम का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना होगा। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले व्यक्तियों की संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए, पाठ्यक्रम में व्यवस्था करनी होगी। सम्पर्क भाषा के विकास के लिये विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों के अनुवाद करने होंगे तथा बहुभाषी शब्द देने की रचना करनी होगी। नई पीढ़ी को अपने ढंग से अपने प्रतिबोध तथा प्रतिभा में भारत की पुनखोंज करने के लिये प्रोत्साहित करना होगा।
(8) उच्च शिक्षा में सामान्य रूप से तथा तकनीकी शिक्षा में विशेष रूप से अन्तक्षेत्रीय गतिशीलता को विकसित करती है। वांछित योग्यता के द्वारा ऐसे अवसर देने होंगे। विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ है।
(9) अनुसंधान तथा विकास, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा जाल बिछाना होगा कि विभिन्न संस्थानों के स्रोतों का एकत्रीकरण राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजनाओं में भाग लेने हेतु किया जाये।
(10) राष्ट्र को सम्पूर्ण रूप से शैक्षिक रूपान्तरण के सभी कार्यक्रमों को, असमानताओं को कम करते हुये, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण, प्रौढ़ साक्षरता, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा का दायित्व वहन करना होगा।
(11) शैक्षिक प्रक्रिया का चिरसंचित उद्देश्य जीवन पर्यन्त शिक्षा है। सार्वभौम साक्षरता की यह उपेक्षा है। युवकों, गृहणियों, कृषकों, श्रमिकों तथा अन्य व्यवसायों में लगे लोगों को अपनी रुचि की शिक्षा, जो समय के साथ विकसित हो जायेगी। मुक्त तथा सुदूर अधिगम इस दिशा में भावी प्रयास है।
(12) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने तथा सशक्त बनाने में सहयोग देने वाली संस्थायें- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, अखिल भारतीय कृषि शिक्षा परिषद् तथा अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् हैं। इन संस्थाओं के मध्य सम्मिलित योजना बनायी जायेगी जिससे कार्यात्मक संपर्क के द्वारा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाये। यह कार्य एन०सी०ई०आर०टी, (NCERT), इन्स्टीटयूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेसन, इन्स्टीटयूट ऑफ एजुकेशनल टैक्नोलॉजी के सहयोग से होगा। शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में इनको सम्मिलित किया जायेगा।
एक सार्थक साझेदारी
1976 के संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इसके अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों का दायित्व महत्वपूर्ण है। यह दायित्व, आर्थिक, प्रशासनिक रूप से सातत्यपूर्ण है। राज्यों के शैक्षिक दायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय एवं सम्मिलित विशेषता वाली शिक्षा को लागू करने का दायित्व वहन करेगी। शिक्षा के गुणात्मक (शिक्षण व्यवसाय सभी स्तरों पर) स्तर, देश की शैक्षिक आवश्यकता के अध्ययन एवं नियन्त्रण, कुल मिलाकर विकास के लिये जनशक्ति, शिक्षा, संस्कृति, मानव संसाधन विकास के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आना होगा। शिक्षा के पिरामिड की सार्थकता सम्पूर्ण देश में फैलानी होगी। यह सुमेलिता, साझेदारी के महत्व को प्रदर्शित करती है। यह सार्थक भी है और चुनौतीपूर्ण भी। राष्ट्रीय नीति सही मायनों में प्रभावशाली ढंग से चालू की जायेगी।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- सार्जेण्ट रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश | सा्जेण्ट रिपोर्ट के गुण | सा्जेण्ट रिपोर्ट के दोष
- राष्ट्रीय चेतना की वृद्धि के कारण | राष्ट्रीय चेतना के दौरान माध्यमिक शिक्षा की प्रगति | राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की असफलता के कारण
- भारतीय शिक्षा आयोग-1882 | हण्टर कमीशन | आयोग के सुझाव व संस्तुतियाँ
- कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917-1919) | सैडलर आयोग | आयोग के सुझाव व संस्तुतियाँ
- वर्धा-योजना की रूपरेखा | बुनियादी शिक्षा क्यों पड़ा? | बुनियादी शिक्षण-विधि
- बुनियादी शिक्षा योजना के उद्देश्य | बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त
- विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग | विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य | विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जाँच के विषय | विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव तथा संस्तुतियाँ
- माध्यमिक शिक्षा आयोग | मुदालियर आयोग के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य | माध्यमिक शिक्षा आयोग आयोग के जाँच के विषय
- भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव | कोठारी आयोग (1964-66) के मुख्य सुझाव
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]