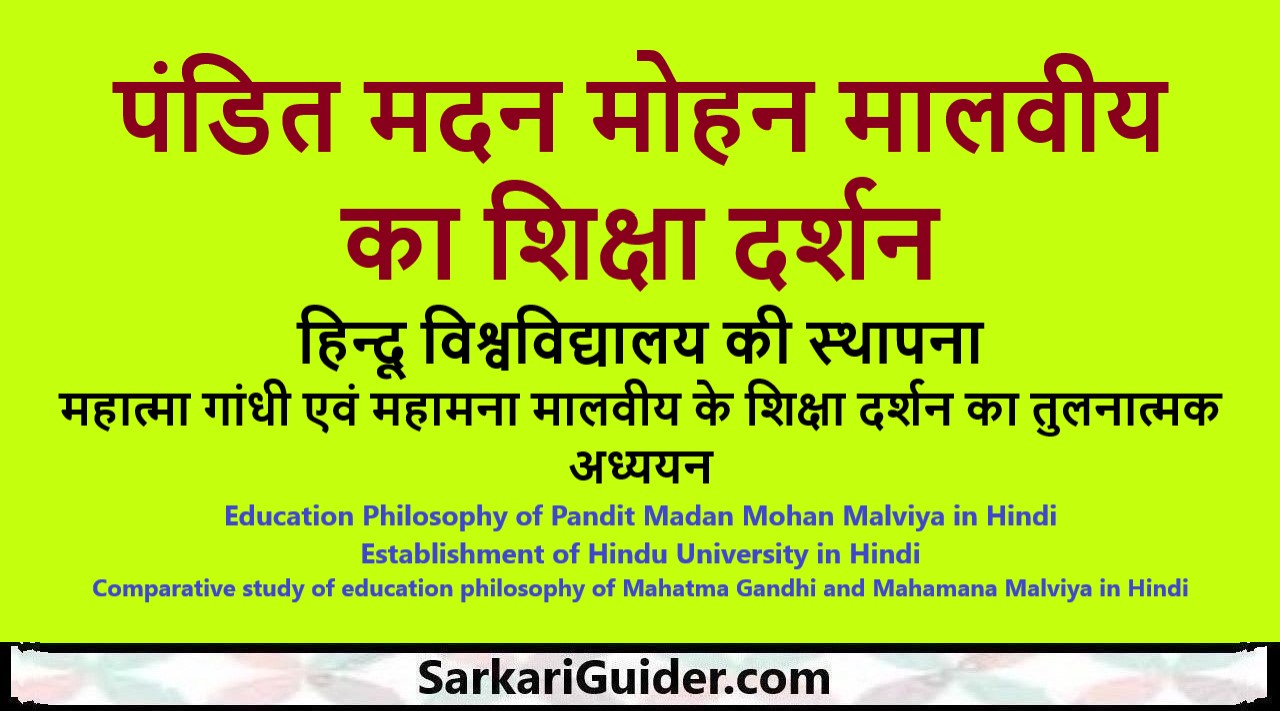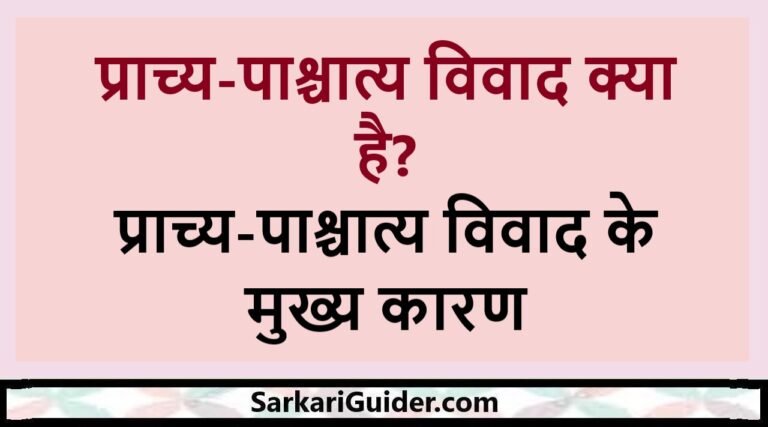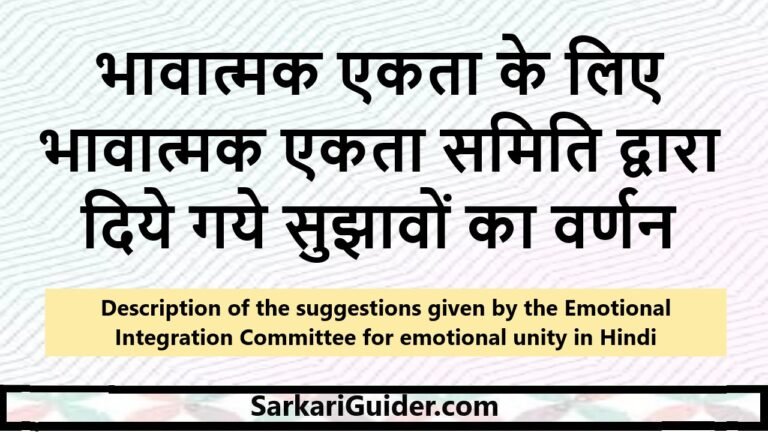पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा दर्शन | हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना | महात्मा गांधी एवं महामना मालवीय के शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन
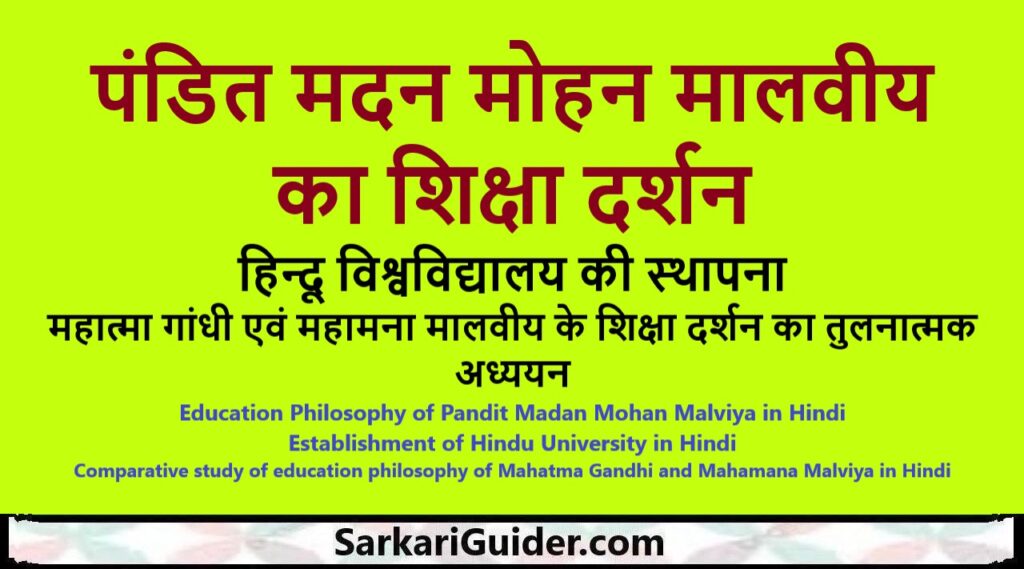
पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा दर्शन | हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना | महात्मा गांधी एवं महामना मालवीय के शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन | Education Philosophy of Pandit Madan Mohan Malviya in Hindi | Establishment of Hindu University in Hindi | Comparative study of education philosophy of Mahatma Gandhi and Mahamana Malviya in Hindi
जीवन वृत्त
पण्डित मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में 25 दिसम्बर सन् 1861 में हुआ। इनके पिता का नाम पण्डित ब्रजनाथ व्यास और माता का नाम श्रीमती मूनादेवी था। मूल रूप में यह परिवार मालवा का निवासी था और प्रयाग में बहुत दिनों से रह रहा था और मल्लई परिवार के नाम से प्रसिद्ध था। महामना मदनमोहन जी ने मल्लई को शुद्ध करके मालवीय कर दिया। धर्म में आस्था, कर्मठता, निर्भीकता, सन्तोष-वृति आदि गुण मालवीय जी को अपने माता-पिता से विरासत के रूप में मिले थे।
मालवीय जी की शिक्षा प्रारम्भ में एक संस्कृत पाठाशाला से शुरू हुई। बाद में वे इलाहाबाद के गवर्नमेण्ट हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजो का अध्ययन बड़े परिश्रम से किया। सन् 1881 में आपने प्योर सेण्ट्रल कालेज से एफ० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन् 1884 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी० ए० की परीक्षा पास की। इस परीक्षा में आपने विशेष योग्यता प्राप्त की। इसके बाद पिताजी की अस्वस्थता के कारण आप एम० ए० की परीक्षा नहीं दे सके और गवर्नमेण्ट हाई स्कूल में पहले 40 रुपये फिर 60 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक के पद को स्वीकार कर लिया।
छात्रावस्था में भी आप देश व समाज की सेवा में रुचि लेते थे। पढ़ते समय ही आपने ‘साहित्य सभा’ एवं ‘हिन्दू समाज’ की स्थापना की थी और उसके माध्यम से समाज की सेवा में रुचि लेने लगे थे।
तीन वर्ष तक सरकारी नौकरी करने के बाद उनका मन सरकारी नौकरी से ऊब चुका था और उधर कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के समय कलकत्ता में उनके भाषण का श्रोताओं पर प्रभाव पड़ चुका था। इस समय के सभापति दादाभाई नौरोजी समेत सभी व्यक्तियों ने उनके भाषण, प्रतिभा और राष्ट्रीयता की सराहना की। वहीं पर आपका परिचय कालाकाँकर-नरेश राजा रामपालसिंह जी से हुआ। उन्होंने मालवीय जी को अपने दैनिक समाचार पत्र ‘हिन्दुस्तान’ का सम्पादक बनकर कालाकौंकर बुलाया। मालवीय जी ने सन् 1877 से 1879 तक ‘हिन्दुस्तान’ का सम्पादन किया और सम्पादन के साथ-साथ आप वकालत भी पढ़ते रहे। सन् 1891 ई० में आपने वकालत पास की और परिश्रम से सन् 1892 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील बन गए।
मालवीय जी को वकालत में भी सफलता मिली और उनकी विलक्षण प्रतिभा की चारगए और धूम मच गई। इसके बाद उनका जीवन पत्रकार जननेता एवं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में बीता। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना करके उन्होंने समाज-सेवा का उच्चतम मानदण्ड स्थापित किया। 12 नवम्बर 1946 को संध्या के समय आपने इस संसार से महाप्रस्थान किया। महाप्रयाण के समय पर आप हिन्दू जाति की रक्षा के विषय में चिन्तित थे और नोआखाली में हिन्दुओं पर अत्याचारों से अत्यन्त क्षुब्ध थे।
कांग्रेस से सम्बन्ध (Association with Congress)
पं० मदन मोहन मालवीय ने सबसे पहले सन् 1886 में कांग्रेस के जन्म दूसरे ही वर्ष कांग्रेस अधिवेशन में भाषण किया। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तब वे कांग्रेस, में बने रहे। अनेक बार कांग्रेस की नीतियों से वे असहमत हुए और कांग्रेसी कुछ नीतियों का उन्होंने विरोध भी किया किन्तु वे अन्त तक कांग्रेसी बने रहे। सन् 1909 में कांग्रेस के चौबीसवें अधिवेशन के सभापति सर फिरोजशाह मेहना चुने गये थे किन्तु किन्हीं कारणों से अधिवेशन के छः दिन पूर्व उन्होंने इस सम्मान को अस्वीकार कर दिया। तल उनके स्थान पर पण्डित मदनमोहन मालवीय ही सभापति चुने गये और उन्होंने इस कर्त्तव्य को कुशलतापूर्वक निभाया। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। दस वर्ष बाद सन् 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन का उन्हें पुनः सभापति चुना गया। यह कांग्रेस का 33वाँ अधिवेशन था।
पत्रकारिता (Journalism)
मालवीय जी ने सन् 1885 से सन् 1887 तक ‘इण्डियन यूनियन’ नामक पत्र का सम्पादन किया। सन् 1887 में मालवीय जी को कालाकाँकर के राजा साहब ने ‘हिन्दुस्तान’ नामक पत्र के सम्पादन का कार्यभार सौंपा। मालवीय जी ने उस समय यह शर्त रखी कि सम्पादन में राजा साहब हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनसे किसी भी दिन मद्यपान किए हुए बातचीत नहीं करेंगे। राजा रामपाल सिंह ने उनको यह शर्त मान ली, फलतः वे कालाकॉर में ढाई वर्ष रहे और प्रथम हिन्दी दैनिक के सम्पादन का कार्य कुशलतापूर्वक करते रहे। उस समय उनके सम्पादकीय विभाग में स्वर्गीय पं० प्रतापरायण मिश्र और स्वर्गीय बालमुकुन्द गुप्त जैसे साहित्यकार एवं पत्रकार थे। सन् 1908 में उन्होंने अभ्युदय’ नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। यह पत्र क्रान्ति का अग्रदूत था और सामाजिक उन्नयन के आदर्शों से भरपूर था। कुछ दिनों तक इसका सम्पादन राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन ने भी किया था। ‘मर्यादा’ नामक मासिक पत्र भी क्रान्ति का सन्देशवाहक था और इसका प्रारम्भ भी मालवीय जी ने ही किया। सन् 1909 की विजयादशमी के दिन से उन्होंने ‘लीडर’ नामक दैनिक अंग्रेजी पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया ! इस पत्र के लिए उन्हें चौतीस हजार रुपया एकत्र करना पड़ा था। प्रयाग से निकलने वाले ‘भारत’ नामक हिन्दी दैनिक और दिल्ली से प्रकाशित ‘हिन्दुस्तान’ दैनिक पत्र भी मालवीय जी की कृपा से ही निकले। सन् 1933 की गुरु पूर्णिमा के दिन से मालवीय जी ने ‘सनातन धर्म’ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया। दिल्ली से श्री फतहचन्द शर्मा ‘आराधक’ के सम्पादकत्व में कुछ वर्षों तक प्रकाशित ‘गोपाल’ नामक साप्ताहिक पत्र के भी मालवीय जी संरक्षक एवं प्रेरणा स्त्रोत थे।
पत्रकार के रूप में मालवीय जी निर्भीक एवं पक्षपात रहित थे। वे व्यर्थ में किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं करते थे। उनकी आलोचना स्वस्थ होती थी। के किसी ऐसे विज्ञापन को भी अपने पत्र में स्थान नहीं देते थे जिसका समाज पर बुरा प्रभात पड़े। समाचारों के संकलन में वे पटु थे, लेखों व समाचारों के सम्पादन में वे कुशल थे और पत्र की साज-सज्जा की कला में वे प्रवीण थे।
जननेता के रूप में (As A Leader of the Masses)
मालवीय जी का जन्म उस समय हुआ जब देश में चारों ओर राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे थे और देश पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजी आतंकवाद का चारों ओर बोलबाला था। भारतीय धर्म, संस्कृति एवं परम्परा का हास हो रहा था। ऐसे समय में जनता का मार्गदर्शन अत्यन्त आवश्यक था। मालवीय जी ने अपने कार्यों से जनता के लोकप्रिय नेता का पद प्राप्त कर लिया। वाइसराय की कार्यकारिणी और प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के वे सर्वप्रथम भारतीय सदस्य थे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, भारती भवन, हिन्दू बोर्डिंग हाउस, सेवा समिति आदि अनेक संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की। उस समय कांग्रेस के माध्यम से जनता का नेतृत्व उन्होंने करना प्रारम्भ किया। किन्तु कभी-कभी कांग्रेस की कुछ नीतियों का उन्होंने विरोध भी किया। हिन्दू संगठन की वे उन्नति करना चाहते थे। हिन्दू महासभा के तो ये जन्मदाता ही थे। किन्तु मुसलमानों के प्रति उनके हृदय में कभी भी द्वेष नहीं रहा। इसीलिए तो बिसमिल इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी और नजर सोहानवी जैसे लोकप्रिय एवं ख्यातिप्राप्त उर्दू कवियों ने मालवीय जी के सम्बन्ध में काव्य रचना करके अपने को धन्य समझा।
मालवीय जी ने तिलक और गोखले जैसे राजनीतिज्ञों का मार्गदर्शन किया और महात्मा गाँधी जैसे राष्ट्रपुरुष को भी समय-समय पर प्रेरणा दी। अन्दलीवे हिन्द ‘नज़र’ की निम्नलिखित पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं-
“सर असर मातम है दुनियाँ, जिस तिलक की मौत पर,
सच तो यह है, उस तिलक का रहनुमा है मालवी।।
गोखले ने जो दिया था, हमको पैगामे अजल,
ऐ ‘नज़र’ उस इब्तिदा की, इन्तिहा है मालवी।”
मालवीय जी को हिन्दू और मुसलमान समान रूप से प्यार करते थे। कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना जैसे साम्प्रदायिक नेता भी उनका लोहा मानते थे और अनेक मुसलमान उनको आराध्यदेव की तरह पूजते थे। ‘नज़र’ के शब्दों में-
“दिल खुदा का घर है, उस घर में बसा है मालवी,
हम पुजारी हैं, हमारा देवता है मालवी।”
यही नहीं नज़र तो यहाँ तक कह डालते हैं कि
“ईंटों का पत्थर से हम देते नहीं हर्गिज जवाब,
वह बुरा है आप, जो समझे बुरा है मालवी।’
मालवीय जी ने कांग्रेस के दो अधिवेशनों का सभापतित्व किया, गोलमेज कांफ्रेन्स में भाग लेने विलायत गए, अनेक अन्य स्थानों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और देशवासियों को अज्ञानान्धकार से निकालने के लिए एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की। सचमुच वे एक महान् जन नेता थे।
भारतीय संस्कृति के पोषक (Indian Culturalist)
मालवीय जी कट्टर हिन्दू थे किन्तु हिन्दू शब्द उनके लिए धर्म का द्योतक न होकर जाति का द्योतक था। अतः वे मानते थे कि भारतवर्ष में रहने वाले सनातन धर्मी, आर्यसमाजी, जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुसलमान सभी हिन्दू हैं।
मालवीय जी सभी धर्मों का आदर करते थे और सभी धर्मों के लोगों को अपने-अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की प्रेरणा देते थे। किन्तु सनातन धर्म की दुर्दशा देखकर वे बड़े खिन्न थे और इस धर्म के अनुयायियों को उन्होंने विशेष रूप से जाग्रत होने का संदेश दिया। उनका आचरण धर्मानकूल था। सम्पूर्ण जीवन धर्ममय था । हिन्दू विश्वविद्यालय के सभी मकानों को वे ‘हिन्दू शिल्प-शास्त्र के अनुसार ही बनाने का आग्रह करते थे।
दिल्ली के लक्ष्मीनारायण मन्दिर को मालवीय जी की प्रेरणा से ही बिड़ला बन्धुओं ने बनवाया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्दर विश्वनाथ मन्दिर को बनवाने की उनकी बड़ी लालसा थी। उनकी यह लाससा उनकी मृत्यु के बाद पूरी हो सकी। वे आयुर्वेद शास्त्र के समर्थक और आयुर्वेद की शास्त्रीयता को प्रमाणित करते थे। उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय हिन्दू संस्कृति का संरक्षक है।
मालवीय जी की कामना थी कि स्वतन्त्र भारत में गो-वध कानूनन बन्द हो जाएगा। मालवीय जी गो-भक्त ब्राह्मण थे और अनेक गो-सेवी संस्थाएँ उनकी प्रेरणा से स्थापित हुई थीं। मालवीय जी अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास से कोई अतिथि बिना भोजन किए जा नहीं सकता था। अतिथि, ब्राह्मण और गो उनके आराध्य थे। मालवीय जी पुराणों की सत्यता में विश्वास करते थे और श्रीमद्भागवत के श्लोकों को भावविभोर होकर पढ़ते थे।
उनका बाह्य व्यक्तित्व भी भारतीय संस्कृति का पोषक था। तिलक विहीन मस्तक उनका कभी नहीं रहता था। सिर पर साफा और शुभ-श्वेत वस्त्र उनको प्रिय थे। ये बड़े शिष्ट, विनयी एवं मृदुभाषी थे। विरोधियों को भी वे स्नेह की दृष्टि से देखते थे।
मालवीय जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता की रक्षा की। भोजन के विषय में भी वे स्पर्शापर्श का विचार रखते थे। विलायत जाते समय यहाँ से गंगाजल व मिट्टी तक ले गए थे किन्तु सामाजिक जीवन में वे हरिजनों के साथ समानता का व्यवहार करते थे। काशी में हरिजनों को उन्होंने ‘ओऽम् नमः शिवाय’ का मंत्र दिया था। हरिजनों को दीक्षित करने का काशी के तत्कालीन पंडितों ने घोर विरोध किया था किन्तु पं० नवदेव मिश्र आदि विद्वानों के विरोध के बावजूद मालवीय जी ने अछूतों को मन्त्र दिया।
मालवीय जी हिन्दी और संस्कृत के समर्थक थे। संस्कृत को भारतीय संस्कृति को वहन करने वाली भाषा मानते थे और प्रत्येक भारतीय के लिए संस्कृत का अध्ययन आवश्यक बतलाते थे। वे उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को उचित बतलाते थे किन्तु पाठ्य- पुस्तकों के अभाव के कारण काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वे हिन्दी को लागू नहीं कर सके थे। किन्तु इस दिशा में उनका चिन्तन स्पष्ट था और वे हिन्दी व संस्कृत के द्वारा विद्या के प्रचार पर बल देते थे।
हिन्दी का समर्थन (Support for Hindi)
मालवीय जी के समय में अंग्रेजी का अत्यधिक बोलवाला था। स्वयं मालवीय जी अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। किन्तु उन्हें यह बात बड़ी असंगत लगती थी कि अंग्रेजी ही उच्च शिक्षा का माध्यम बनी रहे। उनकी कामना थी यह पद हिन्दी को मिलना चाहिए। वे यह अनुभव करते थे। कि उच्च कोटि की शिक्षा मातृभाषा के अध्ययन से ही सम्भव है। राजकाज की भाषा के रूप में भी वे हिन्दी को प्रतिष्ठित करना चाहते थे।
मालवीय जी के समय में सरकारी कार्यालयों और कचहरियों में केवल उर्दू में काम होता था। बड़े कार्यालयों व बड़े न्यायालयों में यह काम अंग्रेजी में होता था। छोटे कार्यालयों व आदलतों में उर्दू चलती थी पर अधिकांश जनता उर्दू जानती नहीं थी। मालवीय जी ने इस सम्बन्ध में आँकड़े एकत्र किए और तर्कों के आधार पर शासकों को स्मृतिपत्र दिया। संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन गवर्नर सर एण्टनी मैकडानल को 2 मार्च सन् 1889 को उन्होंने पत्र में लिखा था-“पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध की प्रजा में शिक्षा का फैलना इस समय सबसे आवश्यक कार्य है और गुरुतर प्रमाणों से सिद्ध किया जा चुका है कि इस कार्य में सफलता तभी प्राप्त होगी जब कचहरियों और सरकारी दफ्तरों में नागरी अक्षर जारी किए जायेंगे। अतएव आज इस शुभ कार्य में जरा-सा भी विलम्ब न होना चाहिए और न राज्य कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के विरोध पर कुछ ध्यान ही देना चाहिए। हमें आशा है कि वे बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक, जिनके प्रबल प्रताप से लाखों जीवों ने इस घोर अकाल-रूपी काल से रक्षा पाई है, अब नागरी अक्षरों को जारी करके इन लोगों की भावी उन्नति और वृद्धि का बीज बोएँगे और विद्या के सुखकर प्रभाव के अवरोधों को अपनी क्षमता से दूर करेंगे।
मालवीय जी के समय में हिन्दी के दो रूप प्रचलित थे-उर्दू मिश्रित हिन्दी और संस्कृत गर्भित हिन्दी । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का सफल नेतृत्व संस्कृत गर्भित हिन्दी के पक्ष में था। मालवीय जी ने भी इसी हिन्दी का प्रचार किया। सन् 1884 में उन्होंने हिन्दी उद्घारिणी प्रतिनिधि सभा की सदस्यता ग्रहण की। यह सभा बाद में नागरी प्रवर्धन सभा कहलाई। इस सभा का काम नागरी लिपि का प्रचार करना था और इसका मुख्य कार्यालय प्रयाग में था। 10 अक्टूबर, 1910 को हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथम बैठक हुई। उसकी अध्यक्षता मालवीय जी ने की और यह बैठक नागरी प्रचारिणी सभा में हुई। इसमें राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन मंत्री नियुक्त हुए। टण्डन जी के प्रयत्नों से और मालवीय जी के मार्गदर्शन से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की बडी उन्नति हुई। सम्मेलन का नवम् अधिवेशन 1 अप्रैल, 1919 में बम्बई में हुआ जिसकी अध्यक्षता पुनः मालवीय जी ने की और इस बार अध्यक्षता स्वीकार करने के लिए महात्मा गाँधी ने मालवीय जी से विशेष आग्रह किया था।
ऊपर यह लिखा जा चुका है कि मालवीच जी ने कचहरियों में हिन्दी को काम-काज के माध्यम के रूप में अपनाने का आन्दोलन किया था और उन्हीं के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 1900 ई० में गवर्नर ने कचहरियों की भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार कर लिया था। इस अवसर पर मालवीय जी ने कहा था-“हमने कहा कि कचहरियों की भाषा हिन्दी भी कर दी जाय। राजा ने हमारे प्रदेशों में कचहरियों की भाषा हिन्दी भी कर दी। इन दिनों इस देश में कचहरियों की जो भाषा है, वह हिन्दी है। यत्न चेष्टा का प्रयोजन है। आदमी जिस बात के लिए यत्न और चेष्टा करता है, वह हो जाती है। “
हिन्दी के पठन-पाठन पर मालवीय जी ने बल दिया है और उत्तर पुस्तकों की रचना की प्रेरणा दी है। अन्य भाषाओं की उत्तम पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद हो एवं मौलिक पुस्तकें रची जायें। इस विषय में मालवीय जी ने कहा है- “जो स्कूल कालेज स्थापित किए गए हैं, उनमें लड़के हिन्दी पढ़ें। यूरोपीय इतिहास, काव्य, कला-कौशल आदि की पुस्तकें हिन्दी में अनुवादित हों। हिन्दी में उपयोगी पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जाय। सरकार ने स्कूलों में हिन्दी जारी कर दी है। अब हमें चाहिए, हम हिन्दी की उत्तमोत्तम पाठ्य-पुस्तकें तैयार करें।”
मालवीय जी जिस समय लगभग 15-16 वर्ष की आयु के थे उस समय उनकी रुचि हिन्दी कविता में भी थी। यह उनके अध्ययन का समय था किन्तु ‘मकरन्द’ उपनाम से उन्होंने कुछ कविताएँ भी लिखी हैं। उनके समय में समस्या पूर्ति का खूब प्रचलन था और भारतेन्दु जी की बैठक कवि-दरबार का काम करती थी। मालवीय जी ने ‘राधिकारानी’ नाम से कविता लिखी किन्तु भारतेन्दु जी के संकोच से कवितापाठ उन्होंने नहीं किया। बाद में डाक से यह कविता भेज दी और भारतेन्दु इसे पढ़कर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उस समस्यापूर्ति वाली कविता के अतिरिक्त भी उन्होंने कुछ कविताएँ लिखीं किन्तु बाद में उनका यह कार्य बन्द हो गया। नमूने के रूप में उनकी समस्यापूर्ति वाली कविता प्रस्तुत है-
“इन्दु सुधा बरस्यो नलिनीन पै,
वे न बिना रवि के हरखानी।
त्यों रवि तेज दिखायो तऊ बिनु,
इन्दु कुमोदिनि ना बिकसानी ।।.
न्यारी कछू यह प्रीति की रीति,
नहीं ‘मकरन्द’ जू जात बखानी।
साँवरे कामलीवारे गुपाल पै–
रीझि लटू भई राधिकारानी।।’
मालवीय जी की कविताओं में भावों की गहनता के दर्शन होते हैं। काव्य के प्रति प्रेम रखने का वरदान ये ईश्वर से माँगते हुए एक स्थल पर लिखते हैं-
“गुणी जनन को साथ,
रसमय कविता मांहि रुचि।
सदा दीजियो नाथ,
जब जब इहाँ पठाइयो ।’
मालवीय जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिन्दी के पठन-पाठन की उच्च व्यवस्था की। प्रसिद्ध आलोचक एवं भाषाविज्ञानी डा० श्यामसुन्दर दास एवं प्रसिद्ध विद्वान् ख्याति प्राप्त आलोचक एवं लब्धप्रतिष्ठ निबन्धकार आचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ल तथा महाकवि अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ जैसे व्यक्तियों ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में शिक्षण का कार्य किया।
मालवीय जी को हिन्दी के सर्वप्रथम दैनिक पत्र का सम्पादक होने का गौरव प्राप्त है। यह पत्र कालाकाँकर से ‘हिन्दुस्तान’ नाम से निकलता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य अनेक हिन्दी पत्रों का सम्पादन एवं प्रकाशन किया। उनके लेख एवं उपदेश हिन्दी की अमूल्य निधि हैं। हिन्दी की सेवा करने वालों में मालवीय जी का नाम आदर से लिया जाता है।
मालवीय जी के प्रयासों से हिन्दी को कचहरियों में राजकाज का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला। मालवीय जी ने हिन्दी आन्दोलन का सफल संचालन किया। अनेक साहित्यकारों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी के पठन-पाठन को उच्च स्तर पर लाने के लिए विद्वान् प्राध्यापकों को जुटाने का कार्य किया। उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी अखिल भारतीय हिन्दी सेवी संस्था को जन्म दिया। अनेकानेक हिन्दी पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने सम्पादन, प्रकाशन एवं संचालन किया। उनके इन प्रयत्नों के लिए हिन्दी-जगत् उनका सदैव ऋणी रहेगा।
शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)
महामना मालवीय जी शिक्षा की शक्ति में अटूट श्रद्धा रखते थे। अतः वे व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा को मूल आधार मानते थे। उनका कहना था- ‘यदि देश का अभ्युदय चाहते हो तो सब प्रकार से यल करो कि देश में कोई बालक और बालिका निरक्षर न रहे।’ मालवीय जी को देश की शैक्षिक दुर्दशा से बड़ी पीड़ा होती थी। देश में व्याप्त निरक्षरता को भारतीयों के पतन का वे कारण मानते थे इसलिए साक्षरता पर उनका बहुत अधिक बल था।
जहाँ तक शैक्षिक उद्देश्यों का सम्बन्ध है, मालवीय जी शारीरिक विकास को त्याज्य नहीं समझते थे। वे सदा शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। ‘मेरा बचपन’ नामक लेख में मालवीय जी लिखते हैं, “स्वास्थ्य के तीन खम्भे हैं आहार, शयन और ब्रह्मचर्य। तीनों का युक्तिपूर्वक सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।’ अन्यत्र वे लिखते हैं कि यदि राष्ट्र के निवासियों का शरीर दुर्बल है तो राष्ट्र भी दुर्बल होगा और शरीर को संयम, पौष्टिक भोजन और व्यायाम से सशक्त बनाना चाहिए।
मालवीय जी के अनुसार शिक्षित व्यक्ति को भारत में भक्ति रखनी चाहिए। भारत हमारी जन्मभूमि है और यहाँ का जर्रा-जर्रा, कोना-कोना हमारे लिए पवित्र है। उनका कहना था-“यह भारत हमारा देश है। सभी बातों के विचार से इसके समान संसार में कोई दूसरा देश नहीं है। हमको इस बात के लिए कृतज्ञ तथा गौरवान्वित होना चाहिए कि उस कृपालु परमेश्वर ने हमें इस पवित्र देश में पैदा किया।’ राष्ट्र के विषय में मालवीय जी का विचार था कि राष्ट्र के निवासियों का शरीर, मन और आत्मा ही राष्ट्र है अतः इन तीनों को सशक्त बनाना चाहिए। संयम, भोजन और व्यायाम से शरीर को, सात्विक विचार और सदाचार से मन को तथा सत्संग, श्रद्धा और प्रार्थना से आत्मा को सबल बनाना चाहिए।
मालवीय जी स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि “भारत, भगवद्गीता, भारती, भाषा और भारतवर्ष में भक्ति करो। जिन बातों से देश में सम्पत्ति बढे उनके विषय में सवेत रहो। देश के निवासियों का सब ओर से उदय हो, स्थायी सुख-सम्पत्ति तथा प्रभाव एवं धर्म रक्षित हो।” मालवीय जी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय का आधार हिन्दुत्व है। हिन्दुत्व की अवनति से संसार की अवनति होगी। उनके अनुसार हिन्दुओं ने हो दार्शनिक सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप दिया है। हिन्दुत्व विहीन राष्ट्रीयता जीवित नहीं रह सकती। अतः वे हिन्दुत्व पर आधारित राष्ट्रभक्ति की शिक्षा का उद्देश्य बनाना चाहते थे। किन्तु मालवीय जी की, ‘हिन्दू’ की धारणा बडी व्यापक थी। भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को वे हिन्दू मानते थे। ‘हिन्दू’ शब्द राष्ट्रीयता का द्योतक है, एक विचारधारा का प्रतिनिधि है, एक दर्शन को परिलक्षित करने वाला है एवं एक जीवन-शैली का नाम है। ‘हिन्दू’ शब्द मनुष्यता का द्योतक है और मनुष्यता के आगे जाति-पाँति का कोई स्थान नहीं। इस प्रकार की राष्ट-भक्ति को वे भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाना चाहते थे।
मालवीय जी सेवा को बहुत महत्व देते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यक्ति यह सीख जाए कि सेवा धर्म ही परम धर्म है। पवित्र और पुरातन गाथाएँ सेवा धर्म की व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। इस सेवा धर्म को अनुभव द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। शब्दों के माध्यम से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
मालवीय जी चारित्रिक उन्नति के पक्षपाती धे और प्रत्येक व्यक्ति का संयम अपनाने का परामर्श देते थे। उनके अनुसार धर्म व नैतिकता को शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार करके युवकों का चरित्र निर्माण करना चाहिए।
मालवीय जी के अनुसार भारतीय शिक्षा का उद्देश्य भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना ही होना चाहिए। इस संस्कृति से समस्त विश्व का कल्याण होगा। हिन्दु शास्त्रों की व हिन्दू संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मालवीय जी के विचार से शिक्षा का उद्देश्य बालक का शारीरिक व मानसिक विकास करते हुए उसे सदाचारी बनाना है और उनको आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान रखना है। सन् 1927 ई० में स्नातकों को आशीर्वाद देते हुए मालवीय जी ने निम्नलिखित दोहे का पाठ किया और इस पर आचरण करने को कहा-
दूध पियो, विद्या पढ़ो, सदा जपो हरिनाम।
सदाचार पालन करो पूरेंगे सब काम।।
पाठ्यक्रम (Curriculum)
जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, मालवीय जी पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाने के पक्ष में थे। वे देश के अभ्युदय के लिए विज्ञान के अध्ययन को आवश्यक मानते थे। विभिन्न उद्योगों और कलाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना भी वे आवश्यक समझते थे। इन विषयों की उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में की।
भारत कृषि प्रधान देश है। अतः कृषि की शिक्षा भी इस देश की शिक्षा में अवश्य होनी चाहिए। मालवीय जी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग की शिक्षा की उच्चतम व्यवस्था की।
भारतीय जनता का कल्याण एलोपैथी के माध्यम से इतना नहीं हो सकता जितना आयुर्वेद के प्रचार से हो सकता है। मालवीय जी के अनुसार आयुर्वेद को पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग होना चाहिए और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के साथ शल्य-चिकित्सा पद्धति का भी उन्होंने प्रबन्ध किया।
संगीत एवं ललित कलाएँ व्यक्ति को सौन्दर्यानुभूति की प्रेरणा देती हैं। अतः इनकी शिक्षा का सुचारु प्रबन्ध होना चाहिए। भारतीय संगीत, भारतीय शिल्पकला आदि से मालवीय जी को विशेष प्रेम था।
पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा की योजना भी होनी चाहिए। मालवीय जी के अनुसार चरित्र निर्माण का आधार धार्मिक शिक्षा है। महामना स्वयं कट्टर सनातनी थे। किन्तु वे सभी धर्मों का आदर करते थे और सभी धर्मावलम्बियों को धर्म के रहस्यों को समझने का परामर्श देते थे। पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा का स्थान तो रहे किन्तु अन्य धर्मों के प्रति सहित उसका लक्ष्य होना चाहिए। इस सान्त्र में मालवीय जी स्वयं लिखते हैं- “धर्म में लगे रहना तो किसी अवस्था में अवनति का कारण हो ही नहीं सकता। कारण यह है कि भारतवासी, धर्म में लगे रहना तो दूर रहा, अपने धर्म को समझते ही नहीं। धर्म को एक खेल मान रखा है। क्या धर्मों के भेद से हिन्दुओं आर्यों, मुसलमानों और ईसाइयों का आपस में झगड़ा करना कोई धर्म का जा सकता है? हिन्दू मूर्तिपूजक हैं और आर्यसमाजी नहीं, इसलिए उन दोनों में सदैव तनातनी रहे यह कोई धर्म है? हिन्दू और मुसलमानों के मत अलग-अलग हैं, तो इस विचार से यदि कोई मुसलमान हिन्दुओं के सदेव विरुद्ध रहे, यहाँ तक कि गवर्नमेण्ट की दृष्टि में उनको बागी साबित करने का झूठा सच्चा प्रयत्न करे, तो क्या वे अपने धर्म में लगे हुए हैं? कदापि नहीं। यदि ऐसा करते हैं तो हिन्दू और आर्य अपने वेदों के, ईसाई अपनी इंजील के और मुसलमान अपने कुरान शरीफ के विरुद्ध चल रहे हैं। धर्म यह है कि प्राणी को प्राणी के साथ सहानुभूति हो, एक-दूसरे को अच्छी अवस्था में देखकर प्रसन्न हों और गिरी हुई अवस्था में सहायता दें।”
मालवीय जी की कल्पना का पाठ्यक्रम विस्तृत है। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में बड़े विस्तृत पाठ्यक्रम की योजना बनाई है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनका पाठ्यक्रम साहित्यिक, नैतिक एवं सौन्दर्यपरक प्रत्ययों को अधिक महत्व प्रदान करता है।
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University)
अपने उद्देश्यों को साकार रूप प्रदान करने के लिए एवं देश में शिक्षा का प्रसार करने के लिए मालवीय जी ने काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 4 फरवरी 1916 को 12 बजे वायसराय लाई हार्डिंग ने इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। नींव में एक ताम्रपत्र रखा है जिसमें 20 श्लोक लिखे हुए हैं। पहला ही श्लोक है-
धर्म सनातनं वीक्ष्य काल वेगेल पीडितम् ।
भूतले दुर्व्यवस्थं च व्याकुलं मानव कुलम् ।।
अर्थात् सनातन धर्म को काल के वेग से पीड़ित तथा सम्पूर्ण भूमण्डल के जीवों को दुर्दशा में और व्याकुल देखकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू विश्वविद्यालय को सनातन धर्म के उद्धार के लिए, हिन्दू जाति को संगठित करने के लिए, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए एवं हिन्दू धर्म ग्रन्थों के अनुशीलन के लिए स्थापित किया गया।
हिन्दू विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ चारित्रिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। इस विश्वविद्यालय के लिए मालवीय जी ने समस्त देश के लोगों से दान की अपील की। मालवीय जी की अपील का प्रभाव पड़ा और हिन्दू, मुसलमान सभी ने हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए दान दिया।
हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना से मालवीय जी कितने प्रसन्न हुए थे, इसका अनुमान 8 जुलाई 1916 को उनके द्वारा रची गई और गाई गई निम्नलिखित रचना से लगाया जा सकता है –
“जपतु विश्वविद्यालय काशी !
मातु गंग पच जाहि पिघावत, मूल धर्म सुखराशी ।
पालत विश्वनाथ विद्या-गुरु, शंकर अज अविनाशी ।
ज्ञान विज्ञान प्रकाशी!
गंग जमुन संगम विच देवी, गुप्त रही चपला सी।
ईस-कृपा तें सोई सरस्वति, वाराणसी प्रकाशी ।।
तिमिर-अज्ञान विनाशी!
ऋषि मुनि संग नृपमंडल सोहत, उच्छव परम हुलासी ।
देत असीम फलहु अरु फूलहु सब विधि भारतवासी ।।
लहहु विद्या-धन राशी!
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मालवीय जी बीस वर्ष तक कुलपति रहे। इसके बाद कुलपति के पद पर भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आसीन हुए। स्वतन्त्रता के बाद कुछ समय तक आचार्य नरेन्द्रदेव भी उपकुलपति रहे। श्री त्रिगुणसेन के कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय की प्रणाली में कुछ परिवर्तन हुए। इस विश्वविद्यालय का वर्तमान स्वरूप शनैः-शनैः बदल रहा है। युग की धारा के अनुरूप बदलना चाहिए किन्तु मालवीय जी के आदर्शों को इस विश्वविद्यालय में साकार रूप देने का यथासम्भव प्रयत्न अभी भी होना चाहिए।
राष्ट्रगुरु और राष्ट्रपति के आदर्श
(Ideals of Teacher of the Nation and Father of the Nation)
गाँधी जी के साथ भारत की विशाल जनसंख्या थी तो मालवीय जी के साथ गुणवानों की जमात थी। मालवीय जी गुण के पक्ष में रहे तो गाँधी जी संख्या के पक्ष में। स्वतन्त्र भारत की प्रगति के लिए गुण और संख्या, दोनों का मेल आवश्यक है। भारत सही माने में भारत तब होगा जब वह मालवीय और गाँधी दोनों के आदर्शों को मूर्तिमान करे।
मालवीय और गाँधी एक-दूसरे के पूरक थे। आज भी उनके आदर्श एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों में कभी-कभी सैद्धान्तिक मतभेद था तो दोनों एक-दूसरे का सदा आदर करते थे। सन् 1946 में पण्डित नेहरू के नेतृत्व में जब पहली बार केन्द्रीय सरकार बनी तो मालवीय जी ने प्रसन्न होकर रोग शैय्या से गाँधी जी को तार भेजा “अपने देश में अपना राज” तार को पढ़कर गाँधी जी की आँखों से हर्ष के आँसू बह चले। दोनों के हृदय के तार उस तार के माध्यम से झंकृत हो उठे थे।
मालवीय और गाँधी में तुलना का कोई प्रश्न नहीं। एक महामना थे तो दुसरे महात्मा, एक पंडित थे तो दूसरे बापू । पद्मकान्त मालवीय के शब्दों में, “मालवीय जी राष्ट्रगुरु थे, महात्मा जी राष्ट्रपिता। वशिष्ठ और राम की तुलना जैसे नहीं हो सकती वैसे ही मालवीय जी और महात्मा जी में तुलना बेकार है। हम तो केवल शिक्षा ले सकते हैं वशिष्ठ और राम तथा मालवीय जी और महात्मा जी के आपसी सम्बन्धों, कार्य करने के उनके अपने तरीकों से और यदि हम उनका कुछ भी अनुकरण कर सके अपने जीवन में, तो हम धन्य हो सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं।”
भारतीय नेताओं को आज राष्ट्रगुरु और राष्ट्रपिता के आदर्शों से शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। हमारे नवयुवकों को उनके आचरण का अनुकरण करना चाहिए। इस समय देश में दोनों की कमी खटक रही है।
उपसंहार (Conclusion)
मालवीय जी कट्टर सनातन धर्मी थे। वे वर्णाश्रम धर्म में विश्वास करते थे किन्तु वे अन्य मतावलम्बियों से घृणा नहीं करते थे। मालवीय जी हिन्दू संस्कृति की सुरक्षा के लिए बड़े प्रयत्नशील थे। किन्तु ‘हिन्दू’ शब्द का अर्थ उनके लिए संकुचित नहीं था। उन्होंने शिक्षाशास्त्र के सिद्धान्तों की विवेचना विधिवत् नहीं की। किन्तु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक होकर उन्होंने व्यावहारिक शिक्षा शास्त्री होने का संसार को परिचय दिया है। उनकी निःस्वार्थ सेवा-भावना, उनकी त्याग-वृत्ति और दीन-दुखियों के प्रति उनकी सहानुभूति वन्दनीय थी। उन्होंने करोड़ों रुपये एकत्र किए किन्तु स्वयं सदा निर्धन ही बने रहे। वे भारत के अभिमानी पुरुष थे और भारत को उन पर अभियान था। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में-
“भारत को अभिमान तुम्हारा,
देश भारत के अभिमानी।
पूज्य पुरोहित थे हम सबके,
रहे सदैव समाधानी ।।
तुम्हें कुशल याचक कहते हैं,
किन्तु कौन उस सा दानी?
अक्षय शिक्षा-सत्र तुम्हारा,
हे ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी।।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- प्रश्नावली | प्रश्नावली की परिभाषा | प्रश्नावली की विशेषताएँ | प्रश्नावली का वर्गीकरण
- श्रेणी मापनी विधि | दर मापक का नमूना | श्रेणी मापनी विधि को नमूना बनाकर स्पष्ट कीजिए
- व्यक्तित्व क्या है | व्यक्तित्व का अर्थ | व्यक्तित्व की परिभाषा | व्यक्तित्व के प्रकार
- बुद्धि और अनुवांशिकता | बुद्धि और वातावरण | बुद्धि, अनुवांशिकता एवं वातावरण
- बुद्धि | बुद्धि का अर्थ | बुद्धि की परिभाषा | बुद्धि का स्वरूप | बुद्धि के प्रकार | बुद्धि के सिद्धान्त | बुद्धि की संरचना | बुद्धि और ज्ञान में अन्तर
- बुद्धि मापन का तात्पर्य | मानसिक आयु और कालिक आयु | बुद्धि-लब्धि
- बुद्धि परीक्षण | बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार | बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता
- ज्ञानोपार्जन परीक्षण | ज्ञानोपार्जन परीक्षण के उद्देश्य | ज्ञानोपार्जन परीक्षण के प्रकार | निबन्धात्मक परीक्षण | निबन्धात्मक परीक्षणों में सुधार
- भारत में बुद्धि परीक्षण | intelligence test in India in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]