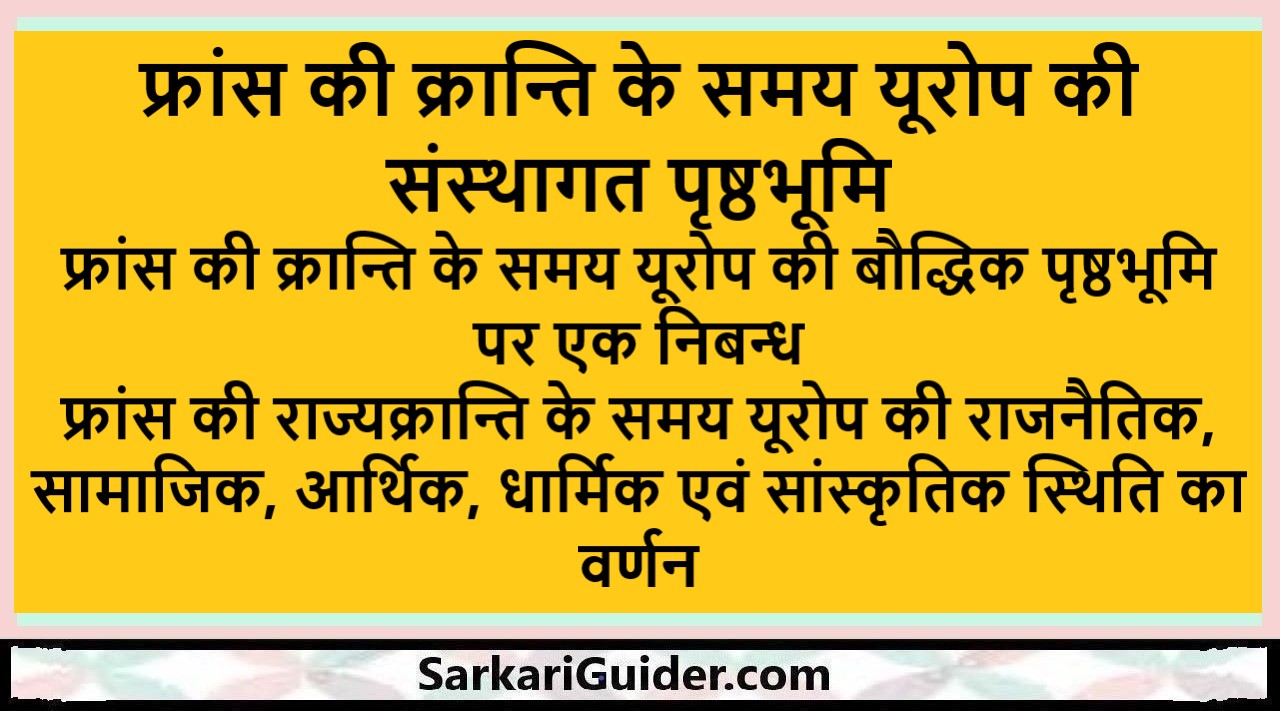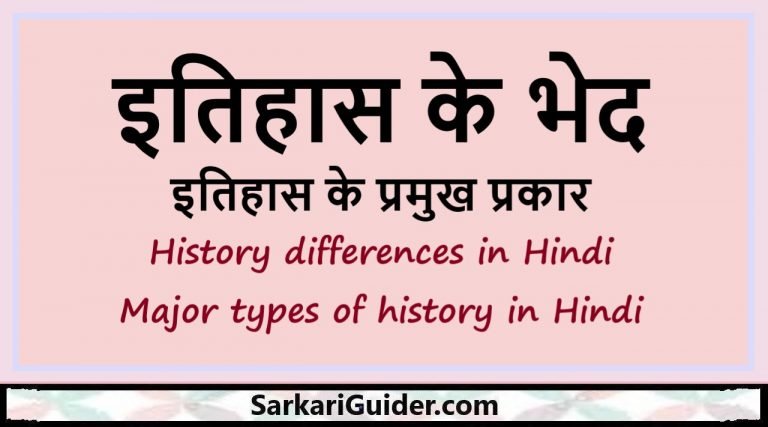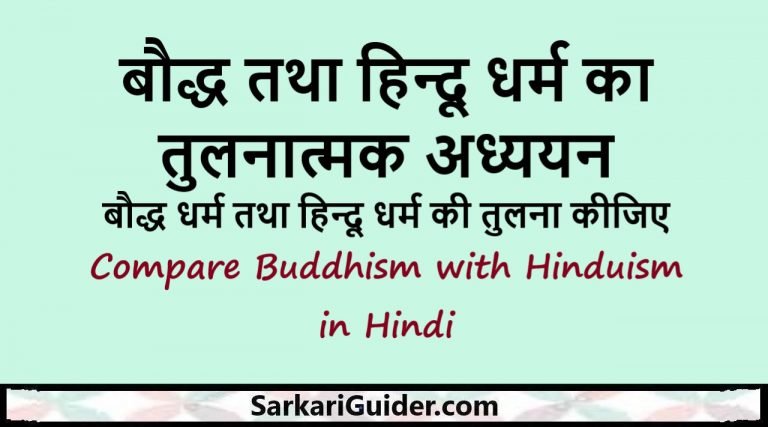फ्रांस की क्रान्ति के समय यूरोप की संस्थागत पृष्ठभूमि | फ्रांस की क्रान्ति के समय यूरोप की संस्थागत तथा बौद्धिक पृष्ठभूमि पर एक निबन्ध | फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय यूरोप की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन

फ्रांस की क्रान्ति के समय यूरोप की संस्थागत पृष्ठभूमि | फ्रांस की क्रान्ति के समय यूरोप की संस्थागत तथा बौद्धिक पृष्ठभूमि पर एक निबन्ध | फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय यूरोप की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन
फ्रांस की क्रान्ति के समय यूरोप की संस्थागत पृष्ठभूमि
1789 ई० की फ्रांस की राज्यक्रांति के समय यूरोप अनेक राज्यों में विभाजित था और कई राज्यों का विघटन हो चुका था। यूरोपीय राजवंश, अर्थात् हैप्पवर्ग, होहेनजोलन, बूबों आदि अपने वंश के स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामाज्य विस्तार में लगे हुए थे, जबकि उनकी प्रजा अनेक कठिनाइयों का सामना कर रही थी। ये राजा वंशगत आधार पर हुआ करते थे। केवल इंगलैंड को छोड़कर समस्त यूरोप में निरंकुश शासन स्थापित था। राजाओं को सारे अधिकार प्राप्त थे और वे जनता से शासन-संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की सलाह नहीं लेते थे। जनता को वे अपने अधीन समझते थे और उनका बुरी तरह शोषण करते थे। राजा अपने राज्य का सर्वेसर्वा था। राय की सारी शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थीं।
सभी यूरोपीय राज्यों में सामंती व्यवस्था का प्रचलन था। राजा सामंतों की सहायता से शासन चलाता था और यह स्वयं भी एक बड़ा सामंत था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि सामंत् सुविधाभोगी हो गए थे और अपने दायित्वों का निर्वाह न कर पूजा का शोषण कर ऐशो-आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। ये किसानों से अनेक तरह के कर वसूल करते थे और उन्हें बेगारी करने के लिए मजबूर करते थे। सामंत व्यापारियों से भी कई तरह के कर वसूलते थे। सामंतों की आपसी लड़ाई के कारण कानून-व्यवस्था ठीक नहीं रहती थी, जिससे व्यापारी परेशान थे। ये सामंत राजा की बातों की भी अवहेलना करते थे और राज्य की सेवा के बदले राजा के अधिकारों को कम कर उसे तरह-तरह से तंग करते थे। चूँकि राजा वंशगत आधार पर होते थे, अतः अधिकतर राजा अनुभवहीन, अयोग्य तथा आलसी हुआ करते थे। उनको साधारण जनता की कोई चिंता न थी। वे केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते थे। चारों ओर अनैतिकता, भ्रष्टाचार और फूट का साम्राज्य था। इसके अतिरिक्त यूरोप के शासक किसी भी प्रकार की संधि की शर्तों की परवाह नहीं करते थे। उनके अनुसार ईसाई धर्म के सिद्धांतों में भी कोई तथ्य न था।
उस समय के प्रमुख यूरोपीय राज्य निम्नलिखित थे- पवित्र रोमन साम्राज्य, फ्रांस, आस्ट्रिया, इटली, रूस, इंगलैंड, पोलैंड, स्वीडेन, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड इत्यादि ।
1 पवित्र रोमन साम्राज्य (Holy Roman Empire)
रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात् यूरोप में जो अराजकता फैली, उसी समय फ्रैंक जाति के लोगों ने यूरोप के कुछ भू-भागों पर अधिकार कर अपना राज्य स्थापित कर लिया। आठवीं शताब्दी के आरंभ में इस जाति ने प्रायः समस्त पश्चिमी यूरोप को अपने अधिकार में कर लिया। इस वश का सबसे महान् राजा शालेमा हुआ। उसने अपने राज्य की सीमा का बहुत विस्तार किया और रोम तक को अपनी राज्य में सम्मिलित किया। उस समय इटली के एक भू-भाग में लोम्बाई जाति के लोग पोप को बहुत परेशान किए हुए थे जिनसे बचने के लिए पोप ने शार्लमा को निमंत्रित किया। शालेमा ने पोप की बहुत सहायता की। इससे प्रसन्न होकर 25 दिसंबर, 800 को रोम के गिर्जे में पोप तृतीय लीओ (Leo) ने शार्लमां के मस्तक पर राजमुकुट रखकर उसका राम के सम्राट के पद पर अभिषेक कर दिया। सवा तीन सौ वर्षों के बाद पुनः पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई।
पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट वंशानुगत नहीं थे, बल्कि जर्मनी के सात बड़े राजा पवित्र रोमन सम्राट को चुनते थे। कई शताब्दियों से आस्ट्रिया का सम्राट ही पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट बनता चला आ रहा था किन्तु वह अब नाममात्र का सम्राट रह गया था। वेस्टफेलिया की सन्धि के बाद वह बिल्कुल कमजोर हो गया था और साम्राज्य के अनेक राज्य अपने को स्वतंत्र मानकर अपना कार्य करने लगे थे। सम्राट न तो अब कोई आज्ञा दे सकता था, न कोई नीति-निर्धारित कर सकता था और न कोई सेना रख सकता था। डाइट साम्राज्य के विभिन्न रियासतों के पारस्परिक संबंध को निर्धारित करती थी, लेकिन वह भी अब शक्तिहीन हो गई थी।
पवित्र रोमन साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण राज्य थे-आस्ट्रिया और प्रशा। ये दोनों राज्य यूरोप की राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेते थे और प्रभावशाली भी थे।
(अ) आस्ट्रिया- आस्ट्रिया का सम्राट पवित्र रोमन सम्राट भी हुआ करता था। वहाँ पर हैप्सबर्ग वंश का शासन था। आस्ट्रिया साम्राज्य यूरोप का एक विशाल साम्राज्य था, जिसमें आधुनिक चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बेल्जियम, इटली के कुछ भाग लोम्बार्डी और वेनिशिया इत्यादि थे, जिनमें अनेक जातियाँ निवास करती थीं। इन विभिन्न तत्वों को एक साथ मिलाए रखना आस्ट्रिया के सम्राट के लिए एक कठिन कार्य था। आस्ट्रिया साम्राज्य को सबसे बड़ी कमजोरी उस साम्राज्य के संगठन में ही सन्निहित थी, फलतः साम्राज्य में बराबर उपद्रव और बलवे होते रहते थे।
तीस वर्षीय युद्ध (1618-48) तक यूरोप की राजनीति में आस्ट्रिया का प्रमुख स्थान था, लेकिन वेस्टफेलिया को संधि से उसका पुराना गौरव समाप्त हो गया और उसका प्राधान्य जाता रहा । जर्मनी में अपनी वास्तविक सत्ता कायम करने में वह सफल नहीं हो सका। इस हालत में आस्ट्रिया के शासकों ने अब पर्व की ओर अपना प्रभाव बढ़ाने का निश्चय किया। सम्राट लियोपोल्ड ने तुर्की से ट्रांसिलवेनिया तथा हंगरी का एक बहुत बड़ा भू-भाग छीन लिया। उसके पश्चातु चार्ल्स छठे ने तुर्कों से हंगरी तथा बेलग्रेड के प्रदेशों को प्राप्त कर लिया। 1740 ई. में मेरिया थेरेसा आस्ट्रिया की सम्राज्ञी बनी। उसके समय में प्रशा ने आस्ट्रिया से साईलीशिया का प्रांत छीन लिया और बहुत प्रयल करने पर भी वह उस प्रांत को वापस नहीं जीत सकी। उसका उत्तराधिकारी द्वितीय जोजेफ (1765-90) था। वह एक योग्य शासक था और प्रजा की भलाई करना अपना कर्तव्य समझता था। उसने प्रजा की भलाई के लिए अनेकानेक कार्य किए। प्रशा के राजा से मिलकर उसने पोलैंड का विभाजन किया तथा पोलैंड के एक बहुत बड़े भाग पर आस्ट्रिया का अधिकार हो गया। फ्रांस में जब क्रांति हुई, उस समय वह आस्ट्रिया का सम्राट था।
(ब) प्रशा- जर्मनी में अनेक छोटी-छोटी रियासतें थीं; जिनमें हैनोवर, बवेरिया, सैक्सानी तथा प्रशा की प्रमुखता थी। लेकिन, इन सभी राज्यों में प्रशा शक्तिशाली और अन्य राज्यों का अगुआ (leader) था।
प्रशा पर लंबी अवधि तक होहेनजोलर्न वंश के शासकों ने शासन किया। फ्रेडरिक महान इस वश का एक शक्तिशाली शासक था, जिसने प्रशा को यूरोप का एक महान राज्य बनाया । फ्रेडरिक में सैनिक संगठन करने की अद्भुत क्षमता थी। अपने शासनकाल में इस प्रतापी शासक ने यूरोपीय शक्तियों से दो बार दीर्घकाल तक युद्ध किया। आस्ट्रिया ने हमेशा प्रशा का विरोध किया और इन दोनों युद्धों में वह प्रशा से विलग रहा। प्रथम युद्ध में फ्रांस तथा द्वितीय युद्ध में बिटेन ने प्रशा का साथ दिया। प्रथम युद्ध में फ्रांस की सहायता पाकर प्रशा ने आस्ट्रिया से साइलेशिया छीन लिया। कालांतर में आस्ट्रिया और रूस के सहयोग से प्रशा ने 1772 ई० में पोलैंड का विभाजन किया और उसके उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। इसकी प्राप्ति से प्रशा का पूर्वी भाग बैंडनबर्ग के राज्य से जा मिला।
इसके अलावा फ्रेडरिक महान ने अपनी प्रजा के कल्याण हेतु अनेक कार्य किए। यूरोप के राज्यों में प्रशा की प्रतिष्ठा बढ़ी और वह महान राज्यों में गिना जाने लगा। लेकिन, आस्ट्रिया ने सदैव अपने को प्रशा का नियंत्रक समझा, फलत: इन दोनों राज्यों में सदैव संघर्ष होता रहा।
(स) इटली- 18वीं शताब्दी में इटली जर्मनी की भाँति कई राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों का आपस में कोई संगठन नहीं था और न शासन-प्रणाली ही एक समान थी। यहाँ की राजनीतिक स्थिति छिन्न-भिन्न और अव्यवस्थित थी। अतएव, राजनीतिक दृष्टिकोण से इटली का कोई महत्व नहीं था। इसके अधिकांश क्षेत्र पर विदेशी प्रभाव स्थापित था। फ्रांस और आस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्य इटली की दुर्बलता से लाभ उठाकर उसके भू-भागों पर हमेशा अधिकार जमाने की चेष्टा किया करते थे। यहाँ के प्रमुख राज्य-पीडमौंट, बेनिस, लोम्बार्डी, नेपल्स और रोम थे। यहाँ के प्राय: सभी राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। अतएव, इटली यूरोप का एक पिछड़ा हुआ राज्य बना रहा था। कैथोलिक संप्रदाय का सर्वोच्च अधिकारी पोप रोम में निवास करता था। इटली तथा इटली के बाहर उसका धार्मिक प्रभाव था। वह अपने धार्मिक प्रभाव का इस्तेमाल कर यूरोपीय युद्धों में संलग्न हो गया। पोप की मौजूदगी इटली की उन्नति में काफी बाधक हुई।
(द) रूस- यद्यपि सीमा के दृष्टिकोण से यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस था, फिर भी वह यूरोप का सबसे पिछड़ा देश था। किन्तु, पोटर महान (1689-1725) के अथक प्रयास के फलस्वरूप रूस की काफी तरक्की हुई। उसके काल में पाश्चात्य सभ्यता का रूस में प्रवेश हुआ तथा वहाँ एक सुसंगठित एवं शक्तिशाली शासन-व्यवस्था की स्थापना हुई। वह रूस की सीमा बाल्टिक सागर तथा कालासागर तक विस्तार करना चाहता था। उसे इस कार्य में आंशिक सफलता भी मिली। उसके अधूरे कार्य को कैथरीन द्वितीय (1762-96) ने पूरा किया। उसने पीटर की नीति का अनुसरण कर रूस को एक शक्तिशाली राज्य का रूप दिया। तुर्की को पराजित् कर कैथरीन् द्वितीय ने रूस की सीमा का विस्तार भी कालासागर तक किया और पोलैंड के विभाजन में आस्ट्रिया और प्रशा का साथ दिया। इस विभाजन में रूस को पोलैंड का एक बहुत बड़ा भाग प्राप्त हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के समय रूस पर कैथरीन द्वितीय का शासन था।
(य) पोलैंड- पोलैंड मध्ययुग में यूरोप का एक महत्वपूर्ण राज्य था, लेकिन 17वीं शताब्दी में पोलैंड की स्थिति शोचनीय थी। शासन में अव्यवस्था होने के कारण पोलैण्ड निरंतर कमजोर होता जा रहा था। उसकी निर्बलता से लाभ उठाकर आस्ट्रिया, प्रशा और रूस तीनों ने मिलकर उसका विभाजन कर लिया। पोलैंड का इस प्रकार तीन बार (1772, 1793 और 1795 ई०) विभाजन हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के समय में पोलैंड का राजनीतिक अस्तित्व अवसान के कगार पर था।
(र) इंगलैंड- 1789 ई० को फ्रांस की क्रांति के समय इंगलैंड में पार्लियामेंट की शक्ति की स्थापना हो चुकी थी। जन-सहयोग के कारण इंगलैंड की सरकार कठिन-से-कठिन समस्या का समाधान आसानी से कर सकती थी। फ्रांस के साथ इंगलैंड का पुराना विरोध था और इस कारण दोनों के बीच उपनिवेश-स्थापना के क्रम में कई भी हुए। महाद्वीपीय शक्ति होने के कारण फ्रांस मुख्यतः महाद्वीप की राजनीति में ही उलझा रहा। इससे लाभ उठाकर इंगलैंड ने उसके साम्राज्य का बहुत बड़ा भाग छीन लिया। लेकिन, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में पराजय इंगलैंड की प्रतिष्ठा के लिए काफी घातक सिद्ध हुई। जार्ज तृतीय के शासनकाल में इंगलैंड की राजनीतिक व्यवस्था पतनोन्मुख थी और शासनतंत्र में तनाव बना हुआ था, लेकिन छोटे पिट के प्रधानमंत्री बनने से इंगलैंड संकट से अपने को बचाने में और नेपोलियन के युद्धों से बचने के लिए सक्षम भी हो सका।
(ल) यूरोप के अन्य राज्य- क्रांति के समय यूरोप के अन्य राज्य स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क, स्वेडेन तथा स्विट्जरलैंड थे। 16वीं शताब्दी तक स्पेन यूरोप का एक महान देश बना रहा, लेकिन 17वीं शताब्दी में उसका निरंतर पत्न होता रहा । फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक चार्ल्स चतुर्थ था। डेनमार्क तथा नार्वे में उस समय क्रिश्चियन सप्तम और स्वीडेन में गस्तवेश तृतीय का शासन था। ये दोनों राजा निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी थे। संपूर्ण यूरोप में स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश था जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी। लेकिन, यूरोपीय देशों में स्विट्जरलैंड की कोई पूछ नहीं थी।
-
क्रांति के समय यूरोप का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन
(Political, Social, Economic, Religious, and Cultural Life of Europe at the Time of the French Revolution)
(क) राजनीतिक जीवन-
फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था सामंती व्यवस्था पर आधुत थी। सामंती व्यवस्था वस्तुतः कोई व्यवस्था न होकर एक असंगठित व्यवस्था थी और रोमन साम्राज्य के पतन के उपरांत उसका उद्भव और विकास हुआ था। इस व्यवस्था के दो पक्ष थे-राजनीतिक और सामाजिक ।
राजनीतिक मामले में सामंतवाद का मूल सिद्धांत शासन का विकेंद्रीकरण था, जबकि सामाजिक मामले में असमानता थी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक इस व्यवस्था ने विकृत रूप धारण कर लिया था। प्रारंभ में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, लेकिन उनके साथ उन्हें कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता था। बाद में सामंतों के विशेषाधिकार तो यथावत् बने रहे, लेकिन वे अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। फलत: जनता का शोषण करना ही सामंती व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य हो गया।
इस काल में यूरोप में इंगलैंड को छोड़कर पूरे यूरोप में निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन व्याप्त था। इस स्वेच्छाचारी शासन का मुख्य आधार मुट्ठी भर सामंत होते थे। जनता का कल्याण न् तो राजा सोचता था और न उसके सामंत । शासन के मुख्य सिद्धांत, स्वेच्छाचारिता और शोषण था। राजा अपना मुख्य पेशा राज्य विस्तार और स्वार्थसाधन मानते थे। वे दूसरों के अधिकारों तथा दिए हुए वचनों की कोई परवाह नहीं करते थे। विश्वासघात और वचनभंग इनकी कूटनीति की कसौटी थी और सबल राष्ट्र निर्बल राष्ट्र को हड़पने में किसी तरह के संकोच का अनुभव नहीं करते थे।
इस काल में शक्ति संतुलन का सिद्धांत (balance of power) कूटनीति का आधार बना। नए देशों की खोज, उपनिवेशों की स्थापना, भौगोलिक ज्ञान का विकास, नवीन व्यापारिक मार्गों का निर्माण एवं खोज, सभ्यताओं के बीच संघर्ष आदि का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। 18वीं शताब्दी में राजनीति का क्षेत्र केवल यूरोप की समस्याओं तक ही सीमित नहीं रहा, वरन् विश्वव्यापी बना। यदि यूरोप में युद्ध के बादल उठते तो उसका प्रभाव एशिया अथवा अमेरिका पर भी अनिवार्य रूप से पड़ता था। उसी प्रकार यूरोप की समस्त घटनाओं एवं विचारधाराओं का प्रभाव संसार के प्रत्येक देश पर पड़ने लगा।
फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व यूरोपीय देशों में साम्राज्य विस्तार के लिए प्रतिस्पर्धी लगी हुई थी। साम्राज्यवादियों ने व्यापार और वाणिज्य के नाम पर एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना आरंभ किया। इस प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अधिक सफल रहे, फिर भी अन्य यूरोपीय राज्य, अर्थात् स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, बेल्जियम आदि देशों ने अपना साम्राज्य अफ्रीकी और एशिया में कायम किया। इस साम्राज्य-विस्तार के दौरान धर्म को भी हथकंडा बनाया गया और ईसाई पादरी इन अविकसित देशों के लोगों को ईसाई बनाने लगे। कभी-कभी तो यह भी कहा गया कि श्वेत लोगों का कर्तव्य है कि वे अश्वेतों को सभ्य बनाएँ और इस तरह साम्राज्यवाद् को उचित ठहराया गया। इस प्रकार यूरोपीय संस्कृति का विस्तार साम्राज्यवादी विस्तार के साथ हुआ।
(ख) सामाजिक जीवन-
यूरोप का समाज दो भागों में विभक्त था-श्रीमानों (haves) और श्रीहीनों (have nosy | श्रीमानवर्ग को सुविधाप्राप्त वर्ग एवं श्रीहीनों को सुविधाहीन वर्ग भी कहा जाता है। सुविधाप्राप्त वर्ग में कुलीन और पादरी थे, जिन्हें कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध थीं और जिन्हें राज्य को कर नहीं देना पड़ता था।
कुलीन- 18वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज में कुलीनवर्ग का विशेष स्थान था। राजा तथा राजपरिवार के व्यक्तियों के बाद समाज में उनका स्थान सर्वोच्च था। राज्य के उच्च पदों पर इसी वर्ग के लोगों को नियुक्त किया जाता था। राजा लोग स्वेच्छा से कुलीनवर्ग के किसी भी व्यक्ति को कोई भी पद प्रदान कर सकते थे, भले ही वह कुलीन उस पद के योग्य न हो। यूरोप की सारी भूमि जागीरों में विभक्त थी और जागीरों के स्वामी कुलीनवर्ग के लोग ही होते थे। उन्हें पुराने सारे सामंती अधिकार अब भी प्राप्त थे। प्रत्येक देश में कुलीनवर्ग राजकरों एवं दायित्वों से मुदत् था। जनसाधारण और मध्यवर्ग के लोग उनसे आतंकित रहते थे। कुलीनवर्ग में दो तरह के कुलीन होते थे-उच्च कुलीन और निम्न कुलीन। उच्च कुलीन बड़े-बड़े शहरों में रहते थे और ऐशो-आराम का जीवन व्यतीत करते थे, जबकि निम्नवर्गीय कुलीन साधारण जनता के साथ गांवों में रहते थे। इनका जीवन आम जनता से अधिक खुशहाल नहीं था। फिर भी ये कम अत्याचारी नहीं थे।
कुलीनों की तरह पादरी भी दो वर्गों में विभक्त थे-उच्च पादरी और निम्न पादरी। उच्च पादरी उच्च कुलीनों के पुत्र थे। वे शहरों में ऐशो-आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे और धार्मिक जीवन से कोसों दूर थे, जबकि साधारण पादरी आम जनता के साथ गांवों में रहते थे और उनका जीवन आम जनता से मिलता-जुलता था। इसलिए ये निम्नवर्ग के पादरी उच्चवर्गीय पादरियों से घृणा करते थे।
श्रीहीन या सुविधाहीन वर्ग में थे किसान, मध्यमवर्ग (जिसमें व्यापारी, वकील, प्राध्यापक इत्यादि) और मजदर। इस काल में यूरोप में अधिकतर जनसंख्या कृषकों को थी। कृषकवर्ग भी दो प्रकार का था-स्वतंत्र तथा अर्द्धदास (serf) । पूर्व यूरोप तथा मध्य यूरोप में अधिकांश कृषक अब भी अर्द्धदास की अवस्था में थे। उनकी दशा पशुओं से भी हीन थी।ये अर्द्धदास अपनी जागीरदार की जमीन पर खेती करते थे। फ्रांस में भी कृषक करों के भार से लदे थे, जहाँ अर्द्धदास-व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। कृषकों को राजा को, सामंतों को तथा चर्च को कर देना पड़ता था और इन करों को देने के बाद किसानों की किसी तरह जीवन निर्वाह करने लायक धन बचता था। किसानों को बेगारी करनी पड़ती थी और कुलीनों द्वारा ढाए गए उत्पीड़न को सहन करना पड़ता था।
यूरोपीय समाज में एक मध्यमवर्ग था। इस वर्ग के अधिकतर लोग नगरों में रहते थे और इसके अंतर्गत समृद्ध व्यापारीवर्ग तथा वकील, सरकारी नौकर और अध्यापक लोग थे। यद्यपि इस वर्ग की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, किंतु कुलीनों के समान इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। तत्कालीन क्रांतिकारी भावना से मध्यमवर्ग काफी प्रभावित था। फ्रांस में इस वर्ग की संख्या अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा अधिक थी और ये क्रांति का नेतृत्व करने को तैयार थे।
यूरोप के नगरों में एक वर्ग शिल्पियों और कारीगरों का था। ये कारीगर लोग अपनी कारीगरी के अनुसार श्रेणियों में बंटे हुए थे। ये श्रेणियाँ अपने-अपने नियम बनाती थीं। यहाँ तक कि ये बनाए हुए माल का विक्रय-मूल्य भी निर्धारित कर देती थीं। इसके फलस्वरूप व्यापार और उद्योग-धंधों में प्रतिस्पर्दा नहीं होती थी, लेकिन श्रेणी-पद्धति के कुछ अवगुण भी थे। इस नियंत्रण के कारण कारीगरों को स्वतंत्रता नहीं थी। वे अपने इच्छानुसार व्यवसाय नहीं कर सकते थे। औद्योगिक क्रांति होने से पूँजीपति बड़े-बड़े कारखाने स्थापित करने लगे, जिसमें कम समय और कुम खर्च में अधिक सामान् उत्पादित होने लगा। परिणामस्वरूप, श्रेणी-पद्धति टूटने लगी और ये कामगार कारखानों में काम करने लगे जहाँ उनकी स्थिति और बिगड़ी।
(ग) आर्थिक जीवन-
यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति (इंगलैंड को छोड़कर) फ्रांस की क्रांति के समय अच्छी नहीं थी। पूरे फ्रांस का राजनीतिक जीवन सामंतवादी व्यवस्था पर आधृत था और ये सामंत भोग-विलास में लगे हुए थे, फलतः राजा को सामंतों के द्वारा उगाहे गए कर पूर्णरूपेण नहीं मिल पाते थे। इतना ही नहीं, सामंती अत्याचार के कारण कृषक और व्यापारी त्रस्त थे। ये सामंत आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसके कारण अमन-चैन ठीक नहीं रह पाता था। ये सामंत व्यापारियों से अनेक तरह के कर भी उगाहते थे, फलत: व्यापारीवर्ग दुखी था। औद्योगिक क्रांति के कारण मध्यमवर्ग के लोग कारखाने स्थापित करने लगे, जिससे कृषकवर्ग के लोगों की आर्थिक अवनति हुई और ये अब कारखानों के मजदूर के रूप में परिणत हो गए जहाँ उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वहाँ के लोगों में तत्कालीन आर्थिक अवस्था के विरुद्ध असंतोष था।
(घ) धार्मिक जीवन-
तत्कालीन यूरोप में ईसाई, यहूदी और मुस्लिम रहते थे। लेकिन, ईसाईधर्म का ही बोलबाला था। तुर्क लोग इस्लामधर्म के अनुयायी थे, जबकि यहूदियों का कोई अपना देश नहीं था, बल्कि ये पूरे देश में फैले हुए थे। ईसाई-धर्म भी तीन संप्रदायों में विभक्त था-(क) रोमन कैथोलिक, (ख) पीक ऑर्थोडॉक्स, (ग) प्रोटेस्टेंट। इन संप्रदायों के धर्मावलंबियों में अक्सरहाँ कटुता रहती थी। रूस और पूर्व के यूरोपीय देश् ग्रीक ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय के अनुयायी थे, जबकि फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली आयरलैंड, पोलैंड इत्यादि देशों के लोग रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। इंगलैंड, जर्मनी और हॉलैंड के लोग प्रोटेस्टेंटधर्म के माननेवाले थे।
पूरे यूरोप में अब भी धर्म का बोलबाला था। यह ठीक है कि शासक अपने स्वार्थी मनसूबों को पूरा करने के लिए धर्म का सहारा लिया करते थे, फिर भी आम जनता धार्मिक कुंठाओं से मुक्त नहीं हो पाई थी। पोप इटली में रहता था और उसका एकमात्र स्वार्थ यूरोपीय राजाओं को धर्म के भय से भयभीत रखकर अपने स्वार्थ को सर्वोपरि बनाए रखना था। पोप के कारण ही इटली में राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो पाया और यह अनेक यूरोपीय संघर्षों में उलझा। फ्रांस की कैथोलिक जनता भी पोप की प्रबल समर्थक थी। हॉलैंड, जर्मनी और इंगलैंड के लोग प्रोटेस्टेंट थे और ये अपने राजाओं के आदेश पर कभी भी किसी कैथोलिक राजा से उलझने को तैयार रहते थे। पुर्तगाल और स्पेन के लोग भी कैथोलिक ही थे। कैथोलिक जनता अपने कैथोलिक राजा से भी पोप के इशारे पर उलझने को तैयार बैठी थी। इस प्रकार हम पाते हैं कि यूरोपीय देश अभी धार्मिक ग्रंथियों से ऊंचे नहीं उठ पाए थे।
(ड.) सांस्कृतिक जीवन-
18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में शिक्षण-संस्थाओं का प्रसार हो चुका था, लेकिन कैथोलिक देशों में ये शिक्षण-संस्थाएँ चर्च के अधीन थीं। ऐसी अवस्था में यह संभव नहीं था कि शिक्षणालय बुद्धि-स्वातंत्र्य के केंद्र बन सकें। इस समय के अधिकांश विद्यालयों का वातावरण संकुचित था। उनमें कुलीनों की संतानें ही शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। साधारण जनता शिक्षा के प्रसार से अछूती थी। शिक्षा में धर्म का प्रभाव था। कुलीन चित्रकला, मूर्तिकला तथा अन्य कलात्मक कार्यों के पोषक थे, अतः इस काल में सांस्कृतिक जीवन का काफी विकास हुआ।
इतिहास – महत्वपूर्ण लिंक
- फ्रांस की पुरातन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं | Main features of the archaic system of France in Hindi
- फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति के कारण | 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारण
- फ्रांसीसी क्रांति के लाने में दार्शनिकों की भूमिका | फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के योगदान
- फ्रांसीसी क्रान्ति का महत्व | क्रांति फ्रांस में क्यों हुई | फ्रांसीसी क्रान्ति के कारण | Importance of French Revolution in Hindi
- फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियाँ | Achievements of the French Revolution in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]