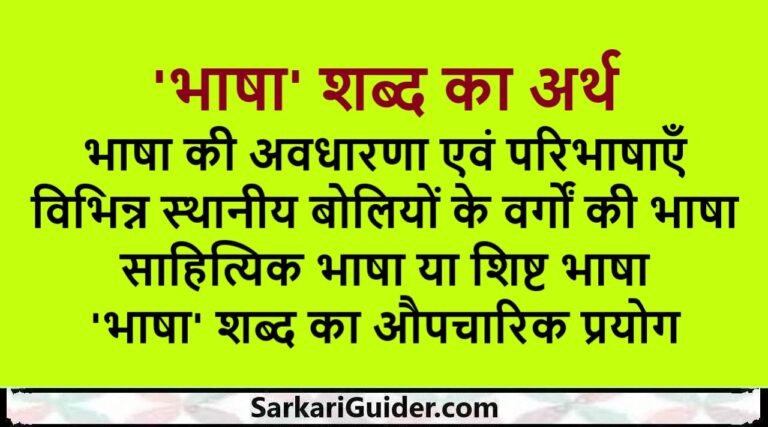प्रतीकों का महत्व बताइए | प्रतीक-विधान | विराम-चिन्ह
प्रतीकों का महत्व बताइए | प्रतीक-विधान | विराम-चिन्ह
प्रतीकों का महत्व
प्रतीकों का क्षेत्र जितना व्यापक और विशाल है उतना ही उनका महत्त्व भी व्यापक है। प्रतीकों का प्रसार भाषा, साहित्य, कला, धर्म, दर्शन और जहाँ तक मानव की नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियां पहुंच सकती हैं, वहाँ तक है। यदि भाषा की उत्पत्ति का इतिहास देखा जाये तो ज्ञात होता है कि भाषा का आदि रूप प्रतीकात्मक था। उस समय मनुष्य प्रतीकों के माध्यम से ही अपने भावों को व्यक्त किया करते थे। आध्यात्मिक एवं साहित्यिक क्षेत्रों में तो प्रतीकों का महत्त्व स्पष्ट नहीं है। आध्यात्मिकता के विवेचकों ने अव्यक्त एवं परम रहस्यमय अगोचर ब्रह्म को तथा उसके साथ तदाकार के परम अनन्यातिरेक को प्रतीकों के द्वारा ही व्यक्त किया है। रहस्यमयी भावनाओं का आधिक्य होने के कारण ही छायावादी काव्यों में प्रतीकों की प्रधानता है।
काव्य में प्रतीकों का प्रयोग केवल दो कारणों से किया जाता है। भावाभिव्यक्ति को सशक्त बनाने हेतु और सौन्दर्य विधान के लिए। काव्य की भाषा साधारण भाव से भिन्न होती है। काव्य में साधारण बात को भी कवि को इस प्रकार कहना पड़ता है कि वह हृदय सम्बन्ध हो सके और . पाठक या श्रोता के मन को गुदगुदा सके। कवि की भाषा को यह शक्ति प्रतीकों से प्राप्त होती है।
‘बाल रजनी सी झलक थी डालती,
भ्रमित हो शशि के बदन के बीच में।’
प्रतीक-विधान
प्रतीक शब्द का सामान्य अर्थ है अवयव, अंग, पता, चिन्ह, निशान और कभी-कभी संकेत भी होता है। किन्तु साहित्य में अथवा काव्य में इसका प्रयोग कुछ विशिष्ट अर्थ में होता है। इस विशिष्ट अर्थ को आधार मानकर हिन्दी के अनेक विद्वानों ने ‘प्रतीक’ शब्द की परिभाषा दी है-
(1) डॉ0 राजाराम रस्तोगी के अनुसार, ‘प्रतीक का अर्थ होता है-प्रतिरूप या प्रतिभा अथवा वह वस्तु या भाव जो अंश होकर भी समय के लिए व्यवहृत हो।’
(2) डॉ० सुधीन्द्र के अनुसार, ‘वस्तुतः अप्रस्तुत की समस्त आत्मा, धर्म या गुण का समन्वित रूप लेकर आने वाले का नाम है। प्रतीक अप्रस्तुत रूप में अवतार ही है।’
उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतीक किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करनेवाला होता है। यह अर्थ परम्परागत होता है अर्थात् प्रतीक में जो अर्थ होता है, वह देश के वातावरणीय सांस्कृतिक प्रभाव के कारण होता है। ‘प्रतीक’ की परिभाषा से स्पष्ट है कि इसमें सांकेतिक अर्थ निहित होता है। इसलिए यहाँ पर सहज ही शंका उत्पन्न हो जाती है कि फिर प्रतीक और संकेत में क्या अन्तर है? इसके अन्तर को स्पष्ट करने के लिए संकेत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक है।
विराम-चिन्ह
‘विराम’ से तात्पर्य है- ‘ठहरना’ या ‘रुकना’ और ‘चिह्न’ का आशय है-‘निशान’ । अर्थात् वह निशान, जिससे वर्तनी या आलेखन में ठहरने या रुकने का संकेत मिले, उसे ‘विराम-चिह्न’ कहते हैं।
भाषा ज्ञान के लिए विराम-चिन्हों का जानना अनिवार्य है।
हिन्दी में निम्नलिखित विराम-चिह्न प्रयुक्त होते हैं-
(1) पूर्ण विराम (Full stop) ।
(2) अर्ध विराम (Semicolon) ;
(3) अल्प विराम (Comma) ,
(4) प्रश्नसूचक चिह्न (Sign of Interrogation) !
(5) विस्मयादिबोधक चिह्न या संबोधन-चिह्न (Sign of Exclamation) –
(6) योजक चिह्न (llyphen) –
(7) निर्देशक (Dash) –
(8) (i) विवरण-चिह्न (Colon) :
(ii) विवरण चिन्ह (Colon and Dash) :-
(9) कोष्ठक (Brackets) | | { } ( )
(10) उद्धरण-चिह्न (Inverted commas) ‘ ‘
हिन्दी – महत्वपूर्ण लिंक
- काव्यभाषा का स्वरूप | काव्यभाषा एवं सामान्य भाषा में अन्तर
- काव्य में बिम्ब-विधान | काव्य बिम्ब का कार्य या उद्देश्य | बिम्ब के गुण एवं तत्व | बिम्बों का वर्गीकरण
- प्राचीन भारतीय आर्य भाषा | वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में साम्य एवं वैषम्य | वैदिक और लौकिक संस्कृत में अन्तर
- पालि भाषा की व्युत्पत्ति | पालिभाषा का प्रदेश | पालि-साहित्य | पालि की विशेषताएं
- परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ठ | अवहट्ठ की विशेषताएं | अवहट्ट भाषा की भाषिक विशेषताएँ | अवहट्ट भाषा की व्याकरणिक विशेषताएँ
- राष्ट्रभाषा हिन्दी की समस्याएँ | राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का भविष्य
- प्रतीक का उद्भव एंव विकास | प्रतीक का अर्थ | प्रतीकों का वर्गीकरण | प्रतीक योजना का आधार | काव्य में प्रतीकों का महत्व
- महाराष्ट्री प्राकृत | महाराष्ट्री प्राकृत की विशेषताएं
- राजभाषा एव राष्ट्रभाषा | संचार भाषा | सम्पर्क भाषा
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]