विद्यापति के पद्यांशों की संसदर्भ व्याख्या | विद्यापत के निम्नलिखित पद्यांशों की संसदर्भ व्याख्या

विद्यापति के पद्यांशों की संसदर्भ व्याख्या | विद्यापति के निम्नलिखित पद्यांशों की संसदर्भ व्याख्या
विद्यापति के पद्यांशों की संसदर्भ व्याख्या
- माधव, बहुत मिनति कर तोय!
दए तुलसी तिल देह समर्पित, दया जनि छाड़बि मोय ।।
गनइत दोसर गुन लेस न पाओबि, जब तुहुं करबि विचार।
तुहू जगत जगनाथ कहाअओसि, जग बाहिर नइ छार।।
किए मानुस पखि भए जनमिए, अथवा कीट पतङ्ग।
करम बिपाक गतागत पुनु पुनु, मति रह तुअ परसङ्ग।।
सन्दर्भ- प्रस्तुत पद्य अंश ‘विद्यापति संग्रह’ से उद्धृत है जिसके रचनाकार मैथिली कोकिल कवि विद्यापति जी हैं।
प्रसंग- यह पद हिन्दी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि विद्यापति की ‘पदावली’ से उद्धृत है। शिव भी भिक्षा मांगकर निर्वाह करते हैं। इससे लज्जित होकर उनकी पत्नी पार्वती उनसे आग्रह करती हुई कहती हैं-
व्याख्या- हे शिव जी! मैंने तुमसे बार बार कहा है कि तुम भिक्षा माँगने मत जाओ, फिर भी तुम अपनी मनमानी करते हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि बिना किये भीख मांगने से गुण और गौरव नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि भिखारी में न कोई गुण समझा जाता है और न कोई उसका आदर करता है। भीख मांगने वाले को सभी लोग निर्धन समझते हैं और निर्धन कहकर उसका उपहास करते हैं। न कोई भिखारी का सम्मान करता है और न कोई उस पर कृपा करता है। तुम्हारे भीख मांगने के कारण ही लोग तुम पर अकौए और धतूरे के फूल चढ़ाते हैं और विष्णु पर चंपा के फूल चढ़ाये जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि तुम भीख मांगने के कारण आक धतूरे के फूल प्राप्त करते हो और विष्णु चम्पा के फूल प्राप्त करते हैं। इसी से मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि तुम खेती का काम करने लगो। तुम्हारे पास खेती करने के सभी साधन हैं। तुम अपना पीठासन अर्थात् एक बगल में सहारे के लिए लगायी जाने वाली लकड़ी के आधार को काटकर हल बना लो। अपने लोहे के बने त्रिशूल को तोड़कर भाला बना लो। तुम्हारा नन्दी नाम का बैल बड़ा शक्तिशाली है। उसे लेकर हल जोतिए और गंगा की जल धारा से खेतों की सिंचाई कीजिए। विद्यापति कहते हैं कि पार्वती जी बोली – हे महादेवी! तुम मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हारी सेवा इसी कारण से की है कि तुम सम्मान का जीवन व्यतीत करोगे। खेती के इस कार्य से जो भी प्राप्ति होगी, वही ठीक है। हे महादेव ! तुम भीख मांगने उधर मत जाओ।
विशेष- (i) अलंकार – बेरि-बोलों, गुन-गौरव, निरधन-नहि, फुल-पाओल, पाओल-फुल, काटि- करु, त्रिसुल-तोड़िय, सुरसरि-सुनहु-सेवा, जे-जाएब-जनि में अनुप्रास, बेरि-बेरि में पुनरुक्तिप्रकाश, बिन सक रहह में विनोक्ति, हर-हर में और बर-बर में यमक अलंकार है। निरधन-जन में ध्वनिसाम्य है। (ii) शिव जी भीख मांगते हैं, यह मान्यता मिथिला या बंगाल में हो सकती है, हिन्दी भाषी प्रदेश में नहीं है। (iii) भाषा मैथिली है, जिसमें संस्कृत और खड़ी बोली के भी पर्याप्त शब्द हैं।
- देख देख राधा रूप अपार।
अपरूप के विहि आसि मिलाओल खिति तल लावनि सार।।
अंगहि अंग अनंग मुरछायत, हेइए पड़ए अधीर।
मनमथ कोटि मथन करु जे जन, से हेरि महि मधि-गीर।।
कत कत लखिमी चरण तल ने ओछए रंगिनि हेरि विभीरि।
करु अभिलाख मनहिं पदपंकज, अहोनिसि कोर अगोरि।।
संदर्भ- प्रस्तुत पद्यांश में ‘विद्यापति संग्रह’ से लिया गया है जिसकी रचना मैथिल कोकिल विद्यापतिजी ने की है।
प्रसंग- प्रस्तुत पद्यांश में कविवर विद्यापति द्वारा राधा रंग रूप का बहुत ही सुन्दर ढंग से वर्णन किया गया है।
व्याख्या- राधा की अपार सुन्दरता का बहुत ही मार्मिक ढंग से औलोकित किया गया है विष्णु जी ने इस संसार में किस प्रकार से धरती पर सौन्दर्य का वर्णन किया है। राधा की अपार सुन्दरता को देखकर कामदेव (जो सौन्दर्य के देवता माने जाते है। उनका भी मन राधा के रूप को देखकर विचलित हो जाता है। उसकी चंचल चितवन को देखकर समस्त देवी-देवताओं के सौन्दर्य को भी पीछे छोड़ देती है तथा मुरली धर स्वयं राधा के अपूर्व सौन्दर्य को देखकर आश्चर्य करने लगते थे। राधा जी को निहारकर सभी देवी लक्ष्मी उनके चरण कमलों में समर्पित रहना चाहती है। और पता नहीं कितनी अप्सराएँ उनके सौन्दर्य को देखकर बेहोश हो जाती है और उन सभी के मन में यह कामना हो जाती है। कि इस कमल के समान पैरो को अपनी गोद में रखकर रात-दिन हर प्रहर उसकी रक्षा किया करें।
विशेष- राधा के अपूर्व सौन्दर्य का अंकन किया गया है।
- सुन रसिया, अब न बजाऊ विपिन बंसिया।
बार-बार चरनार बिन्द गहि सदा रहव बन दसिया।।
कि छलहुँ कि होएब के जाने बृथा होएत कुल हँसिया।
अनुभव ऐसन मदन-भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया।।
नंद नन्दन तुअ सरन न त्यागब, वरु जग होए दुरजसिया॥
विद्यापति कह सुनु बनितामनि, तोर मुख जीतल ससिया।
धन धन्य तोर भाग गोआरिनि, हरिभजु हृदय हुलसिया।।
सन्दर्भ- पूर्ववत्।
प्रसंग- मुरलीघर बाँसुरी बजा रहे है। और राधा उनके बाँसुरी की मधुर आवाज पर मन्त्रमुग्ध है। और कान्हा से विनती करती हैं कि हे नन्दलाल तुम बाँसुरी मत बजाया करों मै सदा के लिए तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहूंगी।
व्याख्या- हे नटखट कान्हा ! मेरी बात सुनो, अब तुम द्वारिका में बाँसुरी मत बजाया करो मैं बारम्बार तुम्हारे चरणों को पकड़कर विनती करती हूँ कि सदा के लिए तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहूंगी समस्त संसार इस बात को अच्छे से जानता है। कि मैं आज कैसी हूँ तब मै पहले कैसी थी। जो तुम इस तरह से बार-बार मुझे पुकारते हो इससे- अनायाश ही मेरे वंश की तौहीन होती है मुझे कुछ ऐसा जान पड़ता है। कि मानो कामदेव रूपी सर्प ने मुझे उस लिया है। हे नन्दलाल! हे मुरलीघर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोडूंगी चाहे पूरे संसार में बुराई फैल जाय।
अपरूप कवि विद्यापति जी कहते है कि नारीयों में श्रेष्ठ जिसके सिर पर मणि हो चन्द्रमा के कमान मुख वाला होक। गाय चराने वाली माता। तू बहुत किस्मत वाली है। तुम प्रसन्न चित होकर मुरलीघर को याद करोगी तो वे तेरी सभी मनोकामना को पूर्ण कर देगें।
- भलहर भलहरि भल टुआ, खन पित बसन खनहिं बघछला।
खन पंचानन खन भुज चारि, खन संकट खन देव मुरारि।
खन गोकुल भए चराइअ गाय, खन भिखि माँगिए डमरू बजाय।
खनगोविन्द भए लिअ महादान, खनहि भसम भरू काँख वो कान।
एक सरीर लेल दुइ वास खन बैकुंठ खनहिं कैलास।
भनइ विद्यापति विपरित बानि, ओ नारायण ओ सूलपानि।
संदर्भ- पूर्ववत्
व्याख्या- प्रस्तुत छंद में शिव की स्तुति करता हुआ कवि कहता है कि हे शिव! तुम अच्छे हो। हे विष्णु (हरि)! तुम भी अच्छे हो, और तुम्हारी कला भी उत्तम है। एक क्षण में ही तुम पीताम्बरधारी बनते हो और दूसरे क्षण में ही व्याघ्र चर्म को धारण करने वाले बनते हो। क्षण में पाँच मुखों वाले और क्षण में चार भुजाओं वाला बन जाते हो। पल में कृष्ण बनकर गोकुल में गायें चराने लगते हो और पल में ही शिव के रूप में डमरू बजाकर भिक्षा मांगने लगते हो। क्षण में ही गोविन्द (कृष्ण) बनकर गोपियों से महावदान की याचना करते हो और क्षण में ही बंगलों और कानों में भस्म लगाने लगते हो। तुम्हारा शरीर तो एक है लेकिन उसका निवास दो स्थानों पर है। एक क्षण में यदि वह वैकुण्ठ में दिखाई देता है तो दूसरे क्षण में कैलाश पर्वत पर। कवि विद्यापति विपरीत बात कहते हैं कि एक नारायण हैं तो दूसरा त्रिशूल को धारण करने वाला महादेव है।
विशेष- यदि इस पद के आधार पर विद्यापति की भक्ति के स्वरूप पर विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि वे शिव और विष्णु में कोई ताश्चिक भेद नहीं मानते।
अलंकार- शिव के अनेक गुणों का वर्णन होने से उल्लेख अलंकार।
- खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन बसन धूलि तनु भरई।
खने खन दसन-छटा छट हास, खने खन अधर आगे गहु बास।
चउँकि चलए खने खन चलु मन्द, मनमथ पाठ पहिल अनुबन्ध।
हिरदय-मुकुल हेरि-हेरि थोर, खने आँचर दय खने होए भोर।
बाला शैशव-तारुन भेंट, लखाए न पारिअ, जेठ-कनेठ।
विद्यापति कह सुनु बर कान, तरुर्निभ शैशव चिन्हइ न जान।।
सन्दर्भ- पूर्ववत् ।
प्रसंग- वय: सन्धि की अवस्था में, नायिका में शारीरिक और मानसिक द्विविध प्रकार प्रतिवर्तन देखे जाते हैं। यहाँ नायिका की ऐसी दुहेली स्थितियों की ओर संकेत किया गया है।
व्याख्या- वयः सन्धि की अवस्था में पहुँचकर नायिका के नेत्र क्षण-क्षण में कटाक्षपात करने लग गये हैं। कभी अपनी शैशव सुलभ असावधानी से उसका वस जमीन पर धूल में गिर जाता है। फिर जबज्ञवह उसे उठाकर अपने वक्षस्थल पर रखती है तो उसका तन धूलि-धूसरित हो जाता है। क्षण-क्षण में उसके दाँतो की छटा उसकी हंसी के साथ बिखर जाती है और क्षण-क्षण में वह ओठों के आगे वस्त्र करके उसे छिपाने का प्रयास करती है। कभी चौंककर तीव्र गति से चल पड़ती है और कभी धीरे चलने लगती है। नायिका को ऐसी क्रियायें तो उसमें काम प्रवेश की भूमिका मात्र का द्योतन करती है। किन्हीं क्षणों में वह अपने वक्षोजों का किंचितमात्र अवलोकन करती है और किन्हीं क्षणों में वह उन्हें अपने आंचल से आवृत कर देती है। क्षण मात्र में कभी वह आनन्द विभोर हो उठती है। उस बाला में शैशव एवं तारुण्य का ऐसा सम्मिलन हो गया है कि उनमें किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं कहा जा सकता है। अभिप्राय यह कि दोनों ही अवस्थाएँ एक दूसरे पर अधिकार जताने का प्रयास कर रही हैं। इसीलिए उसमें कभी शैशव के भावों को देखा जाता है और कभी तारुण्य के भावों को। विद्यापति कहते हैं कि हे कान्ह ! सुनों, उस नायिका के शरीर में शैशव एवं तारुण्य का ऐसा मेल हो गया है कि वे परिचाने नहीं जाते।
विशेष- (i) ‘खन-खने नयन कोन अनुसरई’ में अनुप्रास अलंकार। (ii) हिरदय-मुकुल में रूपक अलंकार। (iii) तरुनिम सैसभ चिन्हए न जान में मीलिह अलंकार।(iv) समस्त छन्द में स्वाभावोक्ति अलंकार। (v) नायिका नव यौवनागम से अंकुरित यौवना मुग्धा है। (vi) कवि ने मुग्धा अज्ञात यौवना नायिका की मानसिक उथल-पुथल का चित्रण कर अपनी प्रकृति मनोवैज्ञानिकता का परिचय दिया है। .
- जुगुल सैल सिम, हिमकर देखल, एक कमल-दुहु जोति रे।
फुललि मधुरि फुल, सिंदुर लोटाएल, पांति बसइलि गज मोति रे।
आज देखल जति, के पतिआएत, अपुरूब बिहि निरमान रे।
बिपरित कवक, कदलि तर शोभित, थल पंकज के रूप रे।
तथहु मनोहर, बाजन बाजए, जनि जागे मनसिज भूप रे।
भनइ विद्यापति, पुरुब पुन तह, ऐसनि भजए रसमन्त रे।
बुझल सकल रस, नृप सिबसिंघ, लखिमा देइ कर कन्त रे।
सन्दर्भ- पूर्ववत् ।
प्रसंग- नायिका की सखी अथवा दूती नायिका के सौन्दर्य का वर्णन कर नायक को उसके प्रति अनुरागी बनाने का प्रयास करती है।
व्याख्या- हमने दो पर्वतों की सीमा (मध्य) में चन्द्रमा का दर्शन किया, अभिप्राय यह कि दोनों उतुंग कूचों के सन्धिस्थल के ऊपर मुख (चन्द्र) को उदय होते देखा। उसी स्थान पर कमल रूप मुख में प्रकाश-बिन्दु रूप नेत्र दिखाई दिये। पुष्पित मधुरी का फूल सिन्दूर में लोट रहा था अर्थात् अरुणिमा संयुक्त उसके भाल में सिन्दूर की लाल बिन्दी लगी हुई थी। यही नहीं, उसमें गजमोतियों की पंक्ति बैठी हुई थी, अभिप्राय यह कि दांतों की पंक्ति-बद्ध छवि पंकि विजड़ित गजमुक्ताओं की भाँति जान पड़ रही थी।
वह विधाता की इतनी अपूर्व रचना थी कि आज हमने उसे जितना देखा उस पर कौन विश्वास करेगा। अर्थात् उसका सौन्दर्य इतना अद्भुत, अपूर्व एवं अद्वितीय था कि सामान्यतः उसके वर्णन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वह विधाता की अनोखी सृष्टि थी। उल्टे स्वर्ण कदली के स्तम्भ के समान उसकी चिकनी एवं शीतल जंघाओं के नीचे कमल के समान उसके चरण सुशोभित थे। उन चरणों के मनोहर घुघरू बज रहे थे, जिसको सुनकर कामोद्दीपन हो जाता था। तात्पर्य यह कि उसके नूपुरों का उन्मादक मधुर निनाद काम-भावना को जगा रहा था। विद्यापति कवि कहते हैं कि जो रसिक ऐसी बाला को भजता (स्मरण करता) है, तो यह उसके पुराकृत पुण्यों के परिणामस्वरूप हो पाता है। इसके सम्पूर्ण रस की जानकारी तो लिखिमादेई के पति राजा शिवसिंह को ही है।
अलंकार-(क) रूपकातिशयोक्ति अलंकार-जुगुल सैल सम हिमकर देखल एक कमल दुई जोति रे। (ख) रूपकातिशयोक्ति अलंकार-विपरित कनक-कदलि तर सोभित थल पंकज अपरूप रे। (ग) हेतुत्प्रेक्षा अलंकार – तथहु मनोरथ बाजन बाजए जागए मनसिज भूप रे।
नायिका- नवयौवनागम के कारण अंकुरित यौबना नायिका।
7. चाँद-सार लए मुख घटना करु लोचन चकित चकोरे ।
अमिय धोय आँचर धनि पोछलि दह दिसि भेल उँजोरे।
जुग जुग के बिहि बूढ़ निरस उर कामिनी कोने गढ़ली।
रूप सरूप मोयं कहइत असंभव लोचन लागि रहली।
गुरु नितम्ब भरे चलए न पारए माझ खानि खीनि निमाई।
भाँगि जाइत मनसिज धरि राखलि त्रिबलि लता अरुझाई।
भनइ विद्यापति अद्भुत कौतुक ई सब बचन सरूपे।
रूप नरायन ई रस जानथि सिबसिंध मिथिला भूपे।
सन्दर्भ- पूर्ववत् ।
प्रसंग– नायिका की दूती या सखी नायक से उस नायिका के सौन्दर्य का वर्णन करती हुई कहती है।
व्याख्या- चन्द्रमा का सार लेकर उस सुन्दरी के मुख की रचना की गई है, जिसे देखकर चकोर (रसिक, रसज्ञ) के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। आँखें उसके मुख को निखरती ही रह गईं। उस रमणी ने अमृत जल से धोकर जब अपने मुख को आँचल से पोंछा तो दसों दिशाओं में उसके मुख-चन्द्र का आलोक फैल गया। युग-युग के ब्रह्मा का हृदय तो नीरस है, तब ज्ञात नहीं, ऐसी सुन्दर कामिनी की रचना किसने की है? विधाता ने तो निश्चय ही इसे नहीं रचा है, क्योंकि उसके सृष्टि सारे संसार में कहीं भी तो नहीं दिखाई पड़ती। उसने रूप का सौन्दर्य वर्णन- मैं कर पाने में समर्थ नहीं हूँ, नेत्र बराबर उसी के सौन्दर्य अवलोकन में लगे रहते हैं। वह सुन्दरी अपने भारी नितम्बों के भार से चल नहीं पाती। उसकी कटि क्या है? मानों क्षीणता की खान है। अभिप्राय यह कि उस (नायिका) की कटि अत्यन्त क्षीण (पतली) है। उसकी इतनी क्षीण कटि (कभर) कहीं टूट न जाए, इसीलिए कामदेव ने विवली रूपी लता में उसे उलझा (बाँध) रखा है। कवि विद्यापति कहते हैं, मैंने जिस रूप को शब्दों में बाँधा है, वह अत्यन्त ही अनूठा और कौतूहल से भरा हुआ है। मिथिला के राजा शिवसिंह (नारायण रूप) इस रूप-रस को भली-भांति समझते हैं।
अलंकार- (क) दीपक अलंकार -‘चाँद सार लए मुख घटना करु लोचन चकित चकोर।’ (ख) व्यतिरेक अलंकार ‘लोचन चकित चकोर।
नायिका- नवयौवन के आगमन के कारण नवयौवना मुग्धा नायिका।
विशेष- इस पद से कवि की मौलिक वन-शक्ति का परिचय मिलता है। ‘अमिअ धोए आँचर धनि पोछल दह-दसि भेल ऊजोरे’ से उसकी स्वच्छन्द एवं मौलिक सूझ का पता चलता है। विद्यापति की नायिका की रचना चन्द्रमा के सार अंश से की गई है। उसके सौन्दर्य से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही हैं। उसके सौन्दर्य-वर्णन में कवि अपने को असमर्थ पा रहा है। वह सोच रहा है कि ऐसी अद्भुत सौन्दर्य कृति की रचना किसने की है।
- सखि हे हमर दुखक नहि ओर।
ई भर बादल माह भादर, सून
मंदिर मोर।।
झंपि घन गरजति संतत, भुवन भरि बरसंतिया।
कन्त पाहुन काम दारुन, सघन खर सर हंतिया।।
कुलिस कत सत पात मुदित, मयूर नाचत मातिया।
मत्त दादुर डाक डाहुक फारि जायत छातिया।।
तिमिर दिग भरि घोर जामिनि अथिर बिजुरिक पाँतिया।
विद्यापति का कइसे गमाओब, हरि बिना दिन रातिया।।
सन्दर्भ- पूर्ववत् ।
प्रसंग- भद्र मास की वर्षा राधा की विरह व्यथा को उद्दीप्त कर देती है। यह बादलों की गरज, बिजली की चमक और मूसलाधार वर्षा से संतृप्त होकर सखी से कहती है
व्याख्या- हे सखी! मेरे दुःख का अन्त नहीं है। भाद्र मास के बादल चारों ओर से घिरकर उमड़ते फिरते हैं और इधर प्रियतम के बिना मेरा मन्दिर शून्य है। बादल चारों ओर से घिरकर गर्जना करते हैं और अविराम वर्षा से बरस कर पृथ्वी को जल से भर रहे हैं, किन्तु ऐसे समय में मेरा प्रियतम प्रवासी हो गया है और इधर महा दारुण कामदेव मुझे अति तीक्ष्ण बाणों से मार रहा है। बिजलियों से शत् – शत् वज्र टूट कर गिर रहे हैं। वर्षा के इस घनीभूत वातावरण में मयूर उन्मत्त होकर नाच रहे हैं। मेंढ़क और डाहुकभीषण स्वर में पुकार रहे हैं, इनके स्वरों को सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है।
चारों ओर सघन अन्धकार छाया हुआ है, जिससे रात्रि भयानक दीख पड़ती है। जब तब विद्युत का अस्थिर और चंचल प्रकाश दिखाई पड़ता है।
विद्यापति कहते हैं कि वियोगिनी सखी से विरहाकुल होकर कहती है कि तू ही बता कि ऐसे समय में प्रियतम के बिना मैं दिवस और रात्रि किस प्रकार व्यतीत करूं।
विशेष – (1) वर्षा का भीषण ओर यथार्थ चित्र वियोग के उद्दीपन के रूप में उपस्थित हुआ है।
अलंकार – अनुप्रास, ध्वन्यात्मकता, शब्द मैत्री, विषम एवं वृत्यानुप्रास।
- चानन भेल बिसम सर रे, भूसन भेल भारी।
सपनहुँ नहिं हरि आएल रे, गोकुल गिरधारी।।
एकसर ठाड़ कदम-तर रे, पथ हेरथि मुरारी।
हरि बिनु देह दगध भेल रे, झामरू भेल सारी।।
जाह जाह तोहें मधुपुर जाहे, चन्द्रवदनि नहिं जीउति रे बध लागत काहे।।
भनहिं विद्यापति तन मन दे, सुन गुनमति नारी।
आज आओत हरि गोकुल रे, पथ चलु झटझारी॥
सन्दर्भ– नायिका राधा अपनी वियोग दशा का वर्णन कर रही है। उसकी सखी उसे आशान्वित करती है कि उसके प्रियतम कृष्ण आयेंगे, अतः वह उनके स्वागत के लिए तैयार रहे-
व्याख्या- कृष्ण के वियोग में चन्दन मुझे तीखे बाण की तरह बेधक लग रहा है और आभूषण भार स्वरूप लगते जब से गिरधारी श्री कृष्ण मथुरा गये हैं, तब से स्वप्न में भी लौटकर नहीं आये।
मैं अकेली कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़ी हुई मुरारी श्री कृष्ण का मार्ग देख रही हूं। उनके बिना मेरा शरीर जलकर राख हो रहा है। हे उद्धव! तुम यहाँ क्यों आये हो? कृपाकर तुम शीघ्र ही मथुरा लौट जाओ। कृष्ण के बिना वह चन्द्रवदनी जीवित नहीं रहेगी। ऐसी दशा में तुम अपना यह उपदेश देकर इसके वध के भागी क्यों बनते हो।
विद्यापति कहते हैं कि सखी राधा का समाधान करती हुई कहती हैं- हे गुणवती बाला सुनो, मैं तन-मन से साक्षी देकर कहती हूँ कि अब हरि गोकुल आयेंगे। तू उनका स्वागत करने के लिए समूह बनाकर सब सखियों को साथ लेकर शीघ्र ही उनके आने के पथ में खड़ी हो।
विशेष -(1) वियोगिनी की विरह-दशा का मार्मिक चित्र उपस्थित हुआ है।
- माधव हमार रहल दुरदेस। केओ न कहे सखि कुसल सनेस।।
जुग जुग जीवथु वसथु लाख कोस। हमर अभग हुनक दोस।।
हमर करम भेल बिहि विपरीत। तेजलन्हि माधव पुरुविल प्रीति।।
हृदयक वेदन बान समान। आनक दुःख आन नाहि जान।।
भनहिं विद्यापति कवि जयराम। कि करत नाह दैव भेल वाम॥
सन्दर्भ- राधा का कधन सखी के प्रति है। उसे जो वियोग जनित दुख प्रिय के वियोग में मिल रहा है, उसके दोष अपने भाग्य को ही देती है। वह लाख कोस दूर रहने पर भी प्रियतम के मंगल की कामना करती है-
व्याख्या- हे सखी! हमारे प्रियतम दूर देश जा बसे। कोई भी उनका कुशल समाचार मुझे नहीं सुनाता, वह मुझे दूर चाहे लाख कोस पर निवास करें, किन्तु मेरी तो यही कामना है कि वे युग-युग तक तीवित रहे। मैं जो विरह का दुःख भोग रही हूं इसमें मेरा भाग्य-दोष ही है, उनका कोई भी दोष नहीं है। मेरे अपने कर्मों से ही विधाता मुझसे विपरीत हो गया और कृष्ण ने मेरे प्रति अपनी पहले की प्रीति भुला दी।
मेरे हृदय में विरह की वेदना बाण के समान दुख दे रही है। अन्य के दुख को अन्य नहीं जानता – (जाके पायं न जाइ बिवाई, सो किमि जानहिं पीर पराई)।
कवि जयराम विद्यापति कहते हैं कि दैव ने मेरे भाग्य में जो विपरीत फल लिख दिया है, उसी के परिणामस्वरूप में यह दारूण दुःख भोग रही हूँ।
विशेष– (i) यहाँ प्रेम की उदात्त भावना प्रकट हुई है। सच्ची प्रेमिका यही चाहती है कि उसका प्रियतम कहीं रहे, परन्तु उसका अमंगल न हो। सूर की गोपियाँ कहती हैं-
“चिर जीवहु कान्ह हमारे।”
x
“सूर असीस देत यह निसि-दिन
न्हात खसैं जनि बाल।”
(ii) विषाद और दैन्य की अनुभूति पूर्ण व्यंजना हुई है।
- सखि हे कि पूछसि अनुभव मोय
सोड़ पिरीति अनुराग बखानइते, तिले तिले नूतन होय॥
जनम अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल।
सोइ मधुर बोल भुवनहि सुनल, श्रुति पथे परसन गेल॥
कत मधु यामिनी रमसे गमाओल, न बुझल कैसन केल।
लाख लाख युग हिये हिये राखल, तैओ हिय जुड़न ने गेल॥
यत यत रसिक जन रसे अनुगमन, अनुभव काहु न पेख।
विद्यापति कह प्राण जुड़ाइत, लाखे न मिलल एक॥
सन्दर्भ- नायिका का कथन सखी के प्रति है। वह प्रेम-भाव का वर्णन करती है।
व्याख्या- हे सखी ! तू मेरे अनुभव के विषय में क्या पूछती है, अर्थात् मैं तुझे क्या अनुभव बताऊं? यदि उस प्रेम तथा अनुराग का वर्णन किया जाये वह क्षण-प्रतिक्षण नवीन ही नवीन दिखाई पड़ता है। अतः उसका वर्णन करना कोई सरल नहीं है। कारण, कि वर्णन तो स्थिर वस्तु का किया जा सकता है। मैंने जीवन भर कृष्ण के रूप को टकटकी बाँधकर देखा, किन्तु मेरे नेत्र उसके दर्शन से न अघाए। उनके मधुर वचनों को सदैव कानों से सुनती रही किन्तु फिर भी ऐसा लगता था जैसे मैंने उन्हें कभी सुना ही न हो। रूप और वाणी की चिर नवीनता मुझे अतृप्त बनाये रखती थी। कितनी ही बसन्त की सुहावनी मादक रातें कृष्ण के साथ प्रेम-क्रीड़ा में व्यतीत हुई, लेकिन मैं किलि-विलास को न समझ पाई। अर्थात् मिलन की उत्कण्ठा आज भी बनी हुई है। मैंने युगों तक अपने हृदय को उनके हृदय से लगाये रखा, किन्तु फिर भी मेरा हृदय शीतल नहीं हुआ अर्थात् हृदय में मिलन की प्यास वैसी ही बनी रही, जैसी कि पहले थी। अनेक रसिक व्यक्ति प्रेम-रस का पान करते हैं, किन्तु कोई भी व्यक्ति उस प्रेम का वास्तविक अनुभव नहीं कर सका।
विद्यापति कहते है कि लाखो व्यक्तियों में एक भी ऐसा नही मिला, जिसका मन प्रेम को प्राप्त कर तृप्ति का अनुभव करता हो। कारण कि प्रेम की अनुमति हो ही नही सकती। प्रेम सदैव चिर- नूतन रहता है, इसलिए उसका वर्णन सम्भव नहीं।
विशेष- (i) इस पद में विद्यापति ने प्रेम की अनिवर्चनीयता और चिर नवीनता का रूप प्रस्तुत किया है। (ii) तिल तिल नूतन होए’ क्षण-क्षण में प्रेम की नवीनता प्रेम की प्रमुख विशेषता है।
हिन्दी – महत्वपूर्ण लिंक
- आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ- राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ
- प्रमुख हिन्दी गद्य-विधाओं की परिभाषाएँ
- नाटक- परिभाषा, प्रथम नाटक, नाटक के तत्त्व, प्रमुख नाटककारों के नाम, प्रसिद्ध नाटकों के नाम
- आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ- प्रवृत्तियों की विशेषताएँ, आदिकालीन साहित्य का महत्त्व
- हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन
- कृष्णभक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि (Krishnbhakti Kavay Dhara Ke Pramukh Kavi)
- कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ /कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषतायें (Krishan Kavay Ki Pravritiitiyan / Krishan Kavay Ki Visheshatayen)
- राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ | रामकाव्य की प्रमुख विशेषताएँ
- भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताएँ | स्वर्ण युग की विशेषताएँ
- भाषा की प्रकृति (विशेषताएँ) – यहाँ पर 18 प्रकृतियों का वर्णन किया गया है
- भाषा क्या है तथा भाषा की परिभाषा (What is language and definition of language)
- भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत – 10 प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या के साथ
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]


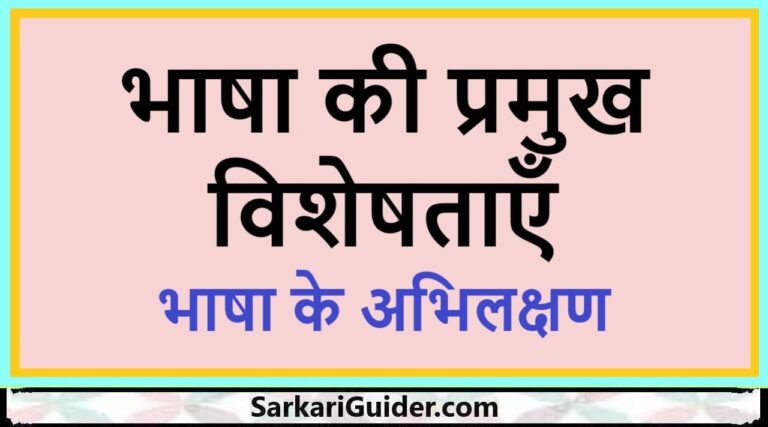
सुपुरुष प्रेम सुधनि अनुराग
इस पध्यांश की व्याख्या?