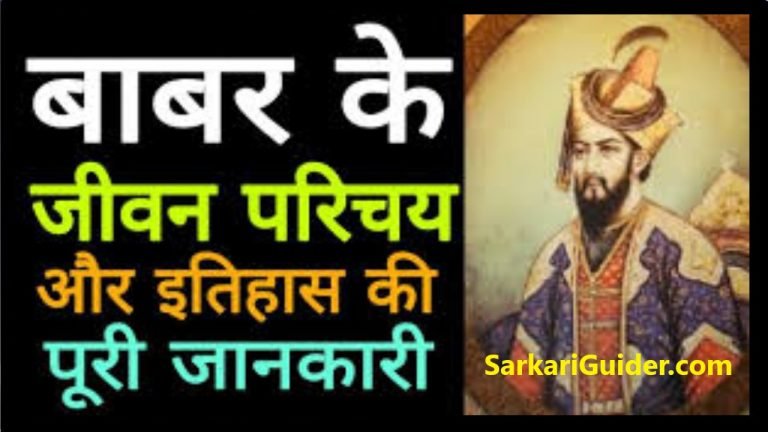सामूहिक सुरक्षा के संकट के कारण | सुरक्षा के उपाय | राष्ट्र संघ की स्थापना और उसकी असफलता
सामूहिक सुरक्षा के संकट के कारण | सुरक्षा के उपाय | राष्ट्र संघ की स्थापना और उसकी असफलता
प्रथम विश्वयुद्ध तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच 1939 से पूर्व यूरोप में सामूहिक सुरक्षा का संकट उत्पन्न हुआ। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं-
सामूहिक सुरक्षा के संकट के कारण
समस्त क्षेत्रीय संधियों ने यूरोप में अत्यधिक राजनैतिक रोमांच और तनाव (Excitement and Tension) को पैदा कर दिया जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध का भड़क उठना माना जाता है। सामूहिक सुरक्षा, इन समस्त क्षेत्रीय संधियों के माध्यम से सुलझने के स्थान पर उलझती चली गई। इस संकट के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं-
(i) अन्तर्राष्ट्रीय सेना की कमी- यूरोप का कोई भी राज्य अपनी सेना को राज्य-संघ के अधीन रखने के लिए तैयार था। कोई भी राज्य अन्तराष्ट्रीय विवादों में तब तक उलझने के लिए तैयार नहीं था जब तक उसके राष्ट्रीय हितों को खतरा न हो।
(ii) वर्साय की संधि और राष्ट्र-संघ की अवहेलना- सामूहिक सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय संधियों पर बल दिया गया था। ये क्षेत्रीय संधियाँ राष्ट्र संघ के महत्व को कम ही नहीं करती थीं बल्कि इन्होंने कुछ गलतफहमियों को पैदा कर दिया। उदाहरणस्वरूप लोकार्ने सन्धि से राज्यों को यह अनुभव हुआ कि वसाय सन्धि का पालन तभी करना होगा जबकि इसके क्रियान्वयन के लिए कोई सन्धि अलग से की जाय।
(iii) क्षेत्रीय संधियों से प्रतिस्पर्धा का वातावरण- क्षेत्रीय सन्धियों के परिणामस्वरूप यूरोप प्रतिस्पर्धो सैन्य खेमों में बंट गया। जिसके परिणामस्वरूप यूरोप की वही स्थिति हो गयी जो 1914 से पहले थी।
(iv) नाजीवाद का अभ्युदय- जर्मनी में नाजीवाद के अभ्युदय के परिणामस्वरूप आक्रामक नीति का अनुसरण किया जाना प्रारम्भ हुआ। छोटे-छोटे राज्यों के अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो गया और विभिन्न राज्यों द्वारा प्रभावशाली विरोध न किये जाने के कारण सुरक्षा पूर्णत: असफल हो गई।
(v) तुष्टिकरण की नीति- यूरोपीय राज्य से भयभीत होकर जर्मन को संतुष्ट करने के प्रयत्न में संलग्न रहे. परिणामस्वरूप जर्मनी प्रोत्साहन प्राप्त कर अग्रसर होता रहा।
(vi) राष्ट्रों के विभिन्न हित- यूरोपीय महाशक्तियों के अपने अलग-अलग हित थे और इनके संवर्धन के लिए राज्यों ने अलग-अलग नीतियों को अपनाया। सामूहिक सुरक्षा में किसी की आस्था नहीं थी। यह तो एक मुकुट था जिसे वेश-भूषा के रूप में विभिन्न राज्यों ने पहन लिया था। जब भी राष्ट्रीय हित से इसका टकराव हुआ यह धराशायी हो गई।
(vil) निःशस्त्रीकरण का अंत- प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् शान्ति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए निःशस्त्रीकरण की दिशा में राष्ट्र-संघ के तत्वावधान में तथा राष्ट्र संघ के बाहर अनेक प्रयत्न किये गये। निःशस्वीकरण के प्रयलों की असफलता के परिणास्वरूप मार्च, 1935 में हिटलर ने खुले तौर पर पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्माय संधि की शतों का खण्डन करते हए अनिवार्य सैनिक सेवा एवं सैन्य वृद्धि की पोषणा ने यूरोप में संकट उत्पन्न कर दी। पुन: शस्त्रीकरण के कारण यूरोप तीव्र गति से उस भयंकर विस्फोट की ओर अग्रसर हुआ जिसकी अन्तिम परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई।
सुरक्षा के उपाय
राष्ट्र संघ की स्थापना और उसकी असफलता-
भविष्य में युद्ध रोकने के लिये विश्व के महान् राष्ट्रों ने एक राष्ट्र संघ का निर्माण किया था जिसमें तय किया गया था कि यदि विभिन्न राज्यों के मध्य किसी प्रश्न पर झगड़ा हो तो उनके मामलों को संघ की ‘कौन्सिल के सामने रख दिया जाये। कौन्सिल का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य हो। यदि किसी पक्ष ने निर्णय का विरोध करते हुए विरोध पक्ष पर आक्रमण किया तो सभी राष्ट्र उसका बहिष्कार कर दें। उससे कोई व्यापार न करे, न उसको कोई कर्ज दे। यदि इस बहिष्कार से काम न चले, तो संघ की कौन्सिल को उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का अधिकार हो। इस राष्ट्र संघ ने बाल्टिक सागर में आलैंड के प्रश्न की फिनलैंड के पक्ष में तय किया। जर्मनी और पोलैंड के बीच साइलोसिया के प्रश्न को हल किया और ग्रीस को बलगेरिया के प्रश्न पर युद्ध करने से रोका। इसके अतिरिक्त अमेरिका में कोलम्बिया तथा पेरू के झगड़ों को तय किया। किन्तु इतना होते हुए भी जहाँ बड़े-बड़े राष्ट्रों के झगड़ों के प्रश्न आये वहाँ राष्ट्र संघ उदासीन रहा जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या जटिल बनी रही। इस समस्या को रोकने के निम्नलिखित उपाय किये गये-
(1) फ्रांस द्वारा सुरक्षा का उपाय– फ्रांस को प्रथम महायुद्ध से भारी क्षति पहुंची थी। उसको जमनी से नुकसान का भय था। उसने जर्मनी को कमजोर करने के लिये राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों को सेना का अधिकार करा दिया था और ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि राइनलैंड से सेनाओं के हटाने पर भी जर्मनी वहाँ किलेबन्दी नहीं कर सकता था। इतने पर भी फ्रांस सन्तुष्ट नहीं था। उसने भी प्रस्ताव रखा कि राष्ट्र संघ के पास एक विशाल सेना होनी चाहिये जो शान्ति भंग करने वाले राष्ट्रों को दण्ड दे सके। किन्तु अमेरिका और ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस पर फांस ने ब्रिटेन और अमेरिका से इस बात की गारण्टी माँगी कि यदि किसी राज्य ने फ्रांस पर आक्रमण किया. तो वे फ्रांस की सहायता करेंगे। अमेरिका को कांग्रेस ने फ्रांस की यह बात भी अस्वीकार कर दी इस परै ब्रिटेन भी फ्रांस को सहायता देने पर संकोच करने लगा। इससे फ्रांस को निराशा हुई और उसने ‘सुरक्षा’ के लिये यूरोप के छोटे राज्यों से सन्धियों का सिलसिला शुरू किया।
(2) त्रिगुट की स्थापना- फ्रांस को ब्रिटेन और अमेरिका से सहायता की आशा न रही। अतएव उसने यूरोप के अन्य राष्ट्रों से सन्धि करके अपनी सुरक्षा करने का निश्चय किया। उसने यरोप के छोटे-छोटे राज्यों से सन्धि को। बेल्जियम, पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ फ्रांस ने सुरक्षा के लिये सन्धि कर ली। इसी समय यूरोप में रूमानिया, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया ने सन्धि करके एक त्रिगुट का निर्माण किया। फ्रांस इस त्रिगुट का अध्यक्ष रहा।
(3) यूरोप में नवीन सन्धियाँ- राष्ट्र संघ की निर्बलता और फ्रांस की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर यूरोप के सभी राज्यों में यह भावना उत्पन्न हो गई थी कि सुरक्षा के लिए उन्हें किसी न किसी गुट में अवश्य ही रहना चाहिये। इस भावना के परिणामस्वरूप यूरोप में विभिन्न गुटबन्दियाँ आरम्भ हो गई थी । इटली में मुसोलिनी शक्तिशाली हो गया था। उसको फ्रांस की शक्ति का बढ़ना सहन नहीं था। उसने चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, स्पेन, रूमानिया, अल्बेनिया, हंगरो, टर्की, ग्रीस और आस्ट्रिया के साथ सन्धि कर ली। इन सन्धियों से यह भी पता चलता है कि यूरोप के राष्ट्रों का एक गुटबन्दी से सन्तोष नहीं था। एक राज्य एक से अधिक गुटबन्दी में भाग लेता था क्योंकि उसको अपने एक गुट के साथियों पर ही निर्भर रहने से सन्तोष नहीं था। इस प्रकार यूरोप का प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा के लिये विभिन्न गुटबन्दियों में भाग ले रहा था। इसलिये इटली से सन्धि करने वाले राष्ट्र फ्रांस के ‘त्रिगुट’ में भी सम्मिलित थे।
(4) रापैलो की सन्धि- रूम और जर्मनी दोनों ही फ्रांस के शत्रु थे और दोनों ही विश्व युद्ध के बाद युरोप को राजनीति से अलग (solate) से हो गये थे। फ्रांस और पालैंड की सन्धि रूस का अच्छा नहीं लगी। जर्मनी फ्रांस के विरुद्ध था अतएव जमना और रूस दोनों ने ‘रापैलो’ के स्थान पर सन्धि कर लो जिसके अनुसार जर्मनी ने रूस को ‘कम्युनिस्ट सरकार’ को मान्यता प्रदान की और रूस के साथ राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये। रूस के साथ सन्धि करके जर्मनो ने भो सुरक्षा की व्यवस्था कर लो।
(5) रूस की अन्य सन्धियाँ- रूस को ‘कम्युनिस्ट सरकार’ अपने देश की उन्नति करना चाहती थी। इटलो को तरह वहाँ पर भी एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। रूस ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये 1924 में टों के साथ सन्धि करके तय कर लिया कि वे दोनों एक-दूसर पर आक्रमण नहीं करेंगे और यदि किसी ने उनमें से किसी पर आक्रमण किया तो व तटस्थ रहेगें और संकट काल में एक-दूसरे के सहयोगी रहेंगे।
(6) जेनेवा प्रोटोकाल- राष्ट्र संघ की विफलता पर फ्रांस ने विश्व के अनेक राष्ट्रों को राष्ट्र संघ को कमियों की ओर आकर्षित किया। फ्रांस के राजनीतिज्ञ इस बात का अच्छी तरह समझते थे कि राष्ट्र संघ अपनी कमियों के कारण अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या को हल करने में असमर्थ है। उनका विचार था कि राष्ट्र संघ के विधान में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि किस अपराध के लिये किस राज्य को विद्रोही ठहराया जाये और विद्रोही राज्य पर काबू पाने के लिये किस उपाय का अवलम्बन किया जाय। राष्ट्र संघ की इन दोनों कमियों को पूरा करने के लिये फ्रांस के राजनीतिज्ञों ने विश्व के अन्य राष्ट्रों से मिलकर एक सभा की जिसमें सुरक्षा के प्रश्न पर नये तराके से वाद-विवाद हुआ। यह वाद-विवाद इतिहास में ‘जेनेवा प्रोटोकाल’ के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रोटोकाल के अनुसार निर्णय किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों में जब कोई राज्य राष्ट्र संघ के निर्णय को न माने तो उसको विद्रोही करार दे दिया जाये और निर्णय पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का यह कर्तव्य हो कि वे विद्रोही राज्य के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करें। जेनेवा प्रोटोकाल फ्रांस के राजनीतिज्ञों ने अपने देश की सुरक्षा के लिये बनाकर तैयार कर दिया था किन्तु ग्रेट ब्रिटेन इस बात को पसन्द नहीं करता था कि वह व्यर्ध में हो अपना समय नष्ट करता रहे। वह प्रोटोकाल के इस धारा के विरुद्ध था कि फैसले पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य द्रोही राज्य के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करें। हेजेन के शब्दों में, “जेनेवा प्रोटोकाल में इंगलैंड पर यह नियन्त्रण लगा दिया गया था कि वह विश्व के किसी भी भाग में संघर्ष होने पर हस्तक्षेप करे। लेकिन इंगलैंड की जनता का मत इसका विरोधी था जिससे प्रोटोकाल के निर्णय कार्यान्वित नहीं किये जा सके।”
(7) जर्मनी और फ्रांस में सन्धि- फ्रांस अब चारों ओर से निराश हो चुका था। उसे जर्मनी की ओर से अधिक भय था। इस समय 1925 में ‘ब्रियां’ नामक राजनीतिज्ञ परराष्ट्र मन्त्री के पद पर नियुक्त थे। वह समझता था कि यदि जर्मनी और फ्रांस दोनों देशों में हो आपस में समझौता हो जाय तो सुरक्षा को समस्या का हल हो सकता है। इससे पूर्व भी फ्रांस और जर्मनी में समझौते की बातचीत चली थी किन्तु किन्हीं कारणों से उनमें समझौता नहीं हो सका था। अब कुछ समय बदला हुआ था। इधर फ्रांस और जर्मनी के सम्बन्ध भी इतने कटु न रहे थे। जेनेवा प्रोटोकाल के असफल हो जाने के कारण फ्रांस को अपनी सुरक्षा के लिये जर्मनी से सन्धि करना आवश्यक हो गया था। इसलिये 1925 में स्विटजरलैंड के नगर ‘लोकानों’ में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। यह सन्धि ‘लोकानों की सन्धि’ कहलाती है। इस सन्धि में जर्मनी और फ्रांस के बीच निम्नलिखित समझौते हो गये-
(अ) यह तय किया गया कि ‘वर्साय की सन्धि’ के द्वारा जर्मनी और फ्रांस की जो सीमा निधारित की गई थी विश्व के सभी राज्य उस सीमा की सुरक्षा की गारण्टी करें।
(ब) जर्मनी और बेल्जियम को भी जो सीमा वर्साय की सन्धि के द्वारा निश्चित की गई थी उसका गारण्टी का उत्तरदायित्व भी सब राष्ट्रों के ऊपर रहे।
(स) यदि जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और चेकोस्लोवाकिया के बीच कोई झगड़ा हो उसका फैसला भी पंचायती तरीके (Arbitration) से किया जाये।
(द) फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड में भी यह सन्धि हो गई कि वे एक-दूसरे की सीमाओं की गारण्टी करेंगे।
(य) यह भी तय किया गया कि यदि फ्रांस अथवा जर्मनी इस सन्धि की शर्तों के विरुद्ध कोई कार्य करेंगे तो ब्रिटन उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगा। किन्तु साथ ही साथ यह भी बात स्पष्ट हो गई थो कि यदि जर्मनी अपनी पूर्वी सीमा को बढ़ाने के लिये या उन प्रदेशों पर कब्जा करने के लिये, जिनमें जर्मन जाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, युद्ध करेगा तो ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिये मजबूर न होगा।
यद्यपि लाकाों को सन्धि से फ्रांस को कुछ संतोष हो गया था किन्तु फिर भी पूर्वी सीमा की ओर से उसे भय बना हुआ था। जहाँ एक ओर लोकार्नो सन्धियों के सम्बन्ध में चैम्बरलेन का यह विचार था, “Indrewareal dividing line between the years of war and the years of Peace.” वहाँ फ्रांस अभी भी अपनी सुरक्षा की ओर से निश्चिंत नहीं था। इधर 1926 में जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य हो गया था, इससे जर्मनी की हिम्मत और भी बढ़ गयी थी। जर्मनी को रोक- थाम के लिये फ्रांस को दृष्टि में लोका! को सन्धि पर्याप्त नहीं थी। इसलिये फ्रांस के परराष्ट्र मन्त्री श्री ब्रियां ने सुरक्षा की खोज को जारी रखा।
(8) कैलौग-ब्रियां पैक्ट (Kellogg-Briand Pact)- अब फ्रांस ने अमेरिका से समझौते की बातचीत शुरू की और यह प्रस्ताव रखा कि फ्रांस और अमेरिका आपस में मिलकर बहुत काल के लिये एक समझौता कर लें। इस समय अमेरिका के विदेश मन्त्री ‘कैलौग’ थे। उन्होंने फ्रांस को यह सलाह दी कि संसार के सारे राज्य मिलकर यह तय करें कि वे आपस में झगड़ों को निपटाने के लिये युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे। कैलाग को इस योजना के अनुसार विश्व के प्रमुख राज्यों के प्रतिनिधि 27 अगस्त, 1927 को पेरिस में इकट्ठे हुए और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे अपने झगड़ों को निपटाने के लिये युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे। विश्व के राज्यों के इस समझौते को इतिहास में ‘पेरिस पैक्ट’ या कैलौग-ब्रियां पैक्ट के नाम से पुकारा जाता है। इस पैक्ट से फ्रांस की बहुत कुछ सन्तोष हुआ।
(9) सुरक्षा की समस्या में असफलता तथा यूरोप में सैनिक सन्धियाँ- (1) कैलौग-ब्रियां पैक्ट पर विश्व के 65 राज्यों ने हस्ताक्षर किये थे। उन सभी राज्यों ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया था कि वे आत्म-रक्षा के अतिरिक्त कभी भी युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे किन्तु इस पैक्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यदि कोई राज्य युद्ध शुरू करे तो उसे कैसे रोका जाय।
(2) यह पैक्ट केवल एक संकल्प मात्र था। इसको कमियों को दूर करने के लिये विश्व के कुछ राज्यों ने राष्ट्रसंघ के विधान में संशोधन करने के लिये कदम उठाया था।
(3) 1929 में विश्व के राज्यों ने एक बार फिर सभा की और राष्ट्र संघ के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि युद्ध का सर्वथा बहिष्कार किया जाय और युद्ध शुरू करने वाले राज्य को दण्ड दिया जाये। इस विषय पर काफी बहस की गई किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। राज्यों की इस सभा की असफलता के बाद अपनी अपनी रक्षा का बहाना करके विश्व के सभी राज्य सैनिक गुटबन्दियों में लग गये।
(4) इधर जर्मनी की शक्ति बढ़ गई थी।
(5) जापान मंचूरिया पर आक्रमण कर रहा था।
(6) इटली ने एबीसीनिया पर अधिकार कर लेने को तैयारी कर ली थी।
(7) जर्मनी ने हर्जाने की रकम को न देने को उद्घोषणा कर दी थी।
(8) यूरोप पर आर्थिक संकट आ गया था।
(9) अमेरिका अपनी रकम वसूल करने पर जोर दे रहा था।
इन सब कारणों से विश्व के सभी राज्य एक-दूसरे से कुछ खिचे हुए थे और यह समझने लगे कि सुरक्षा के लिये सैनिक गुटबंदियों का होना आवश्यक है। उनका यह विचार दृढ़ हो गया था कि कोई भी राज्य सैनिक गुटबंदियों के बिना अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। अपनो रक्षा के लिये किसी न किसी सैनिक गुटबंदी का सदस्य होना आवश्यक है। इस विचारधारा के अनुसार यूरोप के सभी राज्यों ने सैनिक गुटबंदियाँ आरम्भ कर दी। एक एक राज्य कई कई गुटों में शामिल हो गया। सब एक-दूसरे को शंका को दृष्टि से देखने लगे। यरोप और विश्व में गुटबंदियों का वही सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया जिसने प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों को जन्म दिया था। 1939 में इस सनिक गुटबंदी परिणामस्वरूप विश्व के राज्यों को द्वितीय महायुद्ध की प्रचंड अग्नि में कूदना पड़ा। इस प्रकार सुरक्षा की समस्या का अन्त लड़ाई में ही हुआ।
इतिहास – महत्वपूर्ण लिंक
- विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के कारण | महान् मन्दी के निवारण के लिए किये गये उपचार | लन्दन का विश्व अर्थ सम्मेलन | मन्दी के कारण | मन्दी के प्रभाव
- रूस के पुनर्गठन में लेनिन एवं स्टेलिन की भूमिका | कान्ति के पश्चात् रूस का पुनर्गठन | नयी आर्थिक नीति
- चीन में साम्यवाद का उदय | चीन में साम्यवाद की स्थापना | साम्यवादियों द्वारा स्थान परिवर्तन या ‘महाप्रस्थान’ | साम्यवादियों की सफलता के कारण
- तुर्की का आधुनिकीकरण | कमाल पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी संघर्ष | सेव्रे की सन्धि
- दक्षिणी-पूर्वी एशिया में राष्ट्रवाद का विकास | फ्रांस के प्रभुत्व की स्थापना | फ्रांस की युद्धोत्तर नीति | हनोई समझौता
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]