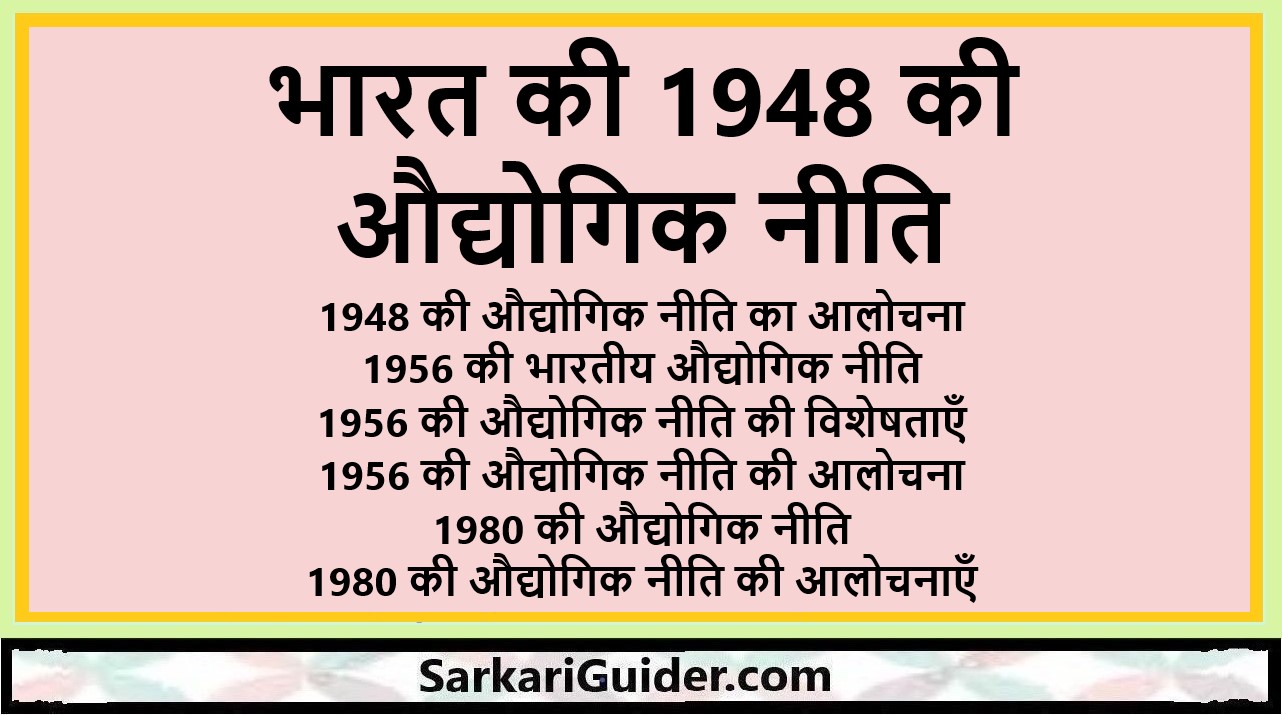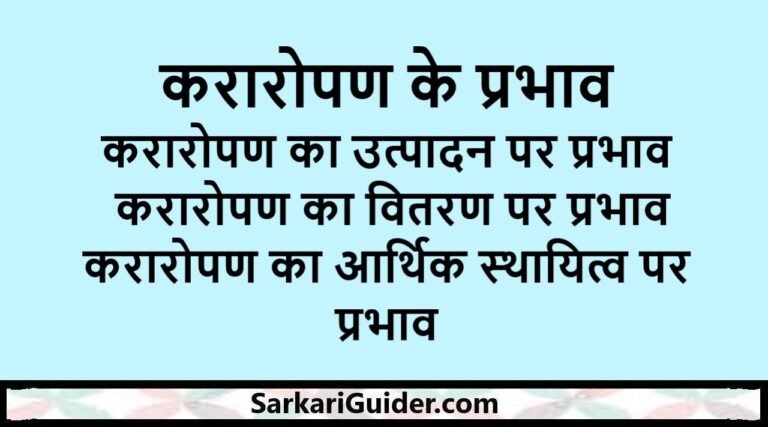भारत की 1948 की औद्योगिक नीति | 1948 की औद्योगिक नीति का आलोचना | 1956 की भारतीय औद्योगिक नीति | 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ | 1956 की औद्योगिक नीति की आलोचना | 1980 की औद्योगिक नीति | 1980 की औद्योगिक नीति की आलोचनाएँ

भारत की 1948 की औद्योगिक नीति | 1948 की औद्योगिक नीति का आलोचना | 1956 की भारतीय औद्योगिक नीति | 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ | 1956 की औद्योगिक नीति की आलोचना | 1980 की औद्योगिक नीति | 1980 की औद्योगिक नीति की आलोचनाएँ | India’s 1948 Industrial Policy in Hindi | Criticism of the Industrial Policy of 1948 in Hindi | Indian Industrial Policy of 1956 in Hindi | Features of Industrial Policy of 1956 in Hindi | Criticism of the Industrial Policy of 1956 in Hindi | Industrial Policy of 1980 in Hindi | Criticisms of the Industrial Policy of 1980 in Hindi
भारत की 1948 की औद्योगिक नीति
किसी देश की आर्थिक विकास पर उसकी औद्योगिक नीति का प्रभाव पड़ता हैं। औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सरकार उन नियमों और सिद्धान्तों के बारे में औपचारिक घोषणा करती है जो किसी देश के उद्योग विशेष से सम्बन्धित हैं। स्वतन्त्रता से पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे देश में कोई सुनियोजित औद्योगिक नीति नहीं थी। अंग्रेजों की यह नीति थी कि ब्रिटेन का तैयान माल भारत में बेचा जाय और भारत से कच्चा माल इंग्लैण्ड भेजा हमारे देश में 21 अप्रैल, 1945 को औद्योगिक नीति से सम्बन्धित विवरण-पत्र जारी किया गया था, लेकिन 15 अगस्त, 1947 को देश के आजाद होने से यह नीति क्रियान्वित नहीं हो सकी।
1948 की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ 15 अगस्त, 1947 को देश की प्रतिकूल औद्योगिक परिस्थितियों के कारण दिसम्बर, 1947 से औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें औद्योगिक नीति पर जोर दिया। गया। अत 6 अप्रैल, 1948 को भारत के तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने औद्योगिक नीति की निम्नलिखित घोषणा की-
उद्योगों का वर्गीकरण-
इस नीति में उद्योगों को निम्नांकित चार भागों में बाँटा गया हैं-
(i) एकाधिकार औद्योगिक क्षेत्र- इस क्षेत्र में आने वाले उद्योगों की स्थापना केवल केन्द्र सरकार द्वारा की जायगी। इसमें शस्त्रों का निर्माण, परमाणु शक्ति का उत्पादन तथा रेलवे परिवहन को मुख्य रूप से शामिल किया गया।
(ii) मिश्रित क्षेत्र- इस वर्ग में कोयला, लोहा व इस्पात, दवाई, जहाज निर्माण, टेलीफोन, तार और तैयार यन्त्र निर्माण तथा खनिज तेल उद्योग को रखा गया हैं। नीति में यह स्पष्ट किया गया कि विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में रखा जायगा और 10 वर्ष पश्चात् इनकी राष्ट्रीकरण के प्रश्न पर विचार किया जायगा। इस बात का प्रयास किया जायगा कि नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना केन्द्र अथवा राज्य द्वारा ही की जाय।
(iii) सरकारी नियन्त्रण का क्षेत्र-इस क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्त्व के 18 उद्योगों को सरकारी नियन्त्रण में रखा गया हैं। मुख्य रूप से नमक, ट्रैक्टर, भारी रसायन, जल परिवहन, बिजली, इन्जीनियरिंग, सूती वस्त्र, सीमेण्ट आदि उद्योगों को इस क्षेत्र में लिया गया।
(iv) निजी क्षेत्र- अन्य उद्योगों को इस क्षेत्र में रखा गया। इसके उद्योगों पर भी सरकारी नियन्त्रण रहेगा।
- कुटीर एवं लघु उद्योग- देश की अर्थव्यवस्था में इन उद्योगो का महत्वपूर्ण स्थान हैं। सरकार इनके विकास पर पूर्ण ध्यान देगी। इस नीति में यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकार बड़े पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों में समन्वय स्थापित करेगी।
- तटकर नीति- तटकर नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि अनुचित भार डाले बिना विदेशी साधनों का प्रयोग किया जायगा।
- कर नीति- कर नीति बचत को प्रोत्साहित करने वाली तथा सम्पत्ति और आय के केन्द्रीकरण को रोकनेवाली होगी।
- श्रमिकों के लिए मकान-श्रमिकों के हितों के लिए आगामी दस वर्षों में दस लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा।
- विदेशी पूँजी- देश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के उद्देश्य से विदेशी पूँजी की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यह भी ध्यान रखा जायगा कि विदेशी पूँजी के कारण देख के हितों को कोई नुकसान न पहुँचे।
- योजना आयोग की स्थापना- प्रस्तुत नीति में योजना आयोग की स्थापना की बात भी कही गयी।
1948 की औद्योगिक नीति का आलोचना
उपर्युक्त नीति की अनेक प्रकारों से आलोचना हुई। कुछ लोगों ने कहा कि इससे उद्योगपतियों के मन में राष्ट्रीयकरण का भय समा जायगा तथा वह पूँजी विनियोजित करने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। इस नीति में उत्पादन वृद्धि पर भी ध्यान नहीं दिया गया। प्रो० शाह ने कहा कि प्रगतिशील तथा उन्नति की आशा रखने वाले देश को ऐसी नीति नहीं अपनाना चाहिए। वामपन्थियों ने कहा सन् 1948 की औद्योगिक नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं। इस सम्बन्ध में वकील ने कहा कि विशुद्ध पूंजीवाद अथवा विशुद्ध समाजवाद की अपेक्षा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर अमल करना अत्यन्त कठिन होता हैं। इस नीति में प्राथमिकताओं का अभाव हैं।
1956 की भारतीय औद्योगिक नीति
1948 की औद्योगिक नीति के कार्यान्वित होने के बाद देश में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसके अतिरिक्त 1948 की नीति की कुछ कमियाँ भी सामने लायी गयी। देश में संविधान लागू किया गया, पंचवर्षीय योजना का आरम्भ हुआ। औद्योगिक विकास एवं नियमन 1951 लागू हुआ तथा समाजवादी समाज के निर्माण के सिद्धान्त पर भी बल दिया गया। इन्हीं सब सन्दर्भों में एक नवीन औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस की गयी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में कहा कि “आठ वर्षों में भारत में काफी विकास और परिवर्तन हुए हैं, नया संविधान बना हैं, मौलिक अधिकारों के साथ-साथ राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त बने हैं। समाजवादी समाज की रचना के उद्देश्य को माने लिया गया। अत इन सभी बातों तथा आदर्शो सिद्धान्त बने हैं। समाजवादी समाज की रचना के उद्देश्य को मान लिया गया। अत इन सभी बातों तथा आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस बात की अत्यन्त आवश्यकता हैं कि नवीन औद्योगिक घोषित की जाय।”
1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ
- उद्योगों का वर्गीकरण- इस नीति में उद्योगों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया गया था- (i) लोक क्षेत्र- इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य पर रखा गया। लोक क्षेत्र में उन 17 महत्वपूर्ण उद्योगों को रखा जिनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती हैं। इस वर्ग में मुख्य रूप से युद्ध तथा शस्त्र निर्माण, अणुशक्ति का उत्पादन, कोयला, लिगनाइट, खनिज तेल, लौह खनिज, टीन, जिप्सम, सोना, चाँदी, ताँबा, जस्ता, हवाई जहाज, रेलवे, टेलीफोन आदि से सम्बन्धित उद्योगों को रखा गया। (ii) मिश्रित क्षेत्र- इस क्षेत्रमें 12 उद्योगों को रखा गया जिनके विकास के लिए सरकार द्वारा अधिकाधिक प्रयास किये जायेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी पूर्ण प्रोत्साहन दिया जायगा, इन उद्योगों में फर्टीलाइजर, सड़क यातायात, औषधि, रंग-रोगन, प्लास्टिक, नकली रबड़, कोयले से कार्बन गैस के उत्पादन आदि को रखा गया। (iii) निजी क्षेत्र- इस वर्ग में शेष सभी उद्योगों को रखा गया, जैसे-सूती वस्त्र, सीमेन्ट, चीनी आदि। इन उद्योगों की स्थापना तथा संचालन का भार निजी क्षेत्र के ऊपर डाला गया हैं। सरकार ऐसे उद्योगों का विकास करने के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन और सहायता देगी।
- निजी क्षेत्र की सहायता- प्रस्तुत नीति में यह स्पष्ट किया गया हैं कि निजी क्षेत्र के उद्योगों को बिजली, परिवहन तथा अन्य उपायों और सेवाओं द्वारा हर प्रकार की सुविधाएँ और प्रोत्साहन दिया जायगा। लेकिन इस सम्बन्ध में शर्त यह रखी गयी कि निजी क्षेत्र के उद्योगों का विकास सरकार की आर्थिक एवं सामाजिक नीति के अनुरूप होगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जायगा।
- लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास- इस नीति में यह कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए हर प्रकार की सहायता सरकार द्वारा दी जायगी। नीति में औद्योगिक सरकारी समितियों को प्रोत्साहन देने तथा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना द्वारा इन उद्योगों की व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही गयी। यह भी स्पष्ट किया गया कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्त्व के सन्दर्भ में बड़े उद्योगों के उत्पादन को सीमित रखा जायगा।
- सन्तुलित औद्योगिक विकास– सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को औद्योगिकीकरण का लाभ देने के लिए विकास सम्बन्धी असमानता को दूर किया जायगा। सभी क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान दिया जायगा। पिछड़े राज्यों में उद्योगो की स्थापना को प्राथमिकता दी जायगी। यह आवश्कता महसूस की गयी कि लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए उद्योगों और कृषि के सम्मिलित विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- विदेशी पूँजी– प्रस्तुत नीति में विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में अलग से कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। 1949 में प्रधानमंत्री ने विदेशी पूँजी सम्बन्धी जिस नीति की घोषणा की थी, इसी को अपनाने की बात कही गयी हैं।
- औद्योगिक शान्ति- नीति में कहा गया कि श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए उनके कार्य करने की दशाओं में सुधार करना तथा उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाया जाना बहुत जरूरी हैं। सरकार द्वारा औद्योगिक अशन्ति को दूर करने के हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। वास्तव में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक शन्ति की स्थापना होना बहुत जरूरी होता हैं।
1956 की औद्योगिक नीति की आलोचना
1956 की औद्योगिक नीति की अनेक आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर आलोचनाएँ की हैं। फैडरेशन ऑफ इण्टियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स समिति ने कहा था, “यह नीति निजी क्षेत्र के साहस को मन्द कर देगी। इसकी अपेक्षा एक लचीली नीति की आवश्यकता थी, जिससे निजी और सर्वाजनिक क्षेत्र दोनों अपना-अपना योगदान भारत के औद्योगिकीकरण में प्रदान कर सकते हैं।” सामान्यत: इस नीति को निम्नांकित आलोचनाएँ बतायी गयी हैं-
- सरकारी पूँजीवादी को अत्यधिक प्रोत्साहन-सी० एच० भाभा ने कहा हैं कि इस नीति से देश में सरकारी पूँजीवाद का जन्म हो जायगा जिससे निजी क्षेत्र के विकास पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र पर अत्यधिक जोर दिया गया हैं। यदि सभी उद्योगों की स्थापना का दायित्व सरकार की ग्रहरण कर ले तो निजी उद्योग कैसे विकास कर सकेगें?
- राष्ट्रीयकरण की अस्पष्ठ नीति- इस नीति में सरकार ने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की कि राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में उसकी क्या नीति रहेगी। राष्ट्रीयकरण की स्पष्ट नीति की घोषणा न होने के कारण उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में उद्योगपतियों में भय और आशंका का वातावरण बना रहेगा।
1980 की औद्योगिक नीति
औद्योगिक नीति, 1980 की घोषणा उद्योग राज्यमंत्री चरणजीत चन्ना द्वारा 23 जुलाई, 1980 को लोकसभा में की गयी थी।
इस नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं-
- उपलब्ध औद्योगिक क्षमताका सर्वोत्तम उपयोग करना।
- उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना।
- क्षेत्रीय औद्योगिक असन्तुलन दूर करना।
- कृषि सम्बन्धी उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान कर कृषि के आधार को मजबूत बनाना।
- निर्यात बढ़ाने वाले तथा आयात कम करने वाले उद्योगों का तेजी से विकास करना।
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
- आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण लगाना।
- ऊंचे मूल्यों तथा घटिया किस्म की वस्तुओं से उपभोक्तओं की रक्षा करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता में सुधार लाना।
विशेषताएँ
- लघु स्तरीय इकाइयों की नवीन परिभाषा- इस नीति में सरकार ने बहुत छोटी औद्योगिक इकाइयों में विनियोग की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये, लघु क्षेत्र की इकाइयों में विनियोग की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख और सहायक उद्योगों में विनियोग की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख कर दी हैं।
- आर्थिक संघवाद को प्रोत्साहन- इस नीति में कहा गया हैं कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में कुछ ऐसे बीजरूपी संयन्त्र स्थापित किये जायेंगे जिनके कारण उस क्षेत्र में अधिकाधिक मात्रा में सहायक एवं लघु तथा कुटीर उद्योग स्थापित किये जा सकें।
- लाइसेंसिंग पद्धति का सरलीकरण- इस नीति में यह भी कहा गया था कि लाइसेन्स देने की पद्धति को और सरल बनाया जाएगा।
1980 की औद्योगिक नीति की आलोचनाएँ
1980 की औद्योगिक नीति की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती हैं-
- आधारभूत परिवर्तनों का अभाव- आलोचकों का कहना है कि 1980 की औद्योगिक नीति 1956 तथा 1977 की औद्योगिक नीति के समान ही हैं। इसमें कोई विशेष आधारभूत परिवर्तन नहीं किये गये है।
- निजी क्षेत्र का अधिक समर्थन- इस नीति में निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ दी गयी हैं। जैसे राष्ट्रीयकरण न करने का आश्वासन, विदेश सीमा को बढ़ावा आदि। इस प्रकार इस नीति में निजी क्षेत्र को अधिक समर्थन दिया गया है।
- रोजगार पर विपरित प्रभाव-इस नीति में उन्नत तकनीक अपनाने की अनुमति देने की बात कही गयी हैं जिससे पूंजी प्रधान उद्योगों बढ़ावा मिलेगा और इसका रोजगार के साधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
अर्थशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- विदेशी विनिमय दर निर्धारण माँग एवं पूर्ति सिद्धान्त | विदेशी विनिमय की माँग की लोच | विदेशी विनिमय दर के भुगतान शेष सिद्धान्त
- विनिमय नियंत्रण का अर्थ | विनिमय नियंत्रण के तरीके | बहुल विनिमय दरें | विनिमय नियंत्रण के अप्रत्यक्ष तरीके | विनिमय नियंत्रण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके
- मुक्त या स्वतंत्र व्यापार | स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तर्क | संरक्षण का अर्थ | संरक्षण व्यापार के पक्ष में तर्क | सस्ते श्रम का तर्क | संरक्षित व्यापार के सम्बन्ध में शिशु उद्योग तर्क की व्याख्या
- स्थिर बनाम लचीली विदेशी विनिमय दरें | परिवर्तनशील विदेशी विनिमय दरें | स्थिर और लोचशील विनिमय दर के गुण और दोषों
- विदेशी विनिमय दर | क्रय शक्ति समता सिद्धान्त का अर्थ एवं परिभाषा | क्रय शक्ति समता सिद्धांत | विनिमय दर निर्धारण के क्रयशक्ति समता सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन
- अवमूल्यन का अर्थ | अधिमूल्यन | अवमूल्यन के उद्देश्य एवं क्रियाविधि | अवमूल्यन के लोच विधि की सविस्तार व्याख्या
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]