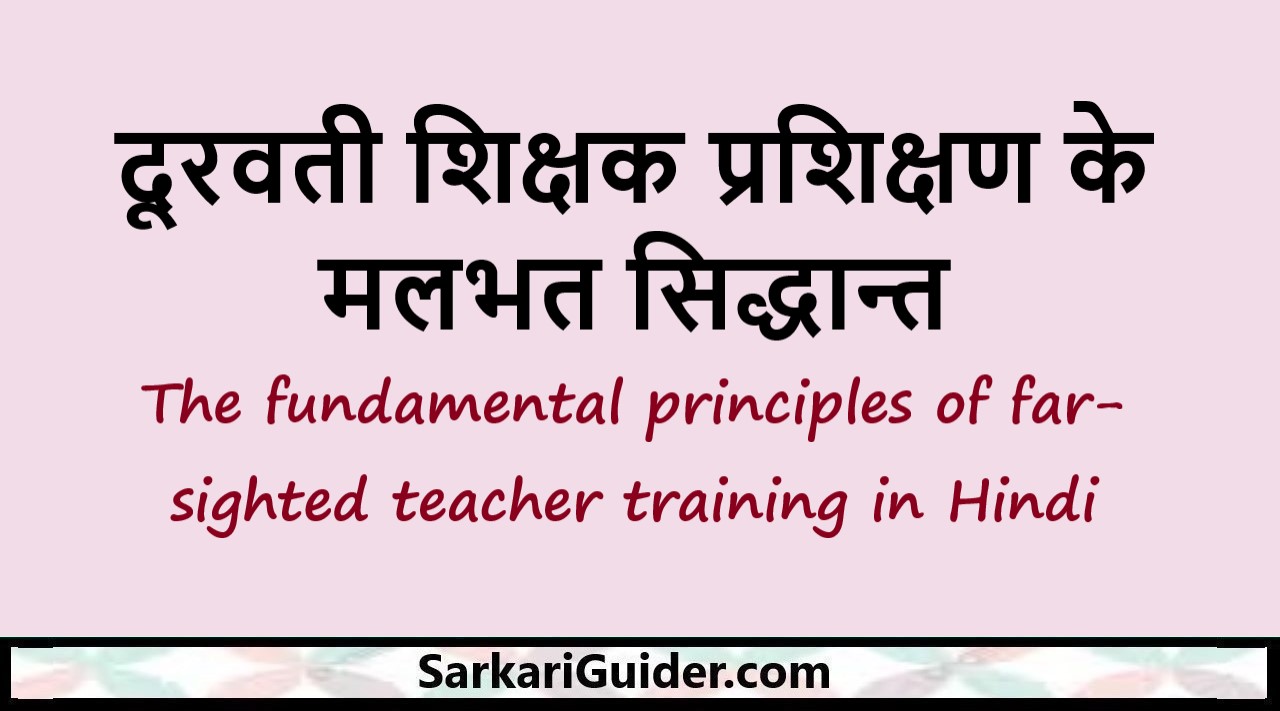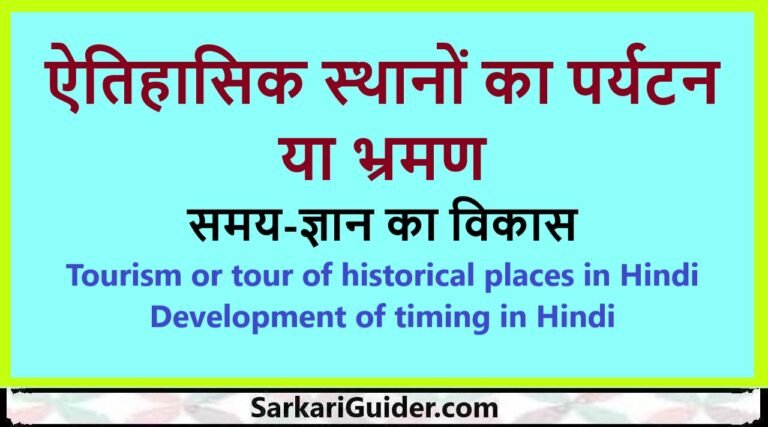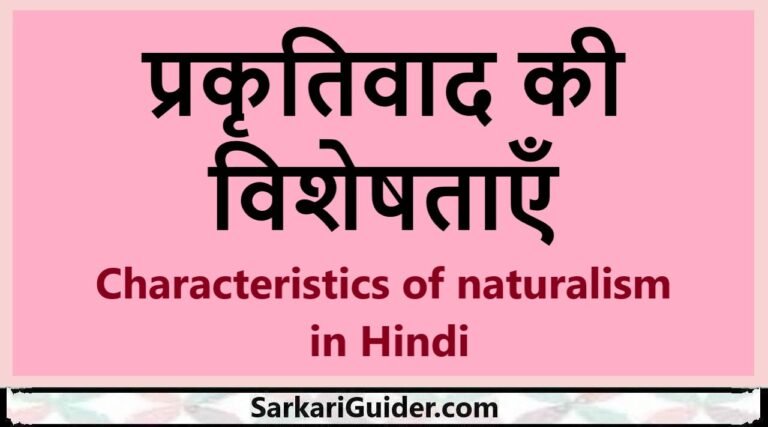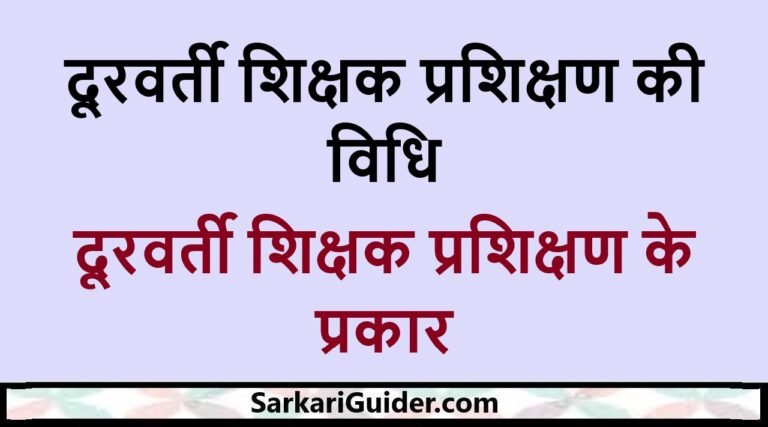दूरवती शिक्षक प्रशिक्षण के मलभत सिद्धान्त | The fundamental principles of far-sighted teacher training in Hindi

दूरवती शिक्षक प्रशिक्षण के मलभत सिद्धान्त | The fundamental principles of far-sighted teacher training in Hindi
दूरवर्ती शिक्षक प्रशिक्षण के मलभत सिद्धान्त-
प्रमुख सिद्धान्त निम्न है-
(i) कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र का पैमानीकरण
(Scaling the Scope of the Programme)-
दूरवर्ती शिक्षा के प्रशिक्षकों एवं शिक्षण संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसके कार्य क्षेत्र के संबंध में निश्चित निर्णय लेना होता है। इससे तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्षेत्र एवं पैमाने की दृष्टि से उपयुक्त एवं पर्याप्त होना चाहिए।
उदाहरणार्थ- एक दूरवर्ती शिक्षा प्रोजेक्ट जिसका मात्र एक ही विशिष्ट उद्देश्य हो, के लिए कार्मिकों की कुशलता प्राप्ति हेतु अधिकतम द्वि-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्याप्त हो सकता है। इसी प्रकार कुछ बड़े पैमाने पर कोई राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी यदि किसी विशेष राष्ट्रीय केन्द्र पर अधिक विस्तृत क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थियों के लिए किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशाला का आयोजन करती है तो इसकी अवधि 8 से 10 दिन तक की हो सकती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पीछे गुणन-प्रभाव (Multiplier-Effect) का उद्देश्य भी हो सकता है क्योंकि बाद में स्थानीय/क्षेत्रीय पर भी प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षक के रूप में उसी तरह की कार्यशालाएँ आयोजित की जा सकती हैं।
(ii) कार्यक्रम के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लाभ
(Short-term and Long-term Advantages of the Programme) –
दूरवर्ती शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में दूसरी महत्त्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात उसके अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लाभ की है। कार्यक्रम के कार्यकषेत्र का पैमानीकरण सम्भवतः इसके उद्देश्यों एवं क्रियाओं को सीमित रखने को बाध्य कर देता है। अतः इससे अल्पकालिक लाभ ही प्राप्त हो पाता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन कार्यक्रमों का क्षेत्र सीमित होने पर भी प्रशिक्षणार्थियों में आगे कार्य करने की अभिप्रेरणा विकसित हो सके अर्थात् इस प्रकार के छोटे पैमाने एवं कार्यक्षेत्र वाले कार्यक्रम दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सरकें। इसी प्रकार दूसरी तरफ विस्तृत कार्यक्षेत्र वाले पैमाने वाले कार्यक्रमों को भी तात्कालिक आवश्यकताओं एवं प्रयोगों पर बल देने की आवश्यकता होती है।
(iii) संस्थागत एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति
(Catering both Institutional and Individual Needs) –
यद्यपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य संस्था के लिए निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जिससे उसे वर्तमान दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली को संचालित करने अथवा इस प्रणाली में संशोधन और सुधार करने हेतु पुनर्बलन मिल सके। किन्तु इस पुनर्बलन का आधार प्रशिक्षण हेतु बढ़-चढ़कर भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थी ही होते हैं। अत: कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशिक्षणार्थियों की व्यक्तिगत संतुष्टि भी आवश्यक है। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से व्यक्तिगत एवं संस्थागत दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पर्ति होनी चाहिए।
(iv) पूर्ति घटित क्रियाओं/घटनाओं को भावी कार्यक्रमों से जोड़ना
(Linking Past Activities/Events with Future Programme)-
जैसा कि पूर्व में कहा जा नका है कि अब प्रशिक्षण की अवधारणा बदल चुकी है तथा इस एक बार प्रशिक्षण’ के स्थान पर जीवन भर सतत् चलने वाली प्रक्रिया माना जाने लगा है। अतः किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूर्व घटित घटनाओं एवं क्रियाकलापों से सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए तथा उसके अन्तर इस प्रकार का क्षेत्र भी निर्मित किया जाना चाहिए जिससे उसे भावी कार्यक्रम से भी जोड़ा जा सके। इस सम्भावना को साकार रूप देने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसी मूल्याकन पद्धति निर्मित की जानी चाहिए जो पश्चात् परिवर्तनों, संशोधनों एवं विस्तारों को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सके। इस प्रकार, इस तरह के उपागम का अन्तिम प्रतिफल सचयात्मक होना चाहिए।
(v) स्वीकार्य एवं अपेक्षित व्यवहारो के प्रतिमान प्रस्तुत करना
(Providing Models of Acceptable and Desirable Behaviour)-
भावात्मक पक्ष की पूर्णता हेतु प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन भी आना चाहिए। ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब प्रशिक्षण के दौरान स्वयं प्रशिक्षकों द्वारा स्वीकार्य एवं अपेक्षित व्यवहार प्रतिमान प्रस्तुत किये जायें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं जैसे- इसकी व्यवस्था, नियोजन, कुशल प्रबन्धन आदि को व्यवहृत रूप प्रदान किया जाना चाहिए तथा प्रशिक्षक को प्रशिक्षणार्थियों के सम्मुख स्वयं प्रशंसनीय व्यवहार का जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- दूरदर्शन | दूरदर्शन का शैक्षिक उपयोग | दूरदर्शन का गुण तथा दोष | शैक्षणिक टेलीविजन की प्रमुख योजनाएँ
- ओवर हेड प्रोजेक्टर | OHP की कार्यप्रणाली | OHP की संरचना | ओवर-हेड प्रोजेक्टर की विशेषतायें
- ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग | ओवरहेड प्रोजेक्टर के लाभ
- रेडियो | भारत में शैक्षिक रेडियो का विकासात्मक इतिहास | रेडियो के उपयोग | रेडियो द्वारा शिक्षण | शैक्षिक समाचारों में रेडियो
- वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कम्प्यूटर का प्रयोग | Use of computer in current education system in Hindi
- टेलीकांफ्रेंसिंग का अर्थ | टेलीकांफ्रेंसिंग के प्रकार | The meaning of teleconferencing in Hindi | Types of teleconferencing in Hindi
- शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर का प्रयोग | Use of computer in the field of education in Hindi
- पाठ्यक्रम का अर्थ | दूरवर्ती शिक्षा मे पाठ्यक्रम विकास के आवश्यक तत्त्व
- पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया | पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान
- अनुदेशनात्मक सामग्री की इकाई संरचना | Unit Structure of Instructional Material in Hindi
- अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री | अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री की विशेषतायें
- इण्टरनेट का अर्थ | इंटरनेट के उपयोग | The meaning of internet in Hindi | Uses of Internet in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]