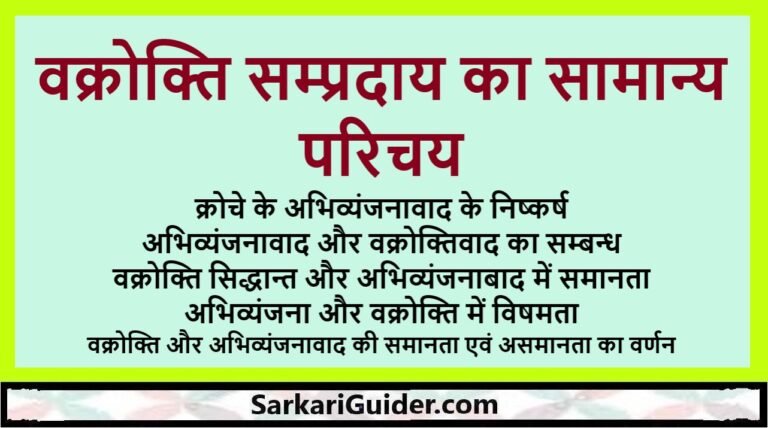राजभाषा एव राष्ट्रभाषा | संचार भाषा | सम्पर्क भाषा
राजभाषा एव राष्ट्रभाषा | संचार भाषा | सम्पर्क भाषा
राजभाषा एव राष्ट्रभाषा
राजभाषा-
दीर्घकालीन संघर्ष के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 1 के अनुसार संघ की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। भारतीय संविधान में हिन्दी को भी राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। उसे संघ की राजभाषा या संघ की भाषा घोषित किया गया है। इस घोषणा के बाद राष्ट्रभाषा का तात्पर्य बदल गया। राष्ट्र की जितनी भाषाएँ हैं, वे सभी राष्ट्रभाषाएँ हैं। सम्पर्क भाषा या राजभाषा या संघ की भाषा है हिन्दी। संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हो गया किन्तु हिन्दी राजभाषा के रूप में तत्काल लागू नहीं की गई। संविधान में ही उल्लेख कर दिया गया था कि राजभाषा के रूप में अंग्रेजी 15 वर्षों तक चलती रहेगी। तत्पश्चात् उसके स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। इस कालावधि में राष्ट्रपति आदेश के द्वारा राजकीय प्रयोजनों में से किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। इस अवधि के पश्चात् भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जैसा कि ऐसी विधि में उल्लिखित है। (अनुच्छेद 343 (3))। अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति इस अविध को शिथिल कर देती है। इसके दुरुपयोग की सम्भावना थी ही जो बाद में प्रत्यक्ष हुई। अनुच्छेद 344 राजभाषा के लिए आयोग बनाने का प्राविधान करता है।
राष्ट्रभाषा
राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र राष्ट्र नहीं कहला सकता। जिस प्रकार किसी राष्ट्र की सीमाएँ, सीमाओं के अन्तर्गत पड़नेवाले भूखंड, देशवासी तथा संस्कृति महत्वपूर्ण हैं उसी प्रकार राष्ट्र के विचारों की संवाहिका सामान्य राष्ट्रीय भाषा भी आवश्यक है। डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा में राजनीतिक एकता अपने आप में महत्व शून्य और बेमानी है यदि राष्ट्र के हृदय एक नहीं हो पाता। हृदय की एकता तब तक असम्भव है जब तक वाणी की एकता न हो। यदि एक व्यक्ति दूसरे की बात समझ ही नहीं पाता तो एकता का अनुभव कैसे हो सकता है। एक राष्ट्र का दो आदमी अपनी भाषा में बात न करे यह लज्जा की बात है। ‘टावर ऑफ वैवन’ की कथा की ओर संकेत करे हुए भाषा की एकता की महत्ता आचार्य क्षितिमोहन सेन ने भी प्रतिपादित की है-‘आदर्श और साधना की एकता मनुष्य को एकता जरूर देती है, परन्तु भाषा की भिन्नता मनुष्य की इस एकता को जाग्रत नहीं होने देती। यूरोपीय प्राचीन कथा में सुना जाता है कि भाषा की मित्रता के कारण ही, ‘टावर ऑफ वैबन’ टूट पड़ा था, और वही मनुष्य जो इस महती साधना के लिए दिन-रात एक कर रहे थे, ‘भाषा की भिन्नता के कारण आपस में ही लड़ने लगे थे और उन्होंने अपनी ही निर्माण की हुई वस्तु को स्वयं ही गिरा दिया था।
भारत बहुभाषाई राष्ट्र है। जिन 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है उनके अलावा भी कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जो अपने स्वतन्त्र अस्तित्व का दावा करती हैं।
संचार भाषा
संचार भाषा- आज का युग सूचना क्रान्तिकारी भाषा इच्छाओं, भावों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचने का मुख्य साधन भाषा मुख्यता वाक् व्यापार है। दो या अधिक व्यक्ति आमने-सामने वार्ता करके विचारों का आदान-प्रदान करते हैं यदि वक्ता और श्रोता दूर स्थित हों तो सीधे सम्पर्क करना सम्भव नहीं होता। यदि व्यक्ति अपने विचारों को दूर-दूर तक फैलाना चाहता है उसे स्थायी बनाना चाहता है तो उसे संचार के अन्य साधनों का उपयोग करना पड़ता है। प्राचीनकाल से ही हस्तलेखों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा पत्रों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावों, मान्यताओं को स्थाई बनाने का प्रयत्न करता रहा है। वर्तमान समय में संचार के दो प्रमुख माध्यम हैं-
(1) मुद्रित माध्यम (2) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम।
- मुद्रित माध्यम-इसमें पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम-इसमें रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि को सममाध्यम किया जा सकता है।
सम्पर्क भाषा
सम्पर्क भाषा- भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा के रूप में इसके वास्तविक प्रयोग की स्थितियां विवादास्पद हैं लेकिन बहसंख्यक की भाषा होने के कारण हिन्दी केवल हिन्दीभाषी राज्यों के नागरिकों के बीच ही सम्पर्क का काम नहीं करती बल्कि हिन्दीतर प्रान्तों में भी लोग हिन्दी को ही सम्पर्क का माध्यम बनाते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कटक से अमृतसर, बीकानेर तक यदि किसी भाषा में विचारों-भावों का आदान-प्रदान हो सकता है तो वह भाषा है हिन्दी। हिन्दी निश्चित रूप से सम्पर्क का कार्य कर रही है। एक बंगला भाषी जब तमिलनाडु जाता है तो वह यदि किसी भारतीय भाषा के सहारे अपना कार्य व्यापार सम्पन्न करना चाहता है तो उसे हिन्दी का व्यवहार करना पड़ता है। भारत के बड़े व्यवसायिक नगरों में हिन्दी का बहुत अधिक प्रचलन है। बम्बई और कोलकाता में तो ऐसा लगता है कि हम हिन्दी प्रदेश के किसी महानगर में हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के कोने-कोने से लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। दिल्ली में आम व्यवहार की भाषा हिन्दी ही है। भारत के तीर्थों में और पर्यटक स्थलों में हिन्दी का ही बोलबाला है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम्, द्वारिका आदि तीर्थों में विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच सम्पर्क का काम हिन्दी ही करती है। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी अपनी भूमिका सम्यक् निर्वाह कर रही है। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी अपनी भूमिका का सम्यक् निर्वाह कर रही है। सम्पर्क भाषा के रूप में इसे जनसाधार में स्वयम् अपनाया।
हिन्दी – महत्वपूर्ण लिंक
- काव्यभाषा का स्वरूप | काव्यभाषा एवं सामान्य भाषा में अन्तर
- काव्य में बिम्ब-विधान | काव्य बिम्ब का कार्य या उद्देश्य | बिम्ब के गुण एवं तत्व | बिम्बों का वर्गीकरण
- प्राचीन भारतीय आर्य भाषा | वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में साम्य एवं वैषम्य | वैदिक और लौकिक संस्कृत में अन्तर
- पालि भाषा की व्युत्पत्ति | पालिभाषा का प्रदेश | पालि-साहित्य | पालि की विशेषताएं
- परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ठ | अवहट्ठ की विशेषताएं | अवहट्ट भाषा की भाषिक विशेषताएँ | अवहट्ट भाषा की व्याकरणिक विशेषताएँ
- राष्ट्रभाषा हिन्दी की समस्याएँ | राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का भविष्य
- प्रतीक का उद्भव एंव विकास | प्रतीक का अर्थ | प्रतीकों का वर्गीकरण | प्रतीक योजना का आधार | काव्य में प्रतीकों का महत्व
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]