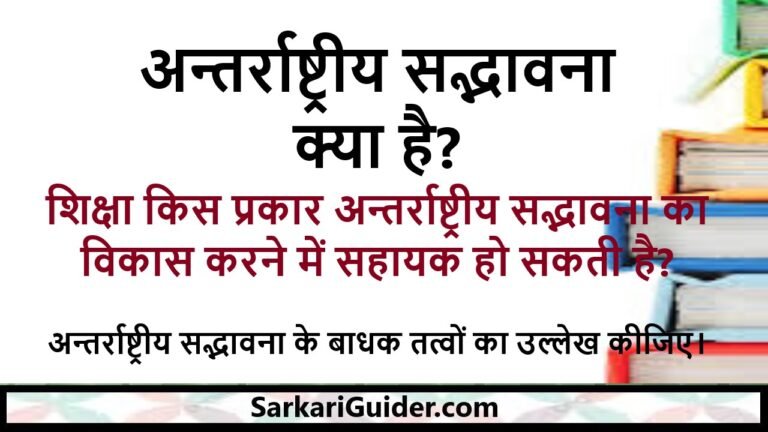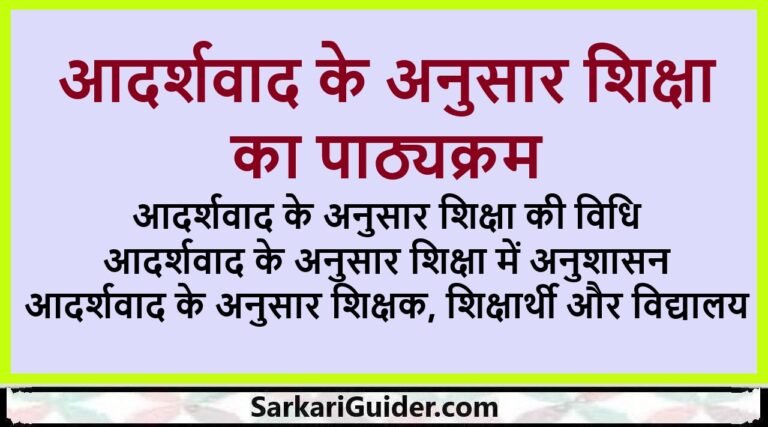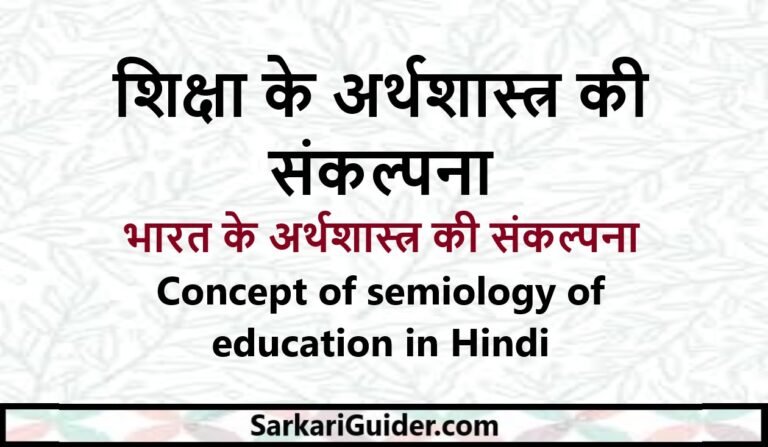सामाजिक स्तरीकरण और शिक्षा | सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ | सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषाएँ | सामाजिक स्तरीकरण के आधार
सामाजिक स्तरीकरण और शिक्षा | सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ | सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषाएँ | सामाजिक स्तरीकरण के आधार
सामाजिक स्तरीकरण और शिक्षा
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का संगठन व्यक्तियों और उसके द्वारा बनाई हुई संस्थाओं से होता है। ऐसी संस्थाएँ समाज की इकाइयाँ होती हैं। ये इकाइयाँ समाज के स्तर को भी प्रकट करती हैं। इन इकाई-संस्थाओं का परस्पर अपना ऊपर-नीचे स्थान पाया जाता है, तथा तदनुकूल उनके सदस्यों की भी सामाजिक संस्थिति (Social status) बन जाती है। जब इस प्रकार की स्थायी संरचना हो जाती है तो वहाँ सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है अर्थात् समाज की विभिन्न इकाइयों को ऊपर-नीचे स्थान दे दिया जाता है। अब स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयों को निश्चित स्थान देने में पाया जाता है।
सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ
संसार के सभी समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक रचना का एक अन्तरंग है। सामाजिक स्तर एक प्रकार से समाज की विभिन्न स्थिति होती है। इसके कारण लोगों में उच्च स्थिति प्राप्त करने की जिज्ञासा पाई जाती है। व्यक्ति नीचे से ऊपर के स्तर पर हमेशा उठने का प्रयास करता है जिससे व्यक्ति और समाज दोनों- प्रगति करते हैं। समाज में विभिन्न प्रतिभा, ज्ञान, कौशल, व्यक्तित्व, शिक्षा वाले लोग होते हैं। सभी लोग अपनी विशेषताओं के आधार पर समाज के विभिन्न स्तर (Different Strata) का निर्माण करते हैं। ऐसी दशा में सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक संरचना और संगठन से सम्बन्धित एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण समाज के सभी लोग अपनी योग्यता, क्षमता एवं स्थिति के अनुकूल कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
ऊपर के विचारों से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज को विभिन्न स्तरों पर बाँट कर कार्यों को पूरा कराने के लिए एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न इकाइयों में सहयोग एवं एकीकरण स्थापित किया जाता है और उससे समाज की समग्रता स्थापित रहती है, विघटन की सम्भावनाएँ दूर होती हैं।
सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषाएँ
सामाजिक स्तरीकरण की कुछ परिभाषाओं को देकर हम उसके अर्थ को और भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। नीचे ये परिभाषाएँ दी जा रही हैं-
(i) प्रो० रेमण्ड मुरे- “स्तरीकरण समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया क्षैतिजीय विभाजन है।”
(ii) प्रो० जिस्बर्ट- “सामाजिक स्तरीकरण समाज के स्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजन हैं जो अधीनता के सम्बन्ध से परस्पर जुड़े होते हैं।”
(iii) प्रो० फेयरचाइल्ड- “सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक तत्व की विभिन्न क्षैतिजीय पर समूहों में एक व्यवस्था है तथा विभिन्न मात्रा में पाई जाने वाली उच्चता और निम्नता के रूप में संस्थिति की स्थापना है।”
(iv) प्रो० कार्ल मार्क्स- सामाजिक स्तरीकरण को सामाजिक वर्ग विभाजन कहा जाना चाहिए। यह आर्थिक संस्थिति होती है जो सामाजिक स्तरीकरण का आधार है।
सामाजिक स्तरीकरण के आधार
सामाजिक स्तरीकरण किन आधारों पर किया जाता है, इस ओर ध्यान देने से हमें नीचे लिखे आधार मिलते हैं। इन्हीं के कारण समाज में ऊँच-नीच, धनी-निर्धन, शासक- शासित, ज्ञानी-व्यापारी आदि पाये जाते हैं। ऐसे आधार निम्न रूप में दिए गए हैं-
(i) जैविक आधार (Biological Basis)- जैविक आधार का तात्पर्य जन्म से प्राप्त तत्वों से है। इसके अन्तर्गत लिंग, वायु एवं स्वास्थ्य रखा जा सकता है। स्त्री एवं पुरुष दो लिंग पाए जाते हैं। समाज की संस्कृति के अनुकूल इन्हें ऊँचा-नीचा, समान पद मिलता है। इसी प्रकार से आय के अनुरूप शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़,वृद्ध के पद पर व्यक्ति रखा जाता है और आयु से सम्बन्धित अनुभव के आधार पर क्रम तथा स्थान मिलता है। स्वास्थ्य के आधार पर निर्बल एवं सबल होते हैं और “जिसकी लाठी उसकी भैस” वाली कहावत चरितार्थ होती है।
(ii) आर्थिक आधार- सामाजिक स्तरीकरण अर्थ विभाजन के अनुसार भी होता है। पूँजीवादी, सर्वहारा, गरीब और अमीर, निम्न, मध्यम एवं उच्च स्तरीय व्यक्ति समाज में पाये जाते हैं। सभी देश में यही स्थिति है, साम्यवादी देशों में यद्यपि भेद मिटाया गया फिर भी सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है।
(iii) राजनीतिक आधार- राजनीतिक सत्ता एवं प्रभुता के आधार पर ऐसा स्तरीकरण होता है। इससे राजा, प्रजा, शासक, शासित, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सहायक मन्त्री आदि होते हैं। इनमें उच्च-निम्न का क्रम पाया जाता है। अतः इसे राजनीतिक आधार पर बना स्तरीकरण कहा जाता है। प्रत्येक कार्य को अलग-अलग स्तर देने से उन पर कार्य करने वालों का स्तरीकरण हो गया है तथा उनमें ऊँचे-नीचे स्थान तथा सम्मान मिलता है।
(iv) प्रजाति, वर्ण और जाति का आधार- सभी देश में एक, दो और अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए अमरीका में अमरीकी, नीग्रो, आंग्ल, फ्रेन्च, जर्मन आदि प्रजातियाँ हैं। अतएव इनके बीच विभाजन सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से भारत में आर्य एवं द्रविण प्रजातियाँ हैं। प्राचीन प्रथा के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र वर्ण हैं और अब बहुत-सी जातियाँ इन वर्गों से प्रादुर्भूत हो गई हैं तो दूसरी उससे नीची है। अपने देश में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों, ऊँची जातियाँ बन गई हैं।
(v) धर्म का आधार- भारत में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि धर्म प्रचलित हैं और इनके कारण समाज के कई स्तर बने हुए हैं। प्रत्येक धर्म के मानने वालों में भी कई स्तर पाए जाते हैं जो एक दूसरे से ऊँचे या नीचे गिने जाते हैं और सभी का पद एवं स्थान स्थायी रूप से निश्चित हो गया है। यहाँ भी सामाजिक स्तरीकरण दिखाई देता है।
(vi) शिक्षा का आधार- औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पाकर लोगों में जो अन्तर आता है उससे सामाजिक स्तरीकरण का बोध होता है। समाज में हाई स्कूल, बी० ए०, एम० ए० पास लोगों के अलग-अलग स्तर हैं। चिकित्सा, इन्जीनियरिंग, अध्यापकीय, वकीली, वाणिज्यीय अथवा तकनीकी एवं कौशल सम्बन्धी शिक्षा पाए लोगों का भिन्न-भिन्न वर्ग-स्तर पाया जाता है। अपने-अपने कार्य को ऊँचा- नीचा मानना स्वभाव है, फिर भी समाज की दृष्टि में अध्यापक जैसे स्तर के लोग नीचे ही गिने जाते हैं। वकील को ऊँचा स्थान देते हैं। डाक्टर और भी ऊँचे पद पर रखा जाता है। यह शिक्षा का आधार ही है जिसके फलस्वरूप सामाजिक स्तरीकरण होता है।
(vii) निवास स्थान का आधार- सामाजिक स्तरीकरण का आधार निवास स्थान भी होता है। शहर के लोगों को ऊँचा स्तर मिलता है, गाँव के निवासियों को नीचा । शहर में भी गली-कूचों, गन्दी बस्तियों के निवासियों को सिविल लाइन्स और विकसित क्षेत्रों के रहने वालों से हमेशा नीचे स्तर पर रखा जाता है। अस्तु सामाजिक स्तरीकरण होना अनिवार्य होता है।
(viii) सांस्कृतिक आधार- सामाजिक जीवन की विधि वास्तव में संस्कृति कहलाती है। अतएव आर्थिक एवं राजनीतिक, व्यावसायिक एवं व्यावहारिक, आचरणिक एवं नैतिक आधार पर जो कार्य-कलाप सम्पन्न होते हैं उनसे भी सामाजिक स्तरीकरण होता है। उदाहरण लिए रिक्शे वाला या मजदूर “बाबू जी”, “मालिक”, “साहब” आदि शब्द का प्रयोग उच्च पद के लिए करता है जो कुछ विशेष लोगों की संस्कृति की ओर संकेत करता है अतः स्पष्ट है कि सांस्कृतिक आधार पर भी सामाजिक स्तरीकरण होता है।
भारतीय समाज भी उपर्युक्त आधारों पर स्तरित है। यहाँ पर विभिन्न प्रजाति (आर्य, द्रविण आदि), जाति, व्यवसाय, धर्म एवं संस्कृति या आचार-विचार वाले व्यक्ति अपना समाज बनाए हुए हैं। गाँव और शहर के समाज भी अलग-अलग हैं। शिक्षित और अशिक्षित समाज के स्तर पाए जाते हैं।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- जनतंत्र और शिक्षा | शिक्षा में जनतंत्र का अर्थ | जनतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता | जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य
- भारतीय जनतंत्र की शिक्षा | जनतंत्र को शिक्षा द्वारा सफल बनाना
- शिक्षा के मूल्य | मूल्य का तात्पर्य | मूल्य, मूल्यों और मूल्यांकन
- शैक्षिक समाजशास्त्र | शिक्षा का समाजशान | शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा | शैक्षिक समाजशास्त्र का विषय-विस्तार
- संस्कृति और शिक्षा | संस्कृति का अर्थ | संस्कृति की परिभाषाएँ | संस्कृति की विशेषताएँ | संस्कृति के सिद्धान्त | संस्कृति और शिक्षा
- संस्कृति और शिक्षा का सम्बन्ध | संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव | शिक्षा का संस्कृति कर प्रभाव
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]