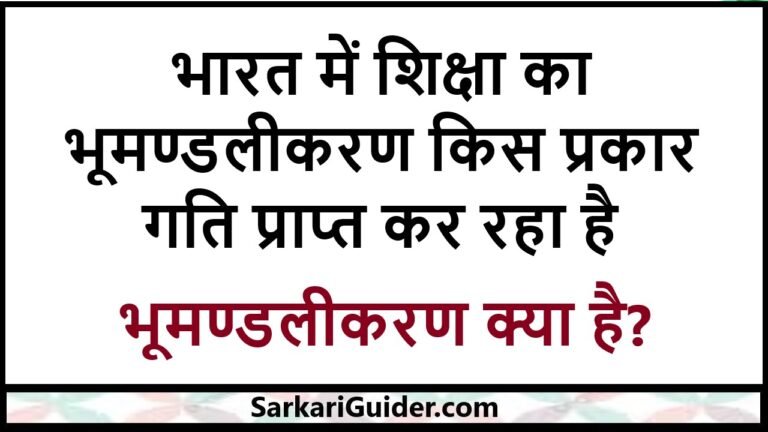प्रकृतिवाद के सिद्धान्त | Principles of naturalism in Hindi

प्रकृतिवाद के सिद्धान्त | Principles of naturalism in Hindi
प्रकृतिवाद के सिद्धान्त
प्रकृतिवाद में कुछ प्रमुख सिद्धान्त मिलते हैं जिन पर भी प्रकाश डालना चाहिए। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :-
(i) प्राकृतिक रचना का सिद्धान्त – इस सिद्धान्त के अनुसार प्रकृति ही संसार का कर्ता, धर्त्ता एवं हर्ता है, उसका मूल कारण एवं परिणाम है। संघटन-विघटन के सिद्धान्त पर यह जगत रचा गया है। जैसे पानी से बर्फ और बर्फ से पानी वैसे ही जीवन-मरण की कहानी है।
(ii) भौतिक पदार्थों का सिद्धान्त- इस सिद्धान्त के अनुसार केवल भौतिक पदार्थों से बना जगत सत्य है, कोई आध्यात्मिक जगत नहीं होता जैसा कि आदर्शवाद कहता है। इस सिद्धान्त के लिए विज्ञान की खोज प्रमाण स्वरूप दी जाती है जिसके अनुसार पदार्थ न कभी बनता है, न कभी नष्ट होता है, उसका रूप केवल बदल जाता है। अतः भौतिक पदार्थ शाश्वत और सत्य है।
(iii) क्रमिक विकास का सिद्धान्त- प्रकृतिवाद इस सिद्धान्त में विश्वास करता है। प्रकृति की विशेषता है कि पर्यावरण के प्रभाव स्वरूप वह बढ़ती है। यह विकास जीवों को एक क्रम से विकसित हुआ समझता है और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ विकसित रूप प्रदान करता है।
(iv) ज्ञानेन्द्रियों का सिद्धान्त- प्रकृतिवाद के अनुसार सभी ज्ञान और अनुभव ज्ञानेन्द्रियों से मिलते हैं। ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष, सरल एवं स्थायी होता है।
(v) सुखपूर्ण जीवन सिद्धान्त- सभी प्राणी सुख से रहना चाहते हैं, विशेष कर मनुष्य। सुख-भोग का अर्थ अपनी रक्षा और इन्द्रियों को सन्तुष्ट रखना है। चार्वाक के सिद्धान्त में यही धारणा पायी जाती है।
(iv) प्राकृतिक नियमों के पालन का सिद्धान्त- मनुष्य यदि सुखपूर्ण जीवन चाहता है तो उसे प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। सरलता व सादगी का नियम, स्वतन्त्र क्रियाशीलता का नियम, पर्यावरण एवं परिस्थिति के साथ अनुकूलता का नियम, सन्तोष का नियम, इनके पालन से जीवन सुखी बनता है।
(vii) भौतिकता का सिद्धान्त- इसके अनुसार मनुष्य का विश्वास ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, अलौकिकता में नहीं होता है। धर्म और आध्यात्म में भी विश्वास नहीं रहता है केवल भौतिक चीजों को मान्यता दी जाती है।
(viii) सामर्थ्यवादी सिद्धान्त – प्रकृतिवाद इस बात पर बल देता है कि मनुष्य को अपने आपको प्रकृति के अनुकूल कार्य करने एवं जीवन रखने के लिए कुछ सामर्थ्य या क्षमता प्राप्त करना जरूरी है जैसे आत्म-रक्षा का सामर्थ्य, जीवन-यापन का सामर्थ्य, पर्यावरण से समायोजन का सामर्थ्य, परिस्थितियों पर नियंत्रण का सामर्थ्य तथा सभी के साथ अनुकूल व्यवहार का सामर्थ्य ।
(ix) व्यावहारिक सत्ता का सिद्धान्त- यह सिद्धान्त मनुष्य समाज के लिए रूसो जैसे प्रकृतिवादी द्वारा बताया गया है। समाज और राज्य की व्यावहारिक सत्ता मिलती है जिससे मनुष्य अपना जीवन धारण करता है, जीवन व्यतीत करता है, शिक्षा लेता है और आगे बढ़ता है। समाज एवं राज्य व्यक्ति के हित का व्यावहारिक रूप से ध्यान देवें, ऐसा सिद्धान्त प्रकृतिवादियों को मान्य है।
(x) प्रकृति की ओर लौटो’ का सिद्धान्त- रूसो और अन्य प्रकृतिवादियों का यह कहना था कि मनुष्य अपने विकास, सुख, शान्ति एवं शक्ति प्राप्ति के लिए प्रकृति की ओर लौटे। मनुष्य की सभ्यता उसे इनसे अलग किये है। अतएव प्रकृति में रहकर, प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत कर, प्राकृतिक सुख-सौंदर्य को प्राप्त कर अपने सरल रूप में यदि मनुष्य जीवन व्यतीत करे तो उसे कभी भी न दुःख होगा, न कोई कष्ट होगा।
(xi) प्रकृति के भ्रष्टा द्वारा अच्छे निर्माण का सिद्धान्त- प्रकृतिवाद के मानने वालों का विश्वास था कि प्रकृति के स्रष्टा के हाथों से आने वाली प्रत्येक वस्तु अच्छी है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति के चीजें सुन्दर और लाभदायक हैं। जैसे फूल है जो दवाओं, पूजापाठ, श्रृंगार एवं सजावट के काम आते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार अन्य पदार्थ भी अच्छे व उपयोगी होते हैं। अतः प्रकृति के साथ हमें रहना चाहिए और अच्छाई ग्रहण करना चाहिए। मानव भी जन्म से अच्छा होता है लेकिन समाज के दूषित वातावरण से उसकी अच्छाई-बुराई में बदल जाती है। शिशु किसी से बैर नहीं रखता लेकिन बड़ा मनुष्य पड़ोसी से दुश्मनी मोल ले लेता है। यही प्रकृति के स्रष्टा द्वारा दी गयी अच्छाई का महत्व मिलता है।
(xiii) शिक्षा को प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए का सिद्धान्त- शिक्षा मानव विकास की उत्तम प्रक्रिया है। इसलिए उसे भी प्रकृति के नियम, प्रकृति के साधन, प्रकृति की वस्तुओं एवं तौर-तरीकों का पालन करना चाहिए। इसका तात्पर्य है शिक्षा मनुष्य को जन्मजात शक्तियों, रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार दी जानी चाहिए। शिक्षा का तात्पर्य इनके विकास से हो, शिक्षा का उद्देश्य स्वाभाविक क्षमताओं का विकास, स्वतंत्र विकास एवं समरूप विकास हो । शिक्षा विधियाँ एवं वस्तुएँ प्राकृतिक और स्वाभाविक, रोचक और सुखद हों। शिक्षा का पाठ्यक्रम भारस्वरूप न होकर रुचि और आनन्द देने वाला हो, जीवनोपयोगी हो, क्रियापूर्ण हो । विद्यालय “बच्चा का बाग” सदृश्य हो । अध्यापक उद्यान के माली सदृश्य सहायता देने वाला, रक्षक एवं प्रेम करने वाला व्यक्ति हो। ऐसे वातावरण में “प्रकृति का अनुसरण” होगा।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- शिक्षा-दर्शन | शिक्षा का तात्पर्य | दर्शन का तात्पर्य
- शिक्षा दर्शन का तात्पर्य | दर्शन और शिक्षा दर्शन में अन्तर | शिक्षा दर्शन का कार्य
- शिक्षा दर्शन के उद्देश्य | शिक्षा दर्शन की आवश्यकता
- आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम | आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा की विधि | आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा में अनुशासन | आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यालय
- प्रकृतिवाद का तात्पर्य | प्रकृतिवाद और भौतिकवाद | भौतिकवाद का तात्पर्य | भौतिकवाद तथा प्रकृतिवाद में समानता | भौतिकवाद या पदार्थवाद: भारतीय व पाश्चात्य दृष्टिकोण
- प्रकृतिवाद की विशेषताएँ | Characteristics of naturalism in Hindi
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]