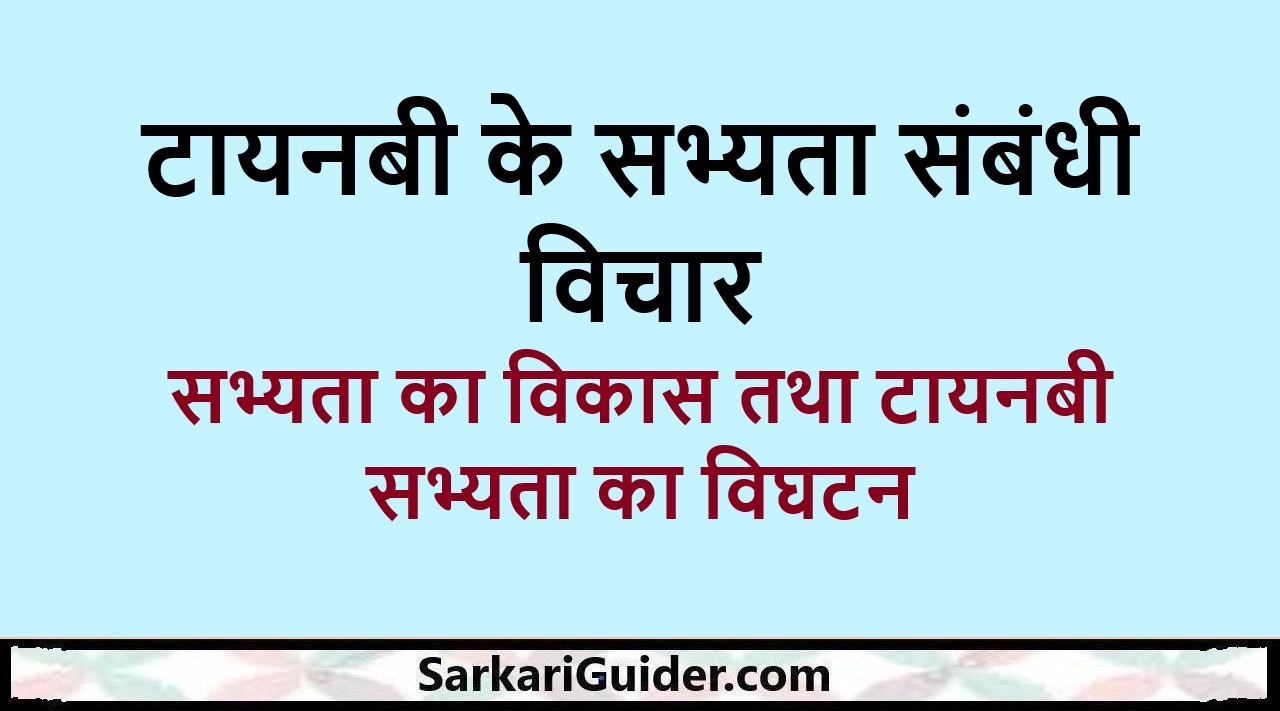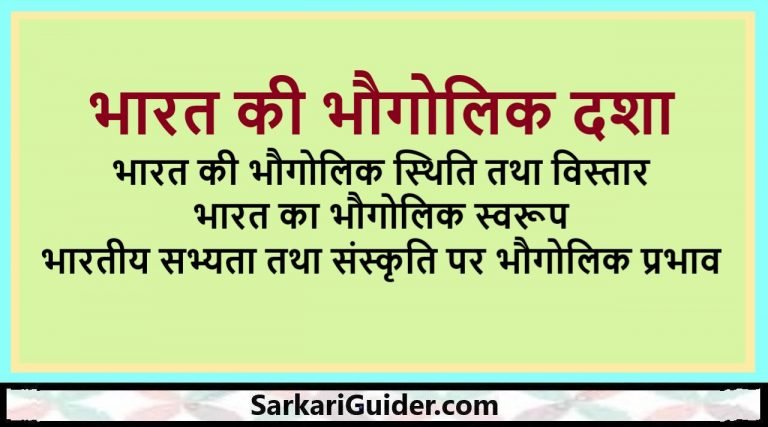टायनबी के सभ्यता संबंधी विचार | सभ्यता का विकास तथा टायनबी | सभ्यता का विघटन

टायनबी के सभ्यता संबंधी विचार | सभ्यता का विकास तथा टायनबी | सभ्यता का विघटन
टायनबी के सभ्यता संबंधी विचार
टॉयनबी का मत है कि सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास भौतिक अथवा भौगोलिक परिवेश का परिणाम नहीं है। वे वास्तव में एक अपरिभाष्य तत्त्व का परिणाम हैं, जो ‘ऊपरी तौर से मनोवैज्ञानिक प्रकार का है। अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये टॉयनबी पुराण का आश्रय लेता है, ‘प्लेटो ने मुझे सिखाया कि विज्ञान और मिथक दोनों का एक साथ प्रयोग अवांछनीय नहीं है। हमें एक क्षण के लिये वैज्ञानिक सिद्धान्तों के प्रति अपनी आँखें मूंद लेनी चाहिए ताकि हम पुराणों की भाषा सुन सकें।’
‘सभ्यताओं की उत्पत्ति का कारण कोई एक नहीं बल्कि अनेक हैं, यह अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं एक सम्बन्ध है।’ सृष्टि दो अलौकिक व्यक्तित्यों के मिलन, उनकी अन्तः क्रियाओं का परिणाम है। हर बार यह योजना एक पूर्ण भिन्न राज्य के रूप में फलीभूत होती है। यह यांग से होकर क्यों गुजरती है? ‘किसी बाह्य प्रेरणा या शक्ति के वशीभूत होकर’ : एडम और ईव की निश्चित दुनियाँ में शैतान का प्रवेश फाउस्ट की दुनियाँ में मेकिस्टो का प्रवेश जो कि ज्ञान के क्षेत्र में पूर्ण है या पौराणिक भाषा में दैवी सृष्टि में शैतान की घुसपैठ। फाउस्ट का न्यू स्टेटामेंट के अन्तर्गत, शैतान की विजय का निश्चित रूप से निषेध है। ज्यादा से ज्यादा वह ईश्वर का उद्देश्य पूरा करता है। लेकिन यह कहना है कि शैतान का प्रलोभन ईश्वर को सृष्टि की पुनर्रचना का अवसर देता है। इस तरह यिन ने यांग तक का दौर पूरा होता है। इस नाटक का सारांश व्यक्ति की अग्नि-परीक्षा है; स्वर्ग में तो मात्र इसकी तैयारी ही होती है। अतः अगला चरण इस संकट का समाधान होता है जब व्यक्ति सजग रूप से ईश्वर की इच्छा का माध्यम बन जाता है। यह वश्यता एक और ब्रह्माण्डीय परिवर्तन लाती है और परिणाम फिर एक यिन राज्य के रूप में प्रकट होता है।
टॉयनबी को पुराणीकरण से दूर रखते हुए या उसकी भाषा में मिथकों की प्रतिमावली को पुनअनुदित’ कहते हुए यह कहा जा सकता है कि उत्पत्ति का कारण एक अन्तः क्रिया है। चुनौती विरोध और अनुक्रिया के इस विचार को लागू करने के लिए व्यक्ति का उसके वातावरण के संदर्भ में पुनः अध्ययन किया जाता है। जाति और वातावरण को एक नए संदर्भ में समझा जा सकता है क्योकि एक अज्ञात तत्त्व ऐसा होता है जो सर्वाधिक सचेत व्यक्तियों की अवज्ञा करता है। तत्पश्चात् हमें विभिन्न सभ्यताओं की उत्पत्ति के विषय में पता लगता है। उदाहरण के लिये मिस्त्र की सभ्यता का जन्म अफ्रीकी एशियाई मरुस्थल शुष्कन की चुनौती के फलस्वरूप विकसित हुई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुपयुक्त भौगोलिक स्थितियाँ अधिक समक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। ‘सौन्दर्य पूर्ण दुःसाध्य होता है यह स्थिति सभ्यताओं के लिये भी विरोधी है। कठिन परिस्थितियाँ कई तरह से लाभकारी सिद्ध होती हैं। ‘उदाहरण के लिए पीली नदी नौ-संचालन के लिये दुःसाध्य है और सामान्यतः यांगत्सी से अधिक कठिनाइयाँ पैदा करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पीली नदी के मुहाने पर भी सिकिन सभ्यता फली-फूली। नए धरातल भी प्रेरणा देते हैं जिससे आप्रवासियों में सृजनात्मक प्रतिभा दृष्टिगत होती है। उदाहरणार्थ, अमेरिका यूरोप के विभिन्न लोगों के एक साथ बस जाने के बाद समृद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त यह प्रेरणा मानवीय स्वरूपों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के दण्डों, दबावों, युद्धों आदि में भी परिणत हो सकती है जिसके फलस्वरूप गुलामी, जातीय भेदभाव, दमन और निर्वासन अस्तित्व पा सकते हैं। फारस के विरुद्ध युद्ध में हेलास हेलामिस की लड़ाई तक पराजयोन्मुख था, लेकिन दबाव का फल यहाँ हासिल हुआ और सेलामिस में फारसी लोग पूर्णतः नष्ट हो गए।
इसके बावजूद विरोध, चुनौती और अनुक्रिया के इस नियम की कुछ अनिवार्य शर्ते हैं-
(1) जितनी अधिक चुनौतियाँ होगी, उसी अनुपात में प्रेरणा होगी; (2) सर्वाधिक प्रेरणास्पद चुनौती अभाव और उसके आधिक्य के साधन के रूप में प्राप्त होती है। परन्तु एक निश्चित अनुपात के बाद चुनौतियों के अनुपात में वृद्धि हो और उसके साथ उसी अनुपात में अनुक्रिया का अनुपात न बढ़े तो हमें ज्ञात होगा कि चुनौती, विरोध और अनुक्रिया की अन्तःक्रिया ‘हासमान-उपलब्धि के नियम’ से संचालित है। अतः टॉयनबी का यह निष्कर्ष है कि कठिनता का एक निर्धारित अनुपात है जिसके अन्तर्गत प्रेरणा चरम-बिन्दु पर होती है। वह इस स्थिति को चुनौती और विरोध की सर्वाधिक अनुपात की स्थिति न मानकर इष्टतम (श्रेष्ठतम) अनुपात की स्थिति मानता है
सभ्यता का विकास तथा टायनबी
टायनबी की मान्यता है कि सभ्यता का विकास तब ही होता है जब व्यक्ति, अल्पसंख्यक वर्ग या सामाजिक वर्ग निरन्तर आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं और यह क्रम निरन्तर चलता रहता है। अर्थात् चुनौतियों का जवाब मिलता है, जिसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप नई चुनौतियों का जन्म होता है और पुनः तत्सम्बन्धी सामाजिक वर्ग उसका उत्तर देता है। इसी क्रम की निरन्तरता में सभ्यता का विकास निहित है। लेकिन सभ्यता के विकास और लक्षण क्या हैं? टॉयनबी इसको बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। सैनिक या सामाजिक शक्ति का विकास सभ्यता के विकास का लक्षण नहीं है, इसके विपरीत यह सभ्यता के पतन का संकेतक है। इसी प्रकार सभ्यता का भौगोलिक विस्तार या वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियाँ सभ्यता के विकास के द्योतक नहीं है। यद्यपि साधारणतः भौतिक विकास सभ्यता का लक्षण माना जाता है, लेकिन टॉयनबी ने भौतिक परिवेश को नगण्य मानकर, सभ्यता के संदर्भ में, उसे महत्त्व नहीं दिया। उसके विचार से सभ्यता का विकास आन्तरिक प्रक्रिया है। सभ्यता के विकास के लिये आत्म-निश्चय आवश्यक लक्षण है। सभ्यता का अपना पृथक् परिवेश बनता है जिसमें उसकी स्वयं की चुनौतियाँ उत्पन्न होती है। अर्थात् बाह्य सृष्टि से आन्तरिक सृष्टि में क्रिया होती है। सभ्यता के विकास का नेतृत्व हमेशा रहस्यवादियों ने किया। रहस्यवादियों को अपने अनुयायी बनाने के लिये अपनी अंतर्दृष्टि की छाप-पूरे समाज पर लगानी होती है। लेकिन इसका सम्पादन कैसे किया जाय यह एक समस्या रही है, क्योंकि यदि रहस्यवादी इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहें तो जन-सामान्य रहस्यवादियों के ज्ञान का उस प्रकार अनुभव नहीं कर सकता जिस प्रकार स्वयं उन्होने किया है। लेकिन यह रचनात्मक प्रक्रिया असमंजसग्रस्त है, क्योंकि एक ओर रहस्यवादी अपने प्रयास में असफल होता है जो स्वतः ही वह अपने कार्य-क्षेत्र से बाहर हो जाएगा और उसे सफलता मिली तो वह जन सामान्य का जीवन तब तक दुष्कर बना देगा जब तक वह स्वयं अपने प्रयल के द्वारा नए सामाजिक वातावरण को न समझे और सामान्य-जन की जड़ता के कारण इस प्रकार की आशा व्यर्थ है। इसलिए इस सभ्यता के केवल दो ही निदान संभव हैं-एक, कि मेधावी परिवर्तन के लिये सतत् प्रयल करता रहे या, दूसरी ओर, रहस्यवाद के द्वारा समाज को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जाए। इनमें दूसरा निदान जिसमें एक-एक व्यक्ति को परिवर्तन किया जाता है निस्संदेह आदर्श है, लेकिन ऐसे आदर्श से समाज की स्थापना संभव नहीं है और यदि मेधावी परिवर्तन के लिए सतत् प्रयल करता रहे तो सामान्य जन के द्वारा उसका अनुकरण सभ्यता के लिए उपादेय नहीं होगा क्योंकि अनुकरण के द्वारा जन-सामान्य का जो भी विचार सामग्री, सम्पत्ति या कोई विशिष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होगा वह उनकी अपनी उपलब्धि न होकर मेधावी के प्रयासों की देन होगी। वास्तव में अनुकरण का मार्ग सरल मार्ग है और ध्येय को पाने के लिये आवश्यक भी है, लेकिन मूलतः संदिग्ध युक्ति है जो सभ्यता को विघटित होने की स्थिति तक ले जाती है।
सभ्यता का विघटन
सभ्यता का विघटन क्यों तथा किस प्रकार होता है इस संदर्भ में इतिहासकारों में आपसी मत विभिन्नता है। भारतीय परम्परा के जिस प्रकार युगों का प्रारंभ तथा सामाप्ति होती है। उसी प्रकार सभ्यता का जीवन उस युग का छोटा काल है। जबकि स्पेंग्लरके अनुसार सभ्यता का विकास जैवकीय सिद्धान्त पर आधारित है इसलिए सभ्यता का विघटन अवश्यम्भावी है। एक मत के अनुसार प्रजातिगण वर्ण-संस्कार सभ्यता के विघटन का मूल कारण है। लेकिन टॉयनबी के अनुसार सभ्यता से प्रजातियों का कोई संबंध नहीं है। सभ्यता के विघटन के लिये एक सामान्य धारण यह भी रही है कि सभ्यताओं का उत्थान और पतन का मार्ग चक्रात्मक है अर्थात् सभ्यता का उत्थान हुआ है जो विघटन और पतन निश्चित है। लेकिन इस संबंध में टॉयनबी का अपना मत है। उसके अनुसार सभ्यताओं का पतन के आधार पर भावी सभ्यताओं की कुण्डली ही बनाई जा सकती है। इसी प्रकार सभ्यता का विघटन न तो भौगोलिक क्षेत्र में सीमित होने से होता है और न ही इसका कारण मानव जन्म या नैसर्गिक विपत्तियां है। वस्तुतः सभ्यता के लिए विघटन का कारण उसका आत्मघात है। जब व्यक्तियों या अल्पसंख्यकों में क्रियात्मक शक्ति का ह्रास होता है तब सभ्यता का विघटन होता है। विघटन होने के बाद मेधावी के अनुकरण का प्रश्न ही नहीं रहता है। इस प्रकार समझा जा सकता है कि पहले समाज में क्रियात्मक शक्ति का ह्रास हुआ और मेधावियों ने शक्ति के द्वारा परिवर्तन लाना चाहा, लेकिन सामान्य-जन जड़ होने के कारण वैचारिक परिवर्तन संभव नहीं हुआ जिसका परिणाम था संघभेद या सभ्यता का विघटन । अर्थात् व्यक्तियों में क्रियात्मक शक्ति का ह्रास ही टॉयनबी के विचार में सभ्यता के विघटन का मूल कारण है जिसे उसने ‘आत्मघात’ की संज्ञा दी है।
सभ्यता के विघटन के समय समाज तीन भागों में बँट जाता है-एक, सत्ताधारी अल्प संख्यक दूसरा, आन्तरिक प्रोतेरिअत और तीसरा, बाह्य प्रोलेतेरिअत। यहां यह स्मरणीय है कि जैसा स्पेंग्लर का मत था कि विघटन के बाद सभ्यता समाप्त हो जातीहै वहाँ टॉयनबी के अनुसार समाज के उपरोक्त तीनों भाग विघटन के पश्चात् भी उपलब्धि करते हैं। विघटन के समय में यह तीनों भाग निस्सारता की स्थिति में नहीं होते हैं बल्कि तीनों को ही महत्त्वपूर्ण काम करना होता है। आन्तरिक प्रोतेरिअत बाहर से प्रेरणा लेकर विश्वजनीन धर्म की सृष्टि करता है, जबकि सत्ताधारी अल्पसंख्यक वर्ग विघटन की गति रोकने के लिए विश्व-साम्राज्य का निर्माण करता है, तथा बाह्य प्रोतेरिअत विघटन को पूरा करने के लिये सभ्यता को आखिरी धक्का देकर पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन वास्तव में बाह्य प्रोतेरिअत को कभी भी पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हुई। जब भी सभ्यता का विघटन हुआ तो उसका कारण आन्तरिक शक्तियाँ थी।
प्रारम्भ में टॉयनबी ने सभ्यता को अध्ययन की इकाई माना था, लेकिन सभ्यता के पतन के बाद आन्तरिक प्रोलेतेरिअता ने बाह्य प्रेरणा लेकर विश्वजनीन धर्म की सृष्टि की। अर्थात् अब टॉयनबी के विचार से अध्ययन का क्षेत्र परिवर्तित हुआ। सभ्यता ने न केवल धर्म की दासता ग्रहण की बल्कि उसकी परिसमाप्ति एक विश्वजनीन धर्म के रूप में परिवर्तित हुई। इस नए परिवर्तन की मूल प्रेरणा बाहरी होते हुए भी उसकी उपलब्धि सभ्यता के अपने आन्तरिक प्रोतेरिअत के द्वारा हुई।
अध्ययन की इकाइयों में परिवर्तन टॉयनबी का अपना व्यक्तिगत मामला है। उसने अनुभव किया कि सभ्यता के पतन के द्वारा मनुष्य जो दुःख अनुभव करते हैं, उसी से प्रगति होती है। दूसरे शब्दों में, कठिनाइयाँ ही आगे बढ़ना सिखाती हैं। टॉयनबी ने सभ्यता और धर्म को एक रथ के रूप में देखा जिसमें पहियों की गति सभ्यता की गति है और रथ धर्म का स्वरूप है; जैसे प्रकट रूप में पहियेघूमते हैं और रथ आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही समय की गति के साथ-साथ सभ्यताओं का उत्थान और पतन होता है, पहिये घूमते जाते हैं, लेकिन धर्म का रथ आगे बढ़ता जाता है। इससे स्पष्ट है कि टॉयनबी ने यहां पर विको के समान इतिहास दर्शन के सर्पिल-सिद्धान्त (स्पारल थ्योरी) का प्रतिपादन किया है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि टॉयनबी प्रारम्भ में सभी सभ्यताओं को दार्शनिक रूप से एक मानता था और अब देवशास्त्र के आधार पर महान् धर्मों को एक मानता है। (टॉयनबी के अनुसार चार महान् धर्म हैं हिन्दू धर्म, ईसाई धर्म, महायान बौद्ध धर्म और इस्लाम)। इससे स्पष्ट है कि टॉयनबी का इतिहास दर्शन सापेक्षतावादी है।
इतिहास – महत्वपूर्ण लिंक
- टायनवी की इतिहास मीमांसा | टायनवी की इतिहास के विषय में अवधारणा
- टायनबी के सभ्यता संबंधी विचार | सभ्यता का विकास तथा टायनबी | सभ्यता का विघटन
- राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है | राज्य का अस्तित्व विश्व में ईश्वर का अभियान है
- हेगल का राज्य दर्शन | हेगल के राज्य के लक्षण | हेगल के राज्य के सिद्धान्त पर विचार | हेगल के मानसिक समाज सम्बन्धी विचार | सम्पत्ति सम्बन्धी हेगल के विचार
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]