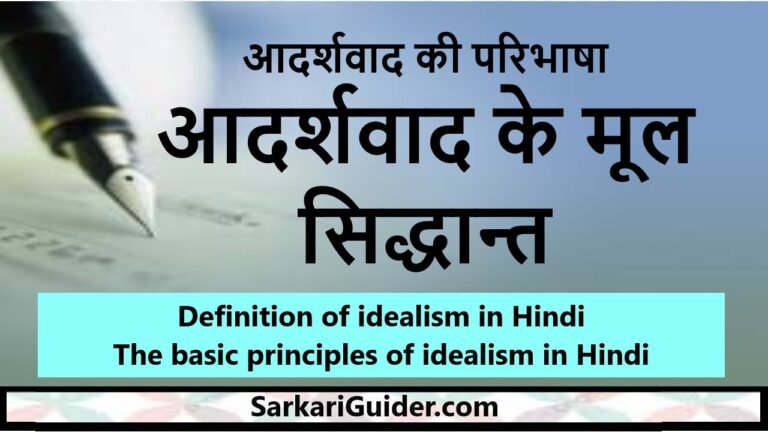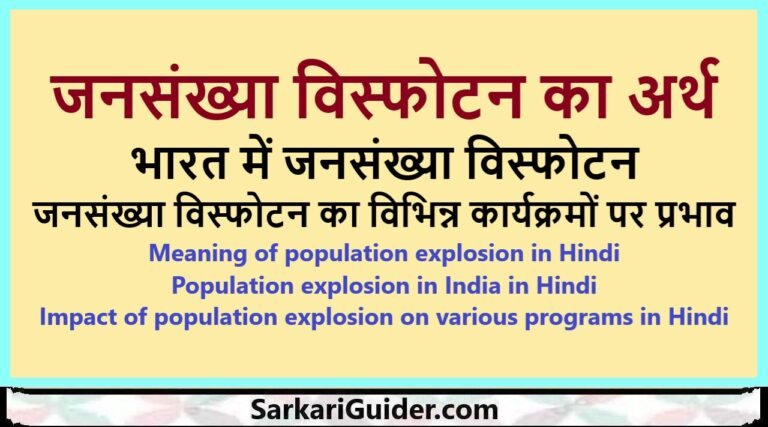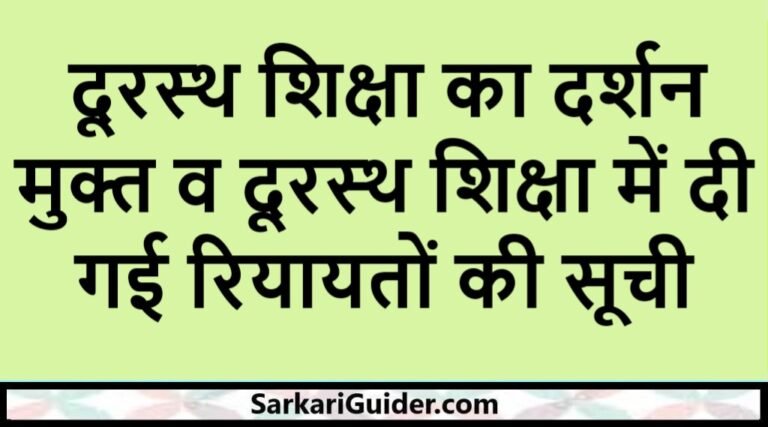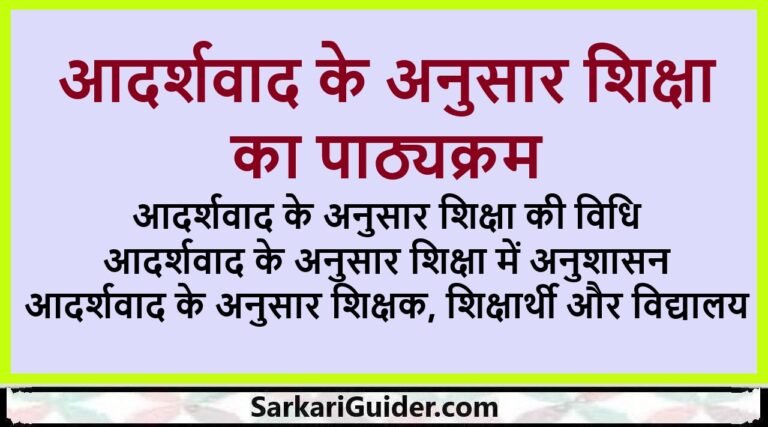वर्धा-योजना की रूपरेखा | बुनियादी शिक्षा क्यों पड़ा? | बुनियादी शिक्षण-विधि

वर्धा-योजना की रूपरेखा | बुनियादी शिक्षा क्यों पड़ा? | बुनियादी शिक्षण-विधि
वर्धा-योजना की रूपरेखा
(Outline of Wardha Scheme)
“वर्धा-योजना” अथवा “बेसिक शिक्षा-योजना” की रूपरेखा इस प्रकार हैं-
(1) बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है।
(2) यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य है।
(3) सम्पूर्ण शिक्षा का सम्बन्ध किसी आधार भूत शिल्प (Basic Craft) से होता है।
(4) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है।
(5) चुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि वह बालकों को अच्छा शिल्पी बनाकर, उनको स्वावलम्बी बना देती है।
(6) शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है, ताकि बालक सीखे हुए शिल्प के द्वारा जीविका का उपार्जन कर सकें।
(7) बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएँ ऐसी होती है, जिनका प्रयोग किया जा सकता है या जिनको बेचकर विद्यालय का कुछ व्यय चलाया जा सकता है।
(8) पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नही है।
(9) शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाता है।
(10) उक्त शिल्प की शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाती है कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्त्व से भली-भाँति परिचित हो जाते हैं।
(11) शिक्षा का बालक के जीवन, गृह एवं ग्राम से और उसके ग्राम के उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।
बुनियादी शिक्षा नाम क्यों ?
(Why Termed Basic Education?)
अंग्रेजी के “Basic” शब्द का हिन्दी अर्थ हैं-“आधारभूत” और उर्दू अर्थ है-“बुनियादी”। क्योंकि यह शिक्षा निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप “आधारभूत” या “बुनियादी” मानी गई है, इसलिए इसका नाम बेसिक शिक्षा पड़ा हैं-
(1) यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य आधारभूत शिक्षा स्वीकार की गई है।
(2) यह शिक्षा बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं और अभिरुचियों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करती
(3) यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा-संगठन का आधार मानी गई है।
(4) यह शिक्षा सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से सम्बन्धित है ।
(5) यह शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा दी जाती है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने भावी जीवन के निर्वाह के लिए कर सकता है।
(6) यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय की आधारभूत सामान्य सम्पत्ति है।
(7) यह शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा आधार भूत ज्ञान प्रदान करती है, जो उनको अपने पर्यावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने और प्रयोग करने में सहायता देता है।
इस प्रकार, जैसा कि स्वयं गाँधी जी ने लिखा है-“बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे व नगरों के हों या ग्रामों के, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से सम्बन्धित करती है।”
बुनियादी शिक्षण-विधि
(Basic Method of Teaching)
रायबर्न के अनुसार-“बेसिक शिक्षा शिक्षण की विधि नहीं है। यह पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। अध्यापक उन विधियों को प्रयोग करता है, जो सबसे अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई हैं। सब प्रगतिशील विधियों का बुनियादी शिक्षा में स्थान हो सकता है। और प्रयोग किया जा सकता है।” बुनियादी शिक्षा में चाहे जिस विधि का प्रयोग किया जायें, पर शिक्षण का वास्तविक कार्य-क्रियाओं और अनुभवों पर अनिवार्य रूप से आधारित किया जाता है। दूसरे शब्दो में शिक्षण-विधि इतनी व्यावहारिक होती है कि बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में प्राप्त करता है। साथ ही उसे यह ज्ञान थोड़े समय में प्राप्त हो जाता है।
छात्रों को विभिन्न विषयों की शिक्षा स्वतंत्र रूप में न दी जाकर, किसी आधार भूत शिल्प के माध्यम से प्रदान की जाती है। गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विषयों आदि के शिक्षण में इसी विधि को प्रयुक्त किया जाता है। यदि किसी विषय के किसी भाग की आधारभूत शिल्प के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती है, तो उसकी शिक्षा किसी अन्य विधि से दी जाती है।
पाठ्यक्रम के सब विषय परस्पर सम्बन्धित ज्ञान क्षेत्रों के रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थति और हस्तकला के माध्यम से अनेक विषयों पर परस्पर संबंध स्थापित किया जा सकता है। बालक को अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जाती है।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- प्राच्य-पाश्चात्य विवाद क्या है? | प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारण
- वुड के घोषणा पत्र के गुण | वुड के घोषणा पत्र के दोष | वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें
- मैकॉले का विवरण पत्र | मैकाले का निम्नवत् छन्नीकरण अथवा निस्यन्दन सिद्धांत | शिक्षा के क्षेत्र में मैकॉले का योगदान | मैकॉले के विवरण पत्र के गुण | मैकॉले के विवरण पत्र के दोष
- शिक्षा के सम्बन्ध में लार्ड कर्जन के उद्देश्य | शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 | लॉर्ड कर्जन के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन
- सार्जेण्ट रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश | सा्जेण्ट रिपोर्ट के गुण | सा्जेण्ट रिपोर्ट के दोष
- राष्ट्रीय चेतना की वृद्धि के कारण | राष्ट्रीय चेतना के दौरान माध्यमिक शिक्षा की प्रगति | राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की असफलता के कारण
- भारतीय शिक्षा आयोग-1882 | हण्टर कमीशन | आयोग के सुझाव व संस्तुतियाँ
- कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917-1919) | सैडलर आयोग | आयोग के सुझाव व संस्तुतियाँ
- बुनियादी शिक्षा योजना के उद्देश्य | बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त
- मैकाले का विवरण पत्र – 1835 | मैकाले का निस्यन्दन सिद्धान्त | बैंटिंक द्वारा विवरण पत्र की स्वीकृति – 1835
- लॉर्ड कर्जन के शिक्षा सम्बन्धी सुधार | शिमला शिक्षा सम्मेलन – 1901 | भारतीय विश्वविद्यालय आयोग – 1902 | भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम – 1904
- विलियम एडम की रिपोर्ट | एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना | एडम रिपोर्ट का मूल्यांकन | एडम योजना की अस्वीकृति
- वुड का घोषणा पत्र- 1854 | वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें
- राष्ट्रीय शिक्षा की माँग | राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धांत | राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धांत की विशेषताएँ | राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना
- ब्रिटिश कालीन शिक्षा के उद्देश्य | ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण | ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष
- गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक की स्वीकृति | बैंटिक की घोषणा के परिणाम
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]