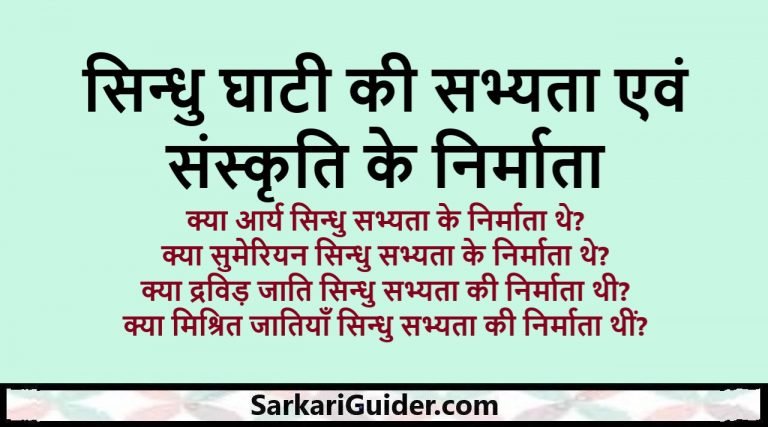वेसर शैली | वेसर शैली एवं उससे बने मन्दिर | चौलुक्य कालीन स्थापत्य | सोलंकी कालीन स्थापत्य
वेसर शैली | वेसर शैली एवं उससे बने मन्दिर | चौलुक्य कालीन स्थापत्य | सोलंकी कालीन स्थापत्य
वेसर शैली
दक्षिण भारत में मन्दिर स्थापत्य की दो कला शैलियों का विकास हुआ। वेसर शैली एवं द्रविड़ शैली। वेसर शैली के मन्दिरों का आकार अर्धगोलाकार था तथा द्रविड़ शैली का अष्टभुजाकार था। वेसर शैली का विकास चालुक्यों के समय में विन्ध्य पर्वतमाला से लेकर कृष्णा घाटी तक हुआ था। वेसर शैली में नागर एवं द्रविड़ शैली के तत्वों का सुन्दर समायोजना दिखाई देता है। चालुक्यकालीन मन्दिर नागर एवं द्रविड़ शैलियों का मिश्रित रूप हमारे सामने रखते हैं। इसे वेसर शैली भी कहा जाता है। एहोल वादामी तथा पत्तदकल में अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ। चालुक्यों ने पहाड़ों एवं चट्टानों को कटवा कर सुन्दर एवं भव्य मन्दिरों का निर्माण करवाया। चालुक्य मन्दिरों में प्रमुख है जिनेन्द्र का मन्दिर, त्रिमूर्ति का गुफा मन्दिर, विष्णु का मन्दिर, विजयेश्वर तथा विरुपाक्ष मन्दिर। होयसलो ने भी कुछ वेसर शैली के मन्दिर बनवाये थे।
चौलुक्य (सोलंकी) कालीन स्थापत्य
ईसा की दसवीं से तेरहवीं शती तक गुजरात, काठियावाड़, कच्छ तथा राजपूताने के पश्चिमी भाग पर चौलुक्य अथवा सोलंकी वंश के राजाओं ने शासन किया। उनकी राजधानी अन्हिलपाटन में थी। अरबों तथा पारसीकों से समुद्री व्यापार के कारण यह राज्य बड़ा समृद्ध था जहाँ अनेक धनाढ्य व्यापारी रहते थे। चौलुक्य शासक उत्साही निर्माता थे तथा उनके काल में अनेक मन्दिर एवं धार्मिक स्मारक बनवाये गये। मन्दिर निर्माण के पुनीत कार्य में उनके राज्यपालों, मन्त्रियों एवं धनाढ्य व्यापारियों ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण समुदाय की कार्यनिष्ठा एवं प्रत्येक व्यक्ति की लगन के फलस्वरूप इस समय गुजरात के अन्हिलवाड़ तथा राजस्थान के आबू पर्वत पर कई भव्य मन्दिरों का निर्माण करवाया गया। ये मुख्यतः जैन धर्म से सम्बन्धित हैं।
सोलंकी मन्दिरों में तीन भाग दिखायी पड़ते हैं-
- पीठ या आधार— इसके ऊपरी भाग पर पूरा निर्माण टिका हुआ है। इसमें कई ढलाइयाँ हैं जो विविध अलंकरणों से युक्त हैं। राक्षस (शृंगरहित सिर), गजपीठ, अश्व तथा मानव आकृतियाँ आदि उत्कीर्ण हैं।
- मण्डोवर अर्थात् मध्यवर्ती भाग- यह पीठ तथा शिखर के मध्य होता था और मन्दिर का प्रमुख भाग माना जाता था। इसकी लम्बवत् दीवारों में ताख बने हैं जिनमें देवी- देवताओं, नार्तिकाओं आदि की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं।
- मीनार या शिखर— यह मन्दिर का सबसे ऊपरी भाग है जो नागरशैली में है। इसके चारों ओर उरुशृंगों (गर्भगृह की मीनार पर चारों ओर बना शिखरनुमा आकार) का समूह बनाया गया है।
मन्दिरों का निर्माण ऊँचे चबूतरे पर किया जाता था। सामान्यतः उनमें एक देवालय तथा एक कक्ष मात्र होता था तथा प्रवेश द्वार पर, बरसाती नहीं रहती थी। ऊपरी शिखर खजुराहो के समान अनेक छोटी-छोटी मीनारों से सुसज्जित रहता था तथा छतें रोड़ादार गुम्बदों जैसी होती थीं। इन भीतरी छतों पर खोदकर चित्र बनाये जाते थे ताकि वे एक वास्तविक गुम्बद जैसे प्रतीत हो सकें।
गुजरात के प्रमुख मन्दिरों में मेहसाना जिले में स्थित ‘मोडेहरा का सूर्य मन्दिर’ उल्लेखनीय है। इसका निर्माण ग्यारहवीं शती में हुआ था। अब यह मन्दिर नष्ट हो गया है, केवल इसके ध्वंसावशेष ही विद्यमान हैं। इनमें गर्भगृह, प्रदक्षिणापथ, मण्डप आदि हैं। इसका निर्माण ऊँचे चबूतरे पर किया गया है। निर्माण में सुनहरे बलुए पत्थर लगे हैं। इसमें स्तम्मों पर आधारित खुला द्वार मण्डप है। इसके दन्तुरित मेहराब (cusped arches) भव्य एवं सुन्दर हैं। पाटन स्थित सोमनाथ के मन्दिर का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसका पुनर्निर्माण इस काल में हुआ। इस वंश के शासक कर्ण ने अन्हिलवाड़ में कर्णमेरु नामक मन्दिर बनवाया था। सिद्धपुर स्थित रुद्रमहाकाल का मन्दिर भी वास्तुकला का सुन्दर उदाहरण है। गुजरात में अन्हिलवाड़ के निकट सुनक स्थित नीलकण्ठ महादेव मन्दिर भी एक विशिष्ट रचना है। इसी का समकालीन काठियावाड का नवलाखा मन्दिर कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट है।
आबू पर्वत पर कई मन्दिर प्राप्त होते हैं। यहाँ दो प्रसिद्ध संगमरमर के मन्दिर हैं जिन्हें दिलवाड़ा कहा जाता है। सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने ग्यारहवीं शती में विमलशाही नामक मन्दिर बनवाया था। अनुश्रुति के अनुसार विमलशाह ने पहले कुम्भेरिया में पार्श्वनाथ के 360 मन्दिर बनवाये थे किन्तु उनकी इष्ट देवी अम्बा ने किसी बात से नाराज होकर पाँच मन्दिरों के सिवाय सभी को जला दिया तथा विमलशाह को दिलवाड़ा में आदिनाथ का मन्दिर बनवाने का आदेश स्वप्न में दिया। उसने परमार नरेश से 56 लाख रुपये में भूमि क्रय कर इस मन्दिर का निर्माण करवाया था। यह 98′ x 48′ के क्षेत्रफल में फैला है। तथा ऊँचे परकोटे से घिरा हुआ है। इसमें पचास से अधिक कक्ष बनाये गये हैं।
मन्दिर का प्रवेश द्वार गुम्बद वाले मण्डप से होकर बनाया गया है जिसके सामने एक वर्गाकार भवन है जिसमें छः स्तम्भ तथा दस गज प्रतिमाएँ हैं। इसके पीछे मध्य में बने मुख्य गर्भगृह में ध्यानमुद्रा में अवस्थित आदिनाथ की मूर्ति है जिसकी आँखें हीरे की हैं। यह मन्दिर अपनी बारीक नक्काशी तथा अद्भुत मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। पाषाण शिल्पकला का इतना बढ़िया उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। मन्दिर का बाहरी भाग अत्यन्त सादा है, किन्तु भीतर का अलंकृत है। श्वेत संगमरमर के गुम्बद का भीतरी भाग, दीवारें, छतें तथा स्तम्भ सभी पर नक्काशी मिलती है। मूर्तिकारी में विविध प्रकार के फूल-पत्ते, पशु-पक्षी, मानव आकृतियाँ आदि इतनी बारीकी से उकेरी गयी हैं मानो शिल्पियों की छेनी ने कठोर संगमरमर को मोम बना दिया हो।
विमलशाही मन्दिर के समीप ही दूसरा मन्दिर स्थित है। इसे तेजपाल ने बनवाया था। निर्माता के नाम पर ही इसे ‘तेजपाल मन्दिर’ कहा जाता है। यह भी पहले जैसा भव्य एवं सुन्दर है। इसके उत्कीर्ण शिल्प सजीव तो नहीं हैं किन्तु कारीगरों ने बारीकी एवं सफाई से उन्हें बनाया है। मन्दिर में ठोस संगमरमर की लटकन है जो स्फटिकमणि से बनी प्रतीत होती है। उसके चारों ओर गोलाई में खोदकर कमल पुष्प बनाया गया है। लम्बवत् पाषाण पर खुदी हुई अनेक आकृतियाँ मनोहर हैं। गर्भगृह में नेमिनाथ की प्रतिमा स्थापित है तथा कक्ष एक द्वार मण्डपों पर उनके जीवन से ली गयी अनेक गाथायें उत्कीर्ण हैं। कलाविद् फर्ग्युसन के शब्दों में, ‘केन्द्रीय गुम्बद अधखिले कमल के समान दिखाई देता है। जिसकी पंखुड़ियाँ इतनी पतली, पारदर्शक तथा कुशलता से उकेरी गयी हैं कि उनकी प्रशंसा करते हुए नेत्र ठहर जाते हैं।’
विमलशाही तथा तेजपाल मन्दिरों के अतिरिक्त आबू पर्वत पर कुछ अन्य जैन मन्दिर भी मिलते हैं। पर्वत शिखर पर मन्दिर निर्माण की होड़ सी लगी हुई थी क्योंकि उत्तुंग पर्वत स्थान को देवता के आवास के लिये सबसे पवित्र माना जाता था। मन्दिर ऊँचे परकोटे से घिरे होते थे जिनके चारों ओर कोठरियाँ बनी होती थीं। कोठरियों में जैन तीर्थंकरों अथवा देवताओं की बैठी प्रतिमायें दिखाई देती हैं। इनके शिखर छोटी मीनारों से अलंकृत हैं। मन्दिर की भीतरी छतों पर खोदकर चित्रकारियाँ की गयी हैं। वास्तु की दृष्टि से ये मन्दिर बहुत सुन्दर तो नहीं हैं किन्तु सभी मन्दिर अपनी सूक्ष्म एवं सुन्दर नक्काशी के लिये प्रसिद्ध हैं। इनमें सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं। कलात्मक होने के साथ-साथ इनके अलंकरण का बाहुल्य दर्शकों को उबा देने वाला प्रतीत होता है।
इतिहास – महत्वपूर्ण लिंक
- खजुराहो मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं | Salient Features of Khajuraho Sculpture in Hindi
- गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला | गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य | गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला का परिचय
- गुप्तोत्तरयुगीन हिन्दू मन्दिर | गुप्तोत्तरयुगीन हिन्दू मन्दिरों और स्थापत्य
- उड़ीसा के मन्दिर | उड़ीसा के मन्दिरों की प्रमुख विशेषताएं | उड़ीसा के मन्दिरों पर निबन्ध
- खजुराहो के मन्दिर | खजुराहो के मन्दिरों के प्रमुख विशेषताएं | खजुराहो के मन्दिरों पर एक विस्तृत टिप्पणी
- पल्लव मन्दिरों की प्रमुख विशेषताएं | पल्लव मूर्ति कला | पल्लव मूर्ति कला पर संक्षिप्त टिप्पणी
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]