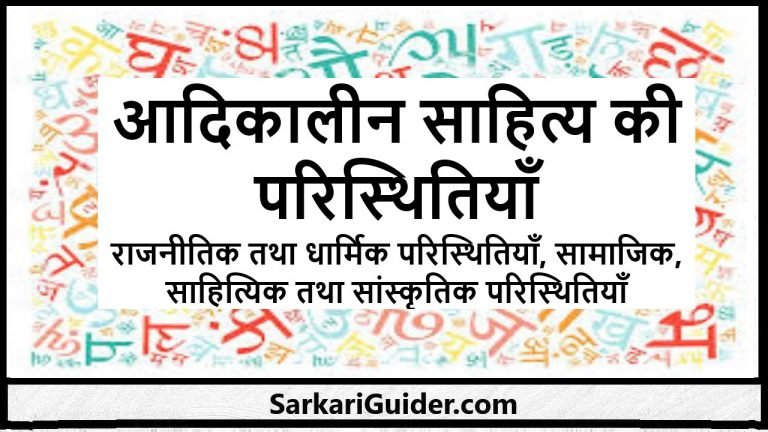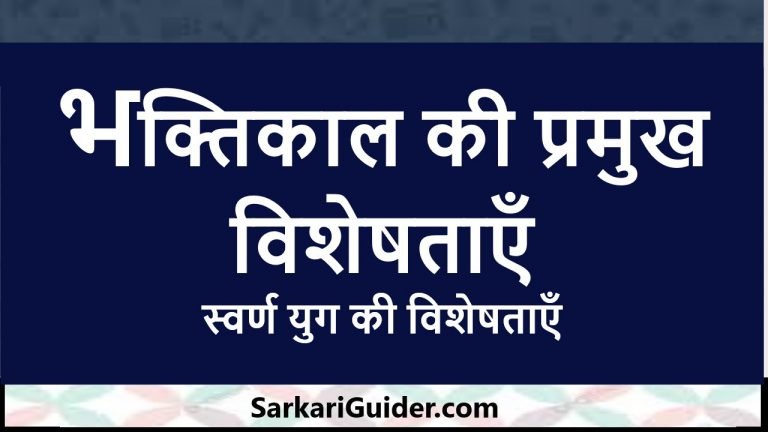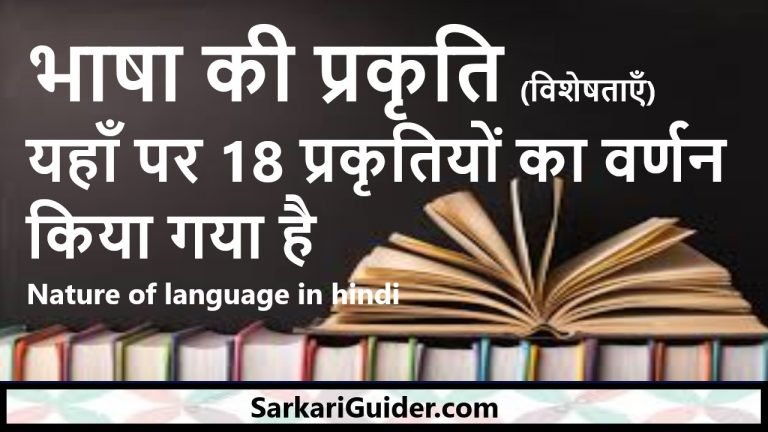बिम्ब का अर्थ | बिम्ब के गुण | बिम्ब विधान | काव्य में बिम्ब की उपयोगिता
बिम्ब का अर्थ | बिम्ब के गुण | बिम्ब विधान | काव्य में बिम्ब की उपयोगिता
बिम्ब का अर्थ
बिम्ब का अर्थ- बिम्ब अंग्रेजी शब्द इमेज (Image) का पर्यायवाची है। यह शब्द अपने आप में बड़ा व्यापक है। साधारणतः बिम्ब शब्द का प्रयोग छाया, प्रतिच्छायां, अनुकृति आदि के रूप में होता है। अंग्रेजी कोश में भी बिम्ब का किसी वस्तु की छाया, अनुकृति, सादृश्यता अथवा समानता माना गया है। बिम्ब शब्द का बड़ा व्यापक प्रयोग होता है। मनोविज्ञान, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में इसका विशेष महत्त्व है।
मनोविज्ञान में बिम्ब शब्द से मानसिक पुनर्निर्माण का अर्थ लिया जाता है। विश्व-कोश के अनुसार ‘बिम्ब’ चेतन स्मृतियाँ जो विचारों की मौलिक उत्तेजना के अभाव में इस विचार को सम्पूर्ण या आंशिक रूप में प्रस्तुत करती है।
आधुनिक कविता के अध्ययन में बिम्ब का प्रयोग आधुनिक है। आधुनिक मानव की वैज्ञानिक दृष्टि, अन्वेषण की प्रवृत्ति, निरन्तर जीवन और जगत् की गहन जटिलताओं को खोलने की प्रवृत्ति, बाह्य यथार्थ के प्रति भावात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति इन सब ने भ्रम, कल्पना के स्थान पर प्रत्यक्ष ठोस अनुभव को आधार बनाकर काव्य में बिम्बों की खोज शुरू की। अमेरिकी विचारक जोजेफाइन माइल्स के अनुसार, ‘बिम्ब सिद्धान्त का आरम्भ उस समय से मानना चाहिए जब लॉक और ह्यूम जैसे इन्द्रियानुभववादी दार्शनिक ने तर्क और अनुमान को अपेक्षा वस्तु की प्रत्यक्ष संवेदना को अधिक प्रामाणिक और महत्त्वपूर्ण सिद्ध किया। काव्य के क्षेत्र में मूर्त भावना के स्थान पर मूर्त ऐन्द्रिय-चित्रों अथवा बिम्ब-विधान का आग्रह इसी क्रान्तिकारी दार्शनिक स्थापना का परिणाम था।”
बिम्ब के गुण
जिस प्रकार निरन्तर प्रयोग से सिक्का घिस जाता है और उसकी चमक कम हो जाती है, उसी प्रकार निरन्तर प्रयुक्त होनेवाली विम्ब भी घिस-पिट जाते हैं और उनकी चमत्कृत करने की शक्ति कम हो जाती है। अतएव पाठक कवि से यह अपेक्षा करता है कि नये-नये विम्बों का प्रयोग करें। परिवर्तित होता हुआ जीवन, सभ्यता के नवीन पृष्ठ, जीव के नये मानदण्ड, विचारों के नये मोड़ आदि भी यह मांग करते हैं कि कविता में नवीन बिम्बों का प्रयोग हो। कहा भी गया है-
‘पुरातनता का यह निर्भीक सहन करती न प्रकति पल एक।’
बिम्ब का दूसरा महत्त्वपूर्ण गुण है उसका विषयानुरूप होना। यदि यह विषय के अनुरूप नहीं है तो प्रभाव डालने में सफल नहीं होगा। बिम्ब और विषय के मध्य गहरा तालमेल होना ही बिम्ब को सफल बनाता है। अत: बिम्ब और विषय की संगति इतनी सुन्दर हो कि उसे पढ़ने की कवि के कौशल पर पाठक यह सोचने को बाध्य हो जाय कि इतने निकट सादृश्य पर आज तक मेरी दृष्टि क्यों नहीं गयी थी?
बिम्ब स्वाभाविक होना चाहिए। पहली दृष्टि से वह भले ही चमत्कारिक प्रतीत हो, परन्तु उसका स्थायी प्रभाव यह पड़े कि उसमें कृत्रिमता नहीं है, स्वाभाविकता है जो बिम्ब अलंकरण के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे स्थायी प्रभाव नहीं डालते।
बिम्ब के अन्य आवश्यक गुण हैं- ताजगी, सफ्नता तथा कवि की अनुभूति को पाठक तक सम्प्रेषित करने की क्षमता। विम्ब का प्रस्तुतीकरण इस प्रकार हो और वह ऐसे भाव का उद्घाटन करे जो पाठक के लिए नया हो। सघनता का अभिप्राय कम-से-कम शब्दों में विराट अनुभूति को व्यक्त करने से है। सफल बिम्ब योजना के लिए कवि का भाषा अबोध अधिकार होना वांछनीय है क्योंकि- तभी उसकी अनुभूति पाठक की अनुभूति बन सकेगी।
काव्य में बिम्ब की उपयोगिता
काव्य में बिम्ब का प्रयोजन और उपयोगिता-काव्य-बिम्ब का प्रयोजन है वर्ण्य विषय को स्पष्ट बनाना, कवि की अनुभूति को तीन बनाना तथा वही अनुभूति पाठक अथवा श्रोता के मन में जागृत करना। आज का मानव जीवन और जगत् की जटिलताओं से पस्त हैं, कुण्ठाओं से ग्रस्त है। कवि स्वस्थ और ताजे बिम्बों का निर्माण करके इस अव्यवस्था की ओर अराजकता की व्यवस्था में बदल सकता है। इसीलिए बिम्बों की तुलना लेविन महोदय ने जादुई दर्पण से की है।
बिम्ब-विधान द्वारा अर्थ को स्पष्टता मिलती है, भाव को तीव्रता मिलती है, वस्तु को प्रत्यक्षता प्राप्त होती है तथा. गुण को हृदय-संवेद्य बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, तुलसी की ये पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं-कनक भूधराकार सरीरा। कुम्भकरण आवत रनधीरा।।
इसमें तुलसी ने एक स्वर्ण पर्वत का बिम्ब प्रस्तुत करके कुम्भकरण के वर्ण और आकार का एक प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार प्रसाद जी ने निम्न पंक्तियों से बिम्ब-विधान द्वारा की अमूर्त लज्जा भाव को मूर्त आकार प्रदान किया है क्योंकि लाज के उत्पन्न से ही नारी के कर्णफूल रक्तिम हो उठते हैं-
कोमल किशोर सुन्दरता की मैं करती रहती रखवाली।
मैं वह हल्की-सी मसलन हूँ बनती कानों की लाली।
बिम्ब विधान
बिम्ब शब्द अंग्रेजी के ‘इमेज’ शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। जिसका अर्थ है-मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिम्ब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा ऐन्द्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है।
बिम्ब विधान हिन्दी साहित्य में कविता की एक शैली है। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कविता में जैसे विषय बदले, वस्तु बदली और कवि की जीवन-दृष्टि बदली वैसे ही शिल्प के क्षेत्र में रूप-विधान के नये आयाम भी विकसित हुए। कविता की समीक्षा के मानदण्डों में एक बारगी युगान्तर आया और नये ढंग पर कविता की इमारत खड़ी की गई। कवि की अनुभूमियां नये अप्रस्तुतों और प्रतीकों को खोजते-खोजते बिम्ब के नये धरातलों को उदघाटित करने में समर्थ हुई। कविता की जीवन्तता में प्राणशक्ति के रूप में विम्ब ने अपना स्थान और महत्व पाया।
काव्यात्मक विम्ब एक संवेदनात्मक चित्र है जो एक सीमा तक अलंकृत-रूपतामक भावात्मक और आवेगात्मक होता है। लीविस ने बिम्ब को भावगर्भित चित्र ही माना है। डॉ. नगेन्द्र के अनुसार, “बिम्ब किसी अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्निर्मित। एजरा पाउण्ड के अनुसार, “बिम्ब वह है जो किसी बौद्धिक तथा भावात्मक संश्लेष को समय के किसी एक बिन्दु पर संभव करता है।” हिन्दी की नयी कविता-धारा के कवि पश्चिम के काव्य और काव्यान्दोलनों से परिचित थे। ‘तार सप्तक में प्रभाकर माचवे ने अपनी कविता को ‘इम्प्रेशनिस्ट’ अथवा बिम्बवादी घोषित किया। फिर भी तीसरी सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह से पहले विम्व-विधान को किसी ने अपने वक्तव्य में प्रमुखता नहीं दी थी। केदार सिंह ने घोषित किया कि “कविता में मैं सबसे अधिक ध्यान देता हूं बिम्ब-विधान पर।” शमशेर की कृतियों में बिम्ब अधिक सजीव और ऐन्द्रिय हैं। उनके समकालीन रचनाकार बच्चन, अज्ञेय, अंचल, दिनकर, नरेन्द्र शर्मा की कृतियां अपनी बिम्बात्मक गुणात्मकता के कारण ही मूल्यवान हैं।
हिन्दी – महत्वपूर्ण लिंक
- काव्यभाषा का स्वरूप | काव्यभाषा एवं सामान्य भाषा में अन्तर
- काव्य में बिम्ब-विधान | काव्य बिम्ब का कार्य या उद्देश्य | बिम्ब के गुण एवं तत्व | बिम्बों का वर्गीकरण
- प्राचीन भारतीय आर्य भाषा | वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में साम्य एवं वैषम्य | वैदिक और लौकिक संस्कृत में अन्तर
- पालि भाषा की व्युत्पत्ति | पालिभाषा का प्रदेश | पालि-साहित्य | पालि की विशेषताएं
- परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ठ | अवहट्ठ की विशेषताएं | अवहट्ट भाषा की भाषिक विशेषताएँ | अवहट्ट भाषा की व्याकरणिक विशेषताएँ
- राष्ट्रभाषा हिन्दी की समस्याएँ | राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का भविष्य
- प्रतीक का उद्भव एंव विकास | प्रतीक का अर्थ | प्रतीकों का वर्गीकरण | प्रतीक योजना का आधार | काव्य में प्रतीकों का महत्व
- महाराष्ट्री प्राकृत | महाराष्ट्री प्राकृत की विशेषताएं
- राजभाषा एव राष्ट्रभाषा | संचार भाषा | सम्पर्क भाषा
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]