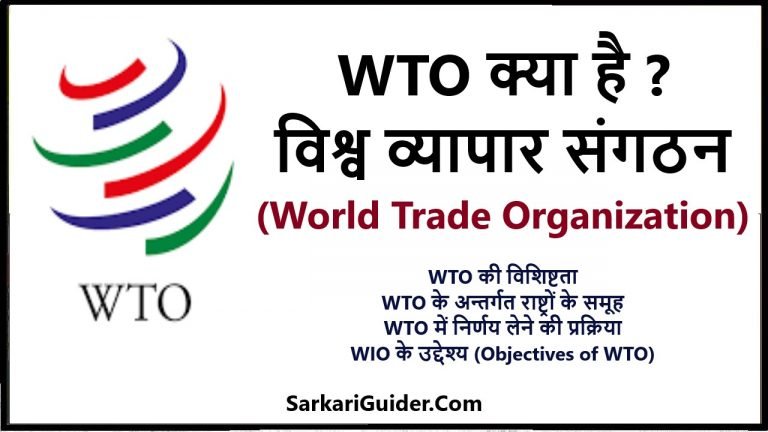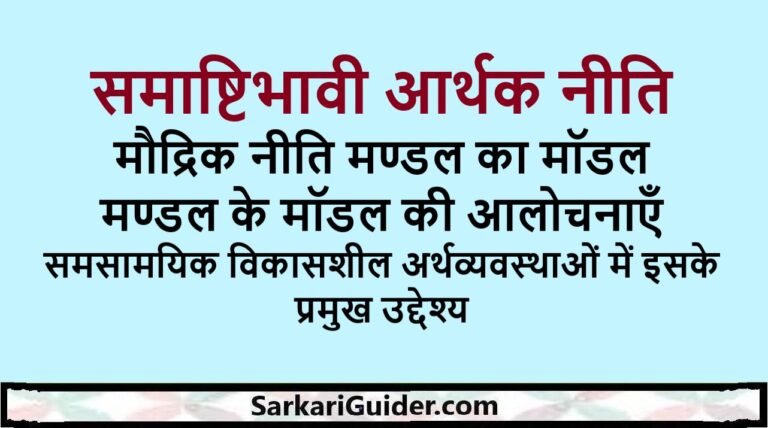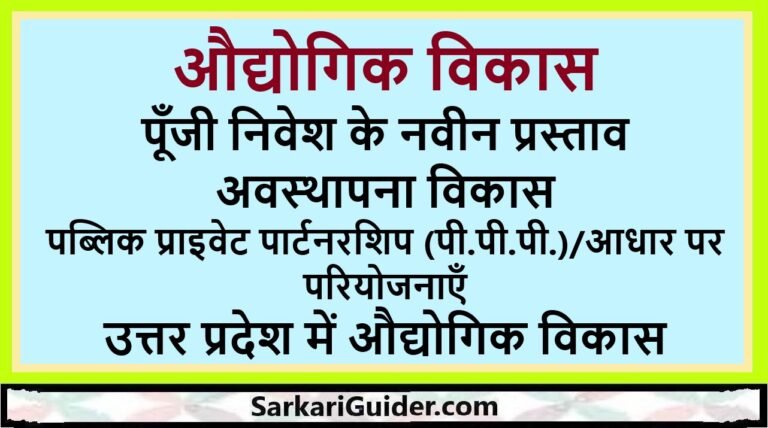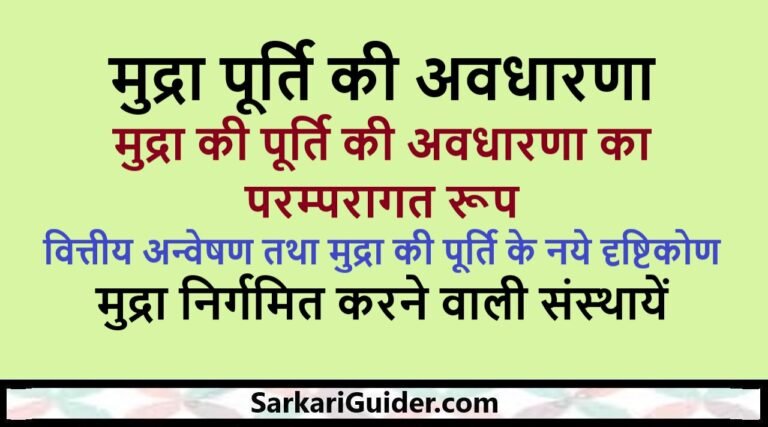आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ | आर्थिक नियोजन की परिभाषा | Definition of economic planning in Hindi | Features of economic planning in Hindi

आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ | आर्थिक नियोजन की परिभाषा | Definition of economic planning in Hindi | Features of economic planning in Hindi
आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ/लक्षण/मान्यताएँ
आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ निम्नलिखित है-
- निश्चित लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्माण- आर्थिक नियोजन का प्रथम उद्देश्य निश्चित लक्ष्य का निर्धारण है। ये लक्ष्य पहले से सोच-विचार कर निर्धारित कर दिये जाते हैंहैं। फिर उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्राथमिकताओं तथा उनका क्रम निश्चित किया जाता है।
- योजना का संचालन एक केन्द्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है- इसमें एक केन्द्रीय नियोजन अधिकारी होता है जो देश के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में निर्णय लेता हैहै। इस प्रकार का अधिकारी या तो सरकारी होता है या कोई अन्य संस्था जिसे सरकार नियुक्त करे, हो सकता है। भारत में इस कार्य के लिए योजना आयोग की नियुक्ति की गयी है।
- सम्पूर्ण कार्य योजना के अनुसार चलना- इसके अन्तर्गत देश के आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहलू को नियन्त्रित किया जाता है। फिर उसी के अनुसार कार्यक्रम को संचालित किया जाता है।
- सीमित साधनों का उचित वितरण- सीमित साधनों का इस प्रकार वैज्ञानिक तथा न्यायपूर्ण रीति से वितरण किया जाता है कि सामान्य हितों का उद्देश्य पूरा हो सके। इस प्रकार उपलब्ध साधनों का उपयोग आवश्यक वस्तुओं के प्राथमिकता क्रम के अनुसार होता है।
- आँकड़ों का विशेष महत्त्व- आँकड़ों के आधार पर सभी विकास योजनाएँ बनायी जाती है। अतः नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विषय से सम्बन्धित सही तथा पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध हों।
- योजनाओं का दीर्घकालीन होना- आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया, है। इसमें एक के बाद दूसरी योजनाएँ चलायी जाती हैं? जिनमें आपस में दीर्घकालीन सम्बन्ध होता है। अल्पकालीन योजनाएँ भी दीर्घकालीन योजनाओं का एक भाग होती हैं। इस प्रकार एक योजना दूसरी योजना के, दूसरी योजना तीसरी के आधार का काम देती है। यही क्रम आगे भी चलता रहता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ पंचवर्षीय आधार पर चलायी जा रही हैं।
- निश्चित अवधि- आर्थिक नियोजन एक निश्चित अवधि के लिए होता है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाते हैं।
अर्द्धविकसित देशों में आर्थिक नियोजन का बड़ा महत्त्व है। स्वर्गीय टी. टी. कृष्णमाचारी के शब्दों में, “आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का वही महत्त्व है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर का है।” ऑस्कर टाँगे के शब्दों में, “आजकल अनेक अल्पविकसित देश यह विश्वास करते हैं कि उनके पिछड़ेपन का एकमात्र समाधान आर्थिक नियोजन ही हैं।
अर्द्धविकसित क्षेत्र में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता अथवा महत्त्व निम्नलिखित कारणों से है।
उपलब्धता साधनों का सर्वोत्तम उपयोग- अल्पविकसित राष्ट्रों से सीमित साधन, अपूर्ण ज्ञान, पर्याप्त निरक्षता, निपुण श्रमिकों का अभाव, पूँजी का अभाव, तकनीकी साधनों का अभाव है जिसके कारण तीव्र गति से विकास करना सम्भव नहीं होता। भारत में भी उपलब्ध साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं हो पाया है। अतः उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम का निर्माण करना आवश्यक है।
विभिन्न क्षेत्रों का समन्वित विकास- अर्द्धविकसित देशों में क्षेत्रीय विषमता पायी जाती है। वन, वृहत् उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार तथा लघु उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्र होते है। देश को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए इनका समन्वित विकास आवश्यक है। आर्थिक नियोजन के द्वारा ही विभिन्न क्षेत्रों का समन्वित विकास किया जा सकता है।
जनसंख्या की समस्या- अर्द्धविकसित देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है जिस कारण से ये देश अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास नहीं कर पाते। आर्थिक नियोजन के माध्यम से यह सरलता से किया जा सकता है।
आर्थिक कुचक्रों की समाप्ति- अर्द्धविकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। इन दुष्चक्रों को तोड़ने के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है क्योंकि इससे कार्यक्षमता बढ़ती है, पूँजी निर्माण तथा विनियोग की दर दोनों बढ़ जाती हैं।
बेरोजगारी की समस्या का समाधान- देश में बेरोजगारी की समस्या बड़ा उग्र रूप धारण किये हुए है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए आर्थिक नियोजन ही एकमात्र हल है।
पूँजी की पूर्ति- अर्द्धविकसित देशों में पूँजी निर्माण की दर कम होने के कारण विनियोग की दर कम रहती है। आर्थिक नियोजन उत्पादन में वृद्धि करता है जिससे पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है तथा राष्ट्रीय विकास तीव्र गति से होने लगता है।
सम्पत्ति व साधनों का समान वितरण- अर्द्धविकसित देशों में सम्पत्ति व साधनों का समान वितरण होता है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना होता है जिससे सम्पत्ति का समान व न्यायपूर्ण वितरण हो जाता है।
शिक्षा का प्रसार- अर्द्धविकसित देशों में अशिक्षा व अज्ञानता का साम्राज्य होता है। प्रशिक्षित व्यक्तियों का भी अभाव होता है। आर्थिक नियोजन से शिक्षा का प्रसार होता है, प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ती हैं जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल, योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध होने लगते हैं और आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है।
आर्थिक नियोजन की परिभाषा
आर्थिक नियोजन के अर्थ, स्वरूप एवं क्षेत्र के सम्बन्ध में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं, अतः इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। आर्थिक नियोजन की प्रमुख विद्वानों द्वारा निम्नलिखित परिभाषाएँ दी गयी हैं
- भारतीय नियोजन आयोग के अनुसार, “आर्थिक नियोजन निश्चित रूप से सामाजिक उद्देश्यों के हितार्थ उपलब्ध साधनों का संगठन तथा लाभकारी रूप से उपयोग करने का एकमात्र ढंग है। नियोजन के इस विचार के दो प्रमुख तत्त्व हैं – (अ) वांछित उद्देश्यों का क्रम जिनकी पूर्ति का प्रयास करना है तथा (ब) उपलब्ध साधनों और उनके सर्वोत्तम वितरण के सम्बन्ध में ज्ञान।”
- राष्ट्रीय नियोजन समिति के अनुसार, “आर्थिक नियोजन उपभोग, उत्पादन, विनियोग, व्यापार तथा राष्ट्रीय लाभांश्ख के वितरण से सम्बन्धित स्वार्थरहित विशेषज्ञों का तकनीकी समन्वय है जो राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परप्राप्त किया जा सके।”
- श्रीमती बारबारा बूटन ने आर्थिक नियोजन की परिभाषा के दो दृष्टिकोण दिये –
प्रथम दृष्टिकोण– “सार्वजनिक अधिकारी द्वारा आर्थिक प्राथमिकताओं का सचेत, विवेकपूर्ण तथा इच्छानुसार किया गया निर्वाचन तथा निर्धारण ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है।”
द्वितीय दृष्टिकोण- “आर्थिक नियोजन वह व्यवस्था है जिसमें विपणि संयन्त्र की कार्यविधि में इस दृष्टि से हस्तक्षेप किया जाता है कि ऐसी व्यवस्था या क्रम उत्पन्न हो जाये जो विपणि संयन्त्र के स्वतन्त्र रूप से कार्य करने पर विकसित होने वाले क्रम से पूर्णतया भिन्न हो।”
- प्रो. एल. लार्विन के अनुसार, “नियोजित अर्थव्यवस्था (नियोजन) आर्थिक संगठन की एक ऐसी योजना है जिसमें समस्त व्यक्तिगत तथा स्वतन्त्र उद्योगों व उपक्रमों तथा औद्योगिक संस्थाओं को समन्वित एवं एकीकृत इकाई के रूप में संचालित किया जाता है तथा जिसका (व्यवस्था) उद्देश्य निश्चित अवधि में उपलब्ध साधनों के माध्यम द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करना होता है।”
इस परिभाषा के अनुसार नियोजन में कुछ निश्चित लक्ष्य, उनकी पूर्ति हेतु देश के समस्त उपलब्ध साधनों का पूर्ण ज्ञान एवं उनसे अधिकतम प्रभावशाली उपयोग के लिए सुव्यवस्थित और नियंत्रित कार्यक्रम होना चाहिए।
- एच. डी. डिकिन्सन के अनुसार, “आर्थिक नियोजन से अभिप्राय महत्त्वपूर्ण आर्थिक मामलों में विस्तृत तथा सन्तुलित निर्णय लेना है।” दूसरे शब्दों में, “क्या तथा कितना उत्पादित किया जायेगा तथा उसका वितरण किस प्रकार होगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक निर्धारक सत्ता द्वारा समस्त अर्थव्यवस्था को एक ही राष्ट्रीय आर्थिक इकाई (व्यवस्था) मानते हुए तथा व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर, सचेत तथा विवेकपूर्ण निर्णय के द्वारा दिया जाता है।”
आर्थिक नियोजन की एक उचित परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है – “आर्थिक नियोजन से आशय पूर्व निर्धारित और निश्चित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतुज्ञअर्थव्यवस्था के सभी अंगों को एकीकृत और समन्वित करते हुए ष्ट्र के संसाधनों के सम्बन्ध में सोच-विचार कर रूपरेखा तैयार करने और केन्द्रीय नियंत्रण से है।”
अर्थशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- असंतुलित आर्थिक विकास सिद्धान्त | असन्तुलित विकास का अर्थ | हर्षमैन का असन्तुलित विकास सिद्धान्त
- सन्तुलित एवं असन्तुलित विकास | सन्तुलित विकास की तुलनात्मक श्रेष्ठता | असन्तुलित विकास की तुलनात्मक श्रेष्ठता | सन्तुलित एवं असन्तुलित विकास के बीच विवाद की निरर्थकता | सन्तुलित एवं असन्तुलित विकास के विवाद की आलोचनात्मक समीक्षा
- लेबेन्स्टीन का आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धान्त | लेबेन्स्टीन का आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन
- निर्धनता का दुश्चक्र | निर्धनता का दुश्चक्र तोड़ने के उपाय
- विकासशील अर्थव्यवस्था | विकासशील अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधायें | अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधायें
- द्वैतीय समाज की प्रमुख विशेषतायें | पश्चिमी आर्थिक सिद्धान्त की द्वैतीय समाज में अप्रयोज्यता
- लुइस का विकास मॉडल | श्रम की समस्या का समाधा | लुइस के असीमित श्रम पूर्ति मॉडल की विवेचना
- अदृश्य बेरोजगारी | प्रच्छन्न बेरोजगारी | अदृश्य बेरोजगारी के रूप | अदृश्य बेरोजगारी-पूँजी निर्माण का एक स्त्रोत | अतिरिक्त श्रम-शक्ति का कृषि से स्थानान्तरण का औचित्य
- सततीय विकास | पोषणीय विकास | सततीय विकास के उद्देश्य | सततीय विकास की कूटनीति | पोषणीय विकास के प्रमुख स्तम्भ/नीतियाँ | सततीय विकास की नीतियाँ
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]