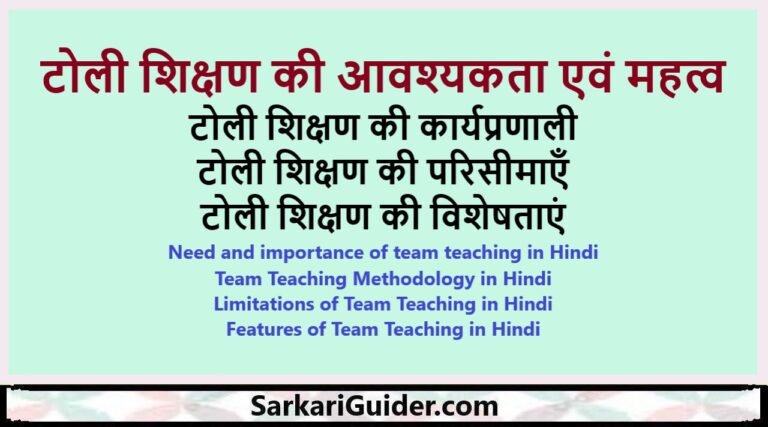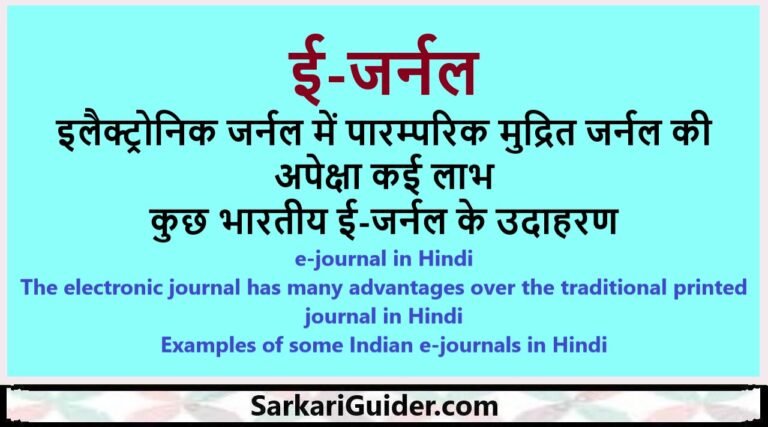अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण के चरण | Steps to build programmed instruction in Hindi

अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण के चरण | Steps to build programmed instruction in Hindi
अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण के चरण
अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण के चरण/सोपान-विद्वान् शिक्षाविदों ने अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण से सम्बन्धित निम्नलिखित नौ सोपानों या चरणों का उल्लेख किया है-
- अनुदेशन निर्माण के लिए प्रसकरण का चयन- लिप्सेट एवं विलियम ने अनुदेशन के प्रकरण के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसरण पर बल दिया है, 1. जिस विषय पर अभिक्रमित अनुदेशन को तैयार किया जाता है उसके प्रकरण पर कार्यक्रम निर्माण पर अध्यापक का स्वामित्व होना तथा उसके प्रति समुचित रुचि भी होनी चाहिए, 2. प्रकरण को ऐसा होना चाहिए, जिसे छोटी-छोटी इकाइयों में बाँटकर उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सके, 3. प्रकरण के आकार को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक होना भी आवश्यक है, 4. सदैव वही प्रकरण चुनना चाहिए जिसका अधिगम परम्परागत विधियों के द्वारा सरलतापूर्वक न किया जा सके और जिसे अधिगम करने में छात्रों को कठिनाई प्रतीत होती हो। अनुदेशन के अन्तर्गत पाठ्यवस्तु के तार्किक क्रम का विशिष्ट महत्व माना जाता है, अतः प्रकरण का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जिसके आधार पर पाठ्य-वस्तु के सभी तत्वों का सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध किया जा सके। छात्रों की आआवश्यकताओ की पूर्ति हेतु प्रकरण किसी विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित होना चाहिए।
- उद्देश्यों के प्रतिपादन एवं उनका व्यावहारिक रूप में लेख- इस अनुदेशन के द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जाता है। ब्लूम (Bloom) ने उद्देश्यों के निर्धारण के लिए ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान प्रयोग, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जैसे उद्देश्य सम्मिलित किए हैं। अभिक्रमित अभिक्रम में भी उद्देश्यों को इन्हीं से निर्धारित किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद उन्हें व्यावहारिक रूप से लिया जाता है। यह कार्य रॉबर्ट मेगर की विधि के अनुसार किया जाता है, जिसे अत्यन्त प्रभावशाली उपयुक्त एवं मनोवैज्ञानिक (व्यवहारवादी) सिद्धान्तों पर आधारित विधि माना गया है।
छात्रों के अन्तिम व्यवहारों के उल्लेख हेतु व्यावहारिक क्रियाओं की पहचान की जाती है, व्यवहार में की जाने वाली परिस्थितियों को परिभाषित किया जाता है, उनके उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने के लिए प्रत्येक उद्देश्य के विषय में रॉबर्ट मेगर के द्वारा उल्लिखित कार्यसूचक क्रियाएँ निर्धारित की जाती है। उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने के लिए पाठ्य-वस्तु के तत्वों, टेक्नोलॉजी में निर्धारित उद्देश्यों और कार्यसूचक क्रियाओं की सहायता प्राप्त की जाती है। इस कार्य में मेगर विधि के अतिरिक्त क्षेत्रीय महाविद्यालय मेंसर की विधि भी सहायक है। चूँकि मेगर विधि में मानसिक क्रियाओं का विशेष महत्व नहीं हैं, अतः आजकल मेंसर विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है।
- अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण के लिए दो तरह के व्यावहारिक उद्देश्यों को प्रतिपादित किया जाता है, प्रथम पूर्व व्यवहार एवं द्वितीय अन्तिम व्यवहार। पूर्व व्यवहार के अन्तर्गत छात्र की अग्रलिखित विशेषताओं को देखा जाता है। 1. अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण के लिए आरम्भ में जिस ज्ञान व कौशल की आवश्यकता होती है, प्रारम्भ में ही उसकी सुस्पष्ट व्याख्या करना, 2. प्रामाणिक प्रवणता परीक्षण के रूप प्रवण के स्तर की व्याख्या करना, 3. परीक्षण के रूप में पूर्ववांछित योग्यताएँ लिखना, 4. छात्रों को वांछित अधिगम की दिशा में अभिप्रेरित करने और पाठ्य वस्तु के प्रति उनकी रुचि को विकसित करने के लिए प्रेरणा के स्तर का उल्लेख करना, 5. छात्रों के बारे में उनकी आयु और स्तर आदि से सम्बन्धित तथ्यों/सूचनाओं का संकलन करना, 6. अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण जिस जनसंख्या के लिए किया जाता हो, उसे परिभाषित करना। पूर्व व्यवहारों का लेखन करने में जनसंख्या का परिभाषीकरण अत्यन्त सहायक माना जाता है।
छात्रों के पूर्व व्यवहारों को ज्ञान करने में परीक्षण का निर्माण, निदानात्मक परीक्षण, संचयी आलेख और छात्रों से सम्बन्धित व्यक्तिगत अनुभव भी पूर्व व्यवहारों का लेखन करने में पर्याप्त सहायता करते हैं।
अभिक्रमित अनुदेशन में उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता देने वाले छात्रों की समस्त अभिक्रियाओं को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है, किन्तु इसके लिए केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों पर ही ध्यान दिया जाता है। छात्रों के अन्तिम व्यवहारों को इन उद्देश्यों, पाठ्य-वस्तु एवं कार्यसूचक क्रियाओं के आधार पर मेगर विधि की ही सहायता से लिखा जाता है। छात्रों में अन्तिम व्यवहारों का मूल्यांकन करने के लिए मानदण्ड परीक्षा का निर्माण करना भी जरूरी माना जाता है। व्यावहारिक उद्देश्यों के लेखन हेतु उनकी विशेषताओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह उद्देश्यों की महत्ता को स्पष्ट करने में सहायक होती है। 1. व्यावहारिक उद्देश्यों के द्वारा उद्देश्यों के स्वरूप को विशेषीकृत करने एवं परीक्षण प्रश्नों के निर्माण में सहायता मिलती हैं, 2. इससे शिक्षण और प्रशिक्षण में समुचित समन्वय बनता हैं, 3. उद्देश्यों की गणना मात्रात्मक रूप में हो सकती है, 4. अपेक्षित अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न किया जा सकता है, 5. अधिगम क्रियाओं का निर्धारण हो सकता है, 6. एक सार्थक मानदण्ड परीक्षण का निर्माण भी किया जा सकता है।
पाठ्य-वस्तु का विश्लेषण – पाठ्य-वस्तु के विश्लेषण हेतु प्रकरण को विभिन्न उप-भागों एवं तत्वों में विश्लेषित किया जाता है। इसके बाद उन्हें तार्किक एवं क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। तार्किक क्रम की उपयुक्तता के निर्धारण में विषय विशेषज्ञों का परामर्श उपयोगी रहता है। पाठ्य- वस्तु विश्लेषण प्रक्रिया के दौरान सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पाठ्य-वस्तु की सूची बनाते समय शिक्षण और अधिगम के आपसी सम्बन्धों पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए ताकि छात्रों को सीखने के समय बाधा न उत्पन्न हो सके।
- मानदण्ड परीक्षण का निर्माण- मानदण्ड परीक्षण को उद्देश्यों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मानदण्ड के अन्तर्गत पाठ्य-वस्तु के स्थान पर उद्देश्यों की माप हेतु कुछ प्रश्नों की रचना की जाती है, जिनमें अमिज्ञान और प्रत्यास्मरण पदों की रचना प्रमुख है। इसमें बहुधा अभिज्ञान सम्बन्धी बहुविकल्पीय मापन सहायक होता है। स्पष्ट है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्नों को मानदण्ड परीक्षण के अन्तर्गत निर्मित करने के पश्चात् इन प्रश्नों की जाँच की जाती है। इस कार्य में सभी पदों को आवश्यक रूप से विश्लेषित किया जाता है। पद-विश्लेषण के अन्तर्गत मानदण्ड परीक्षण में सम्मिलित किए गये प्रश्नों का कठिनाई और विभेदीकरण स्तर भी ज्ञात कर लिया जाता है। विश्लेषण कार्य के बाद कठिनाई स्तर के आधार पर सभी प्रश्नों की व्यवस्था की जाती है। पद- विश्लेषण और अन्तिम मानदण्ड परीक्षण के निर्माण के पश्चात् जनसंख्या में वांछित प्रतिदर्श (Sample) को चुनकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन विश्वसनीयता गुणांक और वैघता गुणांक ज्ञात करके होता है। चूंकि मानदण्ड परीक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है, इस कारण इस परीक्षण के मानकों से ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती।
- अनुदेशन का निर्धारण- अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण के पाँचवें सोपान के अन्तर्गत अनुदेशन प्रारूप से सम्बन्धित निर्णय लिया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित पद निर्धारित किये जाते. हैं—(i) पदों का आकार-रेखीय या शृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के पदों का आकार सुनिश्चित नहीं होता। छात्र एक समय में जितनी पाठ्य-वस्तु को सुगमतापूर्वक अवबोध कर सकता है, उसे ही एक पद (Item) का आकार कहा जाता है। पद का यह आकार छात्रों की आयु व कथानुसार परिवर्तित होता है। पदों के आकार का निर्धारण छात्रों के पूर्व व्यवहार के आधार पर ही होता है।
(ii) अनुक्रिया का रूप- अनुदेशन पदों में अनुक्रिया का रूप पृथक्-पृथक् होता है। प्रायः छात्र स्वयं ही अनुक्रिया निर्माण करते है। छात्रों को उन्हीं पदों में सही अनुक्रिया चुननी होती है। अनुक्रिया के लिए छात्रों को दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का ही चयन करना होता है।
(iii) अनुबोधक का रूप- शिक्षण के पदों में अतिरिक्त उद्दीपन को प्रयुक्त किया जाता है जो कि छात्रों को सही अनुक्रिया के लिए सहायता देते हैं। इनको ही ‘अनुबोधक’ कहा जाता है। चूँकि यह अनुबोधक कई प्रकार के होते हैं, इस कारण इस सन्दर्भ में यह निर्णय भी लिया जाता है कि वस्तुतः किस प्रकार के अनुबोधक को प्रयुक्त किया जाना उचित होगा।
(iv) नियम-उदाहरण प्रणाली- पद-रचना करते समय कुछ उदाहरणों/नियमों का भी प्रयोग होता है। छात्रों को अनुक्रिया हेतु नियम दिये जाते हैं। नियम का उदाहरण अपूर्व रखा जाता है। कभी-कभी कुछ पक्षों में पूर्ण उदाहरण देते हुए उसमें नियम को अपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे अपूर्ण उदाहरण और नियम को छात्र स्वयं ही अनुक्रिया के द्वारा पूर्ण करते हैं। स्पष्ट है कि छात्र स्व अनुक्रिया के माध्यम से नवीन ज्ञान/अनुभव प्राप्त करते हैं। छात्र का अभिक्रमिक ही इस नियम और उदाहरण प्रणाली के बारे में निर्णय लेता है।
(v) सही अनुक्रिया हेतु स्थान- अनुदेशन प्रारूप के निर्धारण के अन्तर्गत छात्रों को सही अनुक्रिया हेतु स्थान की व्यवस्था कई प्रकार से की जाती है। छात्रों को पदों के साथ ही अनुक्रिया प्रदान की जाती है। उन्हें नये पद के साथ पूर्व-पद की सही अनुक्रिया दी जाती है। इस सन्दर्भ में अनुदेशन अभिक्रमिक ही यह निर्णय लेता है कि छात्रों को सही अनुक्रिया हेतु स्थान की व्यवस्था कैसे की जा सकती है।
- अभिक्रमित पदों की रचना और व्यक्तिगत जांच- अनुदेशन पदों का लेखन करना एक कठिन कार्य माना जाता है। अभिक्रमिक को अनुदेशन पदों की रचना करते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यथा- 1. पाठ्य-वस्तु का स्वरूप, 2. अन्तिम व्यवहार का स्वरूप और 3. पूर्व व्यवहार का स्वरूप। छात्रों में वांछित अन्तिम व्यवहार को विकसित करने हेतु एक उचित अनुदेशन के प्रारूप का चयन किया जाता है। इससे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने हेतु एक समुचित उद्दीपन के रूप को चुना जाता है। इसे ही पदों के विषय का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। पद वस्तुतः पाठ्यवस्तु का ही एक अंश है, जिसे छात्र एक समय में पढ़ता है। पद का आकार वस्तुतः कितना हो, दूसरा निर्धारण स्वयं छात्र द्वारा ही किया जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में कुछ ही शब्द या एक दो वाक्य होते हैं। अर्थात् इसका आकार छोटा होता है जबकि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों का आकार बड़ाश्रहोता है। प्रत्येक पद में छात्र द्वारा एक अनुक्रिया की जाती है जो कि दो प्रकार की होती है-1. बाह्य अनुक्रिया, 2. आन्तरिक अनुक्रिया। प्रत्येक पद के तीन भाग होते हैं-(i) उद्दीपन- इसके अन्तर्गत सूचना एवं पाठ्य-वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है और छात्रों के सम्मुख कुछ परिस्थितियों भी उत्पन्न की जाती है।(ii) अनुक्रिया- प्रत्येक उद्दीपन हेतु छात्र या तो एक अनुक्रिया करता है या अनुक्रिया का चयन करता है।
(iii) पुनर्बलन- छात्र स्वयं ही अपनी अनुक्रिया की जाँच करता है। वह सही अनुक्रिया के द्वारा नवीन ज्ञानार्जन करता है, जिसके कारण उसे अगला पद पढ़ने हेतु पुनर्बलन प्राप्त होता है।
पद-लेखन सम्बन्धी नियम- अनुदेशन अभिक्रमक को पद-लेखन के पहले यह निश्चित करना आवश्यक है कि उसे कौन-सी सूचनाएँ प्राप्त हैं और कौन-सी अपेक्षित। सारी सूचनाओं का संकलन और उन्हें व्यवस्थित करने के बाद पद लेखन से पूर्व ही कुछ नियमों पर ध्यान देना चाहिए,
यथा-
- पदों के विश्लेषण मुक्त नहीं होना चाहिए,
- सम्बन्ध कारकों के वाक्यों को उपयुक्त नहीं करना चाहिए,
- पदों को जटिल भाषा में नहीं लिखना चाहिए,
- सुनिश्चित शब्दावली को प्रयुक्त नहीं करना चाहिए।
श्रेष्ठ/उत्तम पदों की विशेषताएँ-
- श्रेष्ठ पदों का आकार सदैव छात्रों के स्तर के अनुकूल ही होता है,
- उत्तम पदों की भाषा सुस्पष्ट और बोधगम्य होती है,
- श्रेष्ठ पदों के विषय में सम्बन्धित शब्दावली प्रयुक्त की जाती है,
- अच्छे पदों से छात्रों में सीखने की संभावना बढ़ती है,
- पदों का स्वरूप न तो बहुत कठिन और न अधिक सरल रखा जाता है,
- श्रेष्ठ पदों की अनुक्रियाओं का सम्बन्ध छात्र के अन्तिम व्यवहार से होता है,
- श्रेष्ठ पद के अन्तर्गत समुचित अनुबोधकों के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है,
- उत्तम पदों का स्वरूप ऐसा होता है, कि विद्यार्थी एक ही प्रकार की अनुक्रिया करने का अवसर पाते हैं,
- श्रेष्ठ पद उद्दीपन और अनुक्रिया की अमिक श्रृंखला पर आधारित होते हैं।
पदों के प्रकार (Types of Items)- अभिक्रमित अनुदेशन के अन्तर्गत प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद इत्यादि चार प्रकार के पद निर्मित किए जाते है। इनमें से प्रस्तावना पदों को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इनके ही अन्तर्गत छात्रों के पूर्व-ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ सम्बन्धित किया जाता है। किन्तु इनका निर्माण अन्य पदों की तुलना में कठिन होता है। दूसरे प्रकार के शिक्षण पद पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतीकरण और उद्देश्य प्राप्ति में सहायता देते हैं। इन्हीं के आधार पर छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर पाते हैं। किन्तु ऐसे पद कभी भी 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। यह तार्किक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इनकी रचना में पर्याप्त अनुबोधकों का ध्यान रखा जाता है। अभ्यास पदों में उर्ध्व अनुबोधक प्रयोग किए जाते हैं और शनैः- शनैः इनकी संख्या न्यूनतम होती जाती है। इन पदों का उद्देश्य छात्रों को प्राप्त हुए ज्ञान का अभ्यास कराना ही है। परीक्षण पदों के उद्देश्य की जाँच करना है। यह अनुबोधकहीन पद होते हैं। सम्पूर्ण अभिक्रम में परीक्षण पदों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
चारों प्रकार के पदों को व्यवस्थित करने के लिए दो क्रमों का अनुसरण होता है—1. तार्किक क्रम, जिसमें अभिक्रम तैयार करने वाला पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतीकरण करता है, 2. व्यावहारिक या मनोवैज्ञानिक क्रम, जिसमें उस क्रम पर ध्यान दिया जाता है, जिसके आधार पर छात्र पाठ्यवस्तु का अधिगम सुगमतापूर्वक कर सकता है। यह क्रम उद्देश्यों की पूर्ति, छात्रों में वांछित व्यवहार का परिवर्तन तथा अभिक्रमित अनुदेशन को प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से अधिक उपयुक्त माना जाता है। पद रचना करते समय यह भी देखा जाता है कि एक पद की अनुक्रिया अगले पद से अधिक उद्दीपन का कार्य है।
- समूह पर जाँच के बाद पुनरावृत्ति, सम्पादन व अन्तिम रूप की तैयारी- पद-रचना के बाद व्यक्तिगत जाँच करके पदों में पायी जाने वाली त्रुटियों को ज्ञात करके और उनमें वांछित सुधार करके अभिक्रम का प्रथम प्रारूप निर्मित किया जाता है। व्यक्तिगत जाँच करने के पश्चात् उसकी कई प्रतिलिपियाँ तैयार कर एक समूह पर उसकी जाँच की जाती है, समूह पर जाँच करने के लिए एक न्यादर्श (सैम्पल) को चुना जाता है। इसमें पूर्व व्यवहार को धारण करने वाला छात्रों को ही सम्मिलित किया जाता है। इनके चयन के लिए पूर्व- परीक्षण को प्रयुक्त करते हैं। इस न्यादर्श में कम-से-कम 40 छात्रों की संख्या आवश्यक मानी जाती है। न्यादर्श के चयन और पूर्व परीक्षण के पश्चात् छात्रों को अभिक्रम के अध्ययन तथा अनुक्रियाओं के बारे में आवश्यक निर्देश भी प्रदान किये जाते है। छात्रों को अभिक्रमित पुस्तिका और उत्तर-पत्रक दिये जाते है। जो छात्र अपना अध्ययन समाप्त कर लेते हैं, उनसे दोनों चीजें वापस ले ली जाती है। छात्रों से उत्तर पत्रक प्राप्त करने के बाद उनका अंकन होता है। जिन पदों की त्रुटि दर 10 प्रतिशत से अधिक होती है उनमें सुधार किया जाता है। इस तरह से अनुदेशन के अन्तिम रूप को तैयार करके पुनः उसकी जाँच, पुनरावृत्ति और सुधार के बाद अभिक्रमित पुस्तिका को मुद्रित होने के लिए भेज दिया जाता है।
- मूल्यांकन और वैधता परीक्षण- इस सोपान के अन्तर्गत समग्र/ जनसंख्या में से एक न्यादर्श का चयन होता है। इसमें छात्र संख्या 50 से 100 तक हो सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुदेशन की विशेषताओं का सम्पूर्ण रूप से मूल्यांकन करना ही है। न्यादर्श चयन के बादश्रअनुदेशन को छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात् छात्र अभिक्रमित पुस्तिका का अध्ययन करके उत्तर-पत्रकों पर अपनी-अपनी अनुक्रियाओं का अंकन करते हैं। प्रत्येक छात्र को इन उत्तर-पत्रकों का अध्ययन करके उत्तर पत्रकों और समाप्त करने का समय भी लिखना पड़ता है। इसके बाद छात्रों के निष्पत्ति और उद्देश्यों के बारे में जानकारी पाने के लिए मानदण्ड परीक्षण को पुनः प्रसारित किया जाता है। अभिक्रमित अध्ययन में छात्रों की अभिवृत्ति- मापन के लिए मानदण्ड परीक्षण के बाद उन्हें अभिवृत्ति सूची भरने के लिए प्रदान की जाती है। जिनक्षमानदण्डों के आधार पर अनुदेशन की प्रभावोत्पादकता के विषय में निर्धारण किया जाता है, वे आन्तरिक और बाह्य दो प्रकार के होते है। प्रथम प्रकार के आन्तरिक मानदण्डों में त्रुटि-पद, अनुदेशन का घनत्व, अनुदेशन-चढ़ाव का क्रम और पद सूची सम्मिलित होती है, जबकि बाह्य मानदण्डों में छात्रों का निष्पत्ति, स्तर, अभिवृत्ति, गुणक और 90/90 स्तर मानदण्ड सम्मिलित किया जाता है।
शैक्षिक तकनीकी – महत्वपूर्ण लिंक
- कम्प्यूटर हार्डवेयर | कम्प्यूटर हार्डवेयर की विभिन्न इकाइयाँ | हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के आधारभूत सिद्धान्त | सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कार्य | Computer Hardware in Hindi | Different Units of Computer Hardware in Hindi | Fundamentals of Hardware and Software in Hindi | Functions of Central Processing Unit in Hindi
- इनपुट यूनिट | इनपुट यूनिट के बारे में बताइए? | कम्प्यूटर इनपुट की विभिन्न इकाइयाँ बताइए? | Input Unit in Hindi
- रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमण | शिक्षा में अनुदेशन शिक्षण, अधिगम एंव प्रशिक्षण | रेखीय अभिक्रमित अध्ययन की विशेषाएँ | शाखीय य आंतरिक प्रकार अभिक्रमित अध्ययन | रेखीय अभिक्रम की मान्यतायें/अवधारणायें | रेखीय अभिक्रम की सीमाएँ | शाखीय अभिक्रम/अनुदेशन की विशेषताएँ | शाखीय अभिक्रम की सीमाएँ
- अनुदेशनात्मक तकनीकी या प्रणाली | अनुदेशन तकनीकी की मान्यताएँ | अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएँ | अनुदेश तकनीकी की विषय-वस्तु | अनुदेशन तकनीकी के सोपन
- अभिक्रमित अनुदेशन | अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार | रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का एक उदाहरण
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]