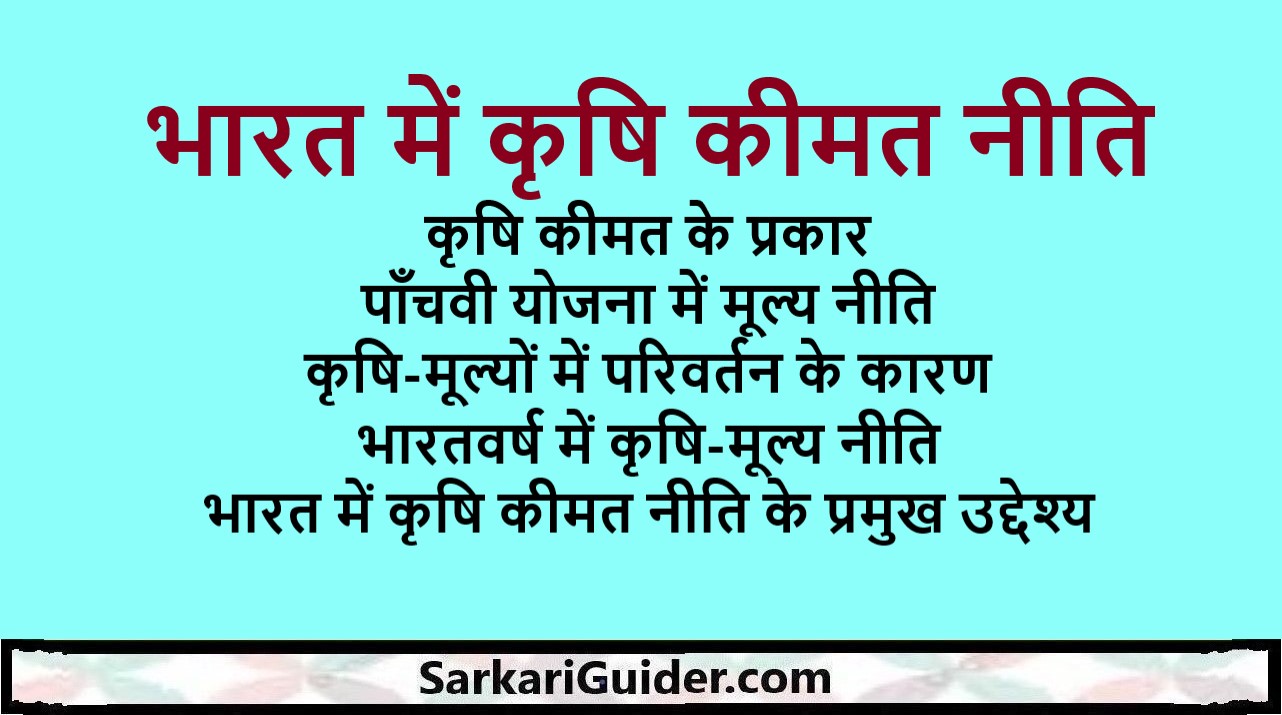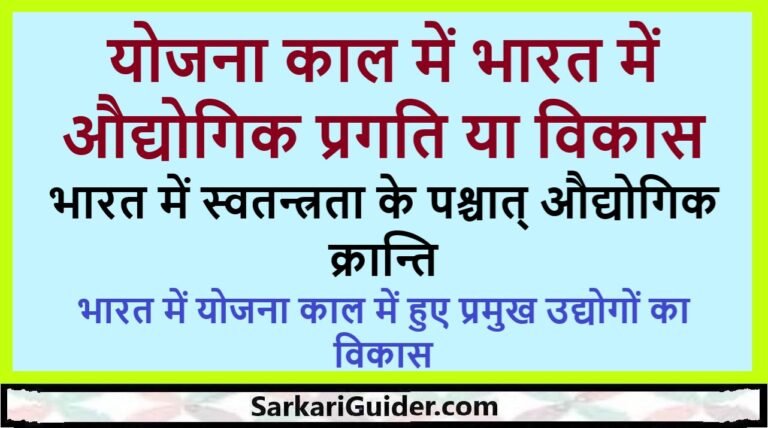भारत में कृषि कीमत नीति | कृषि कीमत के प्रकार | पाँचवी योजना में मूल्य नीति | कृषि-मूल्यों में परिवर्तन के कारण | भारतवर्ष में कृषि-मूल्य नीति | भारत में कृषि कीमत नीति के प्रमुख उद्देश्य

भारत में कृषि कीमत नीति | कृषि कीमत के प्रकार | पाँचवी योजना में मूल्य नीति | कृषि-मूल्यों में परिवर्तन के कारण | भारतवर्ष में कृषि-मूल्य नीति | भारत में कृषि कीमत नीति के प्रमुख उद्देश्य | Agricultural Price Policy in India in Hindi | Types of Agricultural Prices in Hindi | Price Policy in the Fifth Plan in Hindi | Due to change in agricultural prices in Hindi | Agri-price policy in India in Hindi | Major Objectives of Agricultural Price Policy in India in Hindi
भारत में कृषि कीमत नीति
कृषि उत्पादों की कीमतों को कृषि कीमत कहा जाता हैं, अत कृषि कीमत विभिन्न पहलुओं एवं वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करती हैं एवं उनमें प्रारम्भिक संबंध प्रदर्शित करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निश्चित करना हैं।”
कृषि कीमत के प्रकार (Kinds of agriculture price)-
यह निम्न प्रकार की होती हैं- (i) मंडी कीमत (ii) सामान्य कीमत (iii) न्यूनतम समर्थनमूल्य (iv) वसूली खरीद मूल्य (v) निर्गमन आवंट मूल्य
योजना प्रणाली में आरम्भ से ही मूल्यों पर नियन्त्रण रखकर कीमत स्तर में स्थिरता लाने का लक्ष्य रहा हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना- काल (1951-56) में अनुकूल प्रकृति के कारण हुई उत्पादन वृद्धि से कोरिया युद्ध के कारण आयी निर्यात की वृद्धि से तथा मुद्रा-प्रसार में अपेक्षाकृत कम वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि कोई भयानक समस्या नहीं रही।
द्विपीय पंचवर्षीय योजना काल में 1957-58 के बाद जब कृषि उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई, निर्यात से सहयोग नहीं मिला और औद्योगिक विकास पर तेजी से व्यय बढ़ने लगा तब मुद्रा-प्रसार ने जोर पकड़ा और मूल्य-स्तर में वृद्धि समस्या का रूप लेने लगी। यह कीमत-स्तर वृद्धि एक नियोजन के बाद दूसरे नियोजन तक क्रमशः भयानक रूप लेती हुई बढ़ती जा रही हैं।
बढ़ती हुई कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति की दर को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। केवल बढ़ती हुई कीमतें एक अर्द्ध-स्फीति एक अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं हैं। एक विशेश दर पर मुद्रास्फीति एक अर्द्ध-विकसित देश की जनता की क्रयशक्ति बढ़ाती हैं। और उसी बढ़ी क्रयशक्ति के कारण उद्योग-धन्धों तथा रोजी-रोजगार में वृद्धि होती हैं। साथ ही, जब एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के लिये प्रयास करती हैं तो वहाँ मुद्रा-प्रसार अवश्य होता हैं। मुद्रा-स्तर के कारण उस अर्थव्यवस्था में एकाकक क्रय शक्ति बढ़ती हैं, किन्तु क्रय शक्ति की वृद्धि के साथ माँग तो बढ़ जाती हैं, पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति नहीं बढ़ पाती अत कीमतें बढ़ने लगती हैं।
सन् 1961 तक वास्तव में कीमत-नीति के संचालन को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। अत: रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve bank of India) के कन्धों पर कीमतों के नियन्त्रण का भार दिया गया। रिज बैंक अपनी साख व मुद्रा-नीति के माध्यम से कीमतों पर नियन्त्रण करता रहा। मुख्य रूप से बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर चयनात्मक नियन्त्रण के माध्यम से रिजर्व बैंक इस कार्य को कर रहा था, किन्तु इसी बीच कीमतों में वृद्धि के दर ने जो तेजी दिखाई उससे आर्थिक स्थिति पर अशुभ लक्षण स्पष्ट होने लगे थे। फलस्वरूप कीमतों की दिशा में तृतीय पंचवर्षीय योजना में अधिक सतर्कता दिखायी गयी। योजना आयोग ने कीमत नीति का भारत के सन्दर्भ में दो लक्ष्यों की प्राप्ति से सम्बन्ध जोड़ा-
- योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं और टारगेट के अनुरूप ही पारस्परिक कीमतों (Relative prices) में परिवर्तन हो, ताकि लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- निम्न आय-स्तर के लोगों के उपभोग में आने वाली अनिवार्य वस्तुओं की कीमत में होने वाली विशेष वृद्धि को रोके।
ये दो उद्देश्य प्रथम एवं द्वितीय योजना में भी थे, किन्तु जिस प्रकार की मूल्य नीति दोनों (प्रथम व द्वितीय योजनाओं) में अर्थव्यवस्था में साख एवं मुद्रा के नियन्त्रण द्वारा मुख्य रूप से रिजर्व बैंक के माध्यम से इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अपनायी गयी, उससे इच्छित परिणाम तो नहीं मिले वरन् कीमतों पर इस प्रकार की वृद्धि 1957-58 में हुई जो अर्थव्यवस्था में आने वाली आर्थिक विषमता की सूचना देने के लिये पर्याप्त थी। थोक मूल्य-स्तर बढ़ा और रहन-सहन के स्तर की लागत बढ़ी।
तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में चीन संघर्ष तथा प्राकृतिक विपर्यय के कारण कीमतों में वृद्धि बहुत तेजी से होने लगी। सूखा, बाढ़, सरकारी व्यय में वृद्धि, घाटे के वित्त- व्यवस्था, विदेशी व्यापार में कमी तथा पड़ोसी देशों में संघर्ष, कुल मिलाकर यहाँ की अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि की तीव्रता देखी गयी।
पाँचवी योजना में मूल्य-नीति-
पाँचवीं योजना काल में मूल्य-नीति को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया। 1 अप्रैल, 1974 से पाँचवीं योजनाकाल आरम्भ हुई। ‘दामबाँधो’ इस योजनाकाल में प्रमुख नारा था। योजना के प्रथम वर्ष में कीमत-स्तर अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ी, फलस्वरूप कीमत-नीति में कुछ विशेष तथ्यों पर विशेष जोर दिया गया
- माँग पर अंकुश- वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग पर अंकुश रखने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इस दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाये गये
(क) जनसंख्या नियन्त्रण को व्यापक बनाया गया।
(ख) मुद्रा एवं साख पूर्ति पर कड़ा नियन्त्रण रेखा गया।
(ग) अनिवार्य जमा योजना एवं अन्य योजनाओं के द्वारा अतिरिक्त क्रयशक्ति का व्यय रोका गया।
(घ) घाटे की वित्तव्यवस्था की कड़ी समीक्षा हुई।
(इ) अनुत्पादक व्यय घटाये गये।
- उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता का प्रयास- कृषि उत्पादन में सर्वोन्मुखी विकास का प्रयास किया गया। उद्योगों का उत्पादन भी बढ़ाने का प्रयास किया गया। आयात पर तथा विदेशी पूँजी पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा। आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाया गया। सर्वाजनिक उद्योगों का विस्तार किया गया तथा इनके उत्पादन बढ़ाये गये। जमाखोरी पर कड़ा अंकुश रखा गया।
- नयी वितरण व्यवस्था- नियन्त्रित मूल्य पर अनिवार्य वस्तुओं की बिक्री वैधानिक हो गयी। कीमत-सूची एवं कीमत-पट्ट (price tag) लगाना अनिवार्य हो गया। अनिवार्य लेवी- व्यवस्था को खाद्यात्र संग्रह की दृष्टि से मजबूत बनाया गया। सहकारी विक्रय व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया। मिलावट एवं मुनाफाखोरी को कड़ी सजा का विषय ही नहीं समाज में निन्दनीय बनाने के लिए ऐसे लोगों का देश व्यापी प्रचार किया गया।
- एकाधिकारी व कालाधन पर नियन्त्रण- एकाधिकारियों एवं कालेधन के मालिकों के घर पर छापे मारे गये, ताकि मुनाफाखोरी के प्रति भय उत्पन्न हो ।
- औद्योगिक अशान्ति पर अंकुश- हड़ताल तथा तालेबन्दी दोनों की नियन्त्रित किया गया, ताकि उत्पाद कार्य ठीक से चले। सन् 1976 तक इन कठोर कदमों के कारण क्रीमतें गिरने लगी थीं, किन्तु इस गिरावट के असर को पेट्रोलियम उत्पादक देश ने पेट्रोल की कीमते बढ़ाकर बहुत कुछ प्रभावित किया। पुनः आपातकालीन व्यवस्था के विरोध के फलस्वरूप जनता सरकार आयी।
इसमें निम्नलिखित नये उपाय मूल्य-स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए किया गये-
(1) नोट विमुद्रीकरण- रु1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया।
(2) स्वर्ण की बिक्री- रिजर्व बैंक ने स्वर्ण की नीलामी की।
(3) खाद्य जोनों का अन्त- अन्न उत्पादन की दृष्टि से देश को कई जोनों में बाँटा गया था और एक जोन से दूसरे जोन में खाद्यात्र लाना प्रतिबन्धित था। वह प्रतिबन्ध उठा लिया गया।
(4) चीनी तथा कुछ अन्य वस्तुओं पर से नियन्त्रण हटा लिये गये।
(5) ग्राफ परक योजनाओं को चलाया गया तथा उत्पादन वृद्धि के उपाय बढ़ाये गये।
कीमत वृद्धि एवं बेरोजगारी दो ऐसी समस्याएँ हैं जिनसे छुटकारा पाने का प्रयास किया जा रहा हैं, किन्तु कीमतें बढ़ती जा रही हैं। खजिन, कच्चा माल, ईंधन-बिजली, औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि का परिणाम 1977 में मूल्य-स्तर की वृद्धि पर हैं। खाद्यान्न की कीमतें 1977 में घटी थीं, किन्तु इधर खाद्यान्नों की कीमतें भी पुनः वृद्धि की ओर जा रही हैं।
वास्तव में भारतवर्ष में मूल्य वृद्धि को नियन्त्रित करता हैं, तो तीन तरफ का घेरा बनाकर मूल्य को बाँधना होगा-(क) उत्पादन में वृद्धि एवं माँग पर अंकुश रखना होगा। (ख) वितरण-व्यवस्था को चुस्त और भ्रष्टाचार से मुक्त रखना होगा। (ग) ऐसे कानून बनाने होंगे जो कीमत-व्यवस्था को तोड़ने वालों को कम-से-कम 5 वर्ष का सश्रम कारावास का दण्ड दिला सकें और ऐसे अपराधियों का नाम एवं व्यवसाय सम्पूर्ण देश में उनके अपराध-विवरण और सजा की अवधि के वर्णन के साथ प्रचारित हो, ताकि उन्हें मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी भ्रष्ट आचरण करने से रोका जा सके।
भारतवर्ष की कृषि मूल्य-नीति-
भारतवर्ष ऋणग्रस्त; निर्धन एवं छोटे कृषकों का देश हैं। यदि ये कृषक अपनी उपज को सर्वदा लाभ पर नहीं बेच पायेंगे या इन्हें यदि अपनी उपज मूल्य के प्रति भयंकर अनिश्चितता रहेगी तो एक ओर इनकी दुर्दशा बढ़ती ही जायेगी तो दूसरी ओर कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा। जिससे कृषि-पदार्थों का अभाव रहेगा। और अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त रहेगी। इस प्रकार राष्ट्रीय आर्थिक विकास के मार्ग में कृषि क्षेत्र बाधक रहेगा। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही कृषि मूल्य नीति को कृषकों तथा उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से उचित बनाने का प्रयास चल रहा हैं।
कृषि-मूल्यों का स्वरूप-
भारतवर्ष में कृषि-मूल्यों का परिवर्तन प्रथम पंचवर्षीय योजना में गिरावट की ओर था। 1951 की अपेक्षा 1956 में कृषि-मूल्य लगभग 20% कम हुए थे, किन्तु दूसरी योजना में प्रायः कृषि-मूल्य बढ़ते गये और यह वृद्धि लगभग 40.7% रही। दूसरी योजना के बाद जो वृद्धि का क्रम रहा वह निरन्तर चला आया है। तीसरी योजना के अन्त में कृषि-मूल्य 30% बढ़े। तीसरी योजना के अन्त में तीन वार्षिक योजनाएँ चली। सन् 1966-67 से -1968-69 तक। 1966-67 में कृषि-मूल्य बहुत ऊंचे हो गये। 1968-69 में कीमतें अच्छी फसल के प्रभाव में कुछ स्थिर-सी रहीं। इसके बाद पुर कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति आयी जो 1970- 71 में 100, 1980-81 में 257.3 और 1988-89 में 435.3 हो गयी, इस प्रकार 1970- 71 और 1988-89 के बीच 28 वर्षों में थोक कीमतें लगभग साढ़े चार गुना बढ़ गयीं।
वैसे तो कीमतों का बढ़ना दूसरी योजना के समय से शुरू हुआ, लेकिन सातवें दशक के मध्य से कीमत-वृद्धि अधिक तेज हो गयी, फिर भी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहीं। कीमतों का बढ़ना कभी बहुत अधिक, कभी बहुत कम और दो-एक वर्षों में स्थिर रही या घटी गयी। उदाहरणार्थ, कीमतें 1974-75 में 25%, 1979-80 में 21%, 1980-81 में 17 प्रतिशत और 1987- 88 में लगभग 11% से बढ़ी। 1978-79, 1980-81, 1982-83 और 1986-87 में हुई वृद्धि क्रमशः कम थी- क्रमशः 4.5%, 2.4%, 7.2% और 5.1% 1 वर्ष 1977-78 में कीमतें स्थिर रहीं और 1975-76 में तो कीमतें 6.5% से गिर गयीं। वर्ष 1993-94 में कृषि थोक सूचकांक मूल्य 194 थे, जो बढ़कर 2011-12 में 152.19 हो गयी।
कृषि-मूल्यों में परिवर्तन के कारण-
कृषि मूल्यों में उतार-चढ़ाव के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
A माँग सम्बन्धी कारण- जैसे-जैसे नियोजित विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, वैसे-वैसे वस्तुओं की माँग बढ़ती जा रही हैं। इस बढ़ती माँग को दो पक्षों में बाँट कर विश्लेषण किया जा सकता हैं।
- खाद्यान्न की माँग- जनसंख्या की वृद्धि तथा क्रय-शक्ति का विस्तार भारतवर्ष में खाद्यान्त्रों की माँग तेजी से बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर खाद्यान्त्रों के उत्पादन में वृद्धि असन्तोषजनक रही हैं। परिणामस्वरूप कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि अल्प तथा निम्न आय वर्गों के उपभोक्ताओं के लिये भयाकन एवं कष्टदायक होती हैं, इसका प्रभाव व्यापाक रूप लेता हैं क्योंकि जनसंख्या में अल्प तथा निम्न आय वर्ग के उपभोक्तओं का प्रतिशत सर्वाधिक हैं।
- औद्योगिक कच्चे माल की माँग- देश में नियोजित ढंग से उद्योगों का तीव्र विकास किया जा रहा हैं। यह भी प्रयास चल रहा हैं कि रहन-सहन का स्तर उठे और इसलिये औद्योगिक उत्पादनों की खपत बढ़ें। उदाहरण के लिये, औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाले खाद्य पदार्थ चीनी, कपड़ा (सूती रेखमी इत्यादि), जूट के सामान, नारियल इत्यादि के द्वारा बनने वाली वस्तु इत्यादि अनेक पदार्थों की खपत प्रतिवर्ष बढ़ रही हैं। किन्तु इसका उत्पादन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, क्योंकि इनके लिए कच्चे माल जैसे-गन्ना, कपास, जूट, नारियल, मूँगफली, तिलहन इत्यादि का उत्पादन मन्द गति से बढ़ रहा हैं। कभी-कभी इनके उत्पादन घट जाते हैं। फलस्वरूप इनकी कीमतें, साथ ही इनके द्वारा बनने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं।
- पूर्ति सम्बन्धी- कृषि वस्तुओं की पूर्ति सन्तुलित रखना अपने आप में बड़ी समस्या बनी हुई हैं। इस समस्या के भयंकर रूप में निम्नलिखित घटक काम करते हैं-
- उत्पादन में कम वृद्धि- पुरानी कृषि विधि, मानसून पर निर्भरता, प्राकृतिक प्रकोप की बहुलता, अच्छे खाद, बीज और सिंचाई सुविधा का अभाव, कृषकों की निर्धनता और अज्ञानता कृषि उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग में बाधक हैं। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर अत्यन्त कम हैं।
- भण्डारण तथा एकत्रीकरण की कुव्यवस्था- फसल की कटाई से लेकर उनको इकट्ठा करने तक की व्यवस्था इस प्रकार की हैं कि बीच में अनाज बहुत अधिक नष्ट हो जाते हैं। चूहे व कीड़े भी अनाजों की बड़ी हानि करते हैं। फलस्वरूप कृषि की शुद्ध पूर्ति कम होती हैं। .
- विक्रय अधिकोष को अल्पता-जो कुछ उत्पादन होता हैं, उसका बहुत अधिक भाग ग्रामीण उत्पादक स्वयं उपभोग कर लेते हैं। हमारे कृषकों में अभी तक व्यावसायिक प्रवृत्ति पूरी तरह नहीं फैल पायी हैं। फलस्वरूप व्यवसाय के लिए कृषि उनका उद्देश्य नहीं बन पाया हैं। इसलिए बिक्री के लिए उत्पादन का अंश बहुत थोड़ा होता हैं।
- विपणन व्यवस्था में त्रुटि-मण्डियों की स्थिति इतनी कष्टकारी होती हैं कि साधारण किसान मण्डी जाकर बेचने से घबराते हैं। साथ ही परिवहन एवं आवागमन की दुर्दशा भी विपणन के मार्ग में बाधक हैं।
- जमाखोरी- आढ़तियों, बड़े व्यापारी तथा सट्टेबाज जमाखोरी बढ़ाते हैं। फलस्वरूप कृषि वस्तुओं की पूर्ति गड़बड़ाती है और इसका फायदा उठाते हैं।
- बढ़ती लागतें- ऊँचा लगान, ऊंची सिंचाई दर, महँगे खाद-बीच व कृषि यन्त्र कृषि क्षेत्र में लागतों को तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। इन बढ़ती लागतों के कारण कृषि उत्पादन की कीमतों में वृद्धि तेजी से होती जा रही हैं। इन लागतों का प्रभाव छोटे एवं सीमान्त कृषकों पर बहुत अधिक हैं।
भारतवर्ष में कृषि-मूल्य नीति-
कृषि-मूल्य निर्धारण करते समय भारत सरकार के समक्ष निम्नलिखित उद्देश्य स्पष्ट रूप से रहते हैं-
- कीमत स्तर पर नियन्त्रण– इसे कीमत स्थिरीकरण का उद्देश्य भी कहते हैं। कीमतों का बहुत अधिक बढ़ना या बहुत नीचे घटना दोनों को क्रमशः उपभोक्ता एवं कृषकों की दृष्टि से नियन्त्रित करके सदा ऐसे स्तर पर रखना पड़ता हैं कि कृषकों को समुचित लाभ मिले। ऐसा तभी हो सकता हैं जब- (I) कृषि लागतों को देखते हुए ऐसी व्यवस्था का पालन किया जाय कि सामान्य लाभ सहित औसत लागत के नीचे कीमतें कभी न गिरें, वरन् लाभ मर्यादित रूप से मिलता रहे। (II) वितरण व्यवस्था एवं बाजार पर इस प्रकार नियन्त्रण रखना कि कीमतें इतनी ऊँची न बढ़े कि साधारण उपभोक्ता पर आर्थिक भार बढ़े।
- कीमतों के ढाँचे पर नियन्त्रण- विभिन्न कृषि वस्तुओं की कीमतों में या इस प्रकार की कीमतों में परिवर्तन को रोकना जिसका प्रभाव उस वस्तु पर या दूसरी वस्तुओं पर हानिकारक हो या किसी वस्तु का उत्पादन ही हतोत्साहित हो।
- लागतों में नियन्त्रण तथा कृषि क्षेत्र में निवेश एंव आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन- कीमत नीति ऐसी होनी चाहिए कि उत्पादन की प्रक्रिया एवं उत्पादकता दोनों कृषि में बढ़े, अर्थात् कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़े और कृषि कला में उन्नति हो।
अर्थशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- भारत की 1948 की औद्योगिक नीति | 1948 की औद्योगिक नीति का आलोचना | 1956 की भारतीय औद्योगिक नीति | 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ | 1956 की औद्योगिक नीति की आलोचना | 1980 की औद्योगिक नीति | 1980 की औद्योगिक नीति की आलोचनाएँ
- बहुराष्ट्रीय निगमों का अर्थ | बहुराष्ट्रीय निगमों की विशेषताएँ | भारत अर्थव्यवस्था के विकास में बहुराष्ट्रीय निगमों का योगदान | भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों के योगदान
- सार्वजनिक उपक्रम का अर्थ एवं परिभाषा | सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्य | सार्वजनिक उपक्रम के गुण | सार्वजनिक उपक्रम के दोष | भारत अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों को योगदान | सार्वजनिक उपक्रम की प्रमुख समस्याएँ एवं उनके समाधान के सुझाव
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्य
- समाष्टिभावी आर्थक नीति | मौद्रिक नीति मण्डल का मॉडल | मण्डल के मॉडल की आलोचनाएँ | समसामयिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इसके प्रमुख उद्देश्य
- भारतीय कृषि की समस्याएँ | कुल मुख्य देशों का उत्पादन | कृषि समस्याओं के समाधान का उपाय | कृषि की निम्न संवृद्धि दर के प्रमुख कारण
- भारतीय उद्योगों में निकीकरण से लाभ | नवीन आर्थिक नीति में निजीकरण एवं सुधार कार्यों का औद्योगिक उत्पाद पर प्रभाव
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]