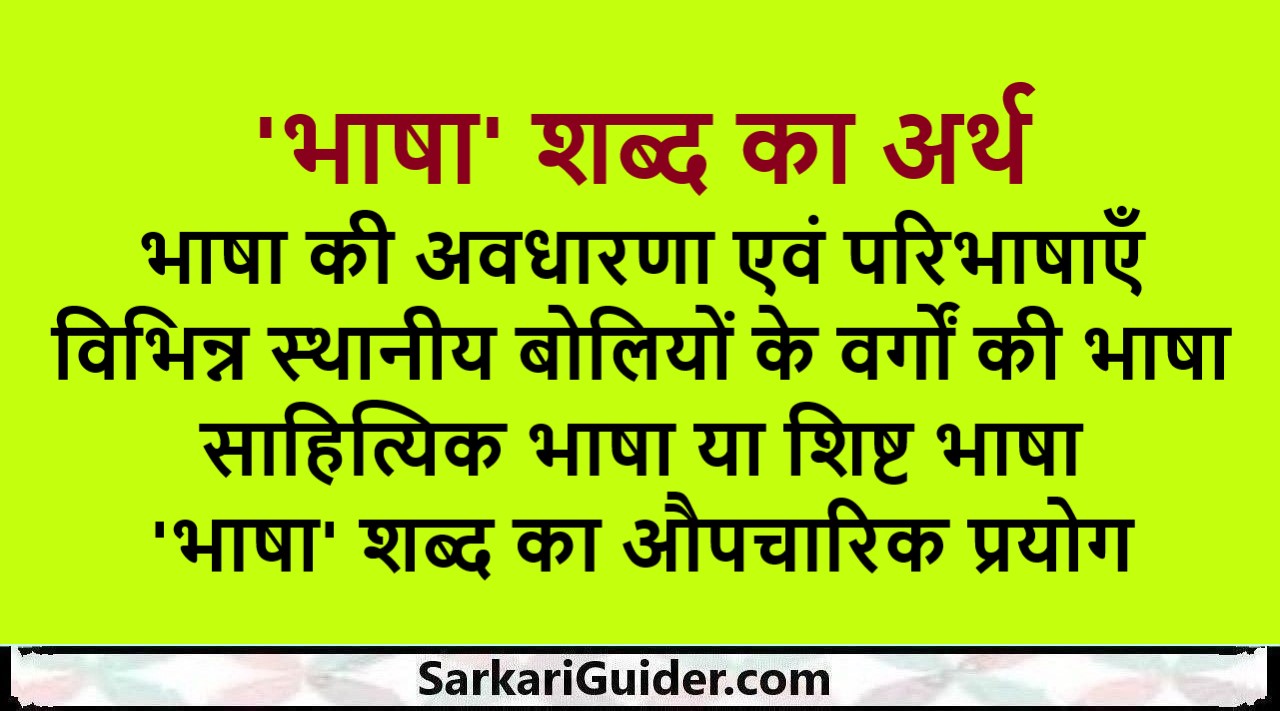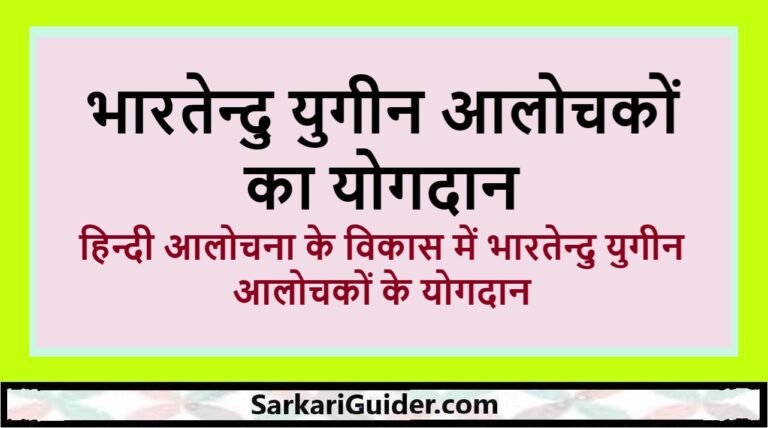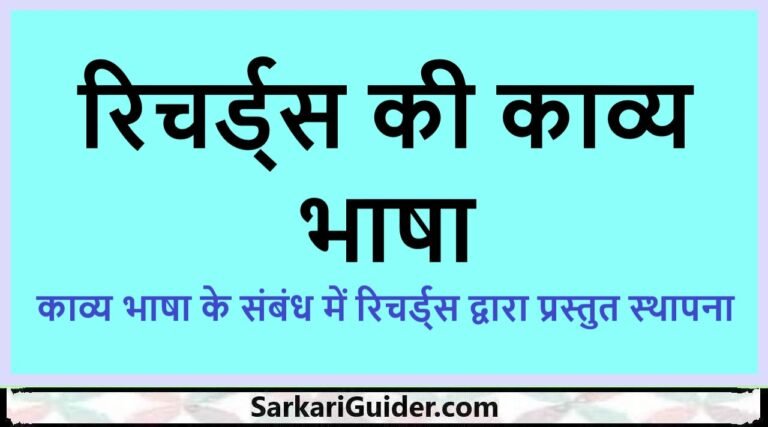‘भाषा’ शब्द का अर्थ | भाषा की अवधारणा एवं परिभाषाएँ | विभिन्न स्थानीय बोलियों के वर्गों की भाषा | साहित्यिक भाषा या शिष्ट भाषा | ‘भाषा’ शब्द का औपचारिक प्रयोग
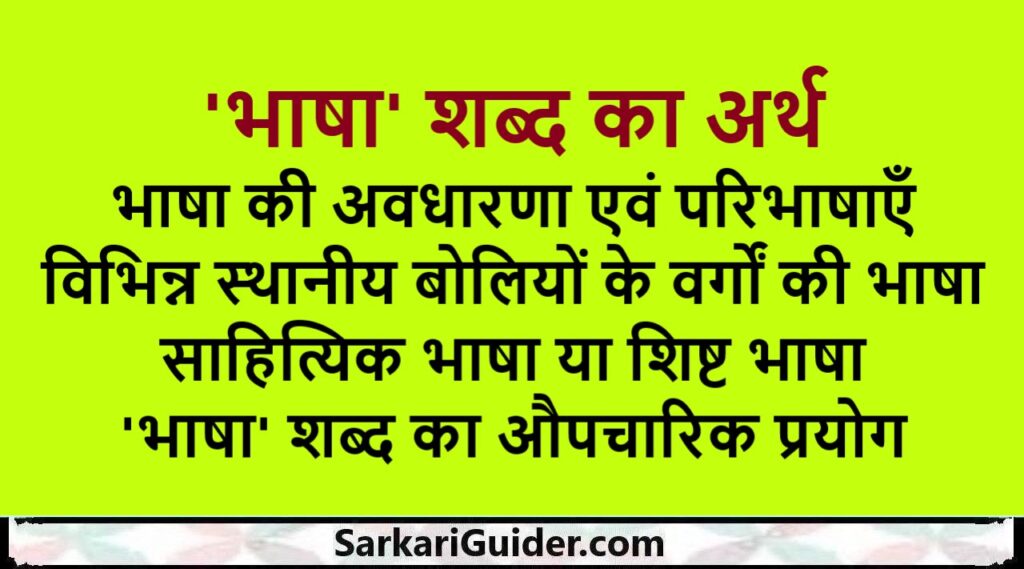
‘भाषा’ शब्द का अर्थ | भाषा की अवधारणा एवं परिभाषाएँ | विभिन्न स्थानीय बोलियों के वर्गों की भाषा | साहित्यिक भाषा या शिष्ट भाषा | ‘भाषा’ शब्द का औपचारिक प्रयोग
‘भाषा’ शब्द का अर्थ
‘भाषा’ शब्द संस्कृत की ‘भाषा’ धातु से बना है। ‘भाषा’ का अर्थ है ‘बोलना’ या कहना। अर्थात् भाषा वह है जिसे बोला जाए। बोलते तो संसार के प्रायः सभी प्राणी हैं। प्रत्येक जीवधारी, गाय, घोड़े, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया आदि परस्पर विचारों एवं भावों के आदान प्रदान हेतु किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। परन्तु हम उनके विचार-विनिमय को भाषा नहीं कहते हैं। उनकी भाषा केवल सांकेतिक होती है जबकि मानव की भाषा का स्वरूप केवल सांकेतिक न होकर लिखित है। विचार और भाव विनिमय के साधन के लिखित रूप को ही हम वस्तुतः भाषा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य के भावों, विचारों और अभिप्रेत अर्थों की अभिव्यक्ति के ध्यनि प्रतीकमत साधन को भाषा कहते हैं।
भाषा की अवधारणा एवं परिभाषाएँ
भाषा-विज्ञान का विषय मानवीय भाषा है। सामान्य रूप से मानव मात्र की भाषा को ‘भाषा’ कहा जाता है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। वह वक्ता और श्रोता दोनों के विचार-विनिमय का साधन है। वास्तव में “भाषा मनुष्य के मुख से निस्त वह सार्थक ध्वनि-समूह है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके।” व्यवहार में भाषा शब्द का कई अर्थों में प्रयोग होता है।
भाषा शब्द का सामान्य अर्थ मानव-मात्र की भाषा लिया जाता है। पशु-पक्षी भी अपनी बोली में भावाभिव्यक्त करते हैं, किन्तु उनकी अस्पष्ट ध्वनियों को भाषा की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार इंगित, स्वर-विकार और मुख-विकृति से भी भाषाभिव्यक्त होती है, परन्तु इसे भी भाषा नहीं कहा जा सकता। मानव के मुख से जो सार्थक ध्वनि-समूह निकलता है और जिसका कुछ-न-कुछ स्पष्ट अर्थ निकलता है, उससे सामान्य भाषा का निर्माण होता है।
किसी देश, देश-विभाग या बड़ी जाति की भाषा के लिए भी ‘भाषा’ शब्द प्रयुक्त होता है। इस अर्थ में तिब्बती चीनी, फारसी आदि भाषाएँ भी ‘भाषा’ कहलाती हैं। एक भाषा में अनेक स्थानीय और प्रान्तीय भेद हो सकते हैं। हिन्दी एक भाषा है, किन्तु इसमें अनेक स्थानीय और प्रान्तीय भेद हैं। किन्तु हिन्दी को अन्तरंग भाषाओं और बोलियों में बोलने वाले भी समझ सकते हैं।
विभिन्न स्थानीय बोलियों के वर्गों की भाषा-
कुछ ऐसी स्थानीय और प्रान्तीय बोलियों के वर्ग के लिए ‘भाषा’ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो किन्हीं अंशों में परस्पर विशेष समता रहती है और स्वयं से सम्बद्ध बोलियों के इसके वर्ग से भिन्न होती हैं। बिहारी, राजस्थानी आदि नाम भिन्न-भिन्न स्थानीय बोलियों के रख लिए गए हैं। डॉ० प्रियर्सन ने आधुनिक प्रान्तीय आर्य भाषाओं को केन्द्रस्थ, मध्यवर्ती और बाह्य-प्रदेशस्थ तीन वर्गों में विभाजित किया है।
साहित्यिक भाषा या शिष्ट भाषा –
विद्वान लोग ‘भाषा’ शब्द का प्रयोग साहित्यिक भाषा के लिए तथा साहित्य-शुन्य असाहित्यिक भाषाओं के लिए बोली का प्रयोग करते हैं, जैसे संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि। ब्रज-मण्डल के घरों में बोली जाने वाली भाषा को ‘बोली’ कहेंगे। साहित्यिक- भाषा और सर्व-साधारण की भाषा में भेद होता है। साहित्यिक भाषा में एक कृत्रिमता आ जाती है, जो उसे सर्वसाधारण की भाषा से पृथक् करती है। सर्वसाधारण की भाषा एक प्रवाहमान सरिता के समान है, तो साहित्यिक भाषा एक कृत्रिम झील की तरह है। सर्वसाधारण की भाषा सदैव विकासशील रहती है। वैदिक संस्कृत ने जब संस्कृति का रूप धारण कर लिया, तब जन-भाषा का प्राकृतों में विकास होने लगा। साहित्यिक भाषा को जीवित रखने के लिए और उसे समृद्ध बनाने के लिए सर्वसाधारण की भाषा से सम्बन्ध रखने की महती आवश्यकता रहती है। सर्वसाधारण की भाषा जहाँ बदलती रहती है, वहाँ साहित्यिक भाषा चिरकाल तक अपने स्थिर रूप में रहती है।
‘भाषा’ शब्द का औपचारिक प्रयोग-
मानव परस्पर विचाराभिव्यक्ति के लिए प्रायः वर्णात्मक भाषा का ही प्रयोग करता है। परस्पर के विचार- विनिमय में वह मुखाकृति, चेष्टा और संकेतों का भी आश्रय लेता है, इन्हें गूंगे-बहिरों की ‘भाषा’ के नाम से पुकारा जाता है। अमेरिका के इण्डियन लोगों में इसी प्रकार की सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। भाषा-विज्ञान का ऐसी भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता।
कृत्रिम भाषा-
‘भाषा’ शब्द का प्रयोग कृत्रिम भाषा के लिए भी होता है। कृत्रिम भाषा उसे कहते हैं जिसे कुछ मनुष्य अपनी सुविधा या उद्देश्य के गढ़ लेते हैं। आजकल इस प्रकार की भाषा का प्रमुख उदाहरण एस्पिरली (Lsperanto) नाम की भाषा है। इनके प्रेमी इसको अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कहते हैं।
उपर्युक्त विवेचन में भाषा का व्यापक अर्थों में प्रयोग दिखाया गया है।
भाषा की परिभाषा –
भाषा की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से प्रस्तुत की है। यहाँ उनका उसी रूप में उल्लेख किया जा रहा है-
- प्लेटो- “विचार आत्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मक वातचीत है। जो ध्वन्यात्मक बनकर होठों पर प्रकट होते ही भाषा कहलाती है।”
- स्वीट- ‘ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है।
- क्रोचे- “भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुगठित ध्वनि को कहते हैं, जो अभिव्यंजना के लिए निर्धारित की जाती है।”
- ब्लाक तथा ट्रेगर- “भाषा व्यक्त ध्वनि-चिन्हों को वह पद्धति है, जिसके माध्यम से समाज के व्यक्ति परस्पर व्यवहार करते हैं। “
- इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भाषा की परिभाषा इस प्रकार की है- “व्यक्त ध्वनि चिन्हों की उस पद्धति को भाषा कहते हैं, जिसके माध्यम से समाज विशेष के सदस्य पारस्परिक विचार-विनिमय करते हैं।
हिन्दी के कुछ लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा प्रस्तुत भाषा की परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-
- कामता प्रसाद गुरु- “भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है।”
- डॉ० मंगलदेव शास्त्री- “भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।”
- डॉ० बाबूराम सक्सेना- “जिन ध्वनि-चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है, उनको समीष्ट रूप से भाषा कहते हैं।”
- डॉ० भोलानाथ तिवारी- “भाषा मानव के उच्चारणावयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार-विनिमय करते हैं। लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों और भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता (Identity) के सम्बन्ध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं।”
हिन्दी के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत भाषा की इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उन्होंने भी कोई मौलिक बात नहीं कही है अतः दोनों ही विद्वान भाषा को एक समान ही परिभाषित करते हैं। वे सभी भाषा की – “मानव मुख से प्रयल विशेष से विस्तृत वह ध्वनि-समूह मानते हैं, जिसे समाज विशेष के सदस्य आपसी विचारविनिमय के लिए व्यवहार में लाते हैं।”
हिन्दी – महत्वपूर्ण लिंक
- अनुकरण सिद्धान्त | अरस्तु के काव्य और कला-सम्बन्धी विचार | अरस्तू का अनुकरण सिद्धान्त | कलाओं में अनुकरण का महत्त्व | अनुकरण सिद्धान्त की समीक्षा
- रीति सम्प्रदाय | रीति शब्द का अर्थ एंव परिभाषा | रीति का विकास | रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए रीति सम्प्रदाय का परिचय
- काव्य गुण | माधुर्य गुण | ओज गुण | प्रसाद गुण | काव्य गुणों के प्रकार
- काव्य की परिभाषा | काव्य के भेद | काव्य भाषा की परिकल्पना तथा स्वरूप | काव्य के मूलभूत लक्षण
- क्रोचे के अभिव्यंजनावाद | क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद पर समीक्षात्मक निबन्ध | अभिव्यंजनावाद के सम्बन्ध में क्रोंचे की मान्यता
- भारतेन्दु युगीन आलोचकों का योगदान | हिन्दी आलोचना के विकास में भारतेन्दु युगीन आलोचकों के योगदान
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]