ब्रूम आशा सिद्धान्त | आशा सिद्धान्त की उपयोगिता | ब्रूम के आशा सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या
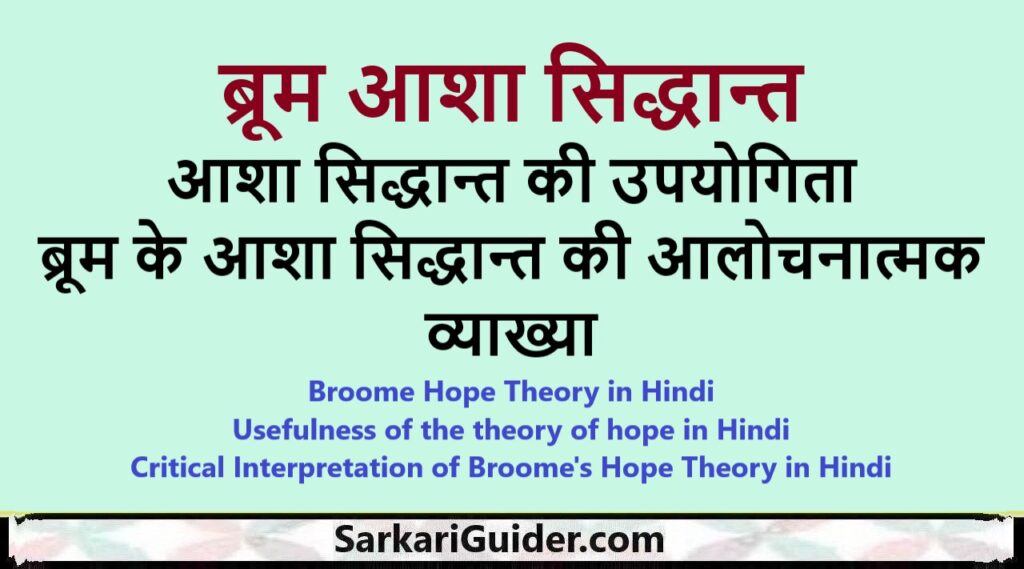
ब्रूम आशा सिद्धान्त | आशा सिद्धान्त की उपयोगिता | ब्रूम के आशा सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या | Broome Hope Theory in Hindi | Usefulness of the theory of hope in Hindi | Critical Interpretation of Broome’s Hope Theory in Hindi
ब्रूम आशा सिद्धान्त
(Vroom’s Expectancy Theory)
अभिप्रेरणा के विषय-वस्तु सिद्धान्तों, जिनमें यह बल दिया गया है कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की आवश्यकतायें एवं उनकी प्राथमिकता पर निर्भर करती है, कि आलोचना करते हुये विक्टर ब्रूम (Victor Vroom) ने अभिप्रेरणा प्रक्रिया के आधार पर इसके सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। ब्रूम का सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि लोग जो कर सकते हैं, वे उसे तब करेंगे जब वे उसे करना चाहें अर्थात् यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है तो वह उसे उस कार्य को तब करेगा, जबकि उसकी उक्त कार्य को करने की इच्छा हों। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिये तब अभिप्रेरित होगा, जबकि उसे आशा हो कि कार्य के परिणाम उसकी आशा के अनुकूल होगें! यह ब्रूम का सिद्धान्त तीन अवधारणाओं पर आधारित हैं- प्रबल, शक्ति और आशा इन तीनों अवधारणाओं के आधार पर किसी व्यक्ति में अभिप्रेरणा की मात्रा निम्नलिखित ससूत् से ज्ञात की जा सकती है-
अभिप्रेरणा (प्रबल) = शक्ति × आशा
(1) शक्ति (Valance) – ब्रूम के अनुसार, शक्ति किसी उद्देश्य के सम्बन्ध में व्यक्ति की इच्छा (प्राथमिकता) की मात्रा को प्रकट करती है। अभिप्रेरणा के अन्य दूसरे सिद्धान्तों में इसे प्रेरणा मनोभाव अथवा प्रत्याशित उपयोगिता का नाम दिया गया है। यह शक्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। व्यक्ति ऐसे व्यवहार में संलग्न होना चाहता है। जिससे वह सकारात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके अथवा नकारात्मक परिणामों से दूर रह सके।
(2) कारणत्व (Instrumentalities)- शक्ति के सम्बन्ध में कारणत्व एक प्रमुख तत्व के रूप में होता है। कारणत्व का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति किस कारण या साधन द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। कारणत्व कई चरणों में हो सकता है और प्रथम चरण के परिणाम द्वितीय या अन्य चरण के परिणाम को प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ, यदि व्यक्ति पदोन्नति उद्देश्य को प्राप्त करना प्रमुख समझता है तो वह प्रथम चरण के कारणत्व में यह निर्धारित करता है कि पदोन्नति किस कारण प्राप्त हो सकती है, जैसे- अच्छा कार्य निष्पादन अथवा अन्य कोई साधन। यदि व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अच्छे कार्य निष्पादन से उसे पदोन्नति प्राप्त हो सकती है तो अच्छा कार्य निष्पादन प्रथम चरण का उद्देश्य होता है और पदोन्नति प्राप्त करना द्वितीय चरण का उद्देश्य हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति प्रथम चरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अभिप्रेरित होता है। इस प्रकार अच्छा कार्य निष्पादन (प्रथम चरण का उद्देश्य) पदोन्नति प्राप्त करने (द्वितीय चरण का उद्देश्य) के निमित्त के रूप में कार्य करता है।
(3) आशा (Expectancy)- अभिप्रेरणा में आशा महत्वपूर्ण तत्व है जो इस सम्भावना को इंगित करती है कि वांछित उद्देश्य प्राप्त करने की आशा कितनी है। व्यक्ति में परिणाम प्राप्त करने की आशा जितनी अधिक होगी वह उतनी ही तीवता से अभिप्रेरित किया जा सकता है। यदि वांछित परिणाम प्राप्त करने की आशा कम होती है तो व्यक्ति में अभिप्रेरणा की मात्रा कम होती है, भले ही परिणाम व्यक्ति के लिये महत्वपूर्ण हो। पदोनति के उदाहरण के सम्बन्ध में यदि व्यक्ति यह अनुभव करता है कि च्चतर कार्य निष्पादन द्वारा उसे पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने की आशा नहीं है तो वह उच्चतर कार्य निष्पादन के प्रति अभिप्रेरित नहीं होगा।
आशा सिद्धान्त की उपयोगिता (Utility of Expectancy Theory)-
मैस्लो और हर्जबर्ग के पश्चात् जब ब्रूम ने अभिप्रेरणा का आशा सिद्धान्त प्रतिपादित किया तो इसका व्यापक स्वागत हुआ। इस सिद्धान्त ने यह इंगित किया है कि मैस्लों और हर्जबर्ग के सरल सिद्धान्तों में अभिप्रेरणा प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल है और अभिप्रेरणा की समस्या के समाधान के लिये इस जटिलता को ध्यान में रखना आवश्यक है। चूंकि इस सिद्धान्त में इन तथ्यों को ध्यान में रखा गया है, अतः यह सिद्धान्त अधिक व्यावहारिक है। थामस क्विक (Thomas Quick) के अनुसार, “अभिप्रेरणा का आशा सिद्धान्त सरल होने के साथ-साथ अधिक व्यावहारिक है, इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह व्यवहार में कार्य करता है।” आशा सिद्धान्त की निम्नलिखित उपयोगितायें हैं-
(1) आशा सिद्धान्त केवल व्यक्ति की आवश्यकताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि व्यक्ति उन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिये किस साधन का उपयोग करता है। साधन के इस उपयोग के अनुसार ही अभिप्रेरणा प्रणाली विकसित की जा सकती है।
(2) आशा सिद्धान्त इस अवधारणा को विकसित करता है कि प्रबन्धकों का मुख्य कार्य कार्य-निष्पादन के लिये उचित वातावरण का निर्माण करना है और इस वातावरण का निर्माण करते समय आकस्मिक घटकों पर ध्यान देना आवश्यक है।
(3) आशा सिद्धान्त उद्देश्यों द्वारा प्रबन्ध के अनुरूप है, अतः यह व्यक्तियों और संगठन के उद्देश्यों में तादात्म्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है।
(4) आशा सिद्धान्त का उपयोग सभी प्रकार के व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने के लिये। किया जा सकता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिये अभिप्रेरणा की प्रक्रिया समान होती है, यद्यपि विभिन्न व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने वाले तत्वों में भिन्नता हो सकती है।
आशा सिद्धान्त के दोष (Demerits of Expectancy Theory)
ब्रूम द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त यद्यपि अभिप्रेरणा प्रक्रिया की व्याख्या करता है, किन्तु इसकी व्यवहारिकता के सम्बन्ध में लोगों के बीच मतभेद पाया जाता है, क्योंकि इसमें निम्नलिखित दोष हैं-
(1) इस सिद्धान्त में प्रयुक्त शब्दावली अत्यन्त कठिन एवं जटिल है जिसे साधारण व्यक्ति सरलता से नहीं समझ सकता है।
(2) आशा सिद्धान्त में प्रस्तावित प्रथम तथा द्वितीय स्तरीय परिणामों, आशाओं और कारण तत्वों की व्याख्या विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा अलग-अलग की जा सकती है जिससे उचित अभिप्रेरणा प्रणाली विकास करने में कठिनाई होती है।
(3) आशा सिद्धान्त के परीक्षण हेतु बहुत कम मात्रा में शोध हुये हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस सिद्धान्त को सभी प्रकार की स्थितियों में व्यावहारिक बनाया जा सकता है अथवा नहीं। इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के पूर्व स्वयं ब्रूम ने भी कोई शोध नहीं किया था, बल्कि अन्य शोधों के निष्कर्षों के आधार पर इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। अतः इस सिद्धान्त की व्यवहारिकता के पक्ष के सम्बन्ध में जो विवरण उपलब्ध हैं, वे प्रबन्धकों के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। इस प्रकार इस सिद्धान्त की व्यावहारिकता संदिग्ध है।
ब्रूम द्वारा प्रतिपादित आशा सिद्धान्त के अनुरूप पोर्टर (Porter) और लॉलर (Lawler) ने अभिप्रेरणा प्रक्रिया सिद्धान्त को और अधिक विकसित किया है जिसमें ब्रूम द्वारा सुझाये गये तत्वों के अतिरिक्त अन्य तत्वों का समावेश किया गया है।
संगठनात्मक व्यवहार – महत्वपूर्ण लिंक
- प्रबन्ध के मानवीय व्यवहार विचारधारा | मानवीय व्यवहार स्कूल की मान्यताएँ एवं विशेषताएँ | मानवीय व्यवहार स्कूल के दोष एवं कमियाँ | प्रबन्ध के सामाजिक विचारधारा | प्रबन्ध के निर्णय सिद्धान्त
- अवबोधन का अर्थ एवं परिभाषा | अवबोधन की प्रक्रिया | Meaning and Definition of Perception in Hindi | Process of Perception in Hindi
- अवबोधन के घटक | अवबोधन को प्रभावित करने वाले घटक | Factors of Perception in Hindi
- समूह के आकार | समूह के विभिन्न प्रकार | समूह निर्माण की विचारधाराये | समूह निर्माण के विभिन्न सिद्धान्त
- अभिप्रेरण से आशय एवं परिभाषा | अभिप्रेरण प्रक्रिया
- मैस्लो का आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धान्त | मैस्लो सिद्धान्त का मूल्यांकन
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]







