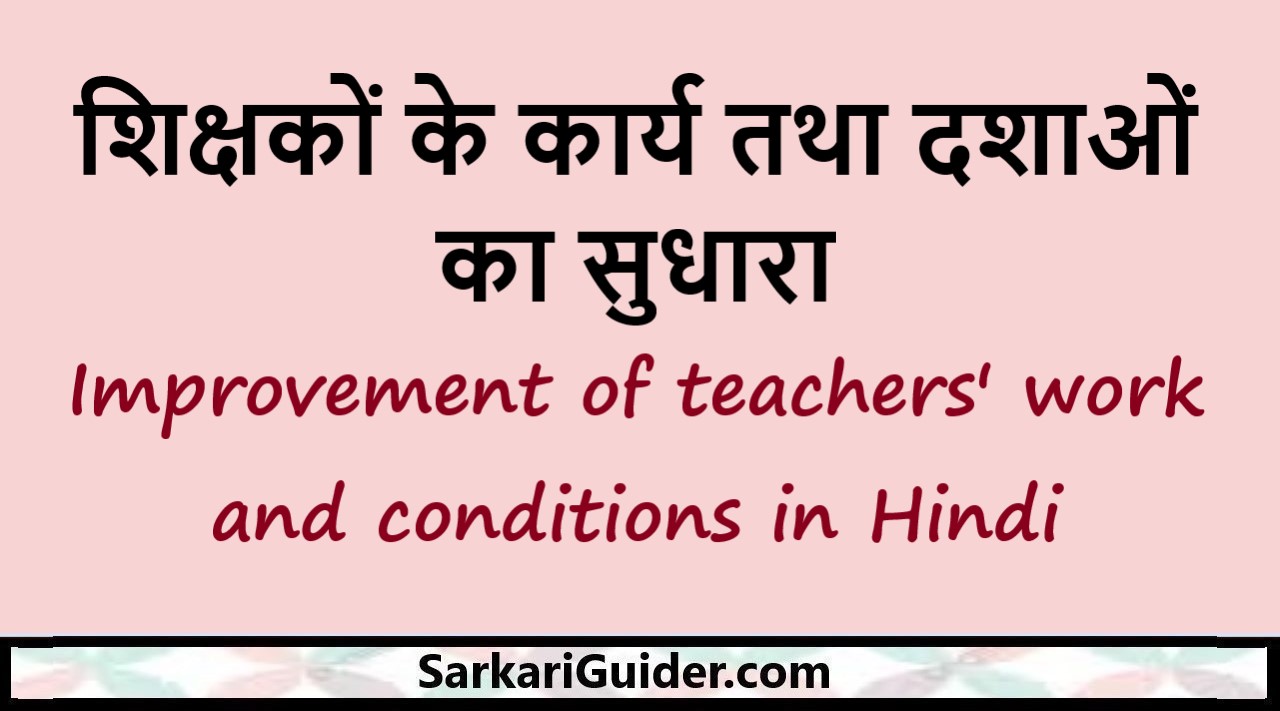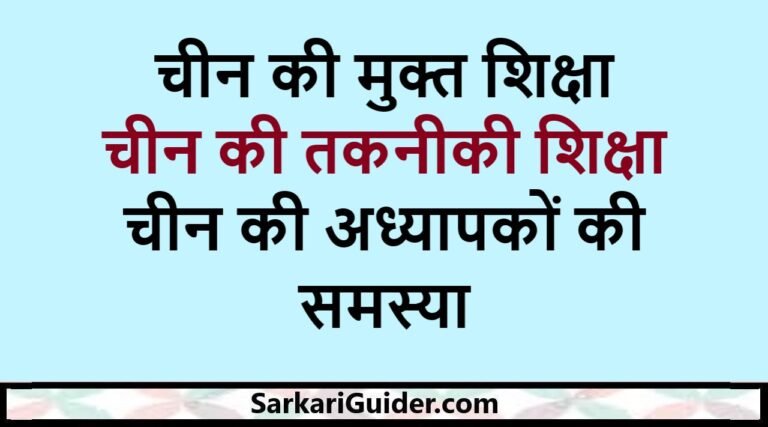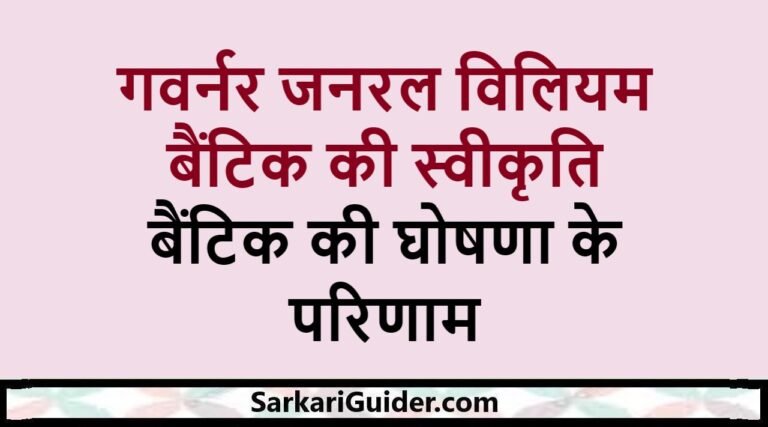शिक्षकों के कार्य तथा दशाओं का सुधारा | Improvement of teachers’ work and conditions in Hindi

शिक्षकों के कार्य तथा दशाओं का सुधारा | Improvement of teachers’ work and conditions in Hindi
शिक्षकों के कार्य तथा दशाओं का सुधारा
हमारे देश में शिक्षकों को जिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, वे अत्यधिक निराशाजन हैं। शासकीय स्कूलों में तो शिक्षकों को काफी सुविधायें हैं, किन्तु उससे भी बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक निजी प्रबन्धों की संस्थाओं में कार्य करते हैं। इन स्कूलों में कार्य करने वाले शिक्षकों की कार्य की दशायें ठीक नहीं हैं। जातिवाद, कम वेतन देना, गुटबन्दी आदि कई ऐसी दशायें है जिनमें शिक्षक चाहते हुए भी काम नहीं कर पाता। इस सम्बन्ध में मुदालियर आयोग के अनुसार-
“अपने दौरे के समय हमें अत्यन्त दुःखपूर्वक इस तथ्य स्वीकार करना पड़ा कि शिक्षकों का सामाजिक स्तर, वेतन तथा अन्य सेवा की दशायें अत्यन्त असन्तोषजनक से अत्यधिक दूर है । हमारा सामान्य विचार यह है कि उनकी दशा पहले से भी बदतर हो गयी है।”
मुदालियर आयोग ने शिक्षकों की कार्य की दशाओं को सुधारने के लिए निम्न सुझाव दिये थे-
(1) शिक्षकों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए शिक्षण व्यवसाय को समाज के अन्य वर्गों से सम्मान प्राप्त होना चाहिये।
(2) शिक्षकों के बच्चों की विद्यालयी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये।
(3) कठिनाइयों का निवारण पंचमण्डल द्वारा होना चाहिये । इस पंचमण्डल में शिक्षा निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि भी हो।
(4) शिक्षा क्षेत्र में त्रिलाभ योजना को लागू किया जाये।
(5) परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष होनी चाहिये।
(6) समान योग्यता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिये ।
(7) समस्त भारत में शिक्षकों के चुनाव तथा नियुक्ति की प्रणाली एक समान होनी चाहिये।
(8) व्यक्तिगत प्रबन्ध तथा स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थाओं में शिक्षकों के चुनाव के लिए एक समिति होनी चाहिये जिसका एक सदस्य प्रधानाचार्य भी हो।
मुदालियर आयोग ने एक महत्वपूर्ण तथा क्रान्तिकारी आवाज शिक्षकों की शिक्षा तथा उनके कार्य की दशाओं को उन्नत करने के लिए दी। शिक्षकों की कार्य की दशायें सरकारी तथा गैर-सरकारी-दोनों ही प्रकार के स्कूलों में दूषित हैं तथा दोनों के ही अपने-अपने तौर-तरीके हैं। सिद्धान्त तथा व्यवहार में असन्तुलन की स्थिति रहती है। परिणामस्वरूप शिक्षकों की शिक्षा में अनेक ऐसे पहलू विकसित हो गये है जिनके कारण अनेक नई समस्याओं ने जन्म लिया है। शिक्षा आयोग द्वारा उन सभी पहलुओं पर विचार किया गया है।
शिक्षा आयोगों की इस परम्परा में आधुनिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन सभी रूपों से अधिक उचित है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रमुख रूप से राधाकृष्णन आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के अनेक पहुलओं पर विचार किया है, किन्तु शिक्षकों के कल्याण के लिए समग्र रूप से चिन्तन करके नयी संस्तुतियों द्वारा विकास तथा सतर का निर्माण करने के सत्प्रयत्न का श्रेय कोठारी आयोग को ही जाता है। आयोग ने सभी स्तरों पर शिक्षकों के लिए नये वेतनमान दिये जाने की संस्तुति की है।
जिस समय आयोग ने इन वेतनमानों की घोषणा की, शिक्षा के क्षेत्र में इनका अत्यन्त स्वागत हुआ। शिक्षकों को उम्मीद की किरण दिखाई दी। आयोग ने इन वेतनमानों को लागू करने के सम्बन्ध में कहा-
“उक्त वेतनमान उच्च-शिक्षा के शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा पहले से ही स्वीकृत हैं। उनको लागू करने के लिए केन्द्र सरकार को 80% तथा राज्य सरकार को 20% सहायता करनी चाहिये। निजी संस्थाओं के लिए तो केन्द्रीय सरकार द्वारा 100% सहायता दी जानी चाहिये । भारत में शिक्षकों के वेतनमान में समानता नहीं है, जबकि उनकी योग्यतायें समान हैं। सामान्य रूप से ये वे वेतन दरें हैं जो आज विश्वविद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में पायी जाती हैं। माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा की दशा तो इनसे भी अधिक बुरी है। केन्द्र सरकार के एक मामूली से चपरासी को भी प्राथमिक कक्षा के शिक्षक से अधिक वेतन मिलता है।”
भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर वेतन-मान लागू करने की सिफारिशों पर जोर दिय है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मॉडल एक्ट की व्यवस्था है। माध्यमिक स्तर पर सेकेण्डरी पास, स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षकों के वेतन-दरों को लागू करने के लिए कहा गया है। आयोग द्वारा सभी प्रकार की उन्नति की सम्भावनाओं पर विचार किया गया है जो कि अग्र प्रकार हैं-
(1) प्राइमरी स्कूल में योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रधानाध्यापक तथा स्कूलों के निरीक्षकों के पदों पर तरक्की देना।
(2) योग्य ट्रेड स्नातकों को स्नातकोत्तर प्रेड देना।
(3) अग्रिम वेतन कम देना।
(4) विश्वविद्यालयों में विद्वान् शिक्षकों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की सिफारिश भी शिक्षकों के स्तर का निर्माण करने के लिए की गयी है। जैसे-
(i) शिक्षकों को अपने नागरिक अधिकारों का सम्पूर्ण उपयोग करने का अधिकार है। वे स्थानीय, जिला राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ सकते हैं।
(ii) सभी श्रेणी तथा वर्गों के शिक्षकों के लिए अवकाश की सुविधायें होनी चाहिये।
(iii) अवकाश ग्रहण करने की आयु स्कूल तथा कॉलेजों में क्रमश: 60 तथा 65 वर्ष होनी चाहिये।
(iv) शिक्षक कल्याण कोष की स्थापना, जिसमें 1.5% वेतन शिक्षक जमा करेंगे। इसके संचालन करते के लिए एक समिति होनी चाहिये।
(v) प्रत्येक पाँचवें वर्ष भारत भ्रमण के लिए कन्सेशनल रेलवे पास की व्यवस्था होनी चाहिये
इसी प्रकार आयोग ने शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि करने की बात कही है।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- अधिगम सामग्रियों काउत्पादन और वितरण | Production and distribution of learning materials in Hindi
- अधिगम के व्यवहारवादी उपागम । अधिगम का व्यवहारवादी दृष्टिकोण
- स्किनर के सक्रिय अनुबन्धन सिद्धान्त | Skinner’s Theory of Operant Conditioning in Hindi
- बेसिक शिक्षा योजना के मूलभूत सिद्धान्त | वर्धा शिक्षा योजना के मूलभूत सिद्धान्त
- बेसिक शिक्षा की समस्यायें | Problems of Basic Education in Hindi
- बेसिक शिक्षा के गुण | बेसिक शिक्षा के दोष | Merits of Basic Education in Hindi | Demerits of Basic Education in Hindi
- मुक्त विद्यालय | मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताएँ | मुक्त शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | लक्ष्य एवं विशेषताएँ | राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का स्वरूप
- उ0 प्रo राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय | विश्वविद्यालय का उद्देश्य तथा लक्ष्य | विश्वविद्यालय की विशेषताएँ एवं सुविधाएँ
- ब्रिटेन में मुक्त विश्वविद्यालय | विवृत विश्वविद्यालय में शिक्षण-विधि | विवृत विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम | विवृत विश्वविद्यालय का महत्त्व
- चीन की मुक्त शिक्षा | चीन की तकनीकी शिक्षा | चीन की अध्यापकों की समस्या
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]