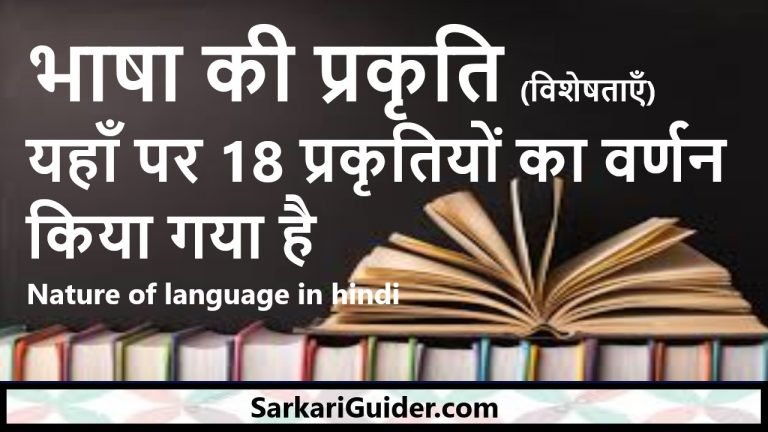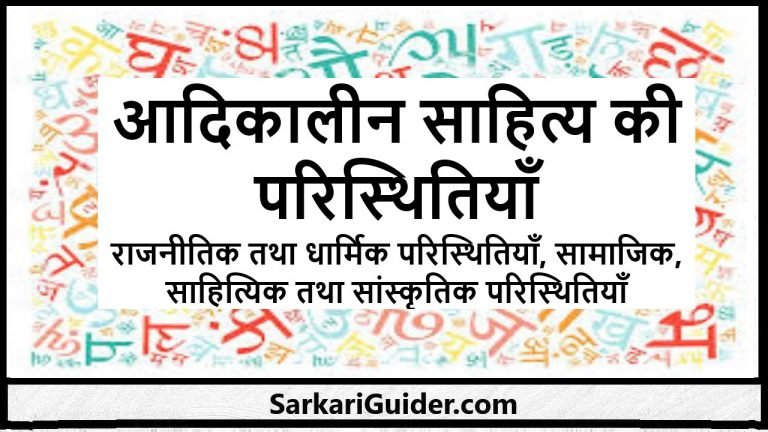उपसर्ग एवं प्रत्यय | हिन्दी के तत्सम, तदभव एवं अर्धतत्सम शब्द | कारक चिन्ह एवं विभक्ति | कारक चिह्न
उपसर्ग एवं प्रत्यय | हिन्दी के तत्सम, तदभव एवं अर्धतत्सम शब्द | कारक चिन्ह एवं विभक्ति | कारक चिह्न
उपसर्ग एवं प्रत्यय
उपसर्ग की परिभाषा-
उपसर्ग शब्द का निर्माण उप+सृज+घञ से हुआ है जिसका अर्थ है, पास छोड़ा हुआ। किसी शब्द में अर्थ का परिवर्तन लाने के लिए उपसर्ग को उस शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है। प्रत्यय और उपसर्ग में मुख्य अन्तर यही है कि उपसर्ग शब्द के पूर्व जुड़ता है किन्तु प्रत्यय शब्द के बाद, जैसे-अनुरूप, अभिज्ञान में अनु, अभि उपसर्ग हैं जो रूप और ज्ञान शब्द के पहले जुड़े हुए हैं। रंगीला और उकुंकू में ईला तथा अंकू प्रत्यय हैं जो रंग और उड़ (ना) के बाद जुड़े हुए हैं।
कुछ उपसर्ग हिन्दी के तद्भव शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। इन्हें विद्वानों ने तद्भव उपसर्ग की संज्ञा दी है, जैसे-
अ (नहीं) अकाज, अनाथ
अन (नहीं) अनमोल, अनपढ़
अध (आधा) अधमरा, अधजला, अधकटा
उन् (एक कम) उन्तीस, उन्तालीस
औ (निषेध, हीनतासूचक) औगुन, औढर
कु (क) कुपूत, कपूत
दु (बुरा, हीन) दुबला, दुधारा
स (सुन्दर) सपूत
प्रत्यय की परिभाषा-
ध्वनि समूह की वह इकाई जो किसी शब्द के अन्त में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देती है, प्रत्यय कहलाती है।
संस्कृत में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं-
- कृत-प्रत्यय- ये प्रत्यय क्रिया के धात् ह्रपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। जैसे-चल (धातु + अक (प्रत्यय) = चालक यहां अक कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदन्त कहलाते हैं।
- तद्धित प्रत्यय- वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, आदि से जुड़े हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें बने शब्द तद्धितान्त कहलाते हैं। जैसे-कृपा + आलु = कृपालु। यहां ‘आलु’ तद्धित प्रत्यय है तथा कृपालु तद्धितान्त शब्द है।
हिन्दी के तत्सम, तदभव एवं अर्धतत्सम शब्द
तत्सम शब्द- ‘तत्सम’ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है ‘तत् + सम’ जिसका अर्थ है- ‘उसके समान’। उसके समान से यहां तात्पर्य है—’सोत भाषा के समान’। हिन्दी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्दों की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को ‘तत्सम शब्द’ कहा जाता है।
जैसे-धन, नारी, पुष्प, जलज, दिवस आदि।
तदभव शब्द- तदभव का अर्थ है- ‘उससे होना’। अर्थात वे शब्द जो ‘स्रोत भाषा’ के शब्दों में विकसित हुए हैं। इन शब्दों का विकास क्रम दिखाते हुए इनके मूल रूप (स्रोत) तक पहुंचा जा सकता है। ये शब्द संस्कृत से चलकर पालि, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचे हैं, अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे—’दही’ शब्द ‘दधि’ से, ‘कान्हा’ शब्द ‘कृष्ण’ से विकसित होकर हिंदी में आए हैं। ऐसे शब्दों को तदभव शब्द’ कहा जाता है।
अर्द्धतत्सम शब्द- संस्कृत से वर्तमान स्थाई तदभव रूप तक पहुंचने के मध्य संस्कृत के टूटे-फूटे स्वरूप का जो प्रयोग किया जाता था उसे अर्द्ध तत्सम कहा जाता है।
जैसे-अग्नि या अगि
यह अग्नि (तत्सम) व आग (तदभव) के मध्य का स्वरूप है।
कारक चिन्ह एवं विभक्ति | कारक चिह्न
कारक का अभिप्राय- संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके सम्बन्ध सूचित हों, उसे ‘कारक’ कहते हैं; जैसे-राम ने मुझको पुस्तक दी। इस वाक्य में राम ने’ और ‘मुझको’ का सम्बन्ध “दी’ क्रिया के साथ है।
‘कारक’ शब्द ‘कर्तृत्व-शांत’ का बोधक है। इसका अर्थ ‘करने वाला’ है। ‘करने वाता’ कोई क्रिया ही करता है। अतः कारक का विशेष उद्देश्य किसी कार्य को करना है। सम्बन्ध कारक को छोड़कर सभी कारकों का सम्बन्ध क्रिया से होता है। अतः कारक वाक्य में प्रयुक्त उस नाम (संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण) को कहते हैं, जिनका अन्वय (सम्बन्ध) क्रिया के साथ होता है।
इस अन्वय या सम्बन्ध के परिचायक कारक चिह्न होते हैं। इनें ‘विभक्ति’ या ‘परसर्ग’ (बाद में जुड़ने वाले) भी कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम आगे रकों के वोध के लिए जो प्रत्यय लगाये जाते हैं, उन्हें व्याकरण में परसर्ग या विभक्ति कहते हैं, जैसे-ने, को, से, मैं का आदि।
कारक के भेद-हिन्दी में आठ कारक होते हैं। विभक्तियों सहित आठ कारक निम्नांकित हैं-
| कारक | परसर्ग | उदाहरण |
| कर्ता (क्रिया करने वाला) | ने | राम ने |
| कर्म (जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े) | को | रावण को |
| करण (जिससे क्रिया की जाय) | से | बाण से |
| सम्प्रदान (जिसके लिए क्रिया की जाय) | को, के लिए | सीता के लिए |
| अपादान (क्रिया जिसके कारण अलग होना प्रकट हो) | से | चित्रकूट से जाकर |
| सम्बन्ध (क्रिया के अन्य कारकों के साथ सम्बन्ध प्रकट करने वाला) | का, की, के | लक्ष्मण की |
| अधिकरण (क्रिया होने का आधार-स्थान व समय) | या, री, ये | सहायता से |
| सम्बोधन (क्रिया के लिए जिसे सम्बोधित किया जाय) | में, पर | युद्ध में मारा |
हिन्दी – महत्वपूर्ण लिंक
- काव्यभाषा का स्वरूप | काव्यभाषा एवं सामान्य भाषा में अन्तर
- काव्य में बिम्ब-विधान | काव्य बिम्ब का कार्य या उद्देश्य | बिम्ब के गुण एवं तत्व | बिम्बों का वर्गीकरण
- प्राचीन भारतीय आर्य भाषा | वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में साम्य एवं वैषम्य | वैदिक और लौकिक संस्कृत में अन्तर
- पालि भाषा की व्युत्पत्ति | पालिभाषा का प्रदेश | पालि-साहित्य | पालि की विशेषताएं
- परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ठ | अवहट्ठ की विशेषताएं | अवहट्ट भाषा की भाषिक विशेषताएँ | अवहट्ट भाषा की व्याकरणिक विशेषताएँ
- राष्ट्रभाषा हिन्दी की समस्याएँ | राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का भविष्य
- प्रतीक का उद्भव एंव विकास | प्रतीक का अर्थ | प्रतीकों का वर्गीकरण | प्रतीक योजना का आधार | काव्य में प्रतीकों का महत्व
- महाराष्ट्री प्राकृत | महाराष्ट्री प्राकृत की विशेषताएं
- राजभाषा एव राष्ट्रभाषा | संचार भाषा | सम्पर्क भाषा
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]