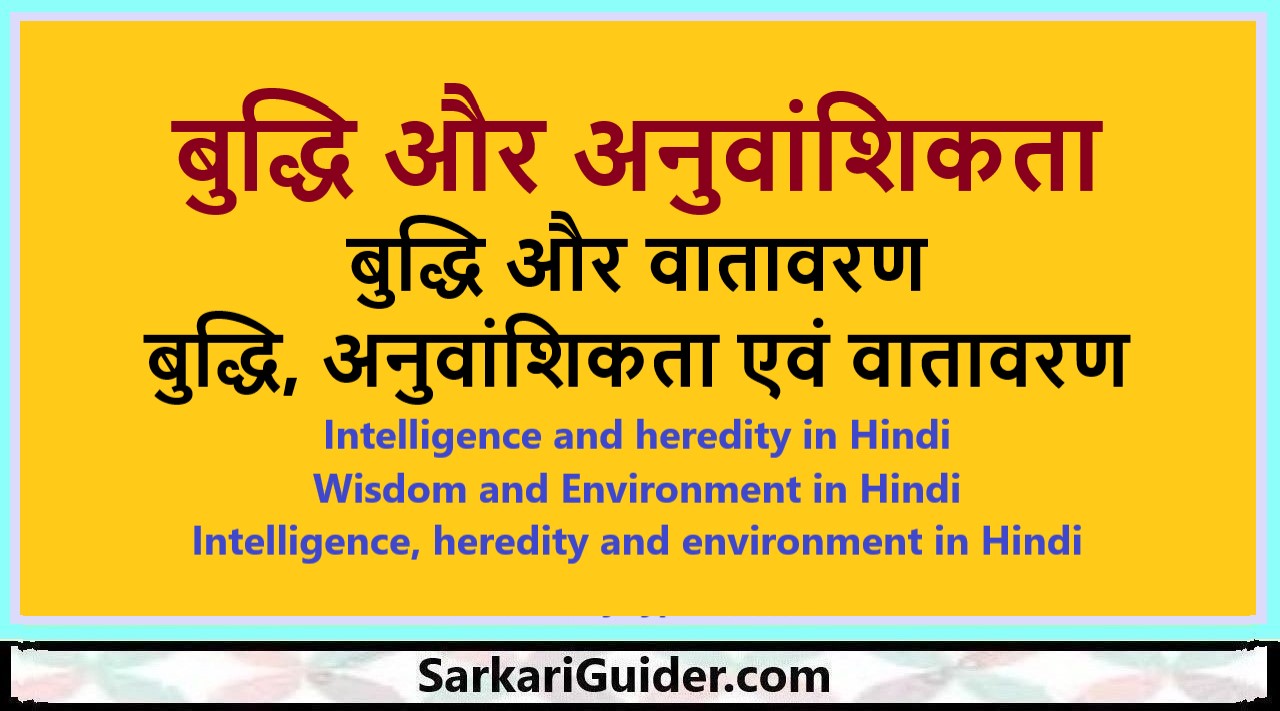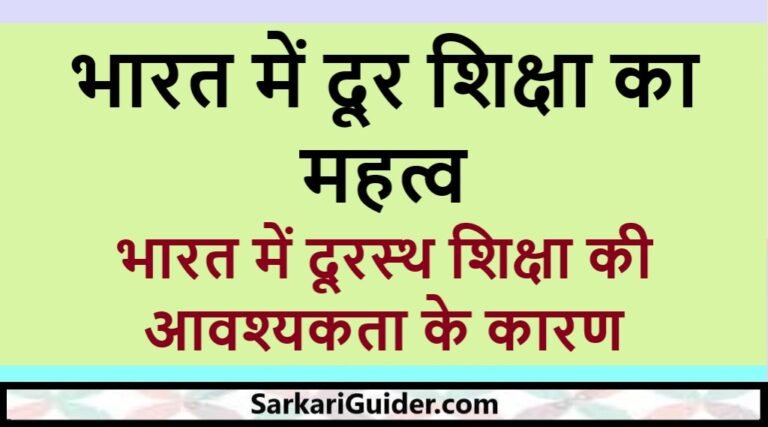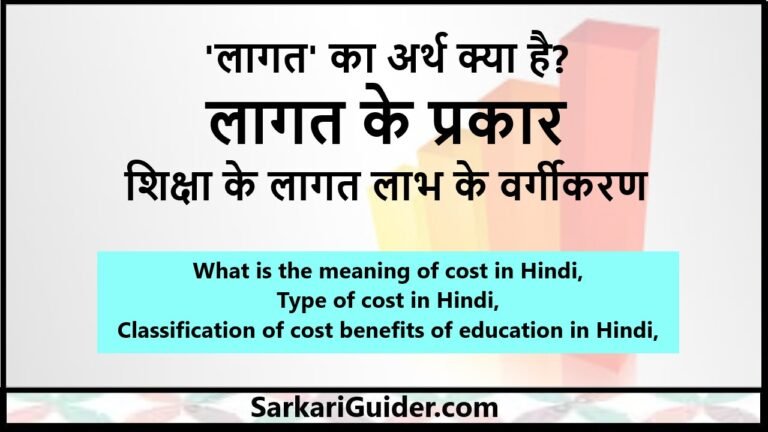बुद्धि और अनुवांशिकता | बुद्धि और वातावरण | बुद्धि, अनुवांशिकता एवं वातावरण
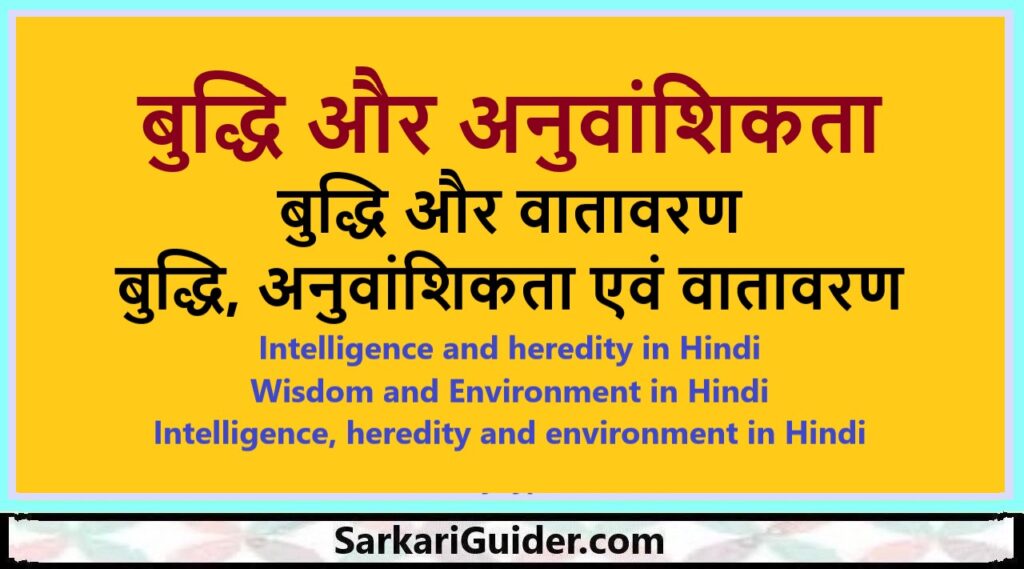
बुद्धि और अनुवांशिकता | बुद्धि और वातावरण | बुद्धि, अनुवांशिकता एवं वातावरण | Intelligence and heredity in Hindi | Wisdom and Environment in Hindi | intelligence, heredity and environment in Hindi
बुद्धि और अनुवांशिकता–
बुद्धि के संबंध में प्राचीन मत यह रहा है कि इस क्षमता का निर्धारण अनुवांशिकता के हाथों में होता है। वर्तमान शताब्दी के पूर्वार्ध का मनोवैज्ञानिक साहित्य एवं शोध सामग्री पर्याप्त सीमा तक गाल्टन, केटेल, स्टैनले हाल, गोडार्ड विशिष्ट तथा डुग्डेल के विचारों से प्रभावित दिखलाई पड़ती है जो अनुवांशिकता के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। गाल्टन ने 1977 उच्च स्तरीय बुद्धि के व्यक्तियों और इतने ही साधारण बुद्धि के व्यक्तियों के पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जिससे पता चला कि अधिकांश बुद्धिमान व्यक्तियों के पूर्वज भी बुद्धिमान एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इसके विपरीत साधारण बुद्धि के व्यक्तियों के पूर्वजों में बहुत कम लोग ऐसे निकले जिनके तीव्र बुद्धि होने का कोई प्रमाण मिलता हो। बुद्धि पर अनुवांशिकता का प्रभाव देखने के लिए जुड़वा बच्चों (Twins) का अध्ययन कई प्रकार से नियंत्रित दशाओं में किया गया है। भिन्न वातावरण में विकसित होने के बाद भी बुद्धि में जितनी समानता जुड़वा बच्चों में दिखलाई पड़ी उतनी सगे भाई- बहनों में नहीं। इसी प्रकार बुद्धि की मात्रा में जो समानता सगे भाई- बहनों में पाई जाती है उतनी तो भिन्न परिवारों के बच्चों में नहीं मिलती। बर्क्स ने कुछ ऐसे बच्चों का अध्ययन किया जो अपने असली घरों से अलग अन्य व्यक्तियों के घरों में पले थे। यह बच्चे बुद्धि में अपने पालक माता- पिता (Foster Parents) की अपेक्षा अपनी वास्तविक माता-पिता से अधिक मिलते-जुलते थे। इन अन्वेषणों सेफ भली-भांति प्रमाणित होता है कि बुद्धि का निवान सकता से बहुत गहरा संबंध होता है। गोडार्ड द्वारा इस दिशा में किया गया ध्यान बड़ा ही महत्वपूर्ण सामझा जाता है। उसे मार्टिन कालीकाक नामक एक सैनिक के परिवार का अध्ययन किया। मार्टिन कालीकाक नेपाली एक मंदबुद्धि पथभ्रष्टा स्त्री के साथ अवैध संबंध स्थापित किया जिससे कई संतानों की उत्पत्ति हुई। इस महिला के जो 400 वंशज हुए उनमें से 143 मंदबुद्धि, 46 निम्न नैतिक स्तर के, 26 जार्ज, 33 वेश्याएं, 24 शराबी, हॉट वैश्यालयों के मालिक, तीन अपराधी तथा तीन मिर्गी के रोगी निकले। कालीकाक ने बाद में यह दूसरी भद्र महिला के साथ भी विवाह किया था जिसके प्रायः सभी बंसल सामान्य कोटि के व्यक्ति हुए। अध्ययन के समय तक उक्त भद्र महिला से उपलब्ध कुल 496 बसों में कोई भी मंदबुद्धि नहीं था। बल्कि सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक संबंधों तथा व्यवसाय की दृष्टि से प्रायः सभी श्रेष्ठ पाए गए। यद्यपि अनुवांशिक क्षमताओं का स्वतंत्र अध्ययन वास्तविक अर्थ में संभव नहीं है और इसलिए उपयोग के अध्ययनों की उपलब्धियां कहां तक बाध्य है यह कहना कठिन है, तथापि हम बुद्धि पर अनुवांशिकता के प्रभाव को स्वीकार नहीं कर सकते।
बुद्धि और वातावरण–
बुद्धि-विकास की सीमा अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होती है किंतु उसके विकास की गतिविधि वातावरण पर ही निर्भर करती है। यदि किसी बालक के विकास के लिए सुंदर, स्वस्थ और हर दृष्टि से उपयुक्त वातावरण प्राप्त हो तो नि:संदेह उसकी बुद्धि साधारण या निम्न स्तरीय वातावरण में पलने वाले बालकों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से विकसित हो सकेगी। ‘वातावरण’ एक व्यापक प्रत्यय है और इसके अंतर्गत कई तत्वों का समावेश समझा जाता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक तत्वों को छोड़कर शेष समस्त तत्व वातावरण के ही अंग माने जाते हैं। गर्व कालीन अवस्था में जिस वस्तुओं घटनाओं और रासायनिक द्रव्यों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है सभी वातावरण के अंतर्गत आते हैं। जन्म के उपरांत उपलब्ध आहार, आवासीय दशाएं, पाठशाला का पाठ्यक्रम, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा सांस्कृतिक परंपराएं तो विशेष रूप से बालक के वातावरण का निर्माण करती है। कदाचित इस संदर्भ में सर्वदा सर्वाधिक प्रश्न की वे घटनाएं है जिनका बालक के शिक्षण प्रशिक्षण से सीधा संबंध होता है। एक और बालक की अधिगम संबंधी अनुभूतियां, दंड, पुरस्कार एवं प्रबलन की विधाएं हैं और दूसरी और उसका आर्थिक शैक्षणिक वचन है जिसके कारण उसे अपनी अनुवांशिक क्षमताओं के समुचित विकास का अवसर नहीं मिल पाता। मोटे रूप से वातावरण को उच्च स्तरीय एवं निम्न स्तरीय कोटियों में वर्गीकृत किया गया है और बालक के बौद्धिक विकास की गतिविधि पर उनके विशिष्ट प्रभाव का अध्ययन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है।
स्टील्स, वेलमैन तथा उनके सहपाठी (1938) मैं इस संदर्भ में कुछ ऐसे बालकों का अध्ययन किया है जो यह कहना था लेकिन निर्धन वातावरण में पल रहे थे। इन बालकों की शिक्षा के लिए एक सुंदर नर्सरी स्कूल का प्रबंध किया गया। दो ढाई साल तक की स्कूल के नवीन वातावरण में रह चुकने के बाद उनकी बुद्धि की तुलना में बालकों की बुद्धि से की गई जिन्हें इस स्कूल में पढ़ने की सुविधा जानबूझकर नहीं दी गई थी पूर्णविराम पता चला कि स्कूल के सुंदर वातावरण के कारण उसने पढ़ने वाले बालकों का बुद्धि लब्धि में वृद्धि हुई है। इन बालकों के बुद्धि विकास की गति में बीते ब्रता देखी गई। इसी प्रकार गार्डन (1924) ने कुछ निरंतर नौकाओं में निवास करने वाले मल्लाह ओं के बालकों की आयु के आधार पर विभाजन करके उनकी बुद्धि परीक्षा की। 6 वर्ष के नीचे के बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच थी और नव वर्ष के ऊपर के बालकों की केवल 70 ही थी। अन्वेषणों में यह स्पष्ट प्रमाणित होता है की बुद्धि के विकास और हार्स पर वातावरण की सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशाओं का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में भ्रमण करने केली जातियों के बालकों के भीतर भी बढ़ती हुई आयु के साथ बौद्धिक विकास में हार्स के पैमाने मिलते हैं। इस घटना की व्याख्या में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि जंगलों, पर्वतों तथा नदियों में लंबे समय तक निवास करने वाले परिवारों में बच्चों को सामान्य कोटि का शैक्षणिक परिवेश नहीं मिल पाता और फलस्वरूप यह बच्चे विकास के लिए आवश्यक अवसरों से वंचित रह जाते हैं। ऐसा होने से जो थोड़ी बहुत अनुवांशिक क्षमताएं उन्हें प्राप्त हुई रहती है वह प्रस्फुटित नहीं हो पाती। निम्न स्तरीय वातावरण में पलने वाले छोटी आई के बालकों की बुद्धि लब्धि में भौतिक हार्स नहीं पाया जाता क्योंकि छोटी आयु के लिए निर्मित बुद्धि परीक्षण ओं की समस्याएं कम होता है और केवल औपचारिक शिक्षा के अभाव में भी उनका सही समाधान प्रस्तुत कर पाता है। किंतु जब यह बालक बड़ी आई के हो जाते हैं तो उन पर प्रशासित परीक्षणों की समस्याएं भी अपेक्षाकृत अधिक जटिल होती है और बालक प्रश्नों की यही उत्तर तभी दे सकता है जब उसे पर्याप्त रूप से उत्तेजित करने वाले पाठ सालिय वातावरण में रहने का अवसर मिला हो।
जाने मिस्त्री वातावरण बालक के बौद्धिक विकास पर निषेधात्मक प्रभाव डालता है वही श्रेष्ठ वातावरण बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला तत्व सिद्ध हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि विशेष रूप से दो प्रकार के मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से होती है। अभिन्न यमजों के अनियंत्रित अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि जब यमज बालकों को भिन्न प्रकार के वातावरण में रहने के उपरांत उनके बौद्धिक स्तरों की तुलना की जाती है तो उनकी बुद्धि लब्धि में भिन्नता मिलती है। दो यमजों के बीच शिक्षा संबंधी अवसरों में जितनी अधिक भिन्नता होगी उनके भीतर उतनी ही अधिक बौद्धिक भिन्नता पाई जाएगी। विभिन्न अध्ययनों में बुद्धि लब्धि यह भिन्नता 24 पॉइंट तक पाई गई है। इसी प्रकार बुद्धि के विकास पर उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी धनात्मक प्रभाव पाया गया है। मैक्रेमार (1938) ने स्टैनफोर्ड-बिने बुद्धि परीक्षण के आधार पर पाया है कि अकुशल मजदूरों के बच्चों की और सद्बुद्धि लब्धि केवल 95 थी जबकि व्यवसाय धारियों के बच्चों की औषध बुद्धि लब्धि 125 निकली।
रथ (1979) न्यू उड़ीसा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ब्राह्मण जाति के बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन किया है जिससे सांस्कृतिक वचन के प्रभाव का पता चलता है। रावेन के प्रोग्रेसिव मैट्रीसेज के द्वारा बुद्धि स्तर पर मापन करने पर ब्राह्मण जाति के बच्चे अनुसूचित जाति के बच्चों से सार्थक रूप से उच्च प्राप्तांक प्राप्त किए थे। अन्य समूहों के बीच अंतर सार्थक नहीं थे। त्रिपाठी तथा मिश्र (1976) मैं दीर्घकालिक वंचन का ब्लाउज डिजाइन परीक्षण पर निष्पादन के साथ सार्थक रूप से ऋणात्मक सहसंबंध प्राप्त किया है। सिन्हा (1976) ने प्रत्याधिक कौशलों के विकास पर सामाजिक रूप से दुर्बल होने का सार्थक प्रभाव पाया है। यह प्रभाव आग में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है।
लेयर्ड (1957) ने भी वेक्सलर बुद्धि-परीक्षण (WATS) की सहायता से उच्चस्तरीय और निम्नस्तरीय सामाजिक आर्थिक दशाओं वाले परिवारों के बच्चों की परीक्षा की ओर देखा कि उच्चस्तरीय परिवारों के बच्चों की औसत बुद्धि-लब्धि 115 थी जबकि निम्नस्तरीय परिवारों के बच्चों की औसत बुद्धि-लब्धि केवल 103 थी। परिवार की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव भी बच्चों की बुद्धि पर देखा गया है। प्रायः शहर में रहने वाले बच्चे ग्रामीण वातावरण में पहले वाले बालकों के अपेक्षा कुछ अधिक बुद्धिमान पाये गये हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि तीव्र बुद्धि के लोग धीरे-धीरे शहरों में बसने लगते हैं और शहरों में तीव्र बुद्धि के बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है। यह बात सामाजिक-आर्थिक दशाओं के लिए भी कही जा सकती है। जो व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होते हैं वे अधिक अच्छे काम धन्धे अपनाते हैं और फलस्वरूप वे अधिक धन कमा लेते हैं जिसके कारण वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और अच्छा वातावरण उपलब्ध करा सकने में सफल होते हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि अधिकांश बुद्धि-परीक्षाओं में ऐसी समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नों का अधिक समावेश होता है जो उच्चस्तरीय सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शहरी वातावरणों में बहुलता से पायी जाती है। अतः यह भी सम्भव है कि कोई ऐसा बुद्धि परीक्षण तैयार किया जाय जिससे मापन करने पर ग्रामीण बच्चे शहरी बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान सिद्ध हों।
मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानों से पता चलता है कि आहार (Nutrition) का बुद्धि के विकास पर किसी सीमा तक अवश्य प्रभाव पड़ता है। पाउल (1938) ने आहार का प्रभाव बुद्धि पर देखने के लिए दो बाल समूहों का अध्ययन किया। प्रयोगात्मक समूह को लगभग बोस महीने तक उत्तम भोजन दिया गया जबकि नियंत्रित समूह को साधारण भोजन ही मिलता रहा। बीस महीने के बाद बुद्धि परीक्षा के आधार पर देखा गया कि प्रयोगात्मक समूह की औसत बुद्धि-लब्धि में दस प्वाइन्ट की वृद्धि हुई और नियंत्रित समूह की औसत बुद्धि-लब्धि ज्यों की त्यों हो रही। उत्तम आहार के कारण बुद्धि में जो वृद्धि होती है उसकी मात्रा जीवन के प्रथम चार वर्षों में सबसे अधिक देखी जाती है। सयाने बालकों पर यह प्रभाव कम पड़ता है। बुद्धि और पोषक तत्त्वों का सम्बन्ध निश्चित करने के सन्दर्भ में हैरेल (1946) ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। वर्जीनिया (Virginia) अनाथालय के 55 बच्चों के दो समूहों का अध्ययन हैरेल ने लगभग एक वर्ष तक किया। एक समूह को नित्य विटामिन बी की टिकिया और दूसरे समूह को केवल नकली टिकिया खिलायी गयी। दोनों समूह अन्य शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से पूर्णतः समान थे। प्रयोग की अवधि के बाद अनेक परीक्षणों की सहायता से दोनों समूहों की बुद्धि परीक्षा की गयी। हैरेल ने देखा कि विटामिन खिलाये गये समूह के बालक पढ़ने, याद करने तथा प्रतिस्थापन (Code Substitution ) को क्षमताओं में दूसरे समूह के बालकों से आगे थे। उपरोक्त अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बौद्धिक विकास की गति और सोमा उचित आहार और पोषक तत्त्वों के उपयोग से बढ़ायी जा सकती है। परन्तु ऐसा केवल उन्हीं बालकों में सम्भव है जो उचित आहार न पाते हों। अच्छे आहार पाने वाले बालकों में ऐसा सम्भव नहीं।
पिछले दो दर्शकों में बौद्धिक विकास में सांस्कृतिक या सामाजिक वंचन (Cultural or social deprivation) तथा आर्थिक विपन्नता (Economic disadvantage) के महत्त्व के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने विशेष रुाच प्रदर्शित की है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि बुद्धि में जातिगत और वर्गगत अन्तर निश्चित रूप से पाये जाते हैं। अमेरिकी गोरों और नीग्रो जाति के तुलनात्मक अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि नीग्रो जाति को बौद्धिक सक्षमता कम है। शुए (1966) ने 382 अध्ययनों के विश्लेषण के आधार पर यह परिणाम प्राप्त किया कि नीग्रो वर्ग की बुद्धि-लब्धि गोरों की अपेक्षा 15 अंक (I.Q. Points) कम है। साथ ही यह भी पाया गया है कि वंचन का यह प्रभाव संचयी (Cumulative) होता है। ऐसे परिणाम मैक्कलास्की (1967) तथा ह्वाइटमैन एवं ड्यूश (1968) आदि ने पाया कि गोरों (White) और नीग्रो बच्चों के बीच बौद्धिक स्तर का अन्तर आयु में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता जाता है। इस तरह के परिणामों की आलोचना यह कह कर की गयी है कि बुद्धि-परीक्षण मध्यवर्गीय प्रतिमानों के अनुरूप हैं, अत: निम्न वर्ग के लोगों की बौद्धिक क्षमता का इनके द्वारा निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः यह प्रश्न अभी भी विवादास्पद है क्योंकि तथाकथित सांस्कृतिक पूर्वाग्रह (Cultural bias) को हटाने के बाद भी पहले जैसे परिणाम मिले हैं (लैम्बर्ट, 1964)। जेन्सेन (1976) वे यह भी तर्क दिये हैं कि सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का प्रश्न व्यर्थ है क्योंकि बुद्धि परीक्षण गोरे और नीग्रो दोनों समूहों में एक जैसे परिणाम देते हैं तथा इनके द्वारा बुद्धि के जिस सामान्य तत्त्व का मापन किया जाता है वह भी एक सा है।
जातीय भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए जेन्सन (1969) तथा आइजेंक (1971) ने जननिक (Genetic) व्याख्या दी है। जेन्सेन के अनुसार बुद्धि-लब्धि में पाये जाने वाले अन्तर प्रमुखतः 80 प्रतिशत आनुवंशिक है। इस दृष्टिकोण का काफी विरोध हुआ है। जेन्सेन ने बुद्धि- परीक्षण द्वारा मापी गयी बुद्धि-लब्धि और बुद्धि को एक माना है और परीक्षण की दशाओं, परीक्षार्थी की अभिप्रेरणा आदि के महत्त्व को ध्यान में नहीं रखा है। वैसे बाद के एक अध्ययन में जेन्सेन (1977) ने कैलीफोर्निया और जिआर्जिया के नीग्रो बच्चों के प्रदत्तों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला हैं कि निम्नस्तरीय वातावरण संचयी ह्रास (Cumulative deficit) का कारण है। वस्तुत: बुद्धि एक अमूर्त सम्प्रत्यय है और इसका सर्वांश में मापन नहीं हो पाता और ऐसा भी नहीं है कि बुद्धि स्थिर रूप में (Fixed Intelligence) रहती है। उसका वातावरण से प्राप्त अनुभवों के द्वारा विकास होता है (हण्ट, 1961; 1973) । इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वातावरण और आनुवंशिकता के बीच बुद्धि के निर्धारण में उनकी भूमिका का बँटवारा नहीं किया जा सकता क्योंकि, जैसा हेब्ब (1954) ने संकेत किया है-हमारे व्यवहार और क्षमताओं का निर्धारण शत-प्रतिशत वातावरण और शत-प्रतिशत आनुवंशिकता द्वारा होता है। गर्भाधान के समय से ही ये तत्त्व अपने सर्वांश (Totality) में सक्रिय रहते हैं। वैसे मनोवैज्ञानिकों के लिए बुद्धि और जातिगत भिन्नता का प्रश्न अभी भी रोचक विवाद का प्रश्न बना हुआ है जिसका अनुमान कामिन (1975) को पुस्तक Science and Politics of IQ के शीर्षक से लगाया जा सकता है।
निष्कर्ष –
उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति की बुद्धि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रतिफल होती है। व्यक्ति अपनी दैहिक संरचना, ज्ञानेन्द्रियाँ एवं मस्तिष्क जो बुद्धि अर्जन हेतु आवश्यक है आनुवंशिकता से प्राप्त करता है। यदि उक्त अंग स्वस्थ ढंग से कार्यरत रहे तो बुद्धि का सामान्य विकास होता रहेगा। यदि इनमें किसी प्रकार का विकार आ जाता है तो एक सीमा तक बुद्धि विकास का कुंठित हो जाना अवश्यम्भावी है। ऐसी दशा में वातावरण चाहे जितना उत्तम हो व्यक्ति को लाभ नहीं हो सकता। दूसरी ओर, व्यक्ति मस्तिष्क की दृष्टि से चाहे जितना श्रेष्ठ हो, यह कहना कठिन होगा कि उसके भीतर उच्चस्तरीय बौद्धिक क्रियाएँ विकसित हो सकेगी। वास्तव में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति को वातावरण से किस मात्रा में उद्दीपन उपलब्ध होता है और वह उपलब्ध अवसरों का उपयोग किस प्रकार करता है। समुचित बौद्धिक विकास के लिए उत्तम आनुवंशिकता और उत्तम वातावरण दोनों ही आवश्यक है यद्यपि यह शुद्ध रूप से बता सकना कठिन होगा कि इनमें से किस तत्त्व का योगदान कितना है। ये दोनों तत्त्व बौद्धिक व्यवहार की उत्पत्ति एवं विकास में सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं और इनके प्रभावों को अलग नहीं किया जा सकता।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- परीक्षण की वैधता ज्ञात करने के दृष्टिकोण | अच्छे उपकरण की व्यावहारिक कसौटियाँ | मानक के प्रकार
- परीक्षण निर्माण के सिद्धान्त | परीक्षण योजना के परीक्षण रचना के अनेक चरण
- निकष संदर्भित परीक्षण से तात्पर्य | Criterion-Referenced Test in Hindi
- प्रतिमान सन्दर्भित परीक्षण से तात्पर्य | निकष सन्दर्भित तथा प्रतिमान सन्दर्भित परीक्षण में विभेद
- परीक्षा का अर्थ | परीक्षाओं की उपयोगिता या महत्त्व | परीक्षा के उद्देश्य | परीक्षा के कार्य | परीक्षा के प्रकार
- साक्षात्कार | साक्षात्कार की परिभाषा | साक्षात्कार की विशेषताएँ | साक्षात्कार का उद्देश्य | साक्षात्कार का क्या महत्व
- प्रश्नावली | प्रश्नावली की परिभाषा | प्रश्नावली की विशेषताएँ | प्रश्नावली का वर्गीकरण
- श्रेणी मापनी विधि | दर मापक का नमूना | श्रेणी मापनी विधि को नमूना बनाकर स्पष्ट कीजिए
- व्यक्तित्व क्या है | व्यक्तित्व का अर्थ | व्यक्तित्व की परिभाषा | व्यक्तित्व के प्रकार
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]