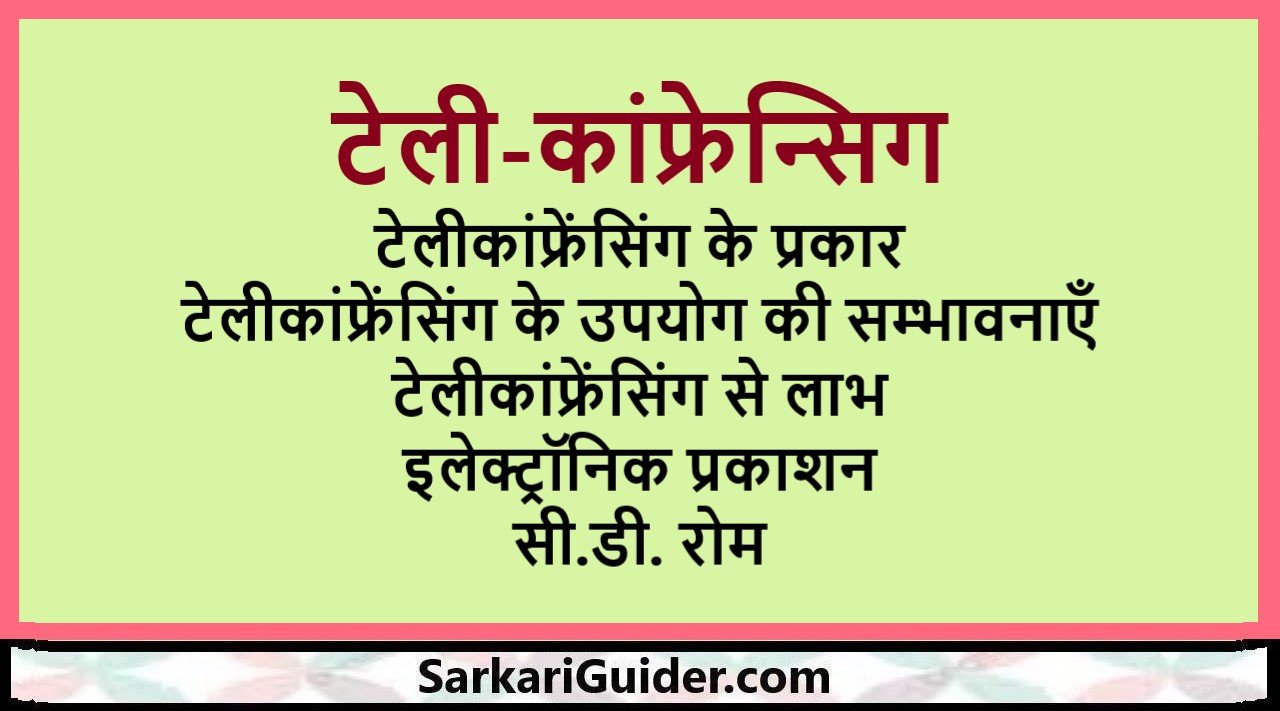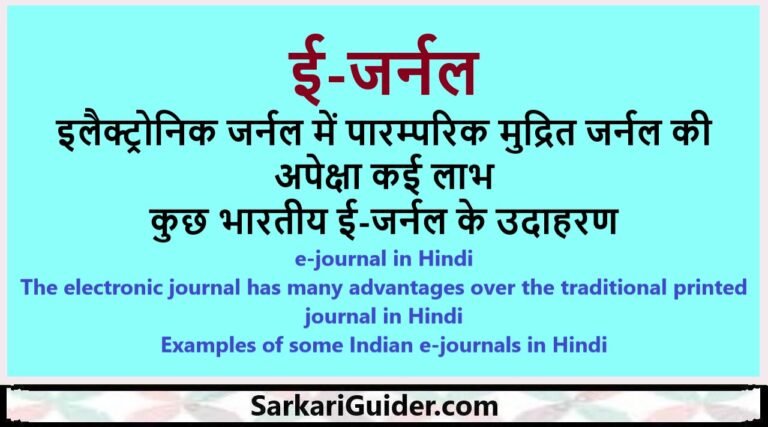टेली-कांफ्रेन्सिग | टेलीकांफ्रेंसिंग के प्रकार | टेलीकांफ्रेंसिंग के उपयोग की सम्भावनाएँ | टेलीकांफ्रेंसिंग से लाभ | इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन | सी.डी. रोम
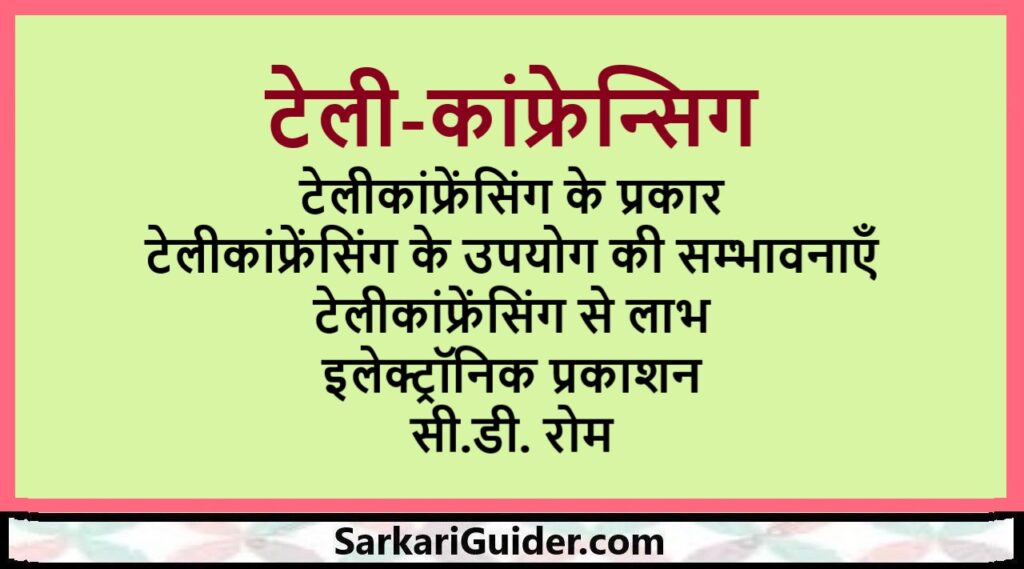
टेली-कांफ्रेन्सिग | टेलीकांफ्रेंसिंग के प्रकार | टेलीकांफ्रेंसिंग के उपयोग की सम्भावनाएँ | टेलीकांफ्रेंसिंग से लाभ | इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन | सी.डी. रोम | Tele-conferencing in Hindi | Types of Teleconferencing in Hindi | Possibilities of using teleconferencing in Hindi | Benefits of Teleconferencing in Hindi | Electronic Publishing in Hindi | CD. Rome in Hindi
टेली-कांफ्रेन्सिग (Tele-conferencing)
वर्तमान समय में कम्प्यूटर, इण्टनेट, टेलीफोन तथा टेलीविजन के आपसी संयोग के आधार पर विचार-विनियम हेतु संगोष्ठी का आयोजन, प्रत्यक्ष रूप से किसी से घर बैठे वार्तालाप करना अत्यन्त आसान हो गया है। इस सर्वसुलभ व्यवस्था को टेलीकांफ्रैंसिंग (Tele-conferencing) कहा जाता है। यह व्यूह रचना शिक्षण/शिक्षा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इसमें विविध संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है तथा द्विमार्गीय प्रसारण द्वारा अन्तः क्रिया समूह को विचार रखने की सुविधा दी जाती है।
टेलीकांफ्रेसिंग मूलतः संचार माध्यमों पर आधारित, विद्युत चालित वह इलेक्ट्रानिक व्यवस्था है, जिसके द्वारा दो या उससे अधिक सुदूर व्यवस्थित व्यक्ति या समूह में किसी भी विषय-वस्तु पर चर्चा, वार्तालाप किया जा सकता है। इसमें दृश्य-श्रव्य दोनों की व्यवस्था होती है और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा भी रहती है। प्रायः आजकल समाचारों की प्राप्ति हेतु सुदूर स्थित संवाददाता से जो सूचना सचित्र रूप से वार्तालाप के माध्यम से दिखाया और सुनाया जाता है वह टेलीकांफ्रैन्सिग पर ही आधारित होता है।
टेलीकांफ्रेसिंग की कार्यप्रणाली एवं तकनीकी मूल रूप से टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट के आपसी संजाल (Network) से विकसित किया गया है। इस व्यवस्था का प्रयोग करने के लिए टेलीफोन के कुछ आवश्यक यंत्रों को जोड़कर किसी भी इण्टरनेट लाइन या टेलीफोन लाइन को प्रयोग में लाया जाता है। बातचती का सजीव प्रसारण टेलीविजन के पर्दे पर मूर्तमान हो उठाता है।
टेलीकांफ्रेंसिंग के प्रकार
टेलीकांफ्रेंसिंग के तीन प्रकार होते हैं।
(i) ऑडियो कॉन्फ्र (ii) वीडियो कॉन्फेन्स (iii) कम्प्यूटर कॉन्फन्स
ऑडियो कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने वाले व्यक्ति के दूसरेक से बातजीत तो कर सकते हैं, किन्तु एक दूसरे को प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। यह मूल रूप से टेलीफोन द्वारा सम्पन्न होती है। जैसे आजकल विविध भारती पर टेलीफोनक वार्ताएँ होती है।
विडियो कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने वाले व्यक्ति के दूसरे को देख एवं सुन सकते है। तथा वार्तालाप भी कर सकते हैं। जैसा आजकल दूरदर्शन पर समाचार के के प्रसारण या चुनाव के नतीजों की प्राप्ति हेतु संवाददाताओं से बातचीत का सजीव प्रसारण किया जाता है।
कम्प्यूटर कॉन्फ्रेन्स में अलग-अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति कम्प्यूटर को प्रयोग में लाकर सूचाओं का आदान-प्रदान करते हैं।
टेलीकांफ्रेंसिंग के उपयोग की सम्भावनाएँ-
टेलीकांफ्रेंसिंग जैसे नूतन व्यवस्था के उपयोग की सम्भावनाएँ अप्रलिखित हो सकती है-
(i) प्रभावी शिक्षण प्रबन्धन में।”
(ii) दूरस्थ शिक्षा/खुले विद्यालयों/खुले विश्वविद्यालयों में।
(iii) सुविधाविहीन लोगों तक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु।
(iv) समस्याग्रस्त बालकों/अधिगम में पिछड़े बालकों की शिक्षा हेतु।
(v) विषय-विशेषज्ञों के विचारों से लाभान्वि होने हेतु।
(vi) शोध-सर्वेक्षण हेतु।
(vii) शिक्षकों की जवाबदेही हेतु।
(viii) विद्यालयी कार्य प्रणाली के मूल्यांकन हेतु।
(ix) नवीन शैक्षिक योजनाओं, नीतियों की जानकारी हेतु।
(x) अभिभावकों से विचार-विनिमय हेतु।
टेलीकांफ्रेंसिंग से लाभ (Advantage of Tele-conferencing)-
टेलीकांफ्रेंसिंग शिक्षण/अनुदेशन की नवीन विधा है। भारत में अभी यह अपने शैशवास्था में है। किन्तु आगामी दशकों में यह शिक्षण/अनुदेशन के अभिन्न अंग के रूप में व्यवस्थित हो जायेगा, ऐसी सम्भावनाएँ परिलक्षित हो रही है। इस सम्भावना के पीछे टेलीकांफ्रेंसिंग से मिलने वाली सहूलियतें और परधन, समय, श्रम की बचत बताया जा सकता है। वास्तव में टेलीकांफ्रेंसिंग के अनेक लाभ है। इसे संक्षेप में निम्नवत् प्रकट किया जा सकता है-
- टेलीकांफ्रेंसिंग वास्तविक एवं प्रत्यक्ष शिक्षण की व्यवस्था प्रदान करता है।
- टेलीकांफ्रेंसिंग में अधिगमकर्ता सक्रिय होकर अधिगमोन्मुख होते हैं, इससे उनके ज्ञान में स्थायित्व आता है।
- टेलीकांफ्रेंसिंग विविध ज्ञान एवं अनुभवों के संग्रहण में उपयोगी है।
- टेलीकांफ्रेंसिंग से विषय विशेषज्ञों की सेवाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती है। 5. टेलीकांफ्रेंसिंग से छात्रों को अभिप्रेरित करने तथा पृष्ठ पोषण आसानी से दिया जा सकता है।
- टेलीकांफ्रेंसिंग द्वारा शिक्षण/अनुदेशन सामग्री का परिमार्जलन एवं परिशोधन कर प्रभावी बनाया जा सकता है।
- टेलीकांफ्रेंसिंग से सुदूर स्थानों तक बिखरे लोगों तक ज्ञान की ज्योति जालायी जा सकती है।
- टैलीकांफ्रेंसिग से विद्यालय के स्थान पर संसाधन केन्द्रों द्वारा छात्रों तक विविध सूचनाएँ पहुँचायी जा सकती है।
- टेलीकांफ्रेंसिंग से उचित निर्देशन एवं परामर्श की प्राप्ति सम्भवक्षहै।
- टेलीकांफ्रेंसिंग दुरस्थ शिक्षा में अत्यन्त प्रभावकारी है।
इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन/सी.डी. रोम क्या है?
सूचना तकनीकी के नवीन आयामों में सी. डी. रोम या इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन का विशेष महत्व है। यह उपकरण त्वरित गति से सूचनाओं को एकत्र करता है तथा असंख्य सूचनाओं के आंकड़ों को उपलब्ध कराता है। इसके उपयोग से वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नवीन सूचनाओं की जानकारी तथा समस्याओं के व्यावहारिक समाधान में विशेष सहायता मिलती है। सी. डी. रोम (C.D. ROM) में जितने भी अक्षर हैं वे सभी अलग-अलग विशेषताओं को उजागर करते हैं
C=Compact (काम्पैक्ट), D=Disc (डिस्क),
R= Read (रीड) O=Only (ओनली) M= Memory (मेमोरी)
इस प्रकार सी. डी. रोम का आशय है- Compact Disc-Read Only Memory अर्थात् सी. डी. रोम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काम्पैक्ट डिस्क पर केवल स्मृतियाँ (Memories) पढ़ी जा सकती हैं।
वास्तव में सी. डी. रोम एक ऐसी आप्टिकल डिस्क है जिसके द्वारा सूचनाओं के विशाल भण्डार (अनुमानतः 1 GB अर्थात् 700 फ्लॉपियों की क्षमता के बराबर) को भण्डारित किया जा सकता है। किन्तु सी. डी. रोम में आँकड़े एकत्रित किये जा सकते हैं परन्तु इन आँकड़ों में किसी प्रकार का बदलाव अथवा अन्य आंकड़ों को पुनः नहीं जोड़ा जा सकता है।
आधुनिक समय में सी. डी. रोम की इस कमी को दूर करते हुए नवीन सी. डी. भी अस्तित्वशाली हुई हैं। ये हैं-सी. डी. आर. डब्ल्यू. (C.D.-R.W.) अर्थात् (Compact Disc- Read and Write)। इसमें किसी भी आँकड़े फ्लापी या हार्डडिस्क की तरह पढ़ा और जरूरत के अनुकूल लिखा अथवा संशोधन भी किया जा सकता है।
सी. डी. रोम से कार्य करने हेतु पर्सनल कम्प्यूटर (Personal Computer), सी. डी. रोम प्लेयर (C.D. Rom Player), सर्च साफ्टवेयर (Search Software), काम्पैक्ट डिस्क (Compact Disk) तथा लेजर प्रिन्टर (Laser Printer) आदि यंत्रों का होना अति आवश्यक है।
शैक्षिक तकनीकी – महत्वपूर्ण लिंक
- शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य | शैक्षिक तकनीकी का महत्व तथा उपयोगिता | Objectives of Educational Technology in Hindi
- शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान | शैक्षिक तकनकी के लिए कार्यरत कुछ महत्वपूर्ण रिसोर्स सेन्टर्स के नाम
- शैक्षिक तकनीकी का महत्व | शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता
- ओवरहेड प्रोजेक्टर | ओवरहेड प्रोजेक्टर का शिक्षा में महत्व | ओवरहेड प्रोजेक्टर का शैक्षिक अनुप्रयोग | ओवरहेड प्रोजेक्टर के प्रयोग की विधि | ओवरहेड प्रोजेक्टर की परिसीमाएं
- भाषा प्रयोगशाला से आशय | भाषा प्रयोगशाला की विशेषताएँ | Language Laboratory in Hindi | Characteristics of Language Laboratory in Hindi
- शिक्षा में तकनीकी का तात्पर्य | शिक्षा में तकनीकी का अर्थ | शिक्षा तकनीकी के प्रयोग के मुख्य सिद्धान्त | शिक्षा तकनीकी को प्रभावित करने वाले तत्व | शैक्षिक तकनीकी के प्रकार
- दृश्य-श्रव्य तकनीकी | शैक्षिक तकनीकी में किये गये प्रमुख शोध कार्य | शैक्षिक तकनीकी में अनुसंधानों पर आधारित नवीन प्रवृत्तियाँ
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]