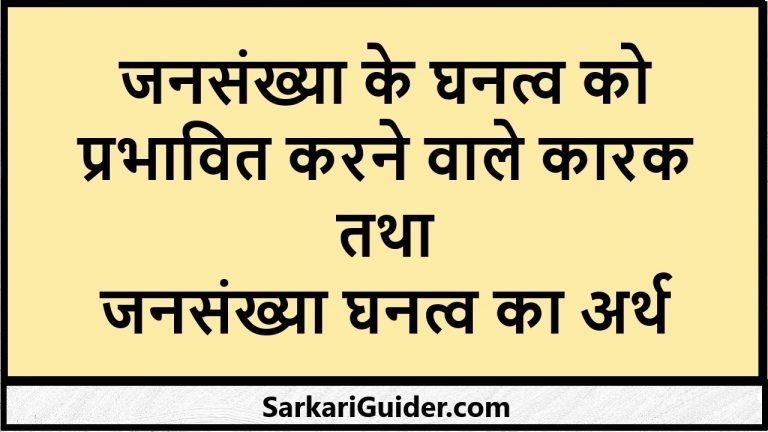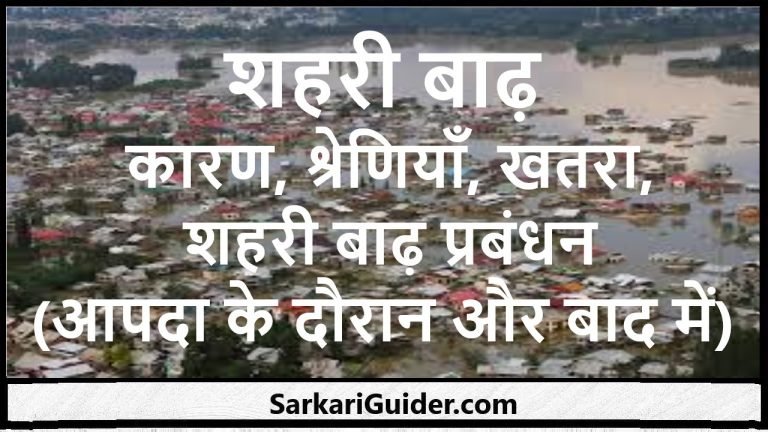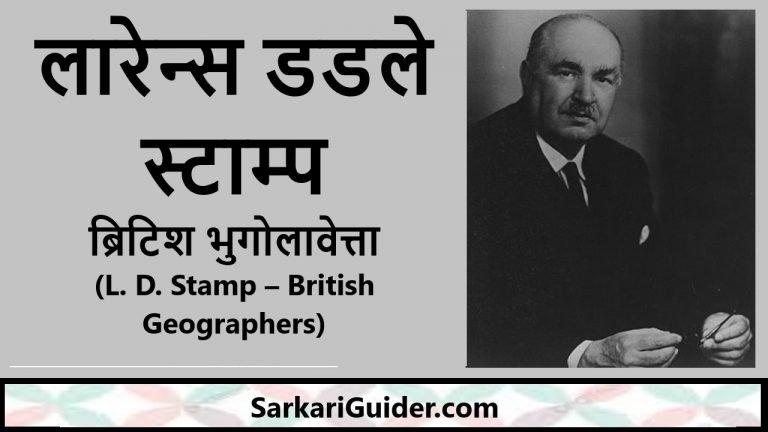शैल या चट्टान क्या है | चट्टानों का वर्गीकरण (प्रकार) | चट्टानों का आर्थिक महत्त्व
शैल या चट्टान क्या है | चट्टानों का वर्गीकरण (प्रकार) | चट्टानों का आर्थिक महत्त्व
सामान्य रूप से भूतल की रचना जिन पदार्थों से हुई है, उन्हें चट्टान या शैल के नाम से पुकारते हैं। चट्टाने अनेक खनिज पदार्थों का सम्मिश्रण होती हैं। खनिज पदार्थों का यह सम्मिश्रण रासायनिक तत्त्वों का योग होता है। वर्तमान वैज्ञानिक युगे में 115 मूल तत्त्वों की खोज कर ली गयी हैं। उपर्युक्त तत्त्वों में धरातलीय संरचना का लगभग 986 भाग केवल आठ तत्त्वों ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऐलुमिनियम, लोहा, कैल्सियम, सोडियम, पोटैशियम एवं मैग्नीशियम द्वारा निर्मित है। शेष 2% भाग 98 त्त्वों के योग से बना है। इसके अतिरिक्त प्रकृति द्वारा प्रदत्त अन्य तत्त्व भी धरातलीय निर्माण में सहायक हुए हैं।
‘चट्टान’ शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी दृढ़ एवं कठोर स्थलखण्ड से लिया जाता हैं, परन्तु भूतल की ऊपरी पपड़ी में मिले हुए सभी पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट की भाँति कठोर हों या चीका की भाँति कोमल, चट्टान कहलाते हैं। आर्थर होम्स का मत है कि “शैल अथवा चट्टानों का अधिकतम भाग खनिज पदार्थों का सम्मिश्रण होता है।” खनिज पदार्थों के सम्मिश्रण कोमल हों या क्वार्ट्जाइट के समान ठोस या बालू के समान ढीले तथा मोटे कण वाले हों, सभी चट्टान कहलाते हैं। इस आधार पर चट्टानों की परिभाषा इन शब्दों में व्यक्त की जा सकती है-“चट्टान अपनी भौतिक स्थिति का वह पिण्ड है जिसके द्वारा धरातल का ठोस रूप परिणत हुआ है।” वास्तव में भूपटल के निर्माण में सहयोग देने वाले सभी तत्त्व शैल या चट्टान कहलाते हैं।

चट्टानों का वर्गीकरण
सामान्य रूप से चट्टानों को निम्नलिखित तीन भागों में बॉटा जा सकता है।
- आग्नेय चट्टाने
‘आग्नेय’ शब्द लैटिन भाषा के Igneous शब्द का रूपान्तरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ ‘अग्नि’ से होता है। भूगोलवेत्ताओं का विचार है कि प्रारम्भ में सम्पूर्ण पृथ्वी आग का तपता हुआ गोला थी, यह धीरे-धीरे ठण्डी होकर द्रव अवस्था में परिणत हुई है। द्रव अवस्था से ठोस तथा इस ठोस अवस्था से अधिकांशत: आग्नेय चट्टानें बनी हैं। जब भूगर्भ का गर्म एवं द्रवित लावा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरातल पर फैलने से ठण्डा होकर ठोस बनने लगा, तभी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इन चट्टानों का निर्माण आज भी होता रहता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अन्य चट्टानों को भी जन्म देती हैं।
- अवसादी या परतदार चट्टानें
भूतल के 75% भाग पर अवसादी या परतदार चट्टानों का विस्तार है, शेष 25% भाग में आग्नेय एवं कायान्तरित चट्टानें विस्तृत हैं। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण से हुआ है। अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा धरातल, झीलों, सागरों एवं महासागरों में लगातार मलबा (Debris) जमा होता रहता है। यह मलबा परतों के रूप में जमा होता रहता है। इस प्रकार लगातार मलबे की परत के ऊपर परत जमा होती रहती है। अत: ऊपरी दबाव के कारण नीचे वाली परतें कुछ कठोर हो जाती हैं। यही परतें कठोर होकर परतदार शैलें बन जाती हैं।
- कायान्तरित या रूपान्तरित चट्टानें
अंग्रेजी भाषा में इन्हें ‘मेटामोरफिक’ कहा जाता है। ‘मेटामोरफिक’ शब्द मेटा एवं मार्फे शब्दों के सम्मिलन से बना है। अत: मेटा का अर्थ परिवर्तन तथा मार्फे का अर्थ रूप से है अर्थात् “जिन चट्टानों में दबाव, गर्मी एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा उनकी बनावट, रूप तथा खनिजों का पूर्णरूपेण कायापलट हो जाता है, कायान्तरित चट्टानें कहलाती हैं।” विश्व के प्राय: सभी प्राचीन पठारों पर कायान्तरित चट्टानें मिलती हैं। भारत में ऐसी चट्टानें दक्षिण के प्रायद्वीप भाग में पायी जाती हैं, इनके अतिरिक्त विश्व में ये चट्टानें दक्षिण अफ्रीका के पठार और दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील के पठार, उत्तरी कनाडा, स्कैण्डेनेविया, अरब, उत्तरी रूस और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार पर पायी जाती है।
चट्टानों का आर्थिक महत्त्व
चट्टानों के आर्थिक महत्त्व को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है
- कृषि के क्षेत्र में
उपजाऊ मिट्टी कृषि का आधार है। उपजाऊ मिट्टी के निर्माण में शैलों का विशेष महत्त्व रहता है। शैल चूर्ण जमकर ही उपजाऊ मिट्टी को जन्म देते हैं। अन्न, फल, शाक-भाजी, कपास, गन्ना, रबड़, नारियल, चाय, कहवा तथा गरम मसाले सभी मिट्टी में ही उगाये जाते हैं।
- बरागाहों के क्षेत्र में
हरी घास के विस्तृत क्षेत्र चरागाह कहलाते हैं। हरी घास पशुओं को पोष्टिक चारा उपलब्ध कराती है। चरागाह पशुपालन के आदर्श. क्षेत्र माने जाते हैं। हरी घास शैलों में ही उगा करती है; अंतः पुशुचारण और पशुपालन में भी शैलों की उपयोगिता अद्वितीय मानी गयी है।
- भवन-निर्माण के क्षेत्र में
पत्थर भवन-निर्माण की प्रमुख सामग्री है। स्लेट, चूना-पत्थर, बलुआ पत्थर तथा संगमरमर भवन-निर्माण में सहयोग देते हैं। भवन-निर्माण का सस्ता और टिकाऊ मसाला चट्टानों से प्राप्त पदार्थों से ही बनाया जाता है। संगमरमर तथा ग्रेनाइट पत्थर भवनों की सुन्दर तथा भव्य स्वरूप प्रदान करते हैं।
- खनिज उत्पादन के क्षेत्र में
खनिज पदार्थों का जन्म भूगर्भ में शैलों द्वारा ही होता है। शैलें सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा, कोयला, मैंगनीज तथा अभ्रक आदि उपयोगी खनिजों को जन्म देकर जहाँ मानव के कल्याण की राह खोलती हैं, वहीं कोयला तथा खनिज तेल देकर ऊर्जा तथा तापमान के स्रोत बन जाती हैं।
- उद्योगों को कच्चे माल प्रदान करने के क्षेत्र में
कृषिगत उपजों, वन्य पदार्थों तथा खनिज पदार्थों पर अनेक उद्योग- धन्धे निर्भर होते हैं। चट्टानें एक ओर तो उद्योगों को कच्चे माल देकर उनका पोषण करती हैं और दूसरी ओर शक्ति के साधनों की आपूर्ति करके उन्हें ऊर्जा तथा चालक-शक्ति प्रदान करती हैं। राष्ट्र का आर्थिक विकास जहाँ उद्योग-धन्धों पर निर्भर है, वहीं उद्योग-धन्धों का विकास शैलों से प्राप्त कच्चे मालों पर निर्भर करता है।
- मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के क्षेत्र में
शेलें मानव को उसकी तीनों प्राथमिक आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र और मकान की आपर्ति कराती हैं। मानव के पोषण में शैलों का विशेष सहयोग रहता है।
- पेयजल स्रोतों के रूप में
पृथ्वी पर मानव के लिए पेयजल भूस्तरीय जल के अतिरिक्त भूगर्भीय जल भी होता है। भूगर्भीय जल चट्टानों में स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। भूस्तरीय जल नदियों, झरनों और झीलों के रूप में तथा भगर्भीय जल हैण्डपम्मों, पम्पसेटों तथा नलकूपों के द्वारा प्राप्त होता है।
- मानवीय सभ्यता के गणक के रूप में
मानव-सभ्यता का ज्ञान प्रदान करने में चट्टानों का विशेष योगदान रहता है। पृथवि की आयु व आंतरिक संरचना चट्टानों की निर्माण-प्रक्रिया को आधार मानकर ही ज्ञात की जाती है।
शैलों की रचना तथा निर्माण-प्रक्रिया के अध्ययन से भूविज्ञान तथा भृगर्भ विज्ञान के अध्ययन में बहुत सहायता मिलता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शैले मानव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं तथा उसे अधिक सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। वतमान विश्व का सम्पूर्ण औद्योगिक ढाँचा तथा प्रौद्योगिकी तन्त्र शैलों से ही अनुप्रमाणित है।
महत्वपूर्ण लिंक
- वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Transpiration)
- मृदा नमी की आवश्यकता एवं महत्व (Need and Importance of Soil Moisture)
- जलीय चक्र पर मानव का प्रभाव (Man’s Influence on Hydrological Cycle)
- वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Evaporation)
- वाष्पीकरण नियन्त्रण (Evaporation Control)
- वाष्पोत्सर्जन का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Transpiration)
- जल विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning And Definition of Hydrology)
- जल विज्ञान का विषय क्षेत्र (Scope of Hydrology)
- भारतीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएँ (SALIENT FEATURES)
- जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Climate)
- जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास
- पारिस्थितिक तंत्र पर मानव का प्रभाव
- प्राकृतिक संसाधन (Natural resource)
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
- चट्टानों के प्रकार – आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रुपांतरित चट्टानें
- मनुष्य का विकास (Human evolution)
- जेट प्रवाह (Jet Streams)
- जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय (EFFORTS TO CHECK POPULATION GROWTH)
- वनों के लाभ (Advantages of Forests)
- श्वेत क्रान्ति (White Revolution)
- द्वितीय हरित क्रांति
- हरित क्रान्ति की सफलता के लिए सुझाव (SUGGESTIONS FOR THE SUCCESS OF GREEN REVOLUTION)
- हरित क्रांति के दोष अथवा समस्याएं (Demerits or Problems of Green Revolution)
- हरित क्रान्ति की उपलब्धियां एवं विशेषताएं
- हरित क्रान्ति (Green Revolution)
- शहरीय परिवहन | यातायात में व्यवधान सिद्धांत | परिवहन की समस्याएं एवं समाधान
- तकनीकी आपदा Technical Hazard
- ओजोन क्षरण Ozone layer degradation
- Soil Resource Degradation (Soil Erosion)
- मानव विकास Human Development in hindi
- गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत ( non conventional energy resources)
- संज्ञानात्मक नक्शा, मानसिक नक्शा या मानसिक मॉडल Cognitive Map
- गतिक संतुलन संकल्पना Dynamic Equilibrium concept
- पारंपरिक एवं लोक ग्रामीण अधिवास के प्रकार Traditional and folk rural house types
- रैवेनस्टीन का प्रवास नियम (Ravenstein – The laws of migration)
- भारतीय गृह की प्रादेशिक विशेषताएँ [ Regional morphological characteristics of Indian village ]
- नगरीय क्षेत्रीय माडल [ Urban realms model ]
- बाई लुंड का सिद्धांत [ Bylund ( Sweden ) settlement diffusion theory ]
- भूमण्डलीय ऊष्मन( Global Warming)|भूमंडलीय ऊष्मन द्वारा उत्पन्न समस्याएँ|भूमंडलीय ऊष्मन के कारक
- मानव अधिवास तंत्र [ Human settlement as a system ]
- बाढ़ आपदा परिभाषा तथा अर्थ,बाढ़ के प्रकार,बाढ़ के कारण,बाढ़ आपदा का प्रबन्धन,
- भूमंडलीकरण (वैश्वीकरण) विशेषताएँ,वैश्वीकरण के लाभ,पक्ष तथा विपक्ष में तर्क
- भारत में वनों का वर्गीकरण – भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण
- वनों का राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्व – वनों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ
- जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक
- जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक तथा जनसंख्या घनत्व का अर्थ
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है | हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है| यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]