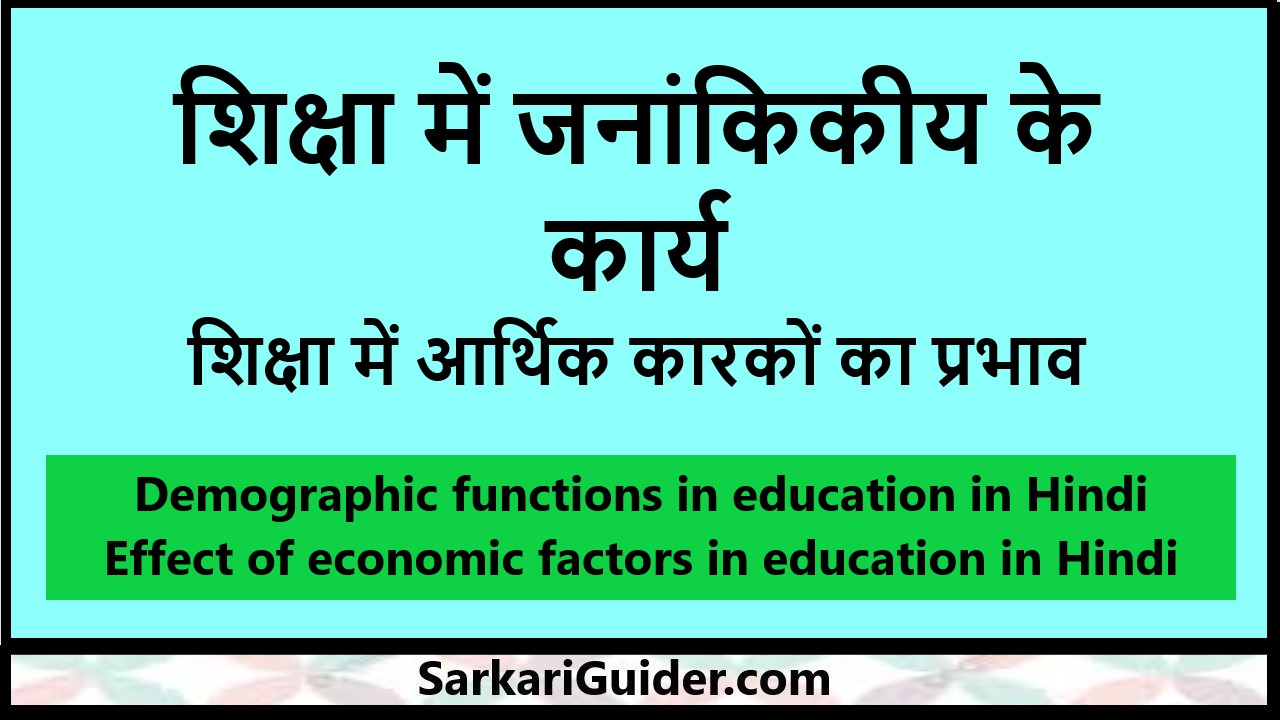शिक्षा में जनांकिकीय के कार्य | शिक्षा में आर्थिक कारकों का प्रभाव

शिक्षा में जनांकिकीय के कार्य | शिक्षा में आर्थिक कारकों का प्रभाव
(1) जनांकिकीय के कार्य (Function of Senses)-(शिक्षा में जनांकिकीय के कार्य) –
द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जनसंख्या के परिवर्तनों की सामान्य उपनति गिरते हुए जन्म दर की ओर थी, परन्तु युद्ध के पश्चात् सभी देशों में जन्म-दर में बहुत वृद्धि हुई है। जनसंख्या में वृद्धि ने शिक्षा के लिए अधिक सुविधाओं का प्रावधान करने की बृहत्तर माँग की। इसके साथ ही उच्चतर शिक्षा के लिए बृहत्तर मांग उठ खड़ी हुई थी। आधुनिक विश्व में काम पाने की समस्या अधिक कठिन तथा स्पर्धा कण्ठ-छेदी हो गई है। जो व्यक्ति प्रारम्भिक शिक्षा तक ही रुक जाते है तथा पैसा कमाना चाहते है, उन्हें रोजगार पाने की अल्प सुविधाएँ रहती है और इस कारण छात्र शैक्षिक संस्थाओं में लम्नी अवधि तक रहना चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए अधिक शिक्षा देने में असमर्थ माता-पिता भी या तो सामाजिक नकल के लिए या अपने बच्चों को जीवन की होड़ में उपयुक्त ढंग से सज्जित करने के लिए अच्छी और अधिक शिक्षा का आग्रह कर रहे हैं। इस प्रकार की उपनीतियों ने शिक्षा के लिए मांग को केवल तीव्र और, पढ़ाई की अवधि को दीर्घ कर दिया है। बट्रेड रसेल ने कहा है कि “किसी भी समय किसी भी समान में एक पर्याप्त सम्भावना रहती है कि जनसंख्या की वृद्धि तकनीकी उन्नति से आगे बढ़े और इसीलिए जीवन-स्तरों को सामान्य रूप से नीचा कर दें।” एल्डस हक्सले ने जनंसख्या की वृद्धि के अन्य प्रभावों की गणना की है। वे कहते है, “व्यक्तियों को एक अपर्याप्त उपजीविका कमाने हेतु अधिक समय तथा अधिक मेहनत से काम करना पड़ता है। इसके साथ ही समस्त समाज की आर्थिक दशा इतनी अनिश्चित रहती है कि छोटी विपत्तियाँ भी, जैसे कि मौसम की असामान्य दशाएँ एक गम्भीर विभंजन में परिणित हो सकती है। सामाजिक अव्यवस्था में वैयक्तिक स्वतंत्रता थोड़ी या शून्यतम हो सकती है और जहाँ सामाजिक अव्यवस्था को शक्तिशाली केन्द्रायित कार्यपालिका द्वारा व्यवस्था में बदला जाता है, वहाँ सर्वाधिकारिता का गम्भीर खतरा रहता है। अर्थ-व्यवस्था, जीवन स्तर तथा शासन के स्वरूप में इस प्रकार के परिवर्तनों का शिक्षा के वित्त प्रबन्धन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न पर इस आशय में अन्कत्र विचार किया गया है।
डब्ल्यू.आर. बरगस द्वारा संचालित एक रोचक अध्ययन ने यह प्रकट किया है कि 1870-1920 की अर्थ शताब्दी के अन्तर्गत जनसंख्या में तीन गुनी विद्यालयी उपस्थिति में चार गुनी, शैक्षिक व्यय में बारह गुनी वृद्धि हुई। उससे यह निष्कर्ष निकाला कि जब जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति सामान्तर श्रेणी में थी, विद्यालय परिव्ययों में वृद्धि की प्रवृत्ति गुणान्तर श्रेणी की थी। सन् 1933 में डब्ल्यू. जी. कार द्वारा किए गए एक दूसरे अध्ययन ने यह प्रकट किया कि यद्यपि प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय में सम्पूर्ण नामांकन की वृद्धि समान्तर श्रेणी में हुई, हाईस्कूल नामांकन की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में हुई। सन् 1930 तक हाई स्कूल नामांकन का वक्र, व्यय के वक्र के निकट रूप में समान्ततिक रहा।
इस प्रकार विभिन्न आयु-समूहों में व्यक्तियों के अनुपात की शैक्षिक वित्त पर अपनी प्रतिक्रिया होती है। दो समूह जो कि परिव्यय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वे 20 और के बीच का उत्पादक समूह तथा 5 से 17 वर्ष की आयु के बीच का विद्यालय- गामी आयु समूह । जनसंख्या में उत्पादक समूह के बड़ा होने पर, शिक्षणीय जनसंख्या का अनुपात कम हो जाता है। कुछ देशों में यह समूह विद्यालय-गामी आयु समूह से पाँच गुना होता है। परन्तु अधिकांश एशियाई देशों में उत्पादन समूह, दूसरे समूह का केवल दो गुना या तीन गुना होता है। अतएव उपरोक्त देशों की विद्यालय गामी बालकों की बृहती संख्या के लिए प्रावधान करना होता है। यह उनके ऊपर दोहरा प्रतिकूल प्रभाव डालता है, एक ओर उन्हें शिक्षा के प्रावधान पर अधिक खर्च करना होता है और दूसरी ओर राष्ट्रीय आय गिर जाती है।
(2) आर्थिक कारकों का प्रभाव (Impact of Economic Factors) –
शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि- आर्थिक कारणों ने शिक्षा के क्रम को निरन्तर प्रभावित किया है। देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था, राष्ट्रीय आमदनी की राशि तथा लोगों में जीवनयापन के स्तर ने बहुधा शिक्षा की स्थिति पर प्रतिक्रिया की है और इसके फलस्वरूप उसके वित्त-प्रबन्धन को प्रभावित किया है। ये कारण यहाँ पर देखे जा सकते है।
सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था (Total Economic System)
अगर चिन्तन में तार्किक ढंग से विचार किया जाये तो ज्ञात होता है कि- शिक्षा, समुदाग, की समस्त अर्थ-व्यवस्था के प्रति, सहायता के लिए ऋणी है। एक निर्वाह अर्थ- व्यवस्था में जहाँ कि जनता केवल अपना भरण-पोषण ही कर पाती है, अधिक सांस्कृतिक प्रगति असम्भव है और शिक्षा आवश्यक रूप से पृष्ठभूमि में चली जाती है। बचत अर्थ- व्यवस्था में जहाँ उत्पादन, उपभोग से अधिक होता है, जनता के पास पर्याप्त अवकाश होता है जिसे वे सांस्कृति प्रगति में लगाते है तथा उनकी शिक्षा सामान्यतः एक महत्वपूर्ण स्थान पाती है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था या व्यापारिक अर्थ व्यवस्था या दोनों मिलकर भी, अपने सर्वाधिक अच्छे दिनों में भी, उच्च तथा उच्च मध्यम वर्गों से अधिक शिक्षण के लिए सहायता देने में समर्थ नहीं हो सके हैं। यह औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था ही है, जिसने विशाल अतिरिक्त राशियाँ एकत्र कर समस्त जनसंख्या के शिक्षण को सम्भव बना दिया है।
मुख्यतः कृषि अर्थ व्यवस्था में विद्यालय उपस्थिति में विलीन प्रत्येक वर्ष का अर्थ-उत्पादक परिसम्पदा का एक प्रभावपूर्ण प्रतयाहार होता है। परन्तु एक यांन्त्रिक अर्थ-व्यवस्था में सत्य इसके विपरीत हैं। शिक्षा, समुदाय की मूल अर्थ व्यवस्था पर निर्भर करती है। यह इस तथ्य द्वारा प्रमाणित हो जाता है कि शिक्षा के उत्थान और पतन के चक्र, आर्थिक चक्रों में सम्पाती होते हैं। इतिहास आर्थिक पतन के समान्तर शैक्षिक पतन के उदाहरणों से भरा पड़ा है। रोमन साम्राज्य का पतन, मध्यकालीन यूरोप का अन्धकार-युग, अमरीका में उन्नीसवीं सदी में सन् 1830 से आरम्भ हुए दो दशकों के समयानुसार के पुनः पुनः होने वाली आर्थिक मन्दी तथा इस शताब्दी के तीसरे दशक में विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, शैक्षिक अपक्षय और आर्थिक हरास के सम्पात के उदाहरण हैं। साधारणतः आर्थिक मन्दी के शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव, उसके पूर्ण परीक्षण में रहने के दो या तीन वर्ष बाद अनुभव किये गये हैं। आर्थिक संकुचन की ये अविधियाँ आर्थिक अभिवृद्धि द्वारा अनुसृत हुई और इसी प्रकार उपरोक्त के साथ शैक्षिक विकास की भी अभिवृद्धि हुई।
शिक्षाशस्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- शैक्षिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र | scope of educational economics
- शिक्षा के अर्थशास्त्र के शिक्षण के उद्देश्य | Objectives of teaching economics of education in Hindi
- शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना | भारत के अर्थशास्त्र की संकल्पना | Concept of semiology of education in Hindi
- शिक्षा के अर्थशास्त्र का क्षेत्र | विकासशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में शिक्षा के अर्थशास्त्र की भूमिका
- भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति | Nature of Indian economy in hindi
- अर्थव्यवस्था के प्रकार | Type of economy in hindi
- शिक्षा का निवेश तथा उपयोग के रूप में वर्णन | Description of education as investment and use in Hindi
- शिक्षा में उपभोग की रणनीतियों का उल्लेख कीजिए | Mention consumption strategies in education in Hindi
- शैक्षिक आय से आप क्या समझते हैं? | शैक्षिक आय के स्त्रोतो का विश्लेषण | शिक्षा के नये स्रोत
- शिक्षा की आय के निजी स्त्रोत | शिक्षा के शैक्षिक व्यय | शिक्षा के प्रत्यक्ष व्यय
- भारत में शैक्षिक वित्त की समस्याएँ | भारत में शैक्षिक वित्त का समाधान
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 | National Education Policy 1986 in Hindi
- शिक्षा जगत में वित्त की समस्या को हल करने के उपाय | Measures to solve the problem of finance in the education world in Hindi
- भारतीय करारोपण के सुधार के बारे में सुझाव | निवेश पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है।
- भारतीय करारोपण के सुधार के बारे में शिक्षा के विभिन्न प्रतिफलों को स्पष्ट कीजिए
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]