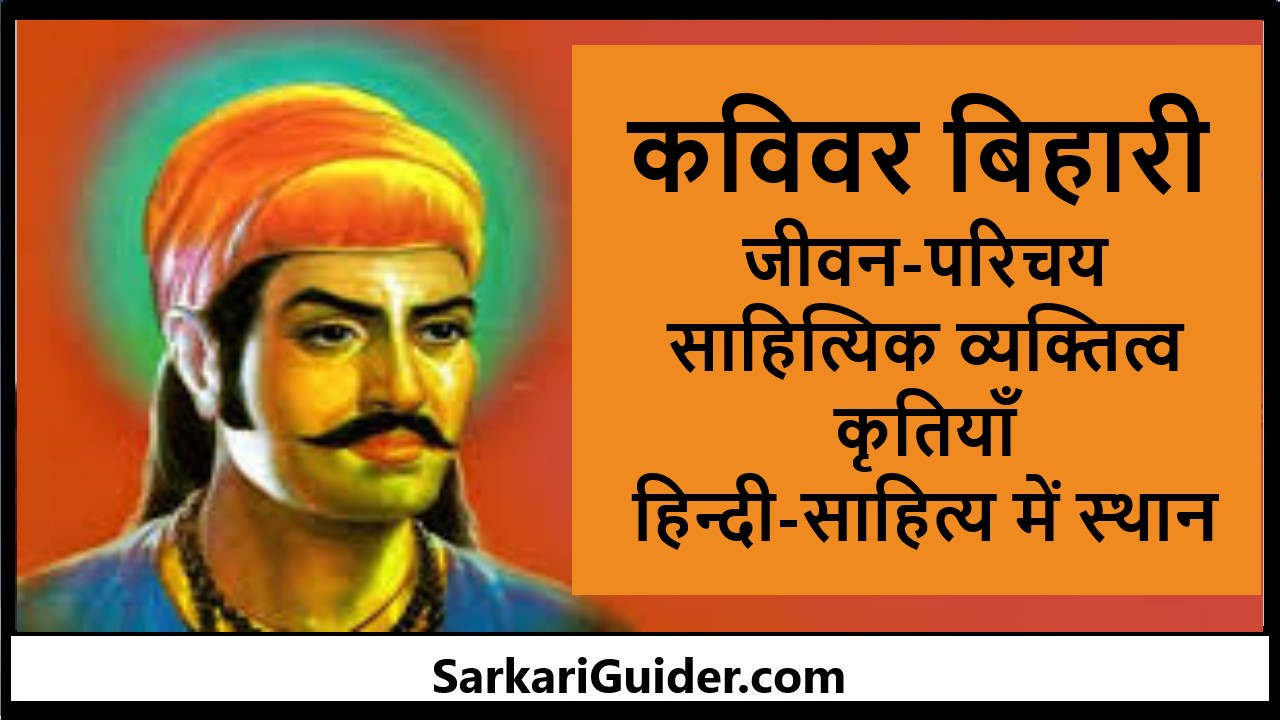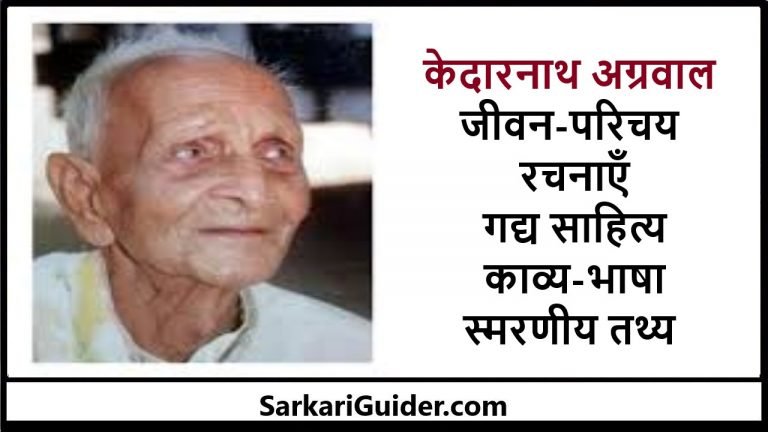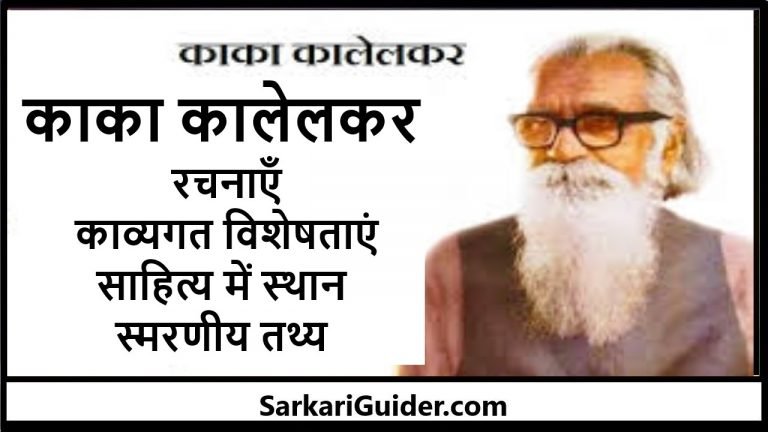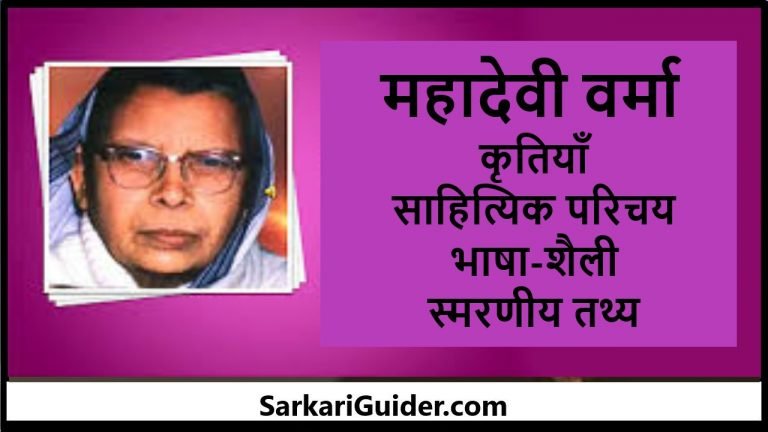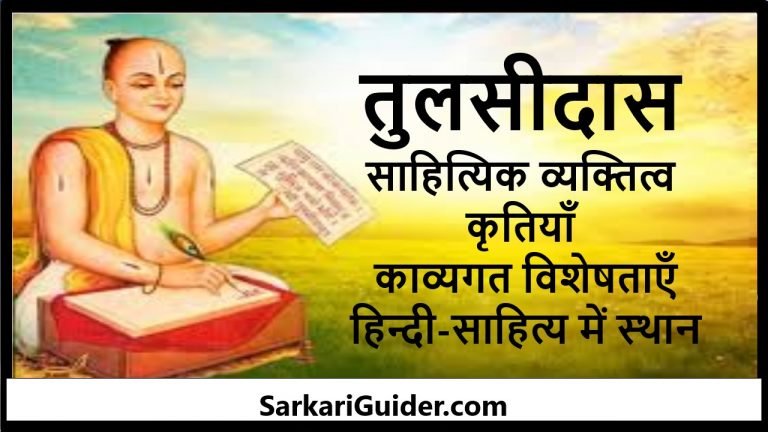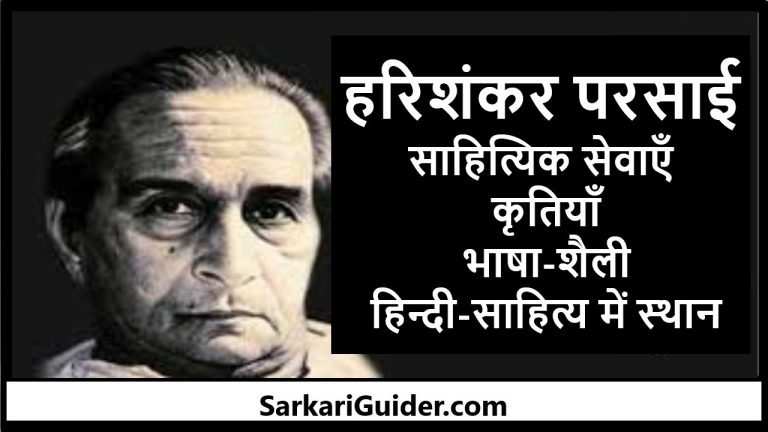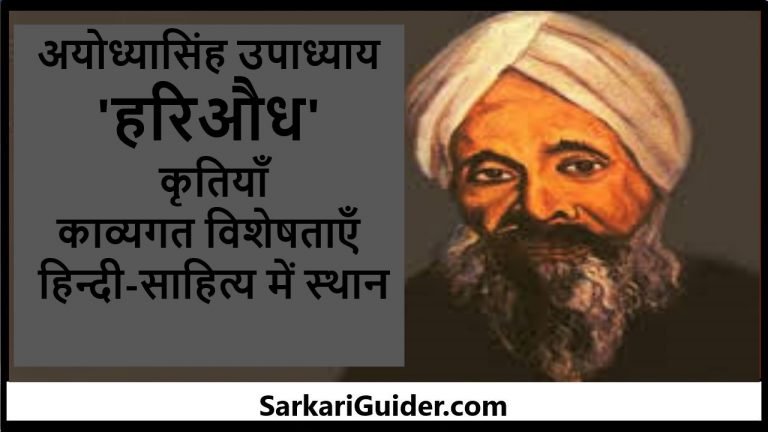कविवर बिहारी

कविवर बिहारी
इस पोस्ट की PDF को नीचे दिये लिंक्स से download किया जा सकता है।
जीवन-परिचय
हिन्दी-साहित्य के जाज्वल्यमान् नक्षत्र, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी का जन्म संवत 1660 (सन् 1603 ई० ) के लगभग ग्वालियर राज्य के बसुआ-गोविन्दुपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशवराय था इनकी बाल्यावस्था बुन्देलखण्ड में और तरुणावस्था अपनी ससुराल (मथुरा) में बीती थी-
जन्म ग्वालियर जानिए, खण्ड बुँदेले बाल।
तरुनाई आई सुघर, मथुरा बसि ससुराल॥
कविवर बिहारी जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह के दूरबारी कवि थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह ने दूसरा विवाह किया था। वे अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ भोग-विलास में लिप्त थे और राज-काज का पूर्णतः त्याग कर चुके थे। महाराजा जयसिंह की यह दशा देखकर बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भेजा-
नहिं परागु नहिं मधुर मधु, नहिं विकासु इहिं काल।
अली कली ही सौं बँध्यो, आगै कौन हवाल।।
इस दोह को पढ़कर राजा जयसिंह बहुत प्रभावित हुए और पुन: करत्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए।
अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी भक्ति और वैराग्य की ओर उन्मुख हो गए और दरबार छोड़कर वृन्दावन चले गए। वहीं संवत् 1720 (सन् 1668 ई० ) में उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर टिया।
साहित्यिक व्यक्तित्व
रीतिकालीन कवियों में महाकवि बिहारी की गणना अपने काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में की जाती है। बिहारी ने सात सौ से अधिक दोहों की रचना की है। इनके दोहे विभिन्न विषय एवं भावों से युक्त हैं। इन्होंने एक-एक दोहे में विभिन्न गहन भावों को भरकर अलंकार, नायिका-भेद, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि रस एवं अलंकार सम्बन्धी जो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की है, वह अद्भुत है। इससे भी विलक्षण एवं अद्भुत यह है कि शास्त्रीय नियमों का पूर्ण पालन करते हुए भी इनके दोहों की भावानुभूति सम्बन्धी तीव्रता अत्यन्त सशक्त है।
कविवर बिहारी के श्रृंगार सम्बन्धी दोहे अपनी सफल भावाबिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इसमें संयोग एवं वियोग श्रृंगारं के मर्मस्पर्शी चित्र मिलते हैं। इनमें आलम्बन के विशद वर्णन के साथ-साथ उद्दीपन के भी चित्र हैं। शृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने नीति, भक्ति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेंद तथा इतिहास आदि विषयों पर भी दोहों की रचना की है, जो श्रृंगार के दोहों की भाँति ही सशक्त भावाभिव्यक्ति से पूर्ण हैं। बिहारी के दोहों का अध्ययन करने के पश्चात् पाठक इनकी बहुमुखी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहते।
कविवर बिहारी की काव्य-प्रतिभा इनके परवर्ती कवियों का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट करती रही। अनेक प्रसिद्ध महाकवियों ने भी इनकी काव्यात्मक प्रतिभा पर टीका लिखने में गर्व का अनुभव किया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनके दोहों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ‘”इनके दोहे क्या हैं? रस की छोटी पिचकारियाँ हैं, जो मुँह से छूटते ही श्रोता को सिक्त कर देती हैं।”
संक्षेप में कविवर बिहारी का काव्य उनकी काव्यात्मक प्रतिभा के ऐसे विलक्षण एवं अद्भुत स्वरूप को प्रस्तुत करता है, जो हिन्दी काव्य-जगत् के विख्यात कवियों के लिए भी विस्मयपूर्ण रहा है।
कृतियाँ
कविवर बिहारी की मात्र एक कृति बिहारी सतसई’ उपलब्ध है । यह बिहारी रचित सात सौ दोहों का संकलन है। इस कृति ने ही बिहारी को हिन्दी -काव्य-साहित्य में अमर कर दिया है।
काव्यगात विशेषताएँ
कविवर बिहारी का काव्य निम्नांकित विशेषताओं से ओत-प्रोत है-
(अ) भावपक्षीय विशेषताएँ
(1) गागर में सागर- विहारी गागर में सारार भरने के लिए विख्यात हैं। गागर में सागर का अभिप्राय है कि कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक बात कह दी जाए। वास्तव में बिहारी ने ‘दोहा’ जैसे छोटे छन्द में एक साथ विविध भाव भर दिए हैं; यथा-
दृग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर- चित प्रीति।
परति गाँठि दुरजन हिए, दई नई यह रीति।।
(2) भक्ति एवं नीतिप्रथान रचनाएँ- श्रिंगरिक कवि होने पर भी बिहारी ने भक्ति और नीति सम्बन्धी अनेक दोही की रचना की है। इन्होंने राधा एवं श्रीकृष्ण की स्तुति पर आधारित अनेक दोहे प्रस्तुत किए हैं। श्रीकृष्ण के प्रति इन्होंने सख्य, दास्य और दैन्य आदि विविध भाव व्यक्त किए हैं श्रीकृष्ण को दिए गए उलाहने और उनके प्रति किए गए व्यंग्य में उनका कौशल दर्शनीय है-
कब की टेरतु दीन है, होत न स्याम सहाइ।
तुमहँ लागि जगतगुरू, जगनाइक जग-बाइ।।
कविवर बिहारी ने बाह्याडम्बरों, जप, छापा, तिलक आदि का कबीर के समान ही विरोध किया है और श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन होने का सन्देश दिया है। नीति सम्बन्धी दोहों में भी बिहारी की सूक्ष्म दृष्टि द्रष्टव्य है।
(3) शृंगार-वर्णन- बिहारी श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि हैं। इन्होंने कहीं राधा-कृष्ण के सीन्दर्य का चित्रण किया है तो कहीं नायक-नायिका के मिलन सम्बन्धी प्रसंगों, नायिका के अंगों, विविध मुद्राओं और विविध हाव भावों का अनुपम ढंग से चित्रण किया है। नख-शिख-वर्णन की परम्परा का पालन करते हुए बिहारी ने ऐसे रसपूर्ण दोहे लिखे हैं, जो इन्हें श्रेष्ठ शृगारी कवि सिद्ध करते हैं; यथा-
कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात।
भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सौ बात।।
बिहारी ने विप्रलम्भ श्रृंगार के भी अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। ऐसे प्रसंगों में प्रायः अतिशयोक्ति का सहारा लिया गया है। नथिका की विरहपूर्ण स्थिति का एक चित्र प्रस्तुत है, जिसमें नायिका को शीतल चन्द्रमा भी कष्ट दे रहा है-
ही ही बौनी बिरह-बस, कै बौरौ सब गाउँ।
कहा जानि ए कहत हैं, ससिहिं सीतकर नाउँ।
(4) प्रकृति-चित्रण– शृंगार-वर्णन में विहारी ने प्रकृति के विविध मनोहारी चित्र अंकित किए हैं। इन्होंने स्वन्त्र रूप से भी प्रकृति का वर्णन किया है मुख्यतः इन्होंने प्रकृति का आलम्बन, उद्दीपन, आलकारिक और ठन्देशात्मक रूप में बर्णत किया है। ऐसे बर्णनों में सरसता सर्वत्र विद्यमान है; यथा-
चुवतु स्वद मकरन्द कन, तरु तरु तर बिरमाइ।
आवतु दच्छिन देस तैं, थक्यौ बटोही बाइ॥
(5) नायिका-मेट निस्रपण– बिहारी ने अपने काव्य में अनेक प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है; जैसे-मुधा प्रीढा, कनिष्ठा, नवोढ़ा, स्वकीया, परकीया, स्वाधीनपतिका तथा अभिसारिका आदि।
(6) कल्पना की समाहार शक्ति– विहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति विद्यमान है। दोहे जैसे छोटे छन्द में अधिक भावी को गूंयने के लिए इस गुण का होना आवश्यक है । संयोग-वियोग के प्रसंगों में बिहारी ने इस गुण का प्रयोग किया है। नाविका की चेतना और विनोदप्रियता में यह मुण देखिए-
बतरस-लालच लाल की, मुरली धरी लुकाइ।
साह करै भौहनु हँसै, दैन कहै नटि जाइ ।।
(7) उक्ति-वैचित्र्य- बिहारी की ठक्तियों में वैचित्र्य है। इनके दोहों में सरलता, अनुपम आकर्षण एवं चमत्कार उत्पन्न करने की विलक्षण शक्त है। ऐसे स्थलों पर अर्थगाम्भीर्य भी दृष्टिगत होता है; यथा-
मेरी भव बाया हरी, राधा नागरि सोया
जा तन की झाँई परे, स्यामु हरित दुति होय॥
(৪) सूक्तियों का प्रयोग- विहारी ने नीति सम्बन्धी सूक्तियों का प्रयोग भी अधिक किया है। स्वर्ण का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि घतूरे को तो खाकर लोग पागल हो जाते हैं, परन्तु स्वर्ण को तो पाकर ही पागल हो जाते हैं-
कनक कनक तै सौ गुरनी, माटकता अधिकाय।
इहि खाए बौराय जग, बहि पाए ही बौराया।
(ब) कलापक्षीय विशेषताएँ
(1) भाषा- बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है, जिसमें पूर्वी-हिन्दी, बुन्देलखण्डी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। शब्द-चयन की दृष्टि से बिहारी अद्वितीय हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों की दृष्टि से भी उनका भाषा-प्रयोग अद्वितीय है।
(2) शैली- बिहारी ने मुक्तक काव्य-शैली को स्वीकार किया है, जिसमें समास शैली का अनूठा योगदान है। इसीलिए ‘दोहा’ जैसे छोटे छन्द में उन्होंने अनेक भावों को भर दिया है।
(3) छन्द- बिहारी को ‘दोहा’ छन्द सर्वाधिक प्रिय है। इनका सम्पूर्ण काव्य इसी छन्द में रचा गया है।
(4) अलंकार- अलंकारों के प्रयोग में बिहारी दक्ष थे। इन्होंने छोटे-छोटे दोहों में अनेक अलंकारों को भर दिया है। इनके काव्य में श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। श्लेष और सांगरूपक का एक उदाहरण द्रष्टव्य है-
चिरजीवौ जोरी जुरै, क्यों न सनेह गँभीर।
को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के बीर।॥
हिन्दी-साहित्य में स्थान
रीतिकालीन कवि बिहारी अपने ढंग के अद्वितीय कवि है। तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित होकर उन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया, वह हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि है। सौन्दर्य-प्रेम के चित्रण में, भक्ति एवं नीति के समन्वय में, ज्योतिष-गणित-दर्शन के निरूपण में तथा भाषा के लाक्षणिक एवं मधुर व्यंजक प्रयोग की दृष्टि से बिहारी बेजोड़ हैं। भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से इनका काव्य श्रेष्ठ है।
अस्तु; सुप्रसिद्ध साहित्यकार पं० पद्मसिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य की सराहना करते हुए लिखा है– “बिहारी के दोहों का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में तो समा गई थी. परंतु उसके बाहर निकलते ही वह इतनी असीम और विस्तृत हो गई कि लम्बी-चौड़ी धरती में भी सीमित न रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इन्द्रधनुष हैं, भाषा के मेष हैं। उनमें सौन्दर्य के मादक चित्र अंकित है।”
For Download – Click Here
महत्वपूर्ण लिंक
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- जेट प्रवाह (Jet Streams)
- चट्टानों के प्रकार
- भारतीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएँ (SALIENT FEATURES)
- Indian Citizenship
- अभिभावक शिक्षक संघ (PTA meeting in hindi)
- कम्प्यूटर का इतिहास (History of Computer)
- कम्प्यूटर की पीढ़ियाँ (Generations of Computer)
- कम्प्यूटर्स के प्रकार (Types of Computers )
- अमेरिका की क्रांति
- माया सभ्यता
- हरित क्रान्ति क्या है?
- हरित क्रान्ति की उपलब्धियां एवं विशेषताएं
- हरित क्रांति के दोष अथवा समस्याएं
- द्वितीय हरित क्रांति
- भारत की प्रमुख भाषाएँ और भाषा प्रदेश
- वनों के लाभ (Advantages of Forests)
- श्वेत क्रान्ति (White Revolution)
- ऊर्जा संकट
- प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय के कार्यकाल की घटनाएँ
- INTRODUCTION TO COMMERCIAL ORGANISATIONS
- Parasitic Protozoa and Human Disease
- गतिक संतुलन संकल्पना Dynamic Equilibrium concept
- भूमण्डलीय ऊष्मन( Global Warming)|भूमंडलीय ऊष्मन द्वारा उत्पन्न समस्याएँ|भूमंडलीय ऊष्मन के कारक
- भूमंडलीकरण (वैश्वीकरण)
- मानव अधिवास तंत्र
- इंग्लॅण्ड की क्रांति
- प्राचीन भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषताएँ
- प्रथम अध्याय – प्रस्तावना
- द्वितीय अध्याय – प्रयागराज की भौगोलिक तथा सामाजिक स्थित
- तृतीय अध्याय – प्रयागराज के सांस्कृतिक विकास का कुम्भ मेल से संबंध
- चतुर्थ अध्याय – कुम्भ की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
- पंचम अध्याय – गंगा नदी का पर्यावरणीय प्रवाह और कुम्भ मेले के बीच का सम्बंध
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है | हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है| यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- sarkariguider@gmail.com