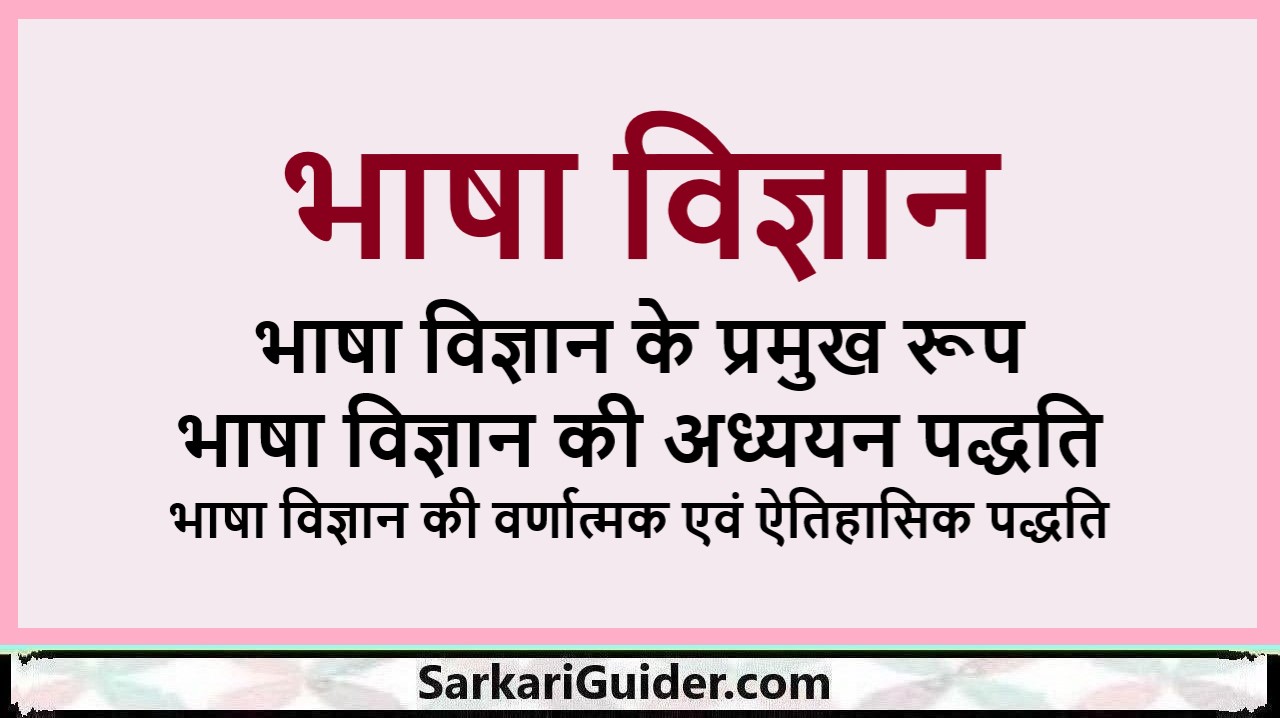भाषा विज्ञान | भाषा विज्ञान के प्रमुख रूप | भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धति | भाषा विज्ञान की वर्णात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति

भाषा विज्ञान | भाषा विज्ञान के प्रमुख रूप | भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धति | भाषा विज्ञान की वर्णात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति
भाषा विज्ञान
भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषां का विस्तृत अध्ययन किया जाता है यह अध्ययन कई दृष्टियों से होता है इसी आधार पर भाषा विज्ञान की अलग-अलग शाखा अथवा रूप निर्धारित किये गये हैं, इन्हें ही इस विज्ञान के अध्ययन की दिशायें भी कहा जाता है, इन तीन रूपों के नाम हैं-
(1) वर्णनात्मक अथवा विवरणात्मक (Descriptive linguistics)
(2) तुलनात्मक भाषा विज्ञान (Comparative linguistics)
(3) ऐतिहासिक भाषा विज्ञान (Historical linguistics)
कुछ लोग चौथे रूप की भी कल्पना करते हैं जिसे वे प्रायोगिक भाषा विज्ञान कहते है। इस का ही पर्याप्त प्रचार है वहाँ हम पाठ्यक्रम में निर्धारित तीनों रूपों का ही वर्णन करेंगे।
- वर्णानात्मक भाषा विज्ञान – इसमें किसी एक भाषा का, किसी काल में ध्वनि, रूप, शब्द, अर्थ, वाक्य रचना का आधार पर अध्ययन किया जाता है। आज का भाषा विज्ञान जिसे वर्णनात्मक भाषा विज्ञान कहते हैं, वास्तव में विश्लेषणात्मक है। इसलिए इसे विश्लेषणात्मक भाषा विज्ञान भी कह सकते हैं। इसमें ध्वनि, रूप, वाक्य, रचना आदि का वर्णन या विवरण होने के साथ सरंचना के उपकरणों का पूरा विश्लेषण भी होता है।
- तुलनात्मक भाषा विज्ञान- जिसमें दो या दो से अधिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है उसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहते हैं। इस रूप का इस में विशेष महत्व है, क्योंकि वस्तुतः तुलनात्मक अध्ययन ने ही भाषा विज्ञान को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए जब प्रारम्भ में पश्चिम के मनौवैज्ञानिकों ने विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में निकटता स्थापित की तो उसका प्रमुख साधन तुलनात्मक अध्ययन ही था। जैसे संस्कृत के पितृ को लेकर उसके अन्य भाषाओं के इसी अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ तुलनात्मक अध्ययन को लिया जा सकता है-
|
संस्कृत |
लैटिन |
ग्रीक |
फारसी |
प्राचीन अंग्रेजी |
आधुनिक अंग्रेजी |
|
पितृ |
Platre |
Pate |
पिदर |
Facter |
Father |
- ऐतिहासिक भाषा विज्ञान- किसी एक भाषा के विभिन्न कालो के विवरण जब मिला दिये जाते हैं तब उसे ऐतिहासिक अध्ययन कहते हैं। इस प्रकार इसमें किसी भाषा के इतिहास का अध्ययन किया जाता है तथा सिद्धान्त की दृष्टि से उस समय के परिवर्तन सम्बन्धी सिद्धान्तों, नियमों तथा कारणों आदि का निर्धारण होता है।
जहां वर्णनात्मक इस में किसी भाषा का सीमित अध्ययन होता है वहीं ऐतिहासिक इस में गतिशीलता होती है क्योंकि इसमें किसी भाषा का विकासात्मक अध्ययन होता है। उदाहरण के लिए यदि हम हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले काम हाथ शब्दों के विकास को जानना चाहें तो प्राकृत आदि में होते हुए संस्कृत भाषा के इसी अध्ययन के सहारे इस प्रकार पहुंच सकते हैं-
|
काम हिन्दी |
> कुम्भ (प्राकृत) |
> कर्म (संस्कृत) |
|
हाथ हिन्दी |
>हत्थ (प्राकृत) |
> हस्त (संस्कृत) |
इस प्रकार हिन्दी के अनेक शब्दों का उद्भव एवं विकास जानने के लिए हमें संस्कृतप्राकृत प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के रूपों का अध्ययन करना पड़ेगा। यह अध्ययन ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार इस का विशेष महत्व है।
भाषा विज्ञान – महत्वपूर्ण लिंक
- भाषा की परिभाषा | भाषा के मूल तत्व या विशेषताएँ | भाषा के अभिलक्षण | भाषा की सरंचना
- घनानन्द के पद्यांशों की व्याख्या | घनानन्द के निम्नलिखित पद्यांशों की संसदर्भ व्याख्या
- विद्यापति सौन्दर्य एवं प्रेम के कवि हैं | विद्यापति मुख्यतः यौवन और शृंगार के कवि हैं | विद्यापति मूलतः शृंगार के कवि हैं | विद्यापति के श्रृंगार चित्रण की विशेषताएँ | विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के कवि है
- विद्यापति के काव्य का भावपक्ष एवं कलापक्ष | विद्यापति के संयोग श्रृंगार की विशेषताएँ | विद्यापति की काव्य भाषा
- विद्यापति के गति काव्य की विवेचना | विद्यापति के तीन प्रमुख तत्व | गीत काव्य परम्परा में विद्यापति की कविता | गीत काव्य परम्परा में विद्यापति की काव्य का महत्व
- विद्यापति के काव्य में श्रृंगार का संयोग पक्ष | विद्यापति के काव्य में श्रृंगार का वियोग-पक्ष
- बहिर्जगत् के चित्रण की विशेषताएं | विद्यापति ने बहिर्जगत् के चित्रण की विशेषताएं
- विद्यापति के अलंकार तथा प्रतीक योजना | ‘पदावली’ के आधार पर विद्यापति के अलंकार योजना | ‘पदावली’ के आधार पर विद्यापति के प्रतीक योजना
- तुलसीदास की भक्ति भावना | तुलसीदास की भक्ति पद्धति के स्वरूप का वर्णन | रामभक्त कवि के रूप में तुलसीदास की भक्ति का मूल्यांकन
- तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएँ | तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं पर आलोचनात्मक निबन्ध
- तुलसीदास के रामचरित मानस का महत्व | राम काव्य परम्परा के अन्तर्गत रामचरित मानस का महत्व
- तुलसीदास की भाषा | तुलसीदास की शैलीगत विशषताएँ | तुलसी के काव्य की छन्द विधान की विशषताएँ
- तुलसी के काव्य में वर्णित लोक आदर्श | तुलसी के काव्य में वर्णित सामाजिक आदर्श
- पद्मावत् के नागमती का विरह वर्णन | नागमती का विरह संपूर्ण भक्ति कालीन कविता में अद्वितीय है
- जायसी के रहस्यवाद की विशेषताएँ | जायसी के रहस्यावाद की समीक्षात्मक विवेचना
- जायसी के पद्मावत में समाज की मनोदशा | पद्मावत की प्रेम-पद्धति
- मीरा की काव्य में प्रकृति | मीरा की काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग | मीरा की काव्य में अनुस्वार युक्त दीर्घ स्वरों का प्रयोग | मीरा के काव्य में मुहावरों का प्रयोग
- गीति काव्य का स्वरूप | गीति काव्य की विशेषताएँ | गीतिकाव्य परम्परा में मीरा के स्थान का निरूपण | मीरा के गीति काव्य परम्परा की विशेषताएँ
- आदिलकाल के विभिन्न नाम | आदिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न मत | आदिकाल के नामकरण की समस्या
- हिन्दी साहित्य के काल विभाजन की समस्या | काल विभाजन के सन्दर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए विभिन्न मत
- साहित्य के इतिहास संबंधी कुछ समस्याएँ | हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएँ
- आदि कालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ | आदिकाल के प्रमुख रासो काव्य | रासो काव्य परंपरा का सामान्य परिचय
- आदिकालीन धार्मिक साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ | सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य एवं जैन साहित्य की प्रवृत्तियाँ
- सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएँ | सगुणोपासक कवियों की समान्य प्रवृत्तियाँ
- भक्तिकाली के विभिन्न काव्यधाराओं का नाम | ज्ञानमार्गी संत काव्य की मूल प्रवृत्तियाँ | निर्गुण संत काव्य के सामाजिक चेतना का मूल्यांकन
- निर्गुण भक्ति काव्यधारा | निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ | निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएँ
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- [email protected]