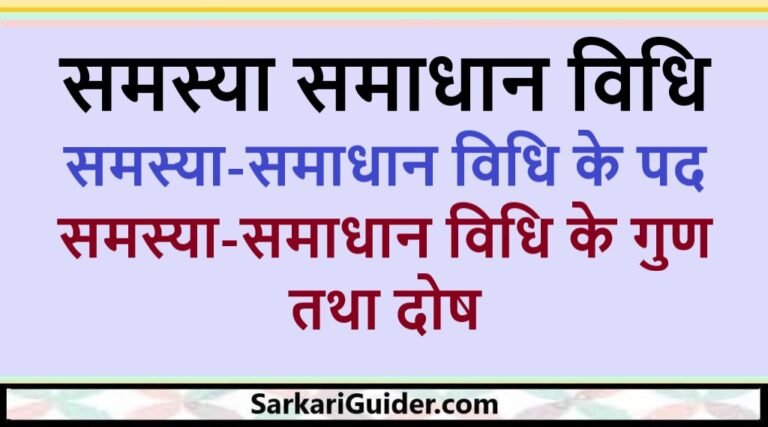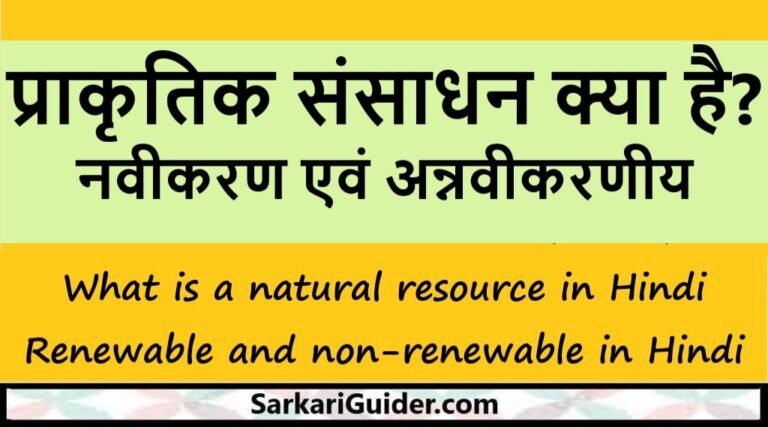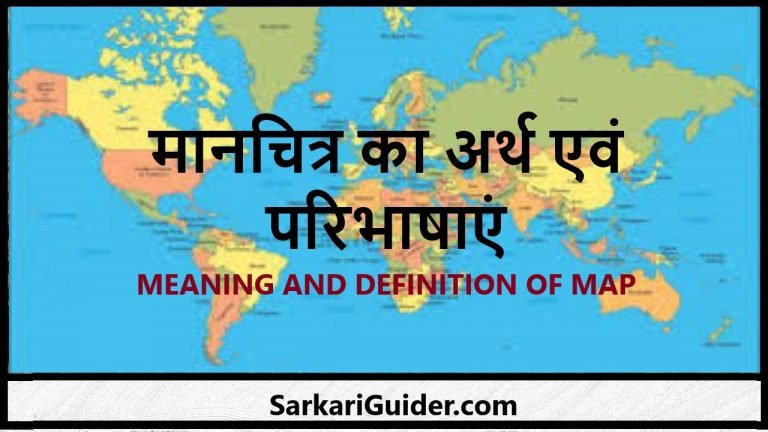पर्यावरण प्रदूषण- परिभाषाएँ, प्रदूषक, प्रदूषकों का वर्गीकरण, प्रदूषण के प्रकार, निष्कर्ष

पर्यावरण प्रदूषण- परिभाषाएँ, प्रदूषक, प्रदूषकों का वर्गीकरण, प्रदूषण के प्रकार, निष्कर्ष
संरचना
- 1 परिचय (पर्यावरण प्रदूषण)
- 1.2 पर्यावरण प्रदूषण: परिभाषाएँ
- 1.3 प्रदूषक
- 1.3.1 प्रदूषकों का वर्गीकरण
- 1.4 प्रदूषण के प्रकार
- 1.4.1 वायु प्रदूषण
- 1.4.2 जल प्रदूषण
- 1.4.3 भूमि प्रदूषण
- 1.4.4 शोर प्रदूषण
- 1.4.5 विकिरण प्रदूषण
- 1.4.6 थर्मल प्रदूषण
- 1.5 निष्कर्ष
-
परिचय
पर्यावरण प्रदूषण हमारे ग्रह के लिए मुख्य खतरों में से एक है। पर्यावरण प्रदूषण जल, भूमि, या वायु में किसी भी पदार्थ या ऊर्जा का निर्वहन होता है जो पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन के लिए तीव्र (अल्पकालिक) या दीर्घकालिक (दीर्घकालिक) अवरोध पैदा करता है या जो जीवन की गुणवत्ता को कम करता है। सरल शब्दों में, पर्यावरण प्रदूषण एक तरह से पर्यावरण को दूषित करने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग करना असुरक्षित हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण हमारे आसपास के अवांछनीय परिवर्तनों का प्रभाव है जो पौधों, जानवरों और मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। एक पदार्थ, जो प्रदूषण का कारण बनता है, प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। प्रदूषक ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ हो सकते हैं जो प्राकृतिक बहुतायत से अधिक सांद्रता में मौजूद होते हैं और मानव गतिविधियों के कारण या प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रदूषक प्राथमिक नुकसान का कारण बन सकते हैं, पर्यावरण पर प्रत्यक्ष पहचान योग्य प्रभाव के साथ, या जैविक खाद्य वेब के नाजुक संतुलन में मामूली गड़बड़ी के रूप में द्वितीयक क्षति जो केवल लंबे समय तक पता लगाने योग्य हैं। हमारे समाज का औद्योगिकीकरण, मोटर चालित वाहनों की शुरुआत, तेजी से शहरीकरण, मानव आबादी का विस्फोट, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ-साथ उद्योगों और शहरों से अनियोजित सीवेज और कचरे का निपटान अपशिष्ट अपशिष्टों में जबरदस्त वृद्धि का कारण रहा है। इस प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण आमतौर पर ऊर्जा रूपांतरण और संसाधनों के उपयोग के परिणामस्वरूप होता है जो पानी, मिट्टी या हवा में अपने उप-उत्पादों को पीछे छोड़ देता है। विश्व स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी है।
पर्यावरण प्रदूषण दुनिया के कई हिस्सों में हो रहा है, खासकर वायु और जल प्रदूषण के रूप में। वायु प्रदूषण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण राजधानी बीजिंग सहित चीन के कुछ शहर हैं, और जल प्रदूषण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण भारत अपनी गंगा नदी प्रदूषण समस्या के साथ है। लेकिन सबसे गंभीर पर्यावरण प्रदूषण तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में हो रहा है क्योंकि न केवल उनके पास स्थायी प्रबंधन के किसी भी रूप की कमी है, बल्कि उनके पास बुनियादी स्वच्छता की भी कमी है। वायु और जल प्रदूषण मानव सहित पारिस्थितिकी तंत्र में कई जीवों की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में मानव आबादी के स्वास्थ्य को प्रभावित करने की बड़ी क्षमता है (फेरीदून एट अल, 2007; प्रगतिशील बीमा, 2005)। पिछले तीन दशकों में पर्यावरण प्रदूषण (किमनी, 2007) के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों पर वैश्विक चिंता बढ़ रही है, माना जाता है कि मानव अस्तित्व में किसी भी अन्य समय की तुलना में प्रदूषण का मानव जोखिम अब अधिक तीव्र है (स्कैल एट अल, 2006)। एनजीओ प्योर अर्थ की रिपोर्ट बताती है कि सात में से एक मौत प्रदूषण के कारण होती है। एक अन्य तुलना से पता चलता है कि प्रदूषण मलेरिया, एचआईवी / एड्स और तपेदिक के मुकाबले 60% अधिक लोगों को मारता है।
-
पर्यावरण प्रदूषण: परिभाषाएँ
भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में एक अवांछनीय परिवर्तन है
पर्यावरण विशेष रूप से हवा, पानी और भूमि जो मानव आबादी और वन्य जीवन, औद्योगिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक संपत्ति (भवन और स्मारक) को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण शब्द लैटिन शब्द पॉल्यूशनियम ’से लिया गया है, जिसका अर्थ है गंदे करना या गंदा करना। प्रदूषण शब्द को विभिन्न वैज्ञानिकों और संगठनों द्वारा विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है।
“पर्यावरण प्रदूषण को हमारे परिवेश के प्रतिकूल परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है जो कि पूरी तरह से या बड़े पैमाने पर ऊर्जा के पैटर्न, विकिरण स्तर, रासायनिक और भौतिक काल संविधान और जीवों की बहुतायत में परिवर्तन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावों के माध्यम से मनुष्य की कार्रवाई के अनुत्पादक के रूप में हो सकता है” (अमेरिकी राष्ट्रपति का) विज्ञान सलाहकार समिति, 1966)। प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है.
“पानी, हवा और मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में एक अवांछनीय परिवर्तन जो मानव, पशु और पौधों के जीवन, औद्योगिक प्रगति, रहने की स्थिति और सांस्कृतिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है” (नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, यूएसए , 1966)।
“प्रदूषण हवा, पानी और मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में एक अवांछनीय परिवर्तन है जो जीवन को हानिकारक रूप से प्रभावित कर सकता है या जीवित जीवों के लिए एक संभावित स्वास्थ्य खतरा पैदा कर सकता है” (ओडुम, 1971)।
“प्रदूषण पर्यावरण में पदार्थों के संचय या प्रवाह की दर से होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को या तो बेअसर कर देता है या उन्हें हानिकारक स्तरों तक पहुँचाता है” (टियासमैन, 1975)।
“प्रदूषण को मानवीय गतिविधियों के अपशिष्ट उत्पादों के रूप में पदार्थों और ऊर्जा की रिहाई के रूप में देखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक वातावरण में हानिकारक परिवर्तन होते हैं” (राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान परिषद, 1976)।
इस प्रकार, प्रदूषण पर्यावरण के किसी भी घटक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन है जो जीवित जीवों के लिए हानिकारक है और विशेष रूप से मनुष्य के लिए अवांछनीय है।
-
प्रदूषक
वातावरण में मौजूद कोई भी पदार्थ ऐसी सांद्रता में होता है जो किसी प्रजाति की विकास दर को नुकसान पहुंचाकर और खाद्य श्रृंखलाओं में हस्तक्षेप करके पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, और स्वास्थ्य, आराम और संपत्ति आदि को प्रभावित करता है, इसे प्रदूषक माना जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रदूषक को “गलत स्थान पर या गलत समय पर गलत मात्रा में घटक” के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार, “एक प्रदूषक को किसी भी ठोस, तरल या के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तरह की सांद्रता में मौजूद गैसीय पदार्थ पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं या हो सकते हैं ”। उद्योगों और ऑटोमोबाइल से धुआं, घरेलू और वाणिज्यिक सीवेज, परमाणु संयंत्रों से रेडियोधर्मी पदार्थ और घरेलू सामान (तिन बोतलें, टूटी क्रॉकरी आदि) को प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं।
-
प्रदूषकों का वर्गीकरण
प्रदूषकों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है।
(ए) प्रकृति में उनके अस्तित्व के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, अर्थात्:
(i) मात्रात्मक और
(ii) गुणात्मक प्रदूषक।
(i) मात्रात्मक प्रदूषक: ये वे पदार्थ हैं जो सामान्य रूप से पर्यावरण में पाए जाते हैं, जो एक प्रदूषक की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जब मनुष्य की अदम्य गतिविधियों के कारण उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, यदि एन्थ्रोपोजेनिक गतिविधियों के कारण सामान्य से अधिक एकाग्रता में वायुमंडल में मौजूद है, तो इसे मात्रात्मक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
(ii) गुणात्मक प्रदूषक: ये वे पदार्थ हैं जो सामान्य रूप से प्रकृति में नहीं होते हैं, लेकिन कीटनाशक जैसे मनुष्य द्वारा जोड़े जाते हैं। पर्यावरण में जारी होने के बाद वे जिस रूप में बने रहते हैं, उसके आधार पर, प्रदूषकों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात् (ए) प्राथमिक और (बी) द्वितीयक प्रदूषक।
(ए) प्राथमिक प्रदूषक: ये वे होते हैं जो सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं और उस रूप में बने रहते हैं जिसमें उन्हें पर्यावरण में जोड़ा गया था। जैसे राख, धुआँ, धुएँ, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि।
(b) द्वितीयक प्रदूषक: ये वे हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों से वातावरण में मौजूद किसी घटक के साथ रासायनिक क्रिया द्वारा बनते हैं। उदाहरण हैं: सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड, केटोन्स, ओज़ोन आदि। प्राथमिक प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सूरज की उपस्थिति में पेरोक्सीसाइल नाइट्रेट (पैन) और ओज़ोन, दो द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं।
(बी) पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में अर्थात उनके प्राकृतिक निपटान के अनुसार, प्रदूषकों को दो मूल समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
(i) जैव-अपघट्य प्रदूषक: ये ऐसे प्रदूषक हैं जो जैविक / माइक्रोबियल क्रिया द्वारा प्राकृतिक तरीकों से या तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं या कुछ इंजीनियर सिस्टम (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) द्वारा। अवक्षेपित प्रदूषकों को आगे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
(a) तेजी से क्षीण या निरंतर प्रदूषक: इन प्रदूषकों का क्षरण बहुत तेज प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जानवरों और पौधों के मल और कचरे का अपघटन एक तेज प्रक्रिया है।
(b) धीरे-धीरे सड़ने योग्य या लगातार प्रदूषक: इन प्रदूषकों का क्षरण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। ऐसा लगता है जैसे प्रदूषक की मात्रा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। उदाहरण के लिए, सिंथेटिक यौगिकों का क्षरण और रेडियो-सक्रिय तत्व जैसे आयोडीन 137, प्लूटोनियम 239 में अधिक समय लगता है।
(ii) गैर-अपघट्य प्रदूषक: ये ऐसे पदार्थ हैं जो या तो प्राकृतिक वातावरण में बहुत धीरे-धीरे नहीं गिरते या ख़राब होते हैं। इनमें पारा लवण, लंबी श्रृंखला फेनोलिक रसायन, डीडीटी और एल्युमीनियम के डिब्बे आदि शामिल हैं। इनमें से अधिकांश म्यूटेंट वातावरण में जमा हो जाते हैं और जैविक रूप से आवर्धित भी हो जाते हैं क्योंकि ये खाद्य अवस्थाओं के तहत एक चालित अवस्था में होते हैं। ये विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करने के लिए पर्यावरण में अन्य यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इन्हें और दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:
(a) अपशिष्ट: उदा। ग्लास, प्लास्टिक, फेनोलिक, एल्यूमीनियम के डिब्बे आदि
(b) ज़हर: उदा। रेडियो-सक्रिय पदार्थ, कीटनाशक, स्मॉग गैसें, भारी धातुएँ।
1.4 प्रदूषण के प्रकार
प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के उपहार के रूप में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं, अत्यधिक प्रदूषित हैं।
प्रभावित क्षेत्र या पर्यावरण के हिस्से के आधार पर, प्रदूषण को मोटे तौर पर निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:
- वायु प्रदूषण
- जल प्रदूषण
- भूमि प्रदूषण
- ध्वनि प्रदूषण
- विकिरण प्रदूषण
- थर्मल प्रदूषण
1.4.1. वायु प्रदूषण
वायु प्रदूषण वर्तमान मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वायु प्रदूषण का मतलब है हवा में किसी भी असामान्य सामग्री या संपत्ति की उपस्थिति जो वायु संसाधनों की उपयोगिता को कम करती है। प्रदूषण शब्द को बाहरी खुली वायुमंडलीय स्थितियों, स्थानीय वायु स्थिति और संलग्न अंतरिक्ष स्थितियों के संदर्भ में संदर्भित किया जा सकता है। वायु प्रदूषण वायु में अवांछनीय ठोस, तरल या गैसीय कणों की मात्रा के कारण होता है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। ज्वालामुखियों जैसे प्राकृतिक कारणों से वायु प्रदूषित हो सकती है, जो राख, धूल, सल्फर और अन्य गैसों को छोड़ देती है, या मानव गतिविधियों द्वारा। हालांकि, मानव गतिविधि के प्रदूषकों के विपरीत, स्वाभाविक रूप से होने वाले प्रदूषक थोड़े समय के लिए वायुमंडल में बने रहते हैं और स्थायी वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं करते हैं।
वायु प्रदूषण के स्रोत
प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में बिजली और गर्मी उत्पादन, ठोस अपशिष्टों का जलना, औद्योगिक प्रक्रियाएँ और विशेष रूप से परिवहन हैं। कोयला, मिट्टी के तेल, जलाऊ लकड़ी, गोबर के केक, सिगरेट से निकलने वाले धुएं आदि के जलने के दौरान निकलने वाली आम प्रदूषक गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), आदि लगभग 90% हैं। वैश्विक वायु प्रदूषण का गठन निम्नलिखित प्रदूषकों द्वारा किया जाता है।
(i) कार्बन डाइऑक्साइड: यह उन प्रमुख गैसों में से एक है जो वायु प्रदूषण में योगदान करती है। यह मुख्य रूप से कारखानों, बिजलीघरों, घरों आदि में ईंधन के दहन के दौरान उत्पन्न होता है
(ii) कार्बन मोनोऑक्साइड: यह कोयला, पेट्रोलियम और लकड़ी के कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। डीजल और पेट्रोलियम का उपयोग करने वाले ऑटोमोबाइल कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रमुख स्रोत हैं।
(iii) सल्फर डाइऑक्साइड: यह वायु प्रदूषण का लगभग 18% हिस्सा है। यह रासायनिक उद्योगों, धातुओं के पिघलने, लुगदी और कागज मिलों, तेल रिफाइनरियों आदि द्वारा उत्पादित किया जाता है।
(iv) नाइट्रोजन के ऑक्साइड: नाइट्रोजन (एनओएक्स) के कुछ ऑक्साइड प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ थर्मल पावर स्टेशन, कारखानों, ऑटोमोबाइल से उत्पन्न होते हैं। और विमान वे वायु प्रदूषण का लगभग 6% हिस्सा हैं।
(v) हाइड्रोकार्बन: हाइड्रोकार्बन यौगिकों का एक समूह होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। वे या तो ईंधन की आपूर्ति से वाष्पित हो जाते हैं या ईंधन के अवशेष होते हैं जो पूरी तरह से नहीं जलते हैं।
(vi) पार्टिकुलेट मैटर: पार्टिकुलेट ठोस पदार्थ के छोटे टुकड़े होते हैं (उदाहरण के लिए, आग से धुएं के कण, एस्बेस्टस के टुकड़े, धूल के कण और उद्योगों से निकलने वाली राख) वायुमंडल में फैल जाते हैं।
वायु प्रदूषण के प्रभाव
(i) मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव: वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर कई प्रभाव जुड़े हैं, जिनमें फुफ्फुसीय, हृदय, संवहनी और तंत्रिका संबंधी दुर्बलताएं शामिल हैं। स्वास्थ्य प्रभाव व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत भिन्न होता है। उच्च जोखिम वाले समूह जैसे कि बुजुर्ग, शिशु, गर्भवती महिलाएं और पुराने दिल और फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित लोग वायु प्रदूषण के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। बच्चों को अधिक जोखिम होता है क्योंकि वे आमतौर पर अधिक सक्रिय होते हैं और उनके फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के संपर्क में तीव्र (अल्पकालिक) और दीर्घकालिक (दीर्घकालिक) स्वास्थ्य प्रभाव दोनों हो सकते हैं।
(ii) पौधों पर प्रभाव: जब कुछ गैसीय प्रदूषक पत्ती छिद्रों में प्रवेश करते हैं तो वे फसल के पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषकों के लिए पत्तियों का पुराना जोखिम मोमी कोटिंग को तोड़ सकता है जो पानी के अत्यधिक नुकसान को रोकने में मदद करता है और बीमारियों, कीटों, सूखे और ठंढ से नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के एक्सपोज़र प्रकाश संश्लेषण और पौधों के विकास में हस्तक्षेप करते हैं, पोषक तत्वों की कमी को कम करते हैं और पत्तियों को पीले, भूरे या पूरी तरह से छोड़ देते हैं।
(iii) सामग्री पर वायु प्रदूषण का प्रभाव: हर साल वायु प्रदूषक अरबों रुपए की सामग्री को नुकसान पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषक कारों और घरों पर बाहरी पेंट को तोड़ते हैं। दुनिया भर के सभी वायु प्रदूषकों ने अपूरणीय स्मारकों, ऐतिहासिक इमारतों, संगमरमर की मूर्तियों आदि को नष्ट कर दिया है,
(iv) जलवायु पर प्रभाव: प्रदूषण से प्रेरित वायुमंडलीय परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं, एक घटना जो कुछ गैसों की एकाग्रता में वृद्धि के कारण होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और सीएफसी। ग्लोबल वार्मिंग के कई प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। एक गर्म पृथ्वी के साथ ध्रुवीय बर्फ की टोपी पिघल जाएगी, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। बांग्लादेश या मालदीव जैसे देशों में यह विनाशकारी होगा। यदि समुद्र का स्तर 3 मीटर बढ़ जाता है, तो मालदीव लहरों के नीचे पूरी तरह से गायब हो जाएगा।
वायु प्रदूषण के लिए नियंत्रण
के उपाय वायु प्रदूषण को दो मूलभूत तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है: निवारक तकनीक और प्रभावी नियंत्रण। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रभावी साधनों में से एक उचित उपकरण होना है। इसमें ग्रिप गैसों से प्रदूषकों को हटाने के लिए उपकरण शामिल हैं, हालांकि स्क्रबर्स, क्लोज्ड कलेक्शन रिकवरी सिस्टम, जिसके द्वारा प्रदूषक को इकट्ठा करना संभव है इससे पहले कि वे बच जाएं, सूखे और गीले कलेक्टरों, फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स, आदि का उपयोग करके अधिक से अधिक ऊंचाई प्रदान करना। ढेर यथासंभव जमीन से दूर प्रदूषकों के निर्वहन को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकते हैं। उद्योगों को स्थानों में स्थित होना चाहिए ताकि स्थलाकृति और हवा की दिशाओं पर विचार करने के बाद प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सके। कच्चे माल का प्रतिस्थापन जो उन लोगों के साथ अधिक प्रदूषण का कारण बनता है जो कम प्रदूषण का कारण बनते हैं।
1.4.2. जल प्रदूषण
जल सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटकों में से एक है जो जीवन को बनाए रखता है। हालाँकि, आजकल पानी अत्यधिक प्रदूषित है और दुनिया में महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। पानी को तब प्रदूषित कहा जाता है जब उसमें “सकारात्मक” गुणों की तुलना में अधिक “नकारात्मक” गुण होते हैं। पानी की गुणवत्ता का तात्पर्य पानी की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं से है। इस प्रकार, सरल शब्दों में, हम कह सकते हैं कि प्रदूषित पानी वह पानी है जिसका किसी तरह से दुरुपयोग किया गया है, ताकि यह अब उपयोग के लायक नहीं है। प्रदूषण को “बहुत अधिक अवांछनीय पदार्थों की उपस्थिति” के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पानी जो पानी की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं की गुणवत्ता को नीचा दिखाता है, जिससे यह लाभकारी उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है ”।
जल प्रदूषण के स्रोत
जल प्रदूषण सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। जल प्रदूषण कई तरह की मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, जैसे कि,
- घरेलू सीवेज को इसके किनारों पर स्थित क्षेत्रों से नदियों में उतारा जाता है।
- जल निकायों में मनुष्यों और जानवरों के उत्सर्जन अपशिष्ट।
- शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का जल निकायों में निपटान।
- औद्योगिक अपशिष्ट तेल, भारी धातुओं और डिटर्जेंट के शहरी क्षेत्रों से अपशिष्टों को नष्ट करते हैं।
- कृषि क्षेत्र से फॉस्फेट और नाइट्रोजन उर्वरकों के साथ खनिज, जैविक अपशिष्ट और फसल की धूल जो झीलों, नदियों और समुद्र तक पहुँचती है (पानी विषाक्त और जहरीला हो जाता है, इस प्रकार, जलीय जीवन का समर्थन नहीं कर सकता है)।
- रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कीटनाशक, शाकनाशी और पौधे। Such औद्योगिक अपशिष्ट जल जिसमें कई रासायनिक प्रदूषक तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, भारी धातु और परमाणु रिएक्टर से रेडियोधर्मी अपशिष्ट।
- जल के प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत मिट्टी का क्षरण, चट्टानों से खनिजों की लीचिंग और कार्बनिक पदार्थों का क्षय है।
जल प्रदूषकों को बिंदु स्रोत प्रदूषण और गैर-बिंदु स्रोत प्रदूषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- बिंदु स्रोत प्रदूषण
जब प्रदूषकों को एक विशिष्ट स्थान से छुट्टी दे दी जाती है, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्टों को सीधे पानी के शरीर में प्रवाहित करने वाले एक नाली पाइप से यह बिंदु स्रोत प्रदूषण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में, बिंदु स्रोत प्रदूषण को प्रदूषण के किसी एकल पहचान योग्य स्रोत के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे प्रदूषकों को छुट्टी दी जाती है।
- गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण
उन स्रोतों में जो प्रदूषकों के निर्वहन के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, जल निकाय में जल प्रदूषण के गैर-बिंदु स्रोतों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, कृषि क्षेत्रों, चराई भूमि, निर्माण स्थलों, परित्यक्त खानों और गड्ढों आदि से भागना।
जल प्रदूषण के प्रभाव
जल प्रदूषण वायु प्रदूषण के बाद जलजनित रोगों और स्वास्थ्य समस्याओं का दूसरा प्रमुख स्रोत है।
(i) मनुष्यों पर प्रभाव
प्रदूषित पानी का सेवन करने पर, मानव अमीबा पेचिश जैसे रोगों से पीड़ित हो सकता है: त्वचा के कैंसर, हैजा, टाइफाइड बुखार, तंत्रिका तंत्र की क्षति, आनुवंशिक परिवर्तन / जन्म दोष, हेपेटाइटिस, मलेरिया। औद्योगिक अपशिष्ट जल में सीसा, जस्ता, आर्सेनिक, तांबा, पारा और कैडमियम जैसी धातुएं मनुष्यों और अन्य जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। आर्सेनिक प्रदूषित पानी के सेवन से त्वचा पर घाव, खुरदरी त्वचा, त्वचा का सूखना और घना होना और अंततः त्वचा का कैंसर हो जाता है। पारे द्वारा जल निकायों के प्रदूषण से मनुष्यों में मीनमाता रोग होता है और मछलियों में गिरावट आती है। सीसा डिस्लेक्सिया का कारण बनता है, कैडमियम विषाक्तता का कारण बनता है – इटाई रोग आदि।
(ii) पौधों और जानवरों पर प्रभाव
जल प्रदूषण के कारण कम फसल की पैदावार होती है, शैवाल की अधिक वृद्धि जलीय जीवन को मार सकती है, प्रकाश संश्लेषण को कम करने, खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को बाधित करता है। निकटवर्ती पानी में तेल रिसाव एक प्रमुख समस्या है और मछली, अन्य जलीय जीवों और पक्षियों और स्तनधारियों को मार या प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। तटवर्ती रेत और चट्टानों में रहने वाले जीवों की आबादी को मार या कम कर सकते हैं, और पक्षियों और अन्य जानवरों के भोजन के रूप में काम करने वाले कीड़े और कीड़े को मार सकते हैं।
जल प्रदूषण को रोकने के लिए नियंत्रण के उपाय
- अपशिष्ट के उपचार के लिए प्रभावी उपचार योजना स्थापित करना।
- औद्योगिक कचरे का निर्वहन से पहले इलाज किया जाना चाहिए।
- जल प्रदूषण और जल प्रदूषण के परिणामों को रोकने के लिए जनता को शिक्षित करना।
- जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का सख्त प्रवर्तन।
- विभिन्न स्थानों पर जल प्रदूषण की निरंतर निगरानी।
- जल उपचार का किफायती तरीका विकसित करना।
1.4.3. भूमि प्रदूषण
भूमि प्रदूषण पृथ्वी की भूमि की सतह के क्षरण के माध्यम से दुरुपयोग है खराब कृषि पद्धतियां, खनिज शोषण, औद्योगिक अपशिष्ट डंपिंग और शहरी और विषाक्त कचरे का अंधाधुंध निपटान। सरल शब्दों में, भूमि प्रदूषण, संसाधनों के दुरुपयोग और कचरे के अनुचित निपटान के कारण पृथ्वी की सतह का क्षरण है। भूमि प्रदूषण पशुओं के प्राकृतिक आवास, वनों की कटाई के नुकसान के लिए जिम्मेदार है और प्राकृतिक संसाधनों को हुई क्षति, और हमारे समुदायों में सामान्य बदबू। हानिकारक रसायनों द्वारा भूमि को प्रदूषित करने से प्रदूषकों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश हो सकता है। यह आमतौर पर कृषि में उर्वरकों के अधिक उपयोग, औद्योगिक अपशिष्टों के गैर-जिम्मेदार डिस्पोजेबल आदि के कारण होता है। यहां तक कि खुले स्थानों में शौच करने से भी प्रदूषण होता है।
भूमि प्रदूषण के स्रोत
भूमि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत नीचे दिए गए हैं:
(i) मृदा अपरदन: मृदा अपरदन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुच्छल गति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मृदा अपरदन वनस्पति क्षय और माइक्रोबियल गिरावट के माध्यम से कई वर्षों में विकसित समृद्ध धरण टोपसोल को हटा देता है और इस प्रकार फसल के विकास के लिए मूल्यवान पोषक तत्वों की भूमि को छीन लेता है। खनिजों और कोयले की परत के लिए खनन से प्रत्येक वर्ष हजारों एकड़ भूमि बर्बाद हो जाती है, जो पृथ्वी को बदनाम करती है और खनन क्षेत्र को व्यापक रूप से क्षरण की समस्याओं के अधीन करती है। जनसंख्या के दबाव के कारण शहरीकरण में वृद्धि अतिरिक्त मिट्टी-क्षरण की समस्याओं को प्रस्तुत करती है; पास की धाराओं में तलछट भार 500 से 1,000 गुना तक बढ़ सकता है।
(ii) औद्योगिक अपशिष्ट: बड़ी संख्या में औद्योगिक रसायन, डाई, एसिड, उर्वरक कंपनियां, दवा कंपनियां आदि मिट्टी में अपना रास्ता तलाशते हैं और कैंसर सहित कई स्वास्थ्य खतरों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं।
(iii) शहरी अपशिष्ट: आधुनिक जीवन शैली और खान-पान की वजह से शहरी अपशिष्ट मानव के लिए बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। शहरी कचरे में वे दोनों शामिल हैं जो लंबे समय में समाज के लिए हानिकारक और हानिकारक सामग्री है।
(iv) कृषि स्रोत: कृषि रसायन विशेष रूप से उर्वरक और कीटनाशक मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इन क्षेत्रों के पानी से निकलने वाले उर्वरक जल निकायों में यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकते हैं। कीटनाशक अत्यधिक जहरीले रसायन होते हैं जो मनुष्यों और अन्य जानवरों को प्रभावित करते हैं जो सांस की समस्याओं, कैंसर और मृत्यु का कारण बनते हैं।
(v) प्लास्टिक की थैलियाँ: कम घनत्व वाली पॉलीथीन से बने प्लास्टिक के थैले, वास्तव में अविनाशी होते हैं, जिससे भूमि प्रदूषण के साथ भारी पर्यावरणीय खतरा पैदा होता है। छोड़े गए बैग नालियों और सीवेज सिस्टम को अवरुद्ध करते हैं।
भूमि प्रदूषण के कारण
- विषाक्त यौगिक पौधे के विकास और मानव जीवन को भी प्रभावित करते हैं।
- जल भराव और लवणता मिट्टी को बांझ बना देती है।
- खतरनाक रसायन जैव रासायनिक प्रक्रिया को परेशान करने वाली मिट्टी से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं।
- नर्वस डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जोड़ों में दर्द, सांस की समस्या इंसान पर दिखने वाले प्रभाव हैं।
मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए नियंत्रण के उपाय
- उचित वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका या नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- उद्योग से सभी अपशिष्ट, घरेलू, उचित उपचार के साथ डंप किया जाना चाहिए।
- सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग से बचना चाहिए बजाय प्राकृतिक उर्वरकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- मृदा प्रदूषण के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करना और मृदा प्रदूषण को रोकना।
- जहरीली और गैर-अपमानजनक सामग्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- औद्योगिक और घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग मिट्टी के प्रदूषण को काफी कम कर सकता है।
1.4.4. ध्वनि प्रदूषण
ध्वनि प्रदूषण की हाल ही में उत्पत्ति हुई है और कम से कम चर्चा की समस्याओं में से एक है। शोर सबसे व्यापक प्रदूषक में से एक है। लोग इस समस्या को कम आंकते हैं क्योंकि इसे सूँघना, देखना या छूना संभव नहीं है। ध्वनि प्रदूषण किसी भी जोर की आवाज़ है जो या तो मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिकारक या कष्टप्रद है। अधिक सटीक होने के लिए, परिभाषा द्वारा शोर “मूल्य के बिना ध्वनि” या “प्राप्तकर्ता द्वारा अवांछित कोई भी शोर” है। अन्य प्रदूषकों की तरह शोर औद्योगीकरण, शहरीकरण और आधुनिक सभ्यता के उत्पाद द्वारा है। डेसीबल (dB) के संदर्भ में शोर का स्तर मापा जाता है। डब्ल्यू.एच.ओएच ने दिन के हिसाब से अधिकतम शोर स्तर 45 डीबी और रात में 35 डीबी निर्धारित किया है। 80 डीबी से ऊपर कुछ भी खतरनाक है।
ध्वनि प्रदूषण के स्रोत
ध्वनि प्रदूषण एक बढ़ती हुई समस्या है। यह मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनियों का एक सम्मिश्रण है सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट जेट की गर्जना के लिए स्टीरियो सिस्टम को नष्ट करने से लेकर गतिविधियाँ। सभी मानवीय गतिविधियाँ ध्वनि प्रदूषण में अलग-अलग सीमा तक योगदान करती हैं। सामान्य वातावरण की तुलना में काम के माहौल में शोर प्रदूषण अधिक तीव्र है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कई हैं और घर के अंदर या बाहर स्थित हो सकते हैं।
(a) इनडोर स्रोतों में रेडियो, टेलीविजन, जनरेटर, बिजली के पंखे, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, एयर कूलर, एयर कंडीशनर और पारिवारिक संघर्ष जैसे घरेलू उपकरणों द्वारा उत्पादित शोर शामिल हैं। आज एक सामान्य घर में औसत पृष्ठभूमि शोर 40 और 50 डेसिबल के बीच है। जनसंख्या और उद्योगों और परिवहन जैसे गतिविधियों की अधिक एकाग्रता के कारण शहरों में शोर प्रदूषण अधिक है।
(b) ध्वनि प्रदूषण के बाहरी स्रोतों में लाउडस्पीकरों का अंधाधुंध उपयोग, औद्योगिक गतिविधियाँ, ऑटोमोबाइल, रेल यातायात, हवाई जहाज और बाज़ार की जगह पर होने वाली गतिविधियाँ, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य, खेल और राजनीतिक रस्में शामिल हैं। त्योहारों, शादी और कई अन्य अवसरों के दौरान, पटाखे का उपयोग ध्वनि प्रदूषण में योगदान देता है।
ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव
अनुसंधान से पता चलता है कि कई बीमारियां ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी हैं, जैसे कि सुनवाई हानि, उच्च रक्तचाप, कोरोनरी हृदय रोग, स्वभाव में कमी, कार्य क्षमता में कमी, नींद न आना, चिंता और वाणी में व्यवधान। प्रभाव परिवर्तनशील होता है, जो व्यक्तिगत संवेदनशीलता, जोखिम की अवधि, शोर की प्रकृति और जोखिम के समय वितरण पर निर्भर करता है। औसतन एक व्यक्ति को कई घंटों के लिए 75 से 80 डीबी के शोर के स्तर के संपर्क में आने पर एक थ्रेशोल्ड शिफ्ट (किसी व्यक्ति की ध्वनि पहचान की ऊपरी सीमा में बदलाव) का अनुभव होगा। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत को हटाने के बाद यह बदलाव केवल कई घंटों तक चलेगा। एक दूसरा शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर दर्द की दहलीज है, जिस पर अल्पकालिक जोखिम भी शारीरिक दर्द (130 से 140 डीबी) का कारण होगा। इस स्तर पर किसी भी शोर को स्थायी थ्रेशोल्ड शिफ्ट या स्थायी आंशिक सुनवाई हानि का कारण होगा। शोर के ऊपरी स्तर (150 डीबी से अधिक) पर, यहां तक कि एक भी अल्पकालिक विस्फोट से कान के अंदर दर्दनाक सुनवाई हानि और शारीरिक क्षति हो सकती है। औद्योगिक शोर जानवरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, व्हेल की नेविगेशन प्रणाली जहाजों की आवाज़ के कारण टूट जाती है।
निवारक तथा उपाय
शोर हर जगह है, अन्य प्रदूषणों को नियंत्रित करना उतना आसान नहीं है। स्रोत पर ध्वनियों को गूंथकर ध्वनि प्रदूषण को कम करना उद्योग में और शहरी जीवन के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। इयरप्लग का उपयोग करना जहां असामान्य शोर उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाना, उचित स्नेहन मशीन द्वारा मशीनों के कंपन को नियंत्रित करना, सड़क के किनारे और निकट भवन में वृक्षारोपण करना, ध्वनि को अवशोषित कर सकते हैं, ध्वनि प्रमाण कक्ष का निर्माण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू करना और ध्वनि प्रदूषण और इसके परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। नगरपालिका सड़कों और खदानों से सटे ग्रीन कवर का निर्माण ध्वनि प्रदूषण को कम करने का तरीका है। यह देखा गया है कि हर 10 मीटर चौड़े ग्रीन बेल्ट के विकास में शोर का स्तर 10 डेसिबल कम हो जाता है।
1.4.5. विकिरण (रेडिएशन) प्रदूषण
विकिरण प्रदूषण गंभीर प्रकार के प्रदूषणों में से एक है और यह भी उपेक्षित है। ये है पर्यावरण में असामान्य विकिरण के कारण प्रदूषण। विकिरण प्रदूषण मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाले आयनीकरण या गैर-आयनीकरण विकिरण का कोई रूप है। रेडियोधर्मी न्यूक्लाइड्स के क्षय से निकलने वाले विकिरण विकिरण प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। परमाणु उपकरणों के विस्फोट और परमाणु-ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों द्वारा सेल और मोबाइल टावरों से, वायरलेस इंटरनेट एक्सेस मोडेम आदि के उपयोग द्वारा ऊर्जा के नियंत्रित रिलीज से सबसे प्रसिद्ध विकिरण परिणाम है। विकिरण के अन्य स्रोतों में खर्च किए गए ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र शामिल हैं। खनन संचालन और प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के उप-उत्पाद। मेडिकल एक्स-रे के संपर्क में वृद्धि और माइक्रोवेव ओवन और अन्य घरेलू उपकरणों से विकिरण उत्सर्जन के लिए, हालांकि काफी कम परिमाण में, सभी पर्यावरणीय विकिरण के स्रोतों का गठन करते हैं।
विकिरण प्रदूषण के प्रभाव
पर्यावरण में विकिरण की रिहाई पर सार्वजनिक चिंता बहुत बढ़ गई परमाणु हथियारों के परीक्षण से जनता के लिए संभावित हानिकारक प्रभावों के प्रकटीकरण के बाद, हैरिसबर्ग के पास थ्री माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में दुर्घटना (1979), और चेरनोबिल, एक सोवियत परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भयावह 1986 विस्फोट। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, अमेरिकी परमाणु हथियारों के रिएक्टरों में प्रदूषण की बड़ी समस्याओं के खुलासे ने आशंकाएँ और भी अधिक बढ़ा दीं। जापान में परमाणु विकिरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर युद्ध के बाद के अध्ययनों के माध्यम से उच्च-स्तरीय आयनीकरण विकिरण के संपर्क में आने के पर्यावरणीय प्रभावों को बड़े पैमाने पर प्रलेखित किया गया है। । कैंसर के कुछ रूप तुरंत दिखाई देते हैं।
निवारक तथा उपाय
रेडियोधर्मी परमाणु कचरे का उपचार पारंपरिक रासायनिक विधियों और द्वारा नहीं किया जा सकता है जैविक निवास से दूरदराज के क्षेत्रों में भारी परिरक्षित कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। वर्तमान में उपयोग की जाने वाली भंडारण साइटों में सबसे सुरक्षित हैं गहरी गुफाएं या परित्यक्त नमक की खदानें। हालांकि, अधिकांश रेडियोधर्मी कचरे में सैकड़ों से हजारों वर्षों के आधे जीवन होते हैं, और आज तक कोई भंडारण विधि नहीं मिली है, जो बिल्कुल अचूक है।
1.4.6. थर्मल प्रदूषण
थर्मल प्रदूषण ऊर्जा अपव्यय के माध्यम से ठंडा पानी में अपशिष्ट गर्मी का निर्वहन है और बाद में पास के जलमार्ग में। सरल शब्दों में, यह प्रदूषण थर्मल पावर प्लांटों से अतिरिक्त गर्मी, धातु ढलाई में शामिल उद्योगों आदि के कारण उत्पन्न होता है। गर्मी को आसपास के वायु में छोड़ा जाता है, जिससे इलाके का तापमान काफी बढ़ जाता है। थर्मल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जीवाश्म-ईंधन और परमाणु विद्युत-ऊर्जा पैदा करने की सुविधाएं हैं, और कुछ हद तक, औद्योगिक विनिर्माण से जुड़े कूलिंग ऑपरेशन, जैसे स्टील फाउंड्री, अन्य प्राथमिक धातु निर्माता, और रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उत्पादक हैं।
पावर प्लांट- थर्मल और न्यूक्लियर, केमिकल और अन्य उद्योगों में बहुत सारे पानी का उपयोग होता है (लगभग 30% सभी अमूर्त पानी का और 90% पानी की खपत को छोड़कर सभी में उपयोग किया जाता है) ठंडा करने के लिए और उपयोग किए गए गर्म पानी को नदियों, नालों और महासागरों में बहा दिया जाता है। । गर्म पानी का निर्वहन परिवेश के पानी के तापमान से प्राप्त पानी के तापमान को 5 से 11 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। एक जलमार्ग में गर्म पानी का निर्वहन अक्सर पारिस्थितिक असंतुलन का कारण बनता है, कभी-कभी निर्वहन स्रोत के पास प्रमुख मछली मार देती है। बढ़ा हुआ तापमान रासायनिक-जैविक प्रक्रियाओं को तेज करता है और पानी की घुलित ऑक्सीजन को धारण करने की क्षमता को कम करता है। स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के विपरीत, जल निकायों का तापमान स्थिर रहता है और बहुत अधिक नहीं बदलता है। तदनुसार, जलीय जीवों को पर्यावरण के एक समान स्थिर तापमान पर अपनाया जाता है और पानी के तापमान में किसी भी उतार-चढ़ाव से जलीय पौधों और जानवरों को गंभीर रूप से प्रभावित किया जाता है। इसलिए बिजली संयंत्रों से गर्म पानी का निर्वहन जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। गर्म उष्णकटिबंधीय पानी में जलीय पौधे और जानवर खतरनाक रूप से तापमान की अपनी ऊपरी सीमा के करीब रहते हैं, खासकर गर्म गर्मी के महीनों के दौरान। इस सीमा से केवल एक मामूली विचलन की आवश्यकता होती है, जिससे इन जीवों को एक थर्मल तनाव हो सकता है। जल शरीर में गर्म पानी का निर्वहन मछलियों में भोजन को प्रभावित करता है, उनके चयापचय को बढ़ाता है और उनके विकास को प्रभावित करता है। उनकी तैराकी दक्षता में गिरावट आती है। शिकारियों से दूर भागना या शिकार का पीछा करना मुश्किल हो जाता है। बीमारियों और परजीवियों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। थर्मल प्रदूषण के कारण जैविक विविधता कम हो जाती है। इस प्रकार जैविक समुदायों में तेजी से और नाटकीय परिवर्तन अक्सर गर्म निर्वहन के आसपास के क्षेत्र में होते हैं। थर्मल प्रदूषण को कम करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक गर्म पानी को ठंडा करने वाले तालाबों में संग्रहित करना है, किसी भी जल निकाय में पानी छोड़ने से पहले पानी को ठंडा करने की अनुमति दें।
-
निष्कर्ष
दुनिया के अधिकांश विकसित समाजों में पर्यावरण प्रदूषण एक चुनौती है; विशेष रूप से विकासशील देशों के समकालीन समाज भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से जूझते हैं और इससे निपटने के उपाय तलाश रहे हैं। इस समसामयिक मुद्दे का स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण और पुनर्वास के लिए कट्टरपंथी कार्यों के लिए कहता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि वैश्विक समुदाय के एकजुट प्रयासों से समस्या का वैश्विक स्तर पर समाधान होना चाहिए।
महत्वपूर्ण लिंक
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- जेट प्रवाह (Jet Streams)
- चट्टानों के प्रकार
- भारतीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएँ (SALIENT FEATURES)
- राजा राममोहन राय की सम्पूर्ण जीवन यात्रा
- मृदा नमी को प्रभावित करने वाले कारक
- भूमिगत जल को प्रभावित करने वाले कारक
- परमाणु रिएक्टर का निर्माता एनरिको फर्मी
- भूमिगत जल के स्रोत
- वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक
- मृदा नमी संरक्षण
- Important aspects related to the life of Netaji Subhash Chandra Bose
- Swami Dayanand Saraswati’s important contribution in social reform
- राजीव गांधी के व्यक्तित्व से जुड़े रोचक तथ्य
- Indian Citizenship
- अभिभावक शिक्षक संघ (PTA meeting in hindi)
- कम्प्यूटर का इतिहास (History of Computer)
- कम्प्यूटर की पीढ़ियाँ (Generations of Computer)
- कम्प्यूटर्स के प्रकार (Types of Computers )
- अमेरिका की क्रांति
- माया सभ्यता
- हरित क्रान्ति क्या है?
- हरित क्रान्ति की उपलब्धियां एवं विशेषताएं
- हरित क्रांति के दोष अथवा समस्याएं
- द्वितीय हरित क्रांति
- भारत की प्रमुख भाषाएँ और भाषा प्रदेश
- वनों के लाभ (Advantages of Forests)
- श्वेत क्रान्ति (White Revolution)
- ऊर्जा संकट
- प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय के कार्यकाल की घटनाएँ
- INTRODUCTION TO COMMERCIAL ORGANISATIONS
- Parasitic Protozoa and Human Disease
- गतिक संतुलन संकल्पना Dynamic Equilibrium concept
- भूमण्डलीय ऊष्मन( Global Warming)|भूमंडलीय ऊष्मन द्वारा उत्पन्न समस्याएँ|भूमंडलीय ऊष्मन के कारक
- भूमंडलीकरण (वैश्वीकरण)
- मानव अधिवास तंत्र
- इंग्लॅण्ड की क्रांति
- प्राचीन भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषताएँ
- प्रथम अध्याय – प्रस्तावना
- द्वितीय अध्याय – प्रयागराज की भौगोलिक तथा सामाजिक स्थित
- तृतीय अध्याय – प्रयागराज के सांस्कृतिक विकास का कुम्भ मेल से संबंध
- चतुर्थ अध्याय – कुम्भ की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
- पंचम अध्याय – गंगा नदी का पर्यावरणीय प्रवाह और कुम्भ मेले के बीच का सम्बंध
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है | हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है| यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- sarkariguider@gmail.com