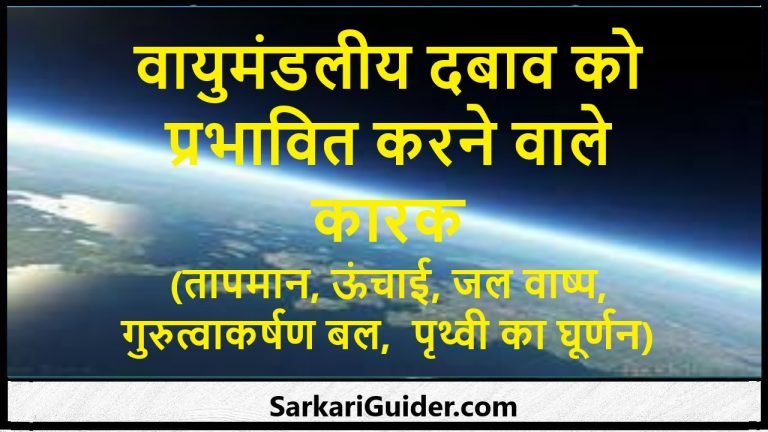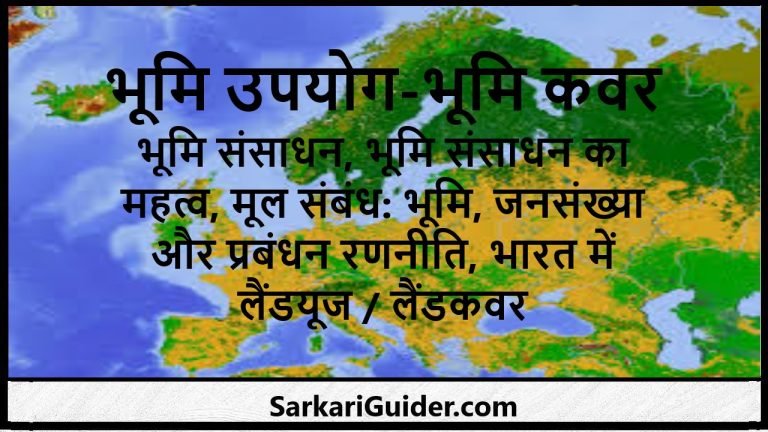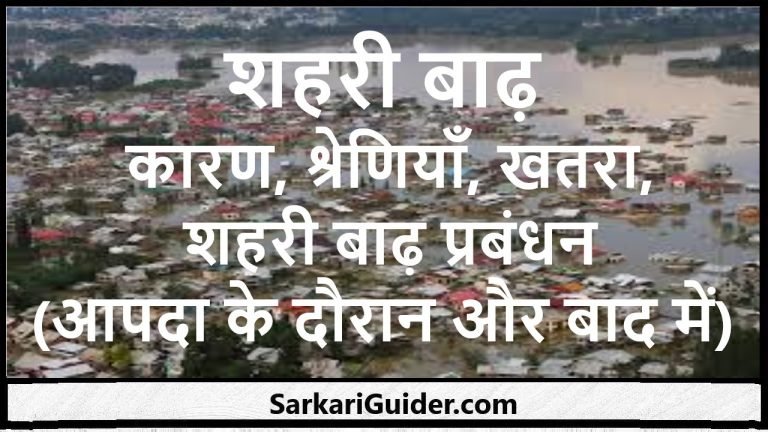संसाधनों का उपयोग एवं संसाधन भूगोल की प्रासंगिकता

संसाधनों का उपयोग एवं संसाधन भूगोल की प्रासंगिकता
संसाधनों का उपयोग
मनुष्य संसाधनों में प्राकृतिक तत्वों और वस्तुओं का विकास करता है। जब तक पुरुषों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, संसाधन एक तटस्थ सामान के रूप में निष्क्रिय रहता है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए प्राकृतिक तत्वों और प्रकृति की शक्तियों का कई तरह से उपयोग किया है।
भूमि मनुष्य को कम से कम तीन सेवाएं प्रदान करती है:
(1) यह आदमी को खड़े कमरे की आपूर्ति करती है और उसे एक जगह देता है जहाँ वह रह सकता है और काम कर सकता है। (२) यह हमारे उद्योगों और व्यवसायों के लिए कच्चा माल प्रस्तुत करता है। कोयला से लेकर अन्य खनिज मानव के दैनिक प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन के लिए अत्यधिक केंद्रित है। (३) प्रकृति से, हम उन बलों को प्राप्त करते हैं जो हमें इन कच्चे माल का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। पशु उत्पाद भी मानव की आर्थिक जरूरतों के लिए उपजाऊ हैं। ये जानवर पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले संसाधनों से अपने अस्तित्व के लिए सीधे जुड़े हुए हैं। पानी से बिजली जो हमारे चक्की के पहियों को मोड़ती है और हवा जो पवनचक्की को चारों ओर घुमाती है वह प्रकृति की अन्य ताकतें हैं जिनका उपयोग मनुष्य जीवन बनाने में करते हैं।
आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में, अंतरिक्ष का प्राकृतिक सेटअप उन प्रकार के उद्योगों को निर्धारित करता है जिन्हें स्थापित किया जा सकता है। क्षेत्र का पर्यावरणीय मेकअप भी उद्योगों के प्रकार को तय करता है जो इसके आसपास के क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं। इंग्लैंड के कोयला और लोहे ने इसे औद्योगिक क्रांति के लिए एक स्वाभाविक सेटिंग बना दिया। इंग्लैंड की द्वीप स्थिति ने यह लगभग अपरिहार्य बना दिया कि इसे एक महान वाणिज्यिक राष्ट्र बनना चाहिए। आधुनिक मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, वनस्पति आदि के सामान्य उपयोग के अलावा, इन संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए काफी भिन्न है जो आधुनिक मानव की तुलना में आर्थिक विकास के एक अलग चरण में हैं। पूंजीवादी दुनिया। स्वदेशी लोग प्राकृतिक भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करते हैं जिसके द्वारा वे घिरे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर के लगभग 300 मिलियन स्वदेशी लोगों में से 60 मिलियन, उदाहरण के लिए, अपनी आजीविका और अस्तित्व (यू०एन०एच०आर०सी० 2007) के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। वे “शिफ्टिंग या स्थायी कल्टीवेटर, चरवाहों, शिकारियों और इकट्ठा करने वालों, मछुआरों, और / या हस्तकला निर्माताओं जो प्रकृति के विनियोग की बहु रणनीति को अपनाते हैं” (वी० टोलेडो 2000.)। वे जमीन, जंगल, वन्यजीव, नदियों, वाटरशेड और जलीय जीवन पर निर्भर करते हैं, पारंपरिक चिकित्सा पर और बीज और पौधों (UNDP-RIPP 2007) पर। उन्होंने पीढ़ियों और जीव-जंतुओं, वनस्पतियों और अन्य संसाधनों के लिए अपने वातावरण को लगातार प्रबंधित किया है। स्वदेशी भूमि और क्षेत्रों पर उपलब्ध उन्हें अपनी आजीविका प्रदान की है और उनके समुदायों का पोषण किया है। स्वदेशी समुदायों का अपनी भूमि और संसाधनों से घनिष्ठ संबंध है और वे स्वयं को पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन न केवल उत्पादन के साधन के रूप में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्वदेशी लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के हिस्से के रूप में, उनकी पहचान के लोगों के लिए केंद्रीय हैं। वास्तव में, स्वदेशी लोगों द्वारा बसाए गए कई क्षेत्रों में जैविक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की दुनिया की प्रमुख सांद्रता है। स्वदेशी लोगों के लिए, प्रकृति का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी उपयोग एक पृथक, संकलित अवधारणा नहीं बल्कि उनके जीवन का एक एकीकृत हिस्सा है। वे संरक्षण क्षेत्रों को परिदृश्य के अभिन्न, कार्यात्मक भागों के रूप में देखते हैं जिसमें वे रहते हैं (जैसे, पवित्र स्थान, खेल के लिए भंडार, आदि)। हाल के वर्षों में, हालांकि, भूमि से फैलाव या प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच पर प्रतिबंध ने आर्थिक दुर्बलता, पहचान की हानि और उनके सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इस कारण से, स्वदेशी एजेंडा लगभग हमेशा अपने पैतृक क्षेत्रों के दावे के साथ शुरू होता है ताकि उनकी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों (डोरिस ज़िंगग 2012) के दीर्घकालिक संरक्षण का आश्वासन दिया जा सके।
संसाधन भूगोल की प्रासंगिकता
संसाधन भूगोल के महत्व को आर्थिक महत्व के प्रकाश में देखा जाना चाहिए जो समाज के राजनीतिक सांस्कृतिक मैट्रिक्स को प्रदान करता है। इस ढांचे के साथ प्राकृतिक संसाधन भूगोल का अध्ययन निम्नलिखित प्रमुखों के तहत किया जा सकता है:
(1) भूमि भंडार,
(2) वन और अन्य पौधों के संसाधन,
(3) जलवायु संसाधन,
(4) भूमि के जल संसाधन,
(5) पशु के संसाधन दुनिया,
(6) पृथ्वी के भीतरी इलाकों में संसाधन, और
(7) दुनिया के महासागरों के संसाधन।
जैसा कि कोमार ने कहा है “भौगोलिक विज्ञान के भीतर, प्राकृतिक संसाधन भूगोल आमतौर पर आर्थिक भूगोल विषयों से संबंधित है; हालांकि, एक राय यह भी है कि यह भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान के बीच एक मध्यवर्ती स्थिति में रखता है और दूसरी ओर आर्थिक भूगोल। पहले से ही पूर्वापेक्षात्मक रूस में संसाधनों का पहलू बहुत भौगोलिक शोध (पी० आई० रिओकोव, वी० एन० तातिशचेव, आई० लेपेकिन, एस० पी० क्रेशिनिकोकोव और ए० आई० वेइकोव की रचनाएँ) की एक पारंपरिक विशेषता थी। सोवियत सत्ता के पहले वर्षों से, जब संसाधनों के अध्ययन और दोहन की मांग और प्रकृति की शक्तियों में तेजी से वृद्धि हुई, तो भौगोलिक कार्य का संसाधन उन्मुखीकरण विशेष रूप से जरूरी हो गया। इस शोध के लिए एक वैज्ञानिक केंद्र को कमीशन फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्टिव फोर्सेस (KEPS) के भीतर स्थापित किया गया था। यूएसएसआर की भौगोलिक कांग्रेस (1960) की तीसरी कांग्रेस के संकल्पों ने प्राकृतिक संसाधनों पर भौगोलिक अनुसंधान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसे एक अधिक उद्देश्यपूर्ण परिवर्तनकारी चरित्र दिया और एक जटिल वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में प्राकृतिक संसाधनों भूगोल की स्थापना की।
प्राकृतिक संसाधनों के भूगोल की वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान में, भौगोलिक और अन्य सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों (औद्योगिक अर्थशास्त्र, भूविज्ञान, और इसी तरह) की पूरी प्रणाली के साथ इसके करीबी संबंधों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन और उपयोग है एक बहुआयामी, जटिल समस्या। भौगोलिक अनुसंधान विधियों का एक पूरा शस्त्रागार प्राकृतिक संसाधनों भूगोल में उपयोग किया जाता है; 1950 के दशक के बाद से नवीनतम गणितीय विधियों, पूर्वानुमान मॉडलिंग और हवाई और अंतरिक्ष सर्वेक्षण विधियों के रूप में ऐसी चीजों का उपयोग विस्तारित हुआ है।
सोवियत भूगोलवेत्ताओं ने प्राकृतिक संसाधनों पर मौलिक कार्यों की एक श्रृंखला बनाने के लिए अन्य विशिष्टताओं में वैज्ञानिकों के साथ सहयोग किया है। सामान्य सारांश में सोवियत संघ के सामूहिक मोनोग्राफ प्राकृतिक संसाधन, उनका उपयोग और पुनरुत्पादन (1963), मल्टीवॉल्यूम (राशन द्वारा) यूएसएसआर के प्राकृतिक परिस्थितियों और प्राकृतिक संसाधनों का प्रकाशन (1964 से), और क्षेत्र में जीवमंडल के संसाधन शामिल हैं। यूएसएसआर (1971) की। प्राकृतिक संसाधनों के आर्थिक मूल्यांकन (जल, भूमि, और इसी तरह) के आर्थिक तरीकों के लिए, और प्राकृतिक विशेषताओं के संरक्षण के उपायों के वैज्ञानिक आधार पर, व्यक्तिगत प्रकार के संसाधनों (विशेष रूप से भूमि के जल संसाधनों पर) पर भी काम किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग के लिए। प्राकृतिक सुविधाओं और संसाधन आधार के विकास और भविष्य के उपयोग की वैज्ञानिक भविष्यवाणी में सामान्य और क्षेत्रीय समस्याएं गहन अध्ययन के अधीन हैं; यह भी विकसित किया जा रहा है, समाज और प्रकृति के बीच पदार्थ के आदान-प्रदान का अनुकूलन है, जो के। मार्क्स के रूप में विख्यात है, श्रम और सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्य द्वारा मध्यस्थता, विनियमित और नियंत्रित है।
प्राकृतिक संसाधनों के भूगोल में सैद्धांतिक पदों का विकास संबद्ध विषयों में उत्कृष्ट वैज्ञानिकों के कार्यों से बहुत प्रभावित था: वी। आई। वर्नाडस्की, ए. ई. फ़र्समैन, और वी.एस. नेमचिनोव। प्राकृतिक संसाधन भूगोल के क्षेत्र में अनुसंधान विशेषज्ञों में आई. पी. गेरासिमोव, डी. एल. आर्मंड, वी. आई. बोट्वनिकोव, एस. एल. वेंद्रोव, इयू शामिल हैं। डी. दिमत्रेवस्की, के. आई. इवानोव, के. वी. ज़्वोरकिन, जी. पी. कलिनिन, आई. वी. कोमार, वी. पी. मस्कोकोवस्की, ए. ए. मिंट्स, एम. आई. लावोविच और आई. यू. जी. सौशीन।
समाजवादी देशों में प्राकृतिक संसाधन भूगोल एक राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से और समग्र रूप से समाज के हितों में प्राकृतिक संसाधनों के सबसे पूर्ण खोज, मूल्यांकन और तर्कसंगत बहुपक्षीय शोषण के लिए तरीके विकसित करता है। इस सब के लिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का नियोजित विकास प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में बड़ी संभावनाओं को खोलता है जो अभी तक विज्ञान या व्यवहार द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किए गए हैं।
पूंजीवादी देशों में प्राकृतिक संसाधनों के भूगोल में, एकाधिकार पूंजी के हित प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन, मूल्यांकन और दोहन से संबंधित समस्याओं के समाधान में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं; विदेशी एकाधिकार उनके द्वारा वशीभूत देशों से प्राकृतिक संसाधनों की लूट में प्रकृति पर भारी नुकसान पहुंचाता है। चूंकि कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति अनिश्चित है, इसलिए प्रमुख पूंजीवादी देशों ने इन संसाधनों (एच० बेनेट, ई० एकरमैन, सी० केलॉग, आर० पारसोन) के संरक्षण की समस्याओं के अध्ययन पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है; ग्रेट ब्रिटेन में एलडी स्टैम्प; और फ्रांस में जे० डोरस्ट। विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधन भूगोल से बहुत अधिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक महत्व जुड़ा हुआ है।
आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति द्वारा प्राकृतिक संसाधन भूगोल को नए कार्य दिए जा रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग और आर्थिक कारोबार में नए प्रकार के संसाधनों की भागीदारी के लिए दूरगामी संभावनाएं प्रस्तुत करता है। यह क्रांति मानव जाति के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों और कच्चे माल के आधार का विस्तार कर रही है और आधार के भौगोलिक वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी ”(कोमार (1970-1979)।
उदाहरण
जल संसाधन भूगोल का विषय समय के साथ बदलता रहा है। शुरुआत में, यह पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में जल के वितरण और केवल हाइड्रोलॉजिकल चक्र का अध्ययन था। वर्तमान में, जल का बढ़ता महत्व, इसके वितरण में असमानता, इसके विभिन्न रूपों में बढ़ती मांग और उपलब्धता कम होने के साथ-साथ इसके संरक्षण की भावी रणनीति, जल संसाधन भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण तत्व बन गए हैं।
20 वीं सदी के उत्तरार्ध और 21 वीं सदी की शुरुआत के दौरान, दुनिया की बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। इसलिए, जल वितरण की असमानता और इसकी गुणात्मक गिरावट के कारण जल संकट, जल संसाधन भूगोल का मुख्य अध्ययन केंद्र माना जाता है।
पर्यावरण की विभिन्न प्रणालियों से संबंधित पानी प्रकृति में एक केंद्रीय स्थान रखता है। सही जगह पर और सही समय पर इसकी उपलब्धता पर्यावरण संतुलन बनाए रखती है। ’इसलिए, यह अंतर्संबंध जल संसाधन भूगोल में भी अपना स्थान पा रहा है।
यह स्पष्ट है कि जल संसाधन भूगोल की विषय वस्तु तेजी से बदल रही है और इसमें निम्नलिखित तथ्यों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है:
- विश्व में जल संसाधनों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन:
यह सभी जल संसाधनों के स्थानिक वितरण की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करता है: समुद्र, जमीन की सतह, उप सतह और भूजल को छोड़कर प्रकृति। अध्ययन में शामिल है कि ग्लेशियरों, नदियों, झीलों और जलाशयों में सूक्ष्म रूपों में पानी कितना और किस रूप में उपलब्ध होता है और मनुष्य द्वारा उनके उपयोग किन रूपों में किए जाते हैं।
- हाइड्रोलॉजिकल साइकल के कार्य का अध्ययन:
जलमंडल में जल का संतुलित वितरण, वायुमंडल (जल वाष्प), स्थलमंडल, और जैवमंडल प्रकृति में केवल हाइड्रोलॉजिकल चक्र के माध्यम से संभव हो जाता है। इसका अध्ययन जल संसाधन भूगोल का मुख्य विषय है। इसमें उप-चक्रों और उन पर मनुष्य के प्रभाव का अध्ययन भी शामिल है।
- पानी के गुणात्मक पहलू का अध्ययन:
इसमें जल प्रदूषण के कारण पानी की गुणात्मक गिरावट और ताजे पानी की उपलब्धता को कम करने के कारण पानी में अवांछनीय तत्वों के मिश्रण का अध्ययन भी शामिल है।
- जल-जनित समस्याओं का अध्ययन:
मनुष्य द्वारा पानी के असमान वितरण के कारण कई समस्याएं पैदा होती हैं। उनमें से महत्वपूर्ण हैं लवणता, क्षारीयता, फ्लोराइड, आर्सेनिक और जल भराव। जल संसाधन भूगोल में इन नई समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है।
- बाढ़-प्रवण और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में जल प्रबंधन का अध्ययन:
इसमें पानी की अधिकता, बाढ़-ग्रस्त और दुर्लभ, जल प्रभावित सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए स्थायी आधार प्रदान करने का अध्ययन शामिल है।
- मनुष्य द्वारा पानी के उपयोग का अध्ययन:
स्वयं के घरेलू उपयोग के अलावा, मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध पानी का उपयोग आर्थिक रूप से विभिन्न रूपों में कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए करता है। इन क्षेत्रों में पानी की लगातार बढ़ती मांग के कारण, इस विषय को महत्व मिला है। इस कारण से, पानी का चक्रीय उपयोग भी महत्वपूर्ण हो गया है।
- वाटरशेड का भौगोलिक अध्ययन:
पिछले एक दशक से, विशेष रूप से 1994 के बाद से, वाटरशेड को जल प्रबंधन के लिए एक भौगोलिक इकाई के रूप में माना जाता है क्योंकि इसमें भौतिक और पारिस्थितिक उत्थान की गतिविधियां शामिल हैं। यह एक सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम है जिसमें जल संरक्षण की विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं।
- पानी के वितरण और उपलब्धता पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों का अध्ययन:
मनुष्य की भौतिकवादी संस्कृति ने 20 वीं शताब्दी में प्रकृति में कई बदलाव लाए हैं। इस संस्कृति का प्रभाव पानी के वितरण और मात्रात्मक पहलू पर देखा जा सकता है। इनमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, बर्फ का पिघलना और अम्लीय वर्षा आदि महत्वपूर्ण हैं।
- जल संकट और जल संरक्षण का अध्ययन:
पिछली सदी के बाद से तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संकट पैदा हो गया है। जल संकट के मुख्य कारणों के अध्ययन के साथ, समाधान खोजने का अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ ही, एक रणनीति विकसित करनी होगी जो विभिन्न रूपों में जल का संरक्षण कर सके। वर्तमान में, पानी के स्थायी प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है, जिसके मूल को 1968 में डेनिस मीडोज के नेतृत्व में एक शोध समूह द्वारा एक रिपोर्ट ‘लिमिट्स टू ग्रोथ’ माना जाता है। 1972 में प्रकाशित, इसने रोकथाम करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया पानी सहित संसाधनों की गिरावट, और इस तरह एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण।
इसके बाद, 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (WCED) ने अपनी रिपोर्ट its अवर कॉमन फ्यूचर ’के साथ निकाली, जिसे लोकप्रिय रूप से अपने अध्यक्ष के नाम के बाद“ ब्रैडलैंड कमीशन ”के रूप में जाना जाता है, जिसने स्थिरता के दृष्टिकोण को भी प्रचारित किया। वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों की पूर्ति के लिए सतत जल प्रबंधन आवश्यक है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को कम किए बिना (RAGHAV n.d.)। इस प्रकार, जैसा कि संसाधन भूगोल के दायरे से ऊपर चित्रण में दिखाया गया है, गतिशील है जैसा कि संसाधन की अवधारणा है।
महत्वपूर्ण लिंक
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- जेट प्रवाह (Jet Streams)
- चट्टानों के प्रकार
- भारतीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएँ (SALIENT FEATURES)
- राजा राममोहन राय की सम्पूर्ण जीवन यात्रा
- मृदा नमी को प्रभावित करने वाले कारक
- भूमिगत जल को प्रभावित करने वाले कारक
- परमाणु रिएक्टर का निर्माता एनरिको फर्मी
- भूमिगत जल के स्रोत
- वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक
- मृदा नमी संरक्षण
- Important aspects related to the life of Netaji Subhash Chandra Bose
- Swami Dayanand Saraswati’s important contribution in social reform
- राजीव गांधी के व्यक्तित्व से जुड़े रोचक तथ्य
- Indian Citizenship
- अभिभावक शिक्षक संघ (PTA meeting in hindi)
- कम्प्यूटर का इतिहास (History of Computer)
- कम्प्यूटर की पीढ़ियाँ (Generations of Computer)
- कम्प्यूटर्स के प्रकार (Types of Computers )
- अमेरिका की क्रांति
- माया सभ्यता
- हरित क्रान्ति क्या है?
- हरित क्रान्ति की उपलब्धियां एवं विशेषताएं
- हरित क्रांति के दोष अथवा समस्याएं
- द्वितीय हरित क्रांति
- भारत की प्रमुख भाषाएँ और भाषा प्रदेश
- वनों के लाभ (Advantages of Forests)
- श्वेत क्रान्ति (White Revolution)
- ऊर्जा संकट
- प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय के कार्यकाल की घटनाएँ
- INTRODUCTION TO COMMERCIAL ORGANISATIONS
- Parasitic Protozoa and Human Disease
- गतिक संतुलन संकल्पना Dynamic Equilibrium concept
- भूमण्डलीय ऊष्मन( Global Warming)|भूमंडलीय ऊष्मन द्वारा उत्पन्न समस्याएँ|भूमंडलीय ऊष्मन के कारक
- भूमंडलीकरण (वैश्वीकरण)
- मानव अधिवास तंत्र
- इंग्लॅण्ड की क्रांति
- प्राचीन भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषताएँ
- प्रथम अध्याय – प्रस्तावना
- द्वितीय अध्याय – प्रयागराज की भौगोलिक तथा सामाजिक स्थित
- तृतीय अध्याय – प्रयागराज के सांस्कृतिक विकास का कुम्भ मेल से संबंध
- चतुर्थ अध्याय – कुम्भ की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
- पंचम अध्याय – गंगा नदी का पर्यावरणीय प्रवाह और कुम्भ मेले के बीच का सम्बंध
Disclaimer: sarkariguider.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है | हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है| यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- sarkariguider@gmail.com